‘उत्तराखण्ड होली के लोक रंग’ शेखर तिवारी द्वारा संपादित एक महत्वपूर्ण पुस्तक है. चंद्रशेखर तिवारी काफल ट्री के नियमित सहयोगकर्ता हैं. उत्तराखण्ड की होली परम्परा (Traditional Holi) पर आधारित और समय साक्ष्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक की रूपरेखा दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र, देहरादून द्वारा तैयार की गयी है. होली के इस मौसम में इस जरूरी किताब में से कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं. अनुमति देने के लिए हमारी टीम लेखक, सम्पादक, प्रकाशक व दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र की आभारी है.
इस क्रम में आज प्रस्तुत है ख्यात पत्रकार-सम्पादक नवीन जोशी का आलेख.
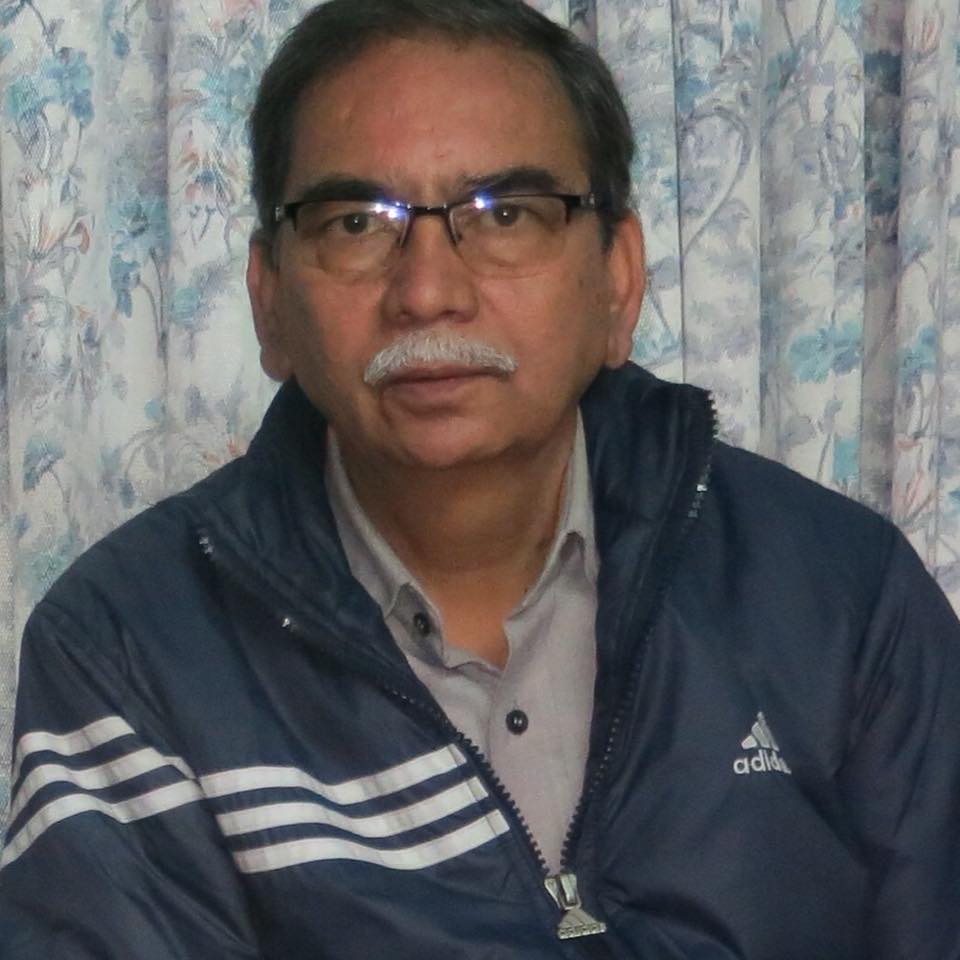
नवीन जोशी
कुमाऊंनी होली की समृद्ध परम्परा है लखनऊ में
नवीन जोशी
सबसे पहले आपको अपने बचपन और किशोरावस्था की स्मृतियों में ले चलता हूँ.
-‘हरदा, आज पुन्यू हो गई पूस की ’ कहते हुए गौर्दा आ धमकते, हम रोटी खा कर बैठे ही होते, खाना पकाते समय बाबू मिट्टी के एक छोटे कुण्डे में कोयले रखते जाते, वही तापते हुए मैं पड़ता और बाबू हुक्का गुड़गुड़ाते,
-“आओ गौरी दत्त, मैं अभी याद ही कर रहा था कि तुम आते होगे, लो हुक्का पीओ,” गौर्दा हुक्के की एक-दो फूक लगा कर उठ जाते- ‘चलता हूँ, अभी विश्वम्भर दत्त जी को भी बुलाना है, आप आओ ’
लखनऊ की कैण्ट रोड पर सिंचाई भवन के पीछे की कैनाल कॉलोनी के सर्वेण्ट क्वार्टर पहाड़ियों से भरे थे, ज्यादातर कुमाऊंनी, वहां सारे तीज-त्योहार पहाड़ी गांवों की तरह ही मनाए जाते थे. घुघुती त्यार, फुलदेई, सब, और होली तो गजब ही झकझोर होती थी. कुमाऊं में पूस की पूर्णिमा से होली गाने की परम्परा है. सो, कैनाल कॉलोनी में भी उसी रात से होली गाना शुरू कर दिया जाता था.
खड़ी होली : गौर्दा की कोठरी में बिछे गद्दों पर ओढ़-आढ़ कर बैठे चार-पांच होल्यार होली गायन की शुरुआत करते, बाबू बहुत मंद्र स्वर में होली लगाते – ‘तुम संतन के हितकारी हरी , तुम…, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त-लड़त गज हारो हरी…, गज के प्राण बचायो हरी….तुम संतन के…’
दिन भर दौड़-भाग की नौकरी से थके वे चंद होल्यार उस रात जल्दी उठ जाते. वसंत पंचमी से गौर्दा की कोठरी भरने लगती और उसमें युवकों की भागीदारी भी होने लगती, होली गायन आधी रात तक चलता. मनोरथ जी होली लगाते – ‘शिव के मन माहिं बसे काशी…, आधी काशी में बामण बनिया, आधी काशी में संन्यासी..’ युवकों को सावधान किया जाता – ‘एक बोल रे, एक बोल’ या ‘अब दो बोल, हाँ!’
शिवरात्रि से होली की यह बैठक कोठरी से बाहर खुले और बड़े अहाते में आ जाती. चंदा किया जाता, दरियां बिछती, चाय और आलू के गुटकों का इंतजाम होता. हम बच्चे उबले आलू छीलते, चाय के गिलास बटोरते-धोते और होली में भाग लगाना भी सीखते- ‘हो रही जै-जै कार जग में, जनम भयो यदुनंदन को…’और ‘शिव जी चले गोकुल नगरी…’ आहा, क्या होली थी! शिव जी भिक्षुक का रूप धर कर गोकुल जा रहे हैं. हाथ में चिमटा, और कांधे में झोली लटकाए घर-घर भिक्षा मांग रहे हैं. यशोदा माई के दरवाजे पर भिक्षा की पुकार लगा रहे हैं. यशोदा माई मोतियों भरा थाल ले आई हैं लेकिन भिक्षुक को यह भिक्षा नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए उसे ? ‘दरश कन्हैया को मांगे हरी, शिव जी चले गोकुल नगरी…’ युवकों की टोली सम पर उत्साह से चीखती – ‘तक्का होई धो, धोई हो!’
एकादशी को सुबह कपड़ों में रंग के छींटे डाले जाते और रात की महफिल अबीर-गुलाल से लाल और जोश से जवान हो उठती, बाबू अपनी पसन्दीदा होली से बैठक की शुरुआत करते – ‘एकादशी चीर, अबीर-गुलाल, द्वादशी रंग रचो है…’ इस दिन पहाड़ के गांवों में चीर बांधी जाती है और रंग खेलना शुरू हो जाता है. लखनऊ के उस मुहल्ले में चीर नहीं बांधी जाती थी लेकिन अबीर-गुलाल खूब चलने लगता. चीर बांधने से जुड़ी बहुत सी होलियां मैंने बाद में सुनी लेकिन बाबू की यह होली और कहीं नहीं सुनने को मिली. अफसोस कि आगे के बोल अब याद नहीं. कुमाऊंनी होली के अब तक देखे संग्रहों में भी यह होली नहीं मिली, खैर…
एकादशी से पुन्यूं तक कैनाल कॉलोनी का वह अहाता भर उठता, घोड़ा अस्पताल, पुराना डाकखाना, दारुल-शफा, हैवलक रोड, जाने किस-किस मुहल्ले से होल्यार जुटने लगते. अनुशासित बुजुर्ग होल्यारों पर छलकते जोश वाले युवकों की टोली भारी पड़ने लगती, एक कोने में सिमटे बुजुर्ग होली लगाते – ‘हर फूलों से मथुरा छाय रही…’ तो युवकों का कोना अधैर्य दिखाता- -‘इस ब्योपारी को नींद बहुत है…’ लगाओ न! बुजुर्ग मुस्कराते और डांट भी लगाते – ‘अरे अभी से बिछौना बिछाओगे तो छलड़ी तक क्या करोगे, रे?’ सयानों की होली चलती रहती और ज्यादा बेचौन युवक धीरे से उठकर अहाते के बाहर मैदान में आ जाते. शराब का चलन उन दिनों उतना नहीं था लेकिन अत्तर की चिलम या बीड़ी खूब चलती थी. होली के लिए पहाड़ी गांवों से वह काली बट्टी बड़े आग्रह से मंगाई जाती. अत्तर की फूक के बाद युवकों की टोली मैदान में झोड़ा गाने-नाचने लगती – ‘देवानी लौंडा द्वारहाटौ को, त्वीले धारो बोला..’ हुड़का बजता, कई बार एक साथ तीन-चार हुडुके. झोड़ा गाने-नाचने वाले इतने हो जाते कि घेरे के भीतर घेरा बनत. अहाते में जब सयाने मंद्र स्वरों में गा रहे होते – ‘श्याम मुरारी के दर्शन को जब विप्र सुदामा गए हो लला…’ तब अहाते से सटे मैदान में हुड़कों की तालों के साथ झोड़ा तार सप्तक में गूंजने लगता – ‘खोलि दे माता खोल भवानी, धरम किवाड़ा…’ थोड़ी देर बाद गौर्दा मनाने आते – ‘चलो रे, होली मत बिगाड़ो… चलो-चलो.’
युवकों की टोली दबे विद्रोह के साथ भीतर आकर होली की बैठक में शामिल हो जाती और जैसे उनको मनाने के लिए ही धर्म सिंह होली लगाते – ‘मन मारी, तन मारी, दिल को गुसैयां, कैसे रहूंगी मन मारी…, हाथ में गडुवा, कान में धोती, नाणा चली, हां-हां नाणा चली, हो-हो नाणा चली, दिल को गुसैंया, कैसे रहूंगी मन मारी.’ यह युवकों की पसंदीदा होलियों में एक थी जिसमें उन्हें शब्दों के थोड़ा हेर-फेर से अश्लील इशारे करने और गाने का मौका मिल जाता था, वैसे, ये चौपद होलियां थीं, जिन्हें गाना और लौटना आसान नहीं होता था, लेकिन वहां चौपद होलियां गाने के उस्ताद हुआ करते थे. मेरी स्मृति में आज भी कई ऐसी होलियां गूजती हैं- ‘धनुष-बाण प्रभु जी के हाथ में, चौकस है तो लछिमन भाई, लंका की तैयारी’, ‘आवन कहि गए, अजहुं न आए, ऊधो श्याम मुरारी…’, ‘बूंद जो बरसे गुलाब की, चादर मोरी भीजै रे, रे रतनारे नैना…’ आदि-आदि.
ऐसा नहीं था कि युवकों को ही होली की मस्ती चढ़ती थी, सयाने इसमें चार हाथ आगे रहते, बस, वे दिनों का लिहाज करते थे. द्वादशी-त्रयोदशी से बूढ़े जवान होने लगते और चतुर्दशी-पूर्णिमा को उनकी जवानी और उन्मुक्तता सीमाएं तोड़ने लगती थी, फिर वे कोई लिहाज नहीं करते थे, युवकों-बच्चों के ही सामने वे इशारे कर-कर के, डोल-डोल कर के गाने लगते- ‘अरे, हां रे, गोरी नैना तुम्हारे रसा भरे, चल कहो तो यहीं रम जाएं, गोरी…’ और ‘तेरे नैन रसीले यार बालम, प्रीत लगा ले नैनन की…’ और ‘अरे, हां रे, जिठानी तुम्हरो देवर हमसे ना बोले…’ और ‘बाजूबंद भुली ऐ छै पलंगै में…’ और ‘चल उड़ि जा भंवर तोको मारूंगी…’ और ‘तू तो करि ले अपनो ब्याह देवर, हमरो भरोसो झन करियो…’ और ‘अरे हां, रे गोरी, चादर दाग कहां लागो…’ और भी जाने कितनी होलियां जिनमें गोरी की स्यूनी-डंडिया से लेकर अंगुली-बिछिया तक हर अंग और उसके वस्त्र व जेवर-विशेष का वर्णन पूरी उन्मुक्तता या कहिए कि उछृंखलता के साथ होता था. कुछ होलियों में तो स्त्री-पुरुष के अंतरंग शारीरिक सबंधों का आंखों देखा हाल तक होता – ‘जब रसिया पलंगा पर आए, चड़कत है दुश्मन खटिया, शहर सितो जागो रसिया..’ भरी महफिल में इन्हें गाने में युवक भले संकोच कर जाते या मुंह छुपा कर हंसते मगर बुजुर्ग न केवल रस ले-ले कर गाते बल्कि स्वर को सप्तम तक पहुंचा कर अश्लील इशारे करने में भी संकोच न करते.
होलियों की विलम्बित तालों की एकरसता से ऊब कर बीच-बीच में कुछ गायक ‘बंजारे’ लगाते जिनकी लय-ताल अपेक्षाकृत द्रुत व चपल होती – ‘गई-गई रे असुर तेरी नारि मंदोदरि, सिया मिलन गई बागै में’ और ‘अरे, कह दीजो रघुनाथ भरत से कह दीजो…’ इन बंजारों में नृत्य की लय भी होती और कुछ लोग खड़े होकर हाव-भाव के साथ झूमते हुए भी गाते.
इन महफिलों में कुछ होल्यार होली ‘लगाने वाले’ होते यानि वे ‘लीड’ गायक होते, कुछ उसे ‘उठाने वाले’ होते यानी वे उसी लय-ताल पर होली के बोल लौटाते. ये सुर-ताल के अच्छे जानकार होते, बाकी भाग लगाते, गाने वालों की दो टोलियां बन जाती, ‘लगाने’ करने वाले की एक टोली और ‘लौटाने’ वाले की दूसरी टोली, ढोलक बजाने वाले की खास जगह होती, वह अक्सर बीच में बैठता, महफिल बड़ी हो जाने पर दो ढोलकिए भी होते, मंजीरे और लोटे तो कई बजते, मुझे कैनाल कॉलोनी की उन होलियों के एक ढोलक वादक की बहुत अच्छी याद है, उनका नाम नरोत्तम था, नरोत्तम बहुगुणा, वे होली गाते नहीं थे, सिर्फ ढोलक बजाते थे, ऐसी ढोलक कि होल्यारों को मजा आ जाता. नरोत्तम जी की ढोलक होली जमा देती थी, वे आंख बंद करके बहुत आनंद से बजाते, अक्सर ढोलक के ऊपर दोहरे हो जाते, ऐसा लगता जैसे सो रहे हों, सिर्फ उनके हाथ हरकत करते और बिल्कुल झुकी गरदन ताल के साथ हिलती जाती.
छलड़ी के दिन होल्यारों की टोली रंग खेलते और गाते-बजाते कैनाल कॉलोनी से डायमण्ड डेरी, हैवलक रोड, घोड़ा अस्पताल और कभी-कभी दारुल शफा तक जाती, हर घर के सामने होली गाते और आशिष देते- ‘गाऊं-खेलूं-देवूं अशीष, हो-हो होलक रे. इनरा नानातिना, नाती-पोथा जी रूं लाक्षे बरी (लाख सौ बरीस) हो-हो-होलक रे…’ इनमें किसी के लड़के-लड़्की का ब्याह होने, किसी के घर संतान हो जाने जैसी आशिषें भी शामिल होती, रिश्तों के हिसाब से मजाकिया आशिष भी दी जाती, उस शाम को कुछ ही होल्यार मिलते और गाते – ‘होली खेली-खाली मथुरा को चले, आज कन्हैया रंग भरे…’ और इस तरह होली का समापन हो जाता, उसके बाद की शामें हमारे लिए सन्नाटा भरी और उदास होतीं.
ये स्मृतियां 1965 से 1980 के दौर की हैं, बाद में ये बैठकें बिखर गईं, पुरानी पीढ़ी रिटायर होकर पहाड़ लौट जाती रही और नई पीढ़ी का मिजाज बदलता रहा, प्रवास का स्वरूप बदला और जीवन शैली भी. लखनऊ में बसा कुमाऊं का ‘लोक’ धीरे-धीरे लोप हो गया, जाहिर है होली भी वैसी नहीं रह गई, हमारे लखनऊ में अब लोक-होली की बैठकें दुर्लभ ही हैं.
बैठी होली : सन 1975 के बाद मेरा सामना लखनऊ की दूसरी तरह की ‘बैठी’ होली से हुआ जो तबला-हामोनियम-मंजीरे या उलटे लोटे पर सिक्कों की संगत में गाई जाती हैं, कुमाऊनी होलियों के आम तौर पर दो प्रकार बताए जाते हैं- ‘खड़ी होली और ‘बैठी’ होली. ‘खड़ी होली वास्तव में लोक-होली है जो खड़े होकर, गोल घेरे में नाचते हुए गाई जाती हैं और बैठ कर भी, ‘बैठी’ होली शास्त्रीय होली है, शास्त्रीय राग-रागिनियों में बंधी हुई और नागर समाज में ज्यादा प्रचलित है, खड़ी होली में बेसुरे-बेताले भी जोर-शोर से भाग लगा ले जाते हैं लेकिन बैठी होली के लिए राग-ताल का ज्ञान और गायन-निपुण होना जरूरी है.
लखनऊ के पहाड़ियों के ‘भद्र लोक’ से परिचय होने के बाद मैंने ये बैठी होलियां भी खूब देखी-सुनीं. शिव रात्रि के आस-पास से ये बैठकें भी शुरू हो जाती हैं. चार-छह अच्छे गायकों की अपनी टोलियां होती हैं जिन्हें होली गवाने के शौकीन अपने घर बुलाते हैं, एक-एक रात की बाकायदा बुकिंग होती है, एकादशी से छलड़ी के बीच ये गायक एक रात में दो-दो तीन-तीन घरों में भी निमंत्रित होते हैं, चार-छह लोग भी तबला-हारमोनियम लेकर बैठ जाते हैं और गायन शुरू हो जाता है, आम तौर पर गायकों से ज्यादा श्रोता होते हैं, खड़ी यानी लोक होलियों की बैठकें जहां अब दुर्लभ हैं वहीं इन बैठी यानी शास्त्रीय होलियों का सिलसिला बना हुआ है, लखनऊ के विभिन्न मुहल्लों में ऐसी बैठकें खूब होती हैं, अच्छी बात यह कि नई पीढ़ी ने इस परम्परा को आगे बढ़ाया है, गिरिजा शंकर पंत लखनऊ के नामी होली गायक थे, चतुरानंद जोशी, चंद्र शेखर पंत, गिरीश शाह, बचीराम जोशी, कैलाश जोशी, ललित मोहन जोशी और जगदीश चंद्र जोशी लखनऊ के अच्छे होली गायको में गिने जाते थे, गिरिजा जी के पुत्र नीरज पंत नई पीढ़ी के उतने ही अच्छे गायक हैं, उनके साथ श्रीधर बिष्ट, चंद्र शेखर, नवीन त्रिपाठी, मनोज जोशी, आदि की अच्छी टोली है.
इन होलियों को सुनने का अलग आनंद है. हाल के वर्षों में मैंने इस युवा टोली से बहुत सुंदर होली गायन सुना है जो आश्वस्त करता है कि लखनऊ में कुमाऊंनी होली के शास्त्रीय स्वरूप की परम्परा ठीक-ठाक बनी हुई है. नीरज हारमोनियम सम्भालते हुए जब गाते हैं- ‘बरसत रंग फुहार, सखी बरसाने चलो, कांधे अबीर-गुलाल की झोली, कर कंचन पिचकारी. ग्वाल-बाल सब श्याम संग, राधे अंगना के पार, कर सोलह श्रृंगार, सखी बरसाने चलो..’ और ‘चटक-मटक रसवंती डगर चली, भरी भीड़ दई मोरी बैंया झटक…’ या श्रीधर जब डूब कर सुनाते हैं – ‘कैसी धूम मचाई बिरज में, आज ग्वालन के संग, तेरो री ललन घनश्याम…’ तो कमरे में अद्भुत वातावरण बन जाता है जिसमें संगीत तो होता ही है, होली का पूरा राग-रंग भी सब पर तारी हो जाता है, गुमानी की प्रख्यात होली ‘मोहन मन ल्हीनो, मुरली नगीना सों…’ भी यहां खूब चाव से गाई-सुनी जाती है. अल्मोड़ा वाले तारी मास्टर (तारा दत्त पाण्डे) की होलियों के कैसेट यहां अब भी कई घरों में सुरक्षित हैं और सुने जाते हैं, सोशल मीडिया के इस जमाने में लखनऊ के विभिन्न परिवारों की होली बैठकों के वीडियो आप यू ट्यूब पर देख सकते हैं.
बैठी होली की शास्त्रीयता में छेडखानी, चुटकियां और श्रृंगार के अतिरेक कम नहीं होते, बचीराम जी को, जिन्हें सब बचदा कहते थे, मैंने कई बार अपने दंत विहीन मुंह से गाते सुना है – ‘खेलत गेंद गिरी जमुना में…, तैं मेरी गेंद चुराई, अंगिया बीच देखो कन्हाई, एक गई दो-दो पाई…’ तब सारे होल्यार ऐसे आनंदित और रस सिक्त होते जैसे कि जयदेव का ‘गीत-गोविंद’ सामने ही मंचित हो रहा हो, तब तबले और हारमोनियम को अपनी खैर मनानी पड़ती, वह होल्यार ही क्या जो बचदा जैसा रसिक न हो! अब यह होल्यार-होल्यार पर निर्भर है कि वह ‘राह रोकने’, ‘बैंया मरोड़ने’ और ‘अंगिया भिगोने’ तक सीमित रहता है या इससे ज्यादा स्वच्छंदता लेता है!
बैठी होली की ये बैठकें जम जाएं तो भोर तक चलती हैं और राग भैरवी के साथ इनका समापन होता है. कुमाऊं परिषद की लोकप्रिय रामलीला में हारमोनियम के उस्ताद प्रकाश चंद्र तिवारी उर्फ प्रभु चच्चा अपने भरी गले से क्या खूब भैरवी सुनाते थे. गिरिजा शंकर पंत के जमाने में भैरवी पर भैरवी का दौर चलता था, भले ही आंगन में धूप आ जाए!
बैठी होली की एक खासियत उसकी ताल-मात्राएं भी हैं. लखनऊ के कई अच्छे तबला वादक इन होली बैठकों में ‘सम’ पर गच्चा खा जाते रहे, अच्छी-खासी ताल पर चल रहा गायक अचानक दो अतिरिक्त मात्राओं की गलियों में कहां भटक कर सम पर लौटा, वह समझ ही नहीं पाता, चौदह की बजाय सोलह मात्राओं की यह ताल कुमाऊनी शास्त्रीय होलियों में कहां से आ गई, यह संगीत के विद्वान ही बता सकते हैं लेकिन लखनवी कुमाऊनियों ने यह विशेषता बचा रखी है.
महिला होली : लखनऊ का शायद ही कोई मुहल्ला या कॉलोनी होगी जहां ड्राइंग रूम के सोफे-साफे किनारे खिसका कर भरी दोपहर कुमाऊंनी महिलाओं की होली बैठक न जमती हो. ढोल-मंजीरे की धमक-झमक के साथ परवान चढ़ती गायकी के बीच ‘कॉमिकल इण्टरवल’ की तरह स्वांग यानी ठेठर भी चल रहे हैं. प्रौढ़ा हेमा दी भरी महफिल में अपने ही जेठ की नकल उतार रही हैं कि रात देर से घर लौटने पर नाराज जेठानी को कमरे के एकांत में वे कैसे मनाते हैं. महफिल में जेठानी भी मौजूद हैं जो शर्म से लाल और हंसी से गोल हुई जा रही हैं.
-‘कैसे-कैसे, हेमा दी? फिर से बताना तो!’ गदगद हो कर अनुनय करती हैं युवतियां. लाड़ से गरियाती हैं बूढ़ियां- ‘इस हेमा को तो जरा भी शर्म नहीं, रे!’
हर होली में नए-नए स्वांग रच लाती हैं औरतें, स्वांग करने, गाने-बजाने में पारंगत महिलाओं की इन बैठकों में बड़ी मांग रहती है. पुरुष काम पर गए होते हैं, इसीलिए दिन के एकांत में खूब जमती हैं कुमाऊनी महिलाओं की होली. गोमती पार के इलाके हों या हुसेनगंज-सुंदरबाग के पुराने मकान या राजाजीपुरम-आलमबाग और जानकीपुरम-विकास नगर की कॉलोनियां, महिलाओं ने अपनी होली बैठकों की रौनक कतई कम नहीं होने दी है. वहां लोक सांस्कृतिक रंग पूरी मस्ती में होता है. एकादशी से छरड़ी तक तो होली की धूम-धमाल मची रहती है. होली गाई जाती है, होली नाची जाती है और होली ‘एक्ट’ की जाती है. महिलाओं पर घर गृहस्थी से लेकर सामाजिक परम्पराओं तक के निर्वाह का जो भारी जिम्मा रहता है, उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप होली जैसे अन्तरंग पर्वों पर उनकी स्वतंत्रता अपने शिखर पर होती है. होल्यार महिला कामकाजी हो तो छुट्टी लेने में कोई गुरेज नहीं होता.
पुरुषों की बैठकों की तरह यहां भी शुरुआती होलियों का स्वरूप भक्तिभाव वाला होता है जिनमें वन को जाते राम-सीता-लखन को देख कर महिलाएं व्यथित होती हैं- ‘वन को चले दोनों भाई, इन्हें समझाओ री माई’ या भभूत रमाए जोगी शिव अथवा गणेश की वंदना होती है, धीरे-धीरे होलियों पर श्रृंगार रस चढ़ने लगता है, बागों में फूल ही नहीं खिलते, मन में भी मंजरियां फूलने लगती हैं, पर्वतीय महिलाओं की बहुत पसंदीदा होली है- ‘आयो नवल वसंत सखी ऋतुराज कहाए, चम्पा जो फूली टेसू जो फूले, फूल ही फूल सुहाए, कामिनी के मन मंजरि फूली, वा बिच श्याम सुहाए.
और जब मौसम की तपन व वसंत के उन्माद के साथ कामिनियों के मन में मंजरियां फूलने लगती हैं तो भीतर का राग-रंग मचल-मचल कर बाहर फूटने लगता है. ढोलक पर उंगुलियों की थाप तेज हो जाती है, मंजीरे के बोलों में चूड़ियों की खनक भी घुलने लगती है. हाथों की तालियों के साथ अंगुलियों व आंखों के इशारे भी महफिल के इस-उस कोने तक उड़ने लगते हैं- ‘ऐसो अनाड़ी चुनर गयो फाड़ी हंसि-हंसि दे गयो गारी, मोहन गिरधारी…’
गिरधारी का नाम तो बहाना है, महफिल में ही अपने-अपने राधा-गिरधारी बन जाते हैं- ‘तुम हो बृज की सुन्दर गोरी, मैं मथुरा को मतवारो, गोरी प्यारो लगो तेरो झनकारो…’ और फिर ऐसे में रंग डालने में क्या लिहाज! ‘मलत-मलत नैना लाल, सुनो जी नंद लाल, किनने डारो नयन में गुलाल. सास को पूत, ननद जी को भैया, दय्या मो पे उनने ही डालो गुलाल.’ या- ‘कामिनियां भर-भर मारत रंग, अपने-अपने महल से उतरी, अपने पिया के संग…’
धीरे-धीरे कामिनियों की महफिल पूरे रंग में आ जाती है. आंखों के इशारे हाथों की शैतानियों तक पहुंच जाते हैं और रूप-लावण्य की बोलियां शारीरिक रस-कथाओं का रूप लेने लगती हैं- ‘या बृजदेश निगोड़ा, तकत मोरी चोली का डोरा, मो सो कहत चलो री कुंजन में, तनक-तनक सा छोरा.’
यहां तक आते-आते बैठक में भाभी-ननद और प्रौढ़ाओं के अलग-अलग कोने बन जाते हैं जहां होली के बोलों का रस अलग-अलग ढंग से लिया-बहाया जाता है- ‘उठता जोबन थमता नाहीं, खबर मंगा दो बालम की..’ या- ‘इस व्यौपारी को नींद बहुत है, सेज सजा दे नथ वाली, झुकि आयो शहर में व्यौपारी…’ इसी मस्ती में स्वांग करने वाली महिलाएं नई उन्मुक्तता लेकर आती हैं जहां, अभिनय, कल्पना, रचना और शैतानियों का पिटारा बूढ़ियों-किशोरियों को समान रूप से जवान बना देता है.
मूलत : होलियां बृज की हैं मगर पर्वतीय सामाजिक स्थितियों और संस्कृति ने न केवल उनका रूपान्तरण किया है, बल्कि नई रचनाएं भी की हैं. नौकरी के लिए पुरुषों के सामूहिक पलायन ने पहाड़ी होलियों में बिरह, रोमांस और पीड़ा का अजब कौतुक व संयोग भर दिया है- ‘सजना घर आवै फागुन में’ या ‘जिनके पिया परदेस बसत हैं, उनकी नारी सोच भरे.’ होली में अकेली औरत के झमेले भी कम नहीं. देवर की आंखों के इशारे समझ वह ताना मारती है- ‘तू तो कर ले अपनो ब्याह देवर, हमरो भरोसो झन करियो.’
प्रवास में यानी लखनऊ के अपेक्षाकृत स्थायित्व भरे जीवन में पहाड़ की जैसी स्थितियां नहीं हैं लेकिन वह समृद्ध सांस्कृतिक विरासत लखनऊ की महफिलों में खूब झलकती है. सिर्फ होली का आनन्द ही नहीं, मस्ती और धमाल ही नहीं, बैठक बिना आशीर्वाद के पूरी नहीं होती. आशिषने के लिए छलड़ी के दिन का इंतजार सम्भव नहीं. इसलिए जिस दिन जिसके घर होली गाई उसी दिन आशिष भी गा दिए कि बरस-बरस होली, बरस-बरस फाग खेलो. जीते रहो और रंग भरो. इस घर का मुखिया जीवे, बाल वृन्द बढ़े पांचों देव दाहिने रहें और वसंत इस घर की देहरी पर उतरता रहे.
लखनऊ की पहाड़ी महिलाओं में होलियों के प्रति इतना ज्यादा उत्साह है कि उनकी बाकायदा मंडलियां तैयार हो गईं हैं. ललिता पंत का कुमाऊनी होलियों का संकलन कई महिलाओं के हाथ में दिखाई देता है. कई शौकीन महिलाओं ने हल्द्वानी व अल्मोड़ा से होली पुस्तकें मंगवा रखी हैं और कई ने अपनी निजी डायरी में होली गीतों का संकलन कर रखा है.
इन महफिलों का खान-पान भी चर्चा का विषय रहता है. किसी के आलू के गुटुक और भांगे की चटनी चर्चित है तो कोई लखनवी चाट का ठेला लगवा लेती हैं. गुझिया तो ठैरी ही, अपने हाथ की बनाई भी और बाजार से ब्राण्डेड वाली भी! कोई दीवाली का पकवान ‘सिंगल’ होली में खिलाने के लिए जानी जाती है. कहीं बैठक देर शाम तक चलती है तो खाने के लिए पुरुष भी आमंत्रित होते हैं, बहरहाल, खाना-पीना चाहे जितना शानो-शौकत वाला हो, उससे होली के आनंद का मूल्यांकन नहीं होता. बैठक तो वही अव्वल, जहां होली ‘जम’ जाए!
तो, यह वसंत, यह होली, यह बैठकें, यह उन्मुक्तता जी रौ लाख सौ बरीस!
वाट्सएप में काफल ट्री की पोस्ट पाने के लिये यहाँ क्लिक करें. वाट्सएप काफल ट्री
 चंद्रशेखर तिवारी. पहाड़ की लोककला संस्कृति और समाज के अध्येता और लेखक चंद्रशेखर तिवारी दून पुस्तकालय एवं शोध केन्द्र, 21,परेड ग्राउण्ड ,देहरादून में रिसर्च एसोसियेट के पद पर कार्यरत हैं.
चंद्रशेखर तिवारी. पहाड़ की लोककला संस्कृति और समाज के अध्येता और लेखक चंद्रशेखर तिवारी दून पुस्तकालय एवं शोध केन्द्र, 21,परेड ग्राउण्ड ,देहरादून में रिसर्च एसोसियेट के पद पर कार्यरत हैं.
काफल ट्री वाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिये यहाँ क्लिक करें: वाट्सएप काफल ट्री
काफल ट्री की आर्थिक सहायता के लिये यहाँ क्लिक करें




































