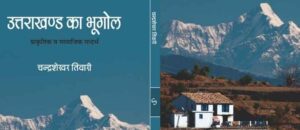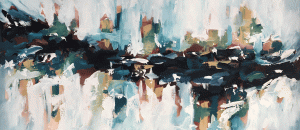नए साल की ईव पर (न्यू इयर्स ईव जैसे फ्रेज़ ने भी जीवन में उन प्रोग्रामों की वजह से ही घुसपैठ की, वर्ना हैप्पी न्यू ईयर जैसे तीन ऊर्जाहीन शब्दों की शरण में ही जाना पड़ता था) दूरदर्शन का सबसे पहला प्रोग्राम साल इक्यासी में आया था जिसे सुनील दत्त साहब ने होस्ट किया था. हमने वो प्रोग्राम नहीं देखा था. आज के इस तब-तुम-कहाँ-थे काल में इतना लीनियर जवाब नहीं चलेगा इसलिए बता दें कि तब तक पड़ोसी के घर जाकर कम्बल में घुस टी वी देखने की स्वस्थ परम्परा का सूत्रपात हो चुका था, हमारे घर में टी वी की आमद भी नहीं हुई थी तो टेक्नीकली हमें वो प्रोग्राम देख ही लेना चाहिए था, लेकिन उम्र बहुत कम थी हमारी. सो इसलिए. नब्बे का निहायत ही शातिर दशक हमारे खेलने-खाने की उम्र में हमारे सामने अनफोल्ड हुआ है. उस लिहाज़ से शटर वाले ब्लैक एंड व्हाइट वेस्टर्न टीवी ने जब गाजे बाजे के साथ हमारे घर की लॉबी कम रीक्रिएशन रूम कम स्टडी कम बैठक में प्रवेश किया, तब तक टीवी पर न्यू इयर्स ईव प्रोग्राम एक क्लासिक क्लीशे के स्तर पर पहुंच चुका था. Doordarshan Nostalgia from Yesteryears
दो-चार साल में ही उस प्रोग्राम ने वो मुकाम हासिल कर लिया कि उसका इंतज़ार उसके खत्म होने के तुरंत बाद ही शुरू हो जाता था. नियमतः उसमें कुछ सपाट चेहरे वालों का सुगम संगीत, हिंदी-अंग्रेज़ी की खचड़-पचड़ से निकले दुर्गम बोल वाले पॉप सांग्स, नींद लहरियों को आमंत्रित करती गज़लें, अतिशय लाउड और सामाजिक सन्देश देते कॉमेडी नाटक, कुछ चुटकुलिया स्टैंड अप्स और चिर युवा शामक डावर द्वारा निर्देशित ग्रुप डांस हुआ करते थे. इन सबके बीच हमारे लिए खतरनाक आकर्षण उन चंद सेकेंड के लिए स्क्रीन चीरकर उभरे हिंदी फिल्मों के नायक-नायिकाओं का हुआ करता जो हमें नए साल की बधाई देने अवतरित होते थे. हीरो-हिरोइन की एक्सेसिबिलिटी के मामले में हमारा बचपना बड़ा माल न्यूट्रिशंड था. अगर रविवार की फिल्में और चित्रहार को छोड़ दिया जाए तो फिल्मों के कलाकार, ख़ासकर हीरो हीरोइनें, टीवी पर सेकेंड के पांचवे हिस्से भर दिखते थे. उतनी ही देर में उसे मुगली घुट्टी पांच सौ पचपन की तरह पी लिया जाता था. अब तो बच्चे दिन भर में जितनी बार अपने बाप का चेहरा देखते हैं, उससे दस गुना ज्यादा बार अम्ताच्चन उन्हें दिख जाते हैं और एक हम थे कि ‘मिले सुर मेरा तुम्हारा’ गीत के आख़िरी हिस्से में जित्तेन्दर, मिथुन और अमिताभ को देखने के लिए गुसल से उठ के भाग आते थे. वो तो अच्छा था कि गीत लम्बा था और हमें फ्रेम बाई फ्रेम कंठस्थ था इसलिए हम समस्त प्रचलित कार्यवाही फ्रेम बाई फ्रेम समाप्त करके ही आते थे. Doordarshan Nostalgia from Yesteryears
जैसा कि नियम था प्रोग्राम में सुगम से लेकर अति दुर्गम संगीत का सफ़र इसी क्रम में हुआ करता था. प्रोग्राम की शुरुआत में सरस्वती वन्दना होती थी या नहीं, मुझे याद नहीं. प्रस्तुतकर्ता (नहीं विज्ञापन वाले नहीं बल्कि कार्यक्रम प्रस्तोता ही प्रस्तुतकर्ता कहलाते थे) आठ-आठ सेंटीमीटर मुस्कान के साथ एकाधा शे’र पढ़ देने की क्षमता प्रदर्शित करने के बाद `और अब पेश करते हैं’…, `लीजिये पेश है’…, `अब आपकी खिदमत में’… `और अब हम कुछ ही पलों में’… जैसे रूढ़ हो चुके वाक्यों को कार्यक्रम के अनुसार भाव में पगाकर बोल देते थे यथा ग़ज़ल पेश करते समय जितनी मुर्दनी चेहरे पर आती थी हास्य नाटिका के समय उतनी ही हंसी. हमारे भी भावों का वितान उसी अनुसार तय हो जाता था. गायक या डांसर या एक्टर-कॉमेडियन के मुफलिसी के इतिहास के अनुसार प्रतिभा पहचान का चलन नहीं हुआ था.
वो पॉप के सिर उठाने का दौर था. अलिशा उन्हीं दिनों सफेद लिबास में हमारे घरों में किसी विदेशी परी की तरह दाख़िल हुईं. हालांकि `परी हूँ मैं’ का दावा करने वाली सुनीता राव बाद में आईं. इन दोनों के बीच शैरोन प्रभाकर भी आती-जाती रहीं. हम तो आज तक उस गुत्थी को नहीं सुलझा पाए कि इन पॉप गायकों के आने पर स्टेज पर इतना धुंवा-धुंवा सा क्यों हो जाता था. कभी-कभी तो गायक की कमर से होते हुए उसके चेहरे तक. उसके पहनावे से पहचानना मुश्किल हो जाता कि कोई गा रहा है, या रही है. आवाज़ के भरोसे तो तब भी नहीं रहा जा सकता था. मिलन सिंह उन्ही दिनों बड़ा कन्फ्यूज़ किया करती थीं.
धुंवा देखकर लगता जाने कौन सिगरेट फूंक रहा है. क्या पता कोई आग लगी हो जिसे बुझाने बाबा सहगल ठंडा-ठंडा पानी लेकर आए. बचपन में सुर-ताल की समझ हमें नहीं थी, (कहने के लिए कहा गया वाक्य क्योंकि आज भी नहीं है) लेकिन (या इसलिए) हसन जहांगीर को टीवी पर लाइव ‘हवा-हवा’ चलाते देखने की बड़ी तमन्ना थी. पूरी नहीं हुई. कोई मामला रहा होगा. शरणार्थी और घुसपैठिये के बीच का कोई फैक्चुअल ट्विस्ट. खाली दिल दा मामला थोड़ी है.
इन सबसे ज्यादा गुरदास मान `दिल दिल दिल, दिल दिल, दिल दिल’ करके हमारा दिल ले जाया करते थे. हालांकि उस उम्र में दिल दे किसी मामले की हमारी जानकारी हमारे पंजाबी ज्ञान के बराबर ही थी, मल्लब मुखड़ा-मुखड़ा समझ जाते थे अन्तरे पर टें बोल जाते, लेकिन गुरदास जरी के किनारी वाली धोती, चटक सुर्ख़ कुर्ते और ईस्टमैन कलर वाली अधबांह खुली बास्केट में ढपली बजाते आते और हम कई दिनों तक दिलदिलाते रहते. उम्र की थाप आज तक उनकी ढपली नहीं बजा पाई उस वक्त तो ख़ैर वो जवाँ ही रहे होंगे. Doordarshan Nostalgia from Yesteryears
एक गुत्थी और है जो अनसुलझी है आज तलक. पीनाज़ मसानी सीढ़ियों पर क्यों बैठी रहती थीं? और जब भी उनके चेहरे पर फोकस होता वो अपनी नुकीली ठुड्डी पतली नाज़ुक उंगलियों भर धर खूब मुस्कराते हुए गातीं. हमें तो ग़ज़ल बहुत उदास कर देती थी, है. ये और बात है कि उदास होने के कारण बदल गए हैं. मैंने बड़े भाइयों को उनके गालों पर बेसाख्ता उभर आए गड्ढो के बारे में डिस्कस करते सुना तो अपने गालों के गड्ढों को फ़ॉलो करना शुरू कर दिया. बचपन में पतरसुटके होने की वजह से साफ़-साफ़ तो नहीं दिखते थे लेकिन ये आभास तो था कि अस्थि-मज्जा की उस जैसी कोई कार्यवाही हमारे गालों पर भी हुई है. अब तो अस्थि-मज्जा का आपसी प्रेम देखकर फूले न समाए मास ने भी दोनों को आगे-पीछे से ऐसे भींच लिया है कि शरीर में कहीं के कहीं पहाड़, पठार और गड्ढों के दर्शन हो जाते हैं कि क्या कहें.
के के नायकर हमारी पीढ़ी के लिए जीवन के पहले स्टैंड अप कॉमेडियन हुए. नायकर को पहली दफ़ा हमने न्यू इयर्स इव प्रोग्राम में ठेले पर गोलगप्पे खाती लड़कियों की टोली का मिमिक करते देखा था. कई सालों तक हम भगेलू के गोलगप्पे खाने जाते तो उन लडकियों को ढूंढते. तब ये टर्म `स्टैंड अप कॉमेडी’ चलन में नहीं था. मिमिक्री थी और रामदास पाध्ये जैसे वेंट्रिलेक्विस्ट अपने गुड्डे के साथ नाना प्रकार के प्रयोग किया करते थे. राजू श्रीवास्तव और फ्लॉप शो जैसा हिट शो लेकर जसपाल भट्टी भी सम्भवतः बाद में पर उसी दौर में आये. जसपाल भट्टी अगर आज के दौर में जिंदा होते तो कमेन्ट बॉक्स आ रही गालियां खा-खा कर ही मर मिटे होते.
इसी तरह के किसी साल इकत्तीस दिसम्बर की रात दूरदर्शन पर एक चरित्र लप्पू झन्ना आया. जहाँ तक मुझे याद है रघुबीर यादव ने वो भूमिका निभाई थी. खूब सारे कपड़े पहने वो शख्स भचक के चलता था. जब उसका शरीर नीचे की ओर झुकता तो आवाज़ आती लप्पू… और जैसे ही वो ऊपर तनता झन्ना…! पूरा कार्यक्रम क्या था वो याद नहीं लेकिन वो ब्लैक एंड व्हाइट कैरेक्टर स्थाई रूप से ज़ेहन में जम गया. हमारी हड्डी प्रदर्शन के लिए बनाई हुई काया पर लटकाई भाई साहब की बुशर्ट और बैगी पैंट में जब हम लचकते चलते तो खुद को लप्पू-झन्ना ही समझते. तब लोग अपने ऊपर हंस सकने की ताब रखते थे.
एक बार कुछ यूं हुआ कि `द वर्ड दिस वीक’ जो कि साल का आख़िरी एपिसोड था इसलिए `द वर्ड दिस इयर’ टाइटिल से आया था, खत्म हो चुका था, दाढ़ी वाले प्रणव रॉय जा चुके थे और कुछ ही पलों में वो रंगारंग कार्यक्रम शुरू होने वाला था जिसके प्री-पोल अलायंस की अभी-अभी घोषणा हुई थी. मतलब अब चूंकि ख़बर-वबर जैसी नीरस चीज़ों के ग्राहक बड़े भाई साहब और पिताजी कम महत्वपूर्ण स्थानों पर बैठ सकते थे सो हमारी और अन्य लोगों के बैठने-लेटने-अधलेटबैठने की जगहों का एक बार फिर से निर्धारण किया गया. टीवी के ठीक सामने, उससे दूरस्थ स्थान पर एक तख्त रखा था. अमूमन उसी पर बैठकर टीवी देखने की इजाज़त थी क्योंकि आँखे खराब होने की अवधारणा प्रचलन में थी. इसके पीछे हालांकि सबसे बड़ा वैज्ञानिक तर्क दूरदर्शन के नाम में छुपा होना बताया गया था. Doordarshan Nostalgia from Yesteryears
तख्ता `मजा नहीं महा मजा’ की तर्ज पर महातखत सा था और उसपर हम सारे भाई-बहन और चाचे-मामे और चरेरे-ममेरे भाई-बहन आराम से सेटल हो जाते थे. होने को तो बैठक में लकड़ी के कृशकाय सोफे भी पड़े थे जिन्हें आज के सोफों के साथ तुलना करने पर बताना मुश्किल हो जाता है कि आज इनको फीलपांव हुआ है या उनको जॉन्डिस हुआ था. लेकिन उन सोफों की कमरे में अवस्थिति टीवी से तीस और एक सौ बीस डिग्री पर थी और उन्हें भी दीवार से इतना चिपकाया गया था कि आज भी बैठक में उन सोफों की बुनाई उभरी हुई है. उन्हें भी टीवी की मेज से यथासंभव दूर रक्खा गया था इसलिए ऑर्डर ऑफ़ प्रेफरेंस में वो नीचे आते थे. तो उनपर भाई साहब और पिताजी का बैठना तय हुआ. उस साल किसी काम से रानू, हमारे छोटके फुफ्फा का लड़का, के छोटके फुफ्फा जी भी इलाहाबाद से आए थे. उसी दिन लौटना था लेकिन उस दशा में रोडवेज़ की माया से लेट होना तय था और प्रोग्राम छूटने की पूरी संभावना थी अतः उन्हें इसरार करके रोक लिया गया था. उन्होंने स्वेच्छा से सोफ़े का चयन किया. तो उस ऐतिहासिक रात में कमरे की भौगोलिक स्थिति ये थी कि दाहिने बाएं और अग्रिम बाएं पर क्रमशः पिताजी, फूफाजी और भाई साहब थे और तख्त पे पूर्वी कोने से शुरू करें तो माँ, बड़की दीदी, मंझलकी दीदी, छोटकी दीदी, चचेरी गुड़िया दीदी, पड़ोस से आई अंजू दीदी, संजू दीदी, रतनदादा, संदीप और हम थे. रेखागणितीय हिसाब से टीवी से नब्बे डिग्री के कोण पर हम थे.
उस शाम फूफाजी चैराहे से उस चीज़ को अच्छी मात्रा में ले आए थे जिसे दुनिया के सबसे स्वादिष्ट टाइम पास होने का रुतबा हासिल था. मूंगफली. न्यूज़ आइटम खत्म होने और मेन प्रोग्राम शुरू होने के बीच वो हमें बता रहे थे कि किस तरह से उनके पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को कलर्ड करने का बड़ा क्रिएटिव जुगाड़ था. उन दिनों टीवी स्क्रीन के ऊपर एक और स्प्लास्टिक की स्क्रीन लगती थी. अमूमन ब्लू कलर की. (इस लिहाज से हर फिल्म को ब्लू फ़िल्म कह सकने वाली पीढ़ी के भी हुए हम). उन्होंने एक दूसरी स्क्रीन लगवाई थी जिसके चार कोने पर तिर्यक कटे हुए चार रंग थे और ‘अपन तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से भी एकदम्मे कलर्ड का मज़ा लेते हैं’ कहते हुए उन्होंने हाथ से फूंगफली तोड़ते हुए दाने मुंह में उछाले ही थे कि अचानक ‘ठर्र… कुर्र’ जैसी एक आवाज़ टीवी से आई और बूंदी छनने लगी. मतलब सॉरी फ़ॉर इन्टरप्शन वाला मामला बन गया. अब तक दो तरीकों के इंटरअप्शन के अभ्यस्त हो चुके थे हम. एक में स्क्रीन पर कुछ ऐसा दृश्य उभरता कि लगता था जैसे किसी कड़ाहे में बूंदी छन रही हो. दूसरे प्रकार में एक टूँ… की तेज आवाज़ होती थी और जबतक वॉल्यूम बटन का कान उमेठते तीसरे घर मे रह रहे उपाध्याय जी को पता चल जाता कि ‘लाला के घरे टीवी चलत हौ.’
ये पहले प्रकार का इंटरअप्शन था. ‘ट्रेकिंग आ गई ट्रेकिंग’ फूफाजी ने हमारे शब्दकोश में इजाफा करते हुए कहा ‘पसारण केंद्र सेई हो रई गड़बड़’. बहुत बाद में हमें पता चला कि दांत में मूंगफली फंसने से प्रसारण का पसारण हो जाता है. तजुर्बा मैनुअल के अनुसार हवा ने कसे हुए एंटीने को थपड़िया कर उसका मुंह घुमा दिया था. तब तक हम घर के छोटे होने की वजह से एंटीना विशेषज्ञ हो चुके थे. गली क्रिकेट और छत्ती क्रिकेट खेलने वाले वो दोहा ज़रूर जानते होंगे ‘मारन बड़न को चाहिए, छोटन को ले आव’. छत पर जाकर एंटीना घुमाना उसी सिद्धांत का दूसरा व्यावहारिक पक्ष था, जिसका पहला पक्ष निस्संदेह नाली से बॉल निकालना था. फूफाजी का हाथ अभी नमक की पुड़िया तक भी न पहुंचा होगा कि किसी के आदेश का इंतज़ार किये बग़ैर हम लपक कर छत पर पहुंच चुके थे और एंटीने की नाभि में घुसी ठंडी लोहे की रॉड घुमानी शुरू कर दी थी. Doordarshan Nostalgia from Yesteryears
छत पर घनघोर अंधेरा था. हमने एंटीने का सिर बस अंदाज़े से दक्षिण-पूरब ओर कर दिया क्योंकि बनारस जाने वाली सड़क का रास्ता वही था तो कायदे से सिग्नल को भी उसी दिशा से आना चाहिए. चूं की आवाज़ के साथ एंटीना घूमा और हमने पूछा ‘आया’?
‘अभी नहीं’
दो-तीन झटका देकर हमने फिर पूछा ‘आया’?
‘अरे… अरे अभी आया था फिर चला गया… जिधर किये थे उधरी करो.’
कोई साढ़े तेरह मिनट की मशक्कत और ‘आया… अभी नहीं’ वार्तालाप के बाद जब सब्र का बांध, जो कि फिलवक्त हमारी दुखती भुजाओं में था, टूटने को था, ‘थोड़ा-थोड़ा आ रहा है’ सुनकर हम नीचे भागे.
हमारे कमरे के अंदर पैर रखने की देर थी कि भाई साहब बोले ‘अरे… य्यार… फिर गया’. हम फिर भागे. फिर कुछ किया, पूछा, नीचे आये, फिर ऊपर भागे. फिर तो ये क्रम सा बन गया.
लगभग वही प्रक्रिया दुहराने, नीचे आने के बाद अब कोई तेईसवीं बार छत पर थे. इस बार फूफाजी ने नया ज्ञान दिया था. ‘काहें नहीं बूस्टर लगवा लेते एन्टीनवा में, केतनौ गड़बड़ हो बुस्टरवा एकदम साफ पिच्चर दिखाता है’. इस नए ज्ञान और भागदौड़ का मिलाजुला असर हुआ कि अब हम बेमुरव्वत हो चुके थे. इस बार हमने एंटीने के पोल को ऐसे घुमाया जैसे सरकारें मुद्दे घुमा देती हैं.
‘अरे धै मर्दवा फिर बिगड़ि ग’ ये आवाज़ भाई साहब की नहीं थी, हमने ध्यान दिया. ये भी ध्यान दिया कि हर बार हमारे एंटीना घुमाने के बाद भाई साहब की आवाज़ के साथ-साथ ऐसी ही कोई आवाज़ और भी आती रही है.
हमने फिर से एंटीने का कान उमेठा और ‘आया’ का आलाप नहीं लिया, चुप रहे. ज़रा देर में आवाज़ आई
‘ईय्या आएस आएस… ग… अबैं आई… लगत हौ रवां होत हौ सिग्नलवा’
ओ तेरी. अब समझे. दरअसल हुआ ये था कि बूंदा-बांदी और अँधेरे की वजह से हम बगल वाले विश्वकर्मा जी की टीवी का एंटीना घुमाए दे रहे थे जो आज ही हमारे एंटीने के बगलगीर हमारी साझी दीवार पर लगाया गया था.
धत्त तेरे की. हमने खुद को करेक्ट किया. एंटीने को अंदाजन सही दिशा में लगाया, पूछा ‘आया’ सुना ‘आ गया’ और नीचे खिसियाये हुए से कमरे में दाख़िल हुए. Doordarshan Nostalgia from Yesteryears
हम बताते कि छत पर इतनी देर से क्या हो रहा था उससे पहले दो-तीन पटाखे फ़टे टीवी पर और शब्बीर कुमार से जबरदस्ती गवाया गया गाना कानों में पड़ गया ‘नए स्साल का, हो… पहला ज्जाम आपके नाम’…!
हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें: Kafal Tree Online

अमित श्रीवास्तव. उत्तराखण्ड के पुलिस महकमे में काम करने वाले वाले अमित श्रीवास्तव फिलहाल हल्द्वानी में पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात हैं. 6 जुलाई 1978 को जौनपुर में जन्मे अमित के गद्य की शैली की रवानगी बेहद आधुनिक और प्रयोगधर्मी है. उनकी तीन किताबें प्रकाशित हैं – बाहर मैं … मैं अन्दर (कविता) और पहला दखल (संस्मरण) और गहन है यह अन्धकारा (उपन्यास).
काफल ट्री वाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिये यहाँ क्लिक करें: वाट्सएप काफल ट्री
काफल ट्री की आर्थिक सहायता के लिये यहाँ क्लिक करें