जीवन यूं ही गुजर रहा था तुम्हारे बिना, तुम्हारी दूसरी बार छुट्टी आने की आस में. चिट्ठी का इंतजार रहता था. नजर रहती, पोस्ट ऑफिस से घर तक आने वाली उस संकरी, घुमावदार और चढ़ाई वाली पगडण्डी पर. एकटक! तुम्हारी वे बातें, वे शरारतें हर वक्त याद आती. तब भी और अब भी. पर अब सिर्फ तुम. बस तुम ही! तब तुम्हारी शिकायत रहती थी मेरे से पर अब मेरी… नहीं-नहीं! मैं शिकायत क्यों जो करूं तुम से. तुम जो मेरे होते, मेरे पास ही न रहते? और मैं तुम्हारी होती तो तुम अकेले ही क्यों चले जाते? तुम्हें उलाहना नहीं दे रही हूँ. वह जो छाती पर सिल (पत्थर) रखा है न, उसे ही घड़ी-दो-घड़ी के लिए नीचे रखना चाहती हूँ. बस! (The Anguish of a Wife of a Mountain Martyr Soldier)
गांव से ढोल-दमौं के साथ जात्रा जाती है कुंजा देवी के लिए, हर बरस. परम्परा वही, जात्रा वही, रास्ता वही पर हर्ष-उल्लास और जात्री नये. रंग-बिरंगे कपड़ों में गांव के लोग और नयी चुनरी नए श्रृंगार के साथ कहारों के कंधे पर इतराती-इठलाती देवी की डोली. जात्रा समाप्त होती है कुंजाधार पहुँचने पर, पूजा-अनुष्ठान के बाद. पर अपनी जात्रा? अपनी जात्रा तो अधूरी रह गयी भुवन! सच, तुम कितने निरुठे हुए ठहरे.
दादा जी अक्सर कहते भी थे कि फौजी निरुठे होते हैं बल, जब जलमपत्री मिलवा रहे थे. दादी बोलती ही रही कि वे गंगाड़ी हैं बल और हम… उनका भात हमारे यहाँ नहीं चलता बल. संजोग ही रहा होगा शायद. पिताजी किसी की बात नहीं माने, न दादा की और न दादी की ही. माँ तो डर से उनके सामने शायद ही कभी मुंह खोल पाई हो. पिताजी बहुत जिद्दी हुये जो ठहरे.
बैसाख में मिले थे हम थौलधार के मेले में. मिले क्या, वह तो ढंग से देखना भी नहीं हुआ. जैसे सिनेमा के परदे पर कुछ ठीक से देखा भी नहीं कि सीन बदल जाय, झट से. छिः! आग लगे उस ज़माने को. माघ में शादी हो गयी. मैं उन्नीस की हुई और तुम तब तेईस के हुए. गांव में तब मैं ही सबसे ज्यादा पढ़ी-लिखी थी— आठवीं पास और तुम हुए पलटण में ल्हैंसनैक. यह घमंड करने वाली बात नहीं रही, पर ससुर जी के हुक्का गुड़गुड़ाते वक्त लोगों से बतियाने और सास के गांव के रास्तों पर ठसक से चलने में यह बात झलक ही जाती थी.
शादी के बाद कहाँ रह पाए थे तुम घर पर, मुश्किल से पांच दिन. ‘सारी छुट्टी शादी की ही तैयारी में कट गयी.’ ऐसा तुमने कहा था प्यार के क्षणों में— फिर से जल्दी आने का आश्वासन देते हुए. करते भी क्या, इकलौते चिराग जो हुये ठहरे घर के.
मुश्किल से पाँच चिट्ठियां ही मिली थी तुम्हारी, पूरे सात महीनों में. मैं डाकिये को उन दिनों अक्सर कोसती थी कि तुम्हारी चिट्ठी क्यों नहीं लाता होगा ये निरमुआं झटपट. तभी तो जवाब लिखूंगी न. यह सोचते करते देखा कि आठवें माह तुम आप ही आ गए. खेतों में फसल पकने लगी थी और बारिस छूट रही थी जो कभी-कभार भिगो भी देती. पर मैं तो भीग ही रही थी उन दिनों, बाहर कम और भीतर ज्यादा. खेतों में साथ ही जाना होता हमारा, साथ ही खाना होता, साथ ही सोना और और… छिः सारी बात कैसे कहूँ.
तुम अपनी कम, पलटण की ज्यादा सुनाते. पलटण में ये होता है, पलटण में वो होता है. और उन पचपन दिनों की दुनिया ही मेरी दुनिया हुयी. और उसके बाद? हाँ! उसके बाद तो सिर्फ नरक ही हुआ न भुवन! उन पचपन दिनों की याद मैंने सम्भाल रखी है आज तक. गठरी बाँध कर. कभी उठाकर इस कोने रखती हूँ और कभी उस कोने. तुम्हारी समूण जो हैं वो यादें. और फिर इत्ता लम्बा अरसा भी तो कट गया उसके सहारे.
गाँव में गाड़-गदेरे के स्यूंसाट के बीच, कभी जंगल जाते वक्त पथरीली पगडंडियों पर चलते हुये और कभी खेतों की मेड़ पर बैठकर तुमने साथ जीने-मरने की कसमें खाई थी. मैं झट्ट से अपनी हथेली तुम्हारे मुँह पर रख देती, तुम्हारे मरने की बात कहने पर. मरने से बहुत डरने वाली जो हुयी मैं. पर तुम फौजियों को तो मरने-मारने के सिवा.
हे राम दा! ये फौजी ऐसा क्यों सोचते होंगे बल? और जब तुम्हारे जाने के ठीक तीन महीने बारह दिन बाद ही तुम्हारे मरने की, नहीं-नहीं शहीद होने की (जैसे कि लोग कहते हैं) खबर सुनी तो भरी दोपहरी में बज्र गिरा हो जैसे. शहीद हो गए तुम लाम पर. तोड़ गए रिश्ता स्यट्ट से सात फेरों, सात बचनों, सात जल्मों का.
बन्धन में तो हम दोनों ही बन्धे थे न भुवन? पर तुम क्यों बन्धन तोड़ गये? बन्धन का धर्म तो मैं निभा रही हूँ न? और निभाऊंगी भी.
‘वीरगति पा गया भुवन!’ तुम्हारे अवशेष घर लेकर आये वे हरी वर्दी वाले निर्दयी फौजी कह रहे थे. कुहराम मचा था दोनों घरों में. दादा, दादी की जली-कटी सुनने और माँ के छाती पीटने पर पिताजी को शायद अपने फैसले पर अफ़सोस जरूर हुआ होगा.
अफ़सोस तो मुझे भी हो रहा था कि… किन्तु नहीं. पचपन दिनों का जो समय, जितना अरसा तुम्हारे साथ जिया भुवन मेरे! वह मेरे लिए संजीवनी है और वही संजीवनी शेष चालीस-पचास बरसों के लिए बहुत है. अगर चालीस-पचास साल जी पाऊंगी तब तो न!
गांव की पगडण्डियों पर चलते हुये सूखे पत्तों की सरसराहट में आज भी लगता है कि तुम लुका-छुपी कर मेरे आगे-पीछे चल रहे हो. खेतों की मेड़ पर बैठे हुये से दिखाई देते हो कभी. गाड के पानी में स्यूंसाट नहीं तुम्हारी फुसफुसाहट सी सुनाई देती है, जैसे तुम मेरे कान में कुछ कह रहे हो— वह जो तुमने कहा था और वह भी, जो तुम तब कहते-कहते रह गए थे. पर कहाँ? तुम तो स्वर्गतारा बन गए न भुवन.
बस, तुम उत्तर दे सको तो, अधिकार से इतना जरूर पूछना चाहती हूँ कि पूरणमासी की रात से ही क्षीण होते चाँद को देखकर तुम्हें कभी पीड़ा होती है क्या?

देहरादून में रहने वाले शूरवीर रावत मूल रूप से प्रतापनगर, टिहरी गढ़वाल के हैं. शूरवीर की आधा दर्जन से ज्यादा किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं. विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में लगातार छपते रहते हैं.
हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें: Kafal Tree Online
काफल ट्री वाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिये यहाँ क्लिक करें: वाट्सएप काफल ट्री
काफल ट्री की आर्थिक सहायता के लिये यहाँ क्लिक करें




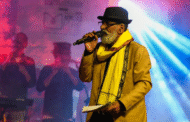

































1 Comments
योगी त्रिपाठी
अत्यंत सुंदर लेखन, गांव की झलकियों को, पहाड़ की संस्कृति को और विशेष रूप से देश सेवा में जुड़े समस्त देश रक्षकों को सलाम।।