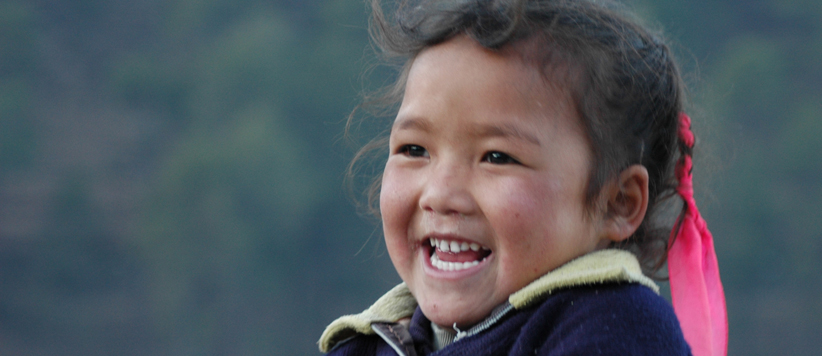महिला अधिकारों के नाम पर रस्म अदायगी का एक दिन और आ कर चला जाएगा 8 मार्च (International Women’s Day) को. साल में 364 दिन पुरुषों के एकाधिकार के और एक दिन महिलाओं के लिये. इस पर भी कथित विचारशील लोग खूब खुश होते हैं. यह एक दिन भी पुरुषों ने ही महिलाओं को दिया. कितना छद्म है हमारे सामाजिक जीवन में? फिर भी हम इसे बड़ी उपलब्धि मानकर अपनी पीठ खुद ठोकते हैं. वाह क्या बात है! पूरे साल 364 दिन महिलाओं के साथ भेदभाव व गैरबराबरी के. उसे सामाजिक व पारिवारिक मामलों में पुरूषों से कमतर समझने के. उसे पारिवारिक मामलों में भी सलाह लेने व देने लायक न समझने के. उसे स्वयं कोई भी निर्णय न लेने लायक समझने के. साल के पूरे 365 दिन महिलाओं के साथ बराबरी के क्यों नहीं?
महिला दिवस के दिन हम महिला अधिकारों की चाहे जितनी बड़ी-बड़ी बातें करें पर आज भी हम महिलाओं को पुरुषों से कमतर ही आंकते हैं. कुछ महिलाएँ भले ही सामाजिक जीवन की वर्जनाओं को तोड़ कर कुछ अलग कर के एक मिसाल बन जाती हों, पर इनकी संख्या होती कितनी है? मात्र अंगुली में गिनने लायक और कथित महिला दिवस पर हम उन गिनी-चुनी महिलाओं के बारे में दो आंखर छाप कर उसे बहुत बड़ी उपलब्धि करार दे देते हैं, जबकि उन्हें वह उपलब्धि अपने पुरुषार्थ से मिली होती है. हम उनके पुरुषार्थ का श्रेय भी उन्हें नहीं देते. पुरुष उनके पुरुषार्थ को भी अपने खाते में बड़ी ही बेशर्मी से जोड़ता है और कहता है कि देखो हमने महिलाओं को कहॉ से कहॉ पहुँचा दिया है? अपनी मेहनत से समाज में नया मुकाम बनाने वाली महिलाओं से अक्सर एक सवाल जरुर पूछा जाता है कि उनके यहाँ तक पहुँचने में उनके परिवार के पुरुषों (पिता, पति व भाई) का कितना योगदान रहा है? वे भी उसका श्रेय परिवार के पुरुषों को देते हुए कहती हैं, “यदि पिता, पति व भाई ने उन्हें सहयोग नहीं दिया होता तो वे यहाँ तक नहीं पहुँचती.” कोई भी उनके वहां तक पहुँचने में माँ, दादी व बहिनों की ओर से मिले सहयोग के बारे में नहीं पूछता है. और न अधिकतर महिलायें इसका श्रेय अपनी माँ, दादी या बहिन को देती हैं. इनको श्रेय तब ही मिलता है, जब परिवार में कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं होता. अधिकतर पुरुष परिवार की महिलाओं को तब ही कथित तौर पर आगे बढ़ने की स्वीकृति देते हैं, जब वे अपने अधिकार के लिये एक तरह से अड़ जाती हैं या परिवार की दूसरी महिलायें उसके पक्ष में खड़ी हो जाती हैं. ऐसी स्थितियों का जिक्र घर से बाहर समाज में नहीं के बराबर ही होता है. इसी कारण उसका श्रेय किसी महिला को मिलने की बजाय परिवार के पुरुषों को ही मिल जाता है.
घर -परिवार में लड़ झगड़ कर जब कोई महिला व लड़की समाज में अपना एक स्थान हासिल कर लेती है तो महिला की उस उपलब्धि को बताने में भी हमारी पुरुषवादी सोच फिर सामने आती है, इस वाक्य के साथ कि “एक बेटी ने बेटा बन कर दिखा दिया”. मतलब ये कि हम बेटियों की उपलब्धि को भी एक तरह से बेटे के हिस्से में डालने की बेहूदा हरकत करते हैं. दूसरे शब्दों में कहें तो हम बेटियों को भी जबरन बेटा बनाने पर ही तुल जाते हैं. कोई उपलब्धि हॉसिल करने से पहले बेटी जब समाज में आगे बढ़ने की कोशिस करती है तो उसे अक्सर यह कहकर चुप रहने व घर की चारदीवारी में ही रहने की नसीहद दी जाती है कि “लड़की हो तो लड़की बनकर रहो. ज्यादा लड़का बनने की कोशिश मत करो”. हम भले ही कथित तौर पर बेटी की उपलब्धि पर कुलांचें मारने का दिखावा करते हों, लेकिन बेटी को फिर भी बेटी नहीं रहने देते. क्यों हम यह नहीं कहते कि हमें बेटी पर नाज है? “बेटी ने बेटा बनकर दिखाया” जैसा अमर व आदर्श वाक्य बोलने में समाज का अधिकतर हिस्सा ही शामिल नहीं है, बल्कि इस तरह का वाक्य समाज में जनचेतना फैलाने का दम्भ भरने वााला मीडिया व समाज के कथित चिंतक भी आमतौर पर प्रयोग करते हैं. इससे साफ पता चलता है कि बाहर से हम चाहे बेटियों के पक्ष में होने का जितना दम्भ भरें, लेकिन हमारे मनों में पुत्रों को लेकर एक अलग तरह का मोह मौजूद है. जो इसी तरह से जाने-अनजाने सामने आता रहता है.
आज भी हम बेटे को ही कुल का दीपक व घर का चिराग जैसे शब्दों से क्यों पुकारते हैं? बेटियॉ कितनी भी बड़ी उपलब्धि हासिल क्यों न कर लें वह घर का चिराग व कुल का दीपक क्यों नहीं हो सकती? भले ही हमें दादा, परदादा के बारे में कुछ भी मालूम न हो, हमें उनका नाम तक पता न हो, लेकिन इसके बाद भी कथित वंश चलाने के लिये एक बेटा होना आज भी आवश्यक क्यों है? कथित वंश चलाने के नाम पर बेटे की यही चाहत आज कोख में ही बेटियों की हत्या का कारण बन रही है. बेटी थोड़ा सा भी मुँहफट व तेज हो तो वह नातेदारी व आस-पड़ोस में बदचलन घोषित हो जाती है और लड़का वास्तव में कितना भी बदचलन क्यों न हो उसे, “क्या करें? बेटा तो आखिर बेटा ही है, या इस उमर में ऐसी नादानी हो ही जाती है” कहकर क्यों बचा लिया जाता है? बेटे की शादी के बाद हर एक को क्यों पोते का ही मुँह देखना होता है? दो-एक बेटी होने के बाद क्यों परिवार के सयाने और रिश्तेदार यह कहते हुये एक तरह से उलाहना देते हैं कि एक बेटा तो होना ही चाहिये? यह देखते व जानते हुये कि उनके पति, पिता, भाई या बेटे ने कौन सी बड़ी मिसाल कायम की?
मेरी एक ही बेटी है 12 साल की. किसी परिवारिक समारोह व शादी ब्याह में नातेदार जब बच्चों के बारे में पूछते हैं और मैं कहता हूँ कि एक बेटी है तो वो मेरे उत्तर के जवाब में ,”बस एक ही बेटी है?” कहकर क्या यह नहीं पूछते हैं कि बेटा नहीं है? मेरे एक नजदीकी रिश्तेदार हैं. उनकी बेटी की जब पहली लड़की हुई तो उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से बताया था कि वे नाना बन गये हैं. जब उनकी बेटी की दूसरी भी लड़की ही हुई तो उन्होंने,”मैं फिर से नाना बन गया” कहने की बजाय हमें इस बात की सूचना तक देना उचित नहीं समझा. जब उनकी नातिन चार महीने की हो गयी तब जाकर हमें पता चला. वह भी तब जब उससे एक पारिवारिक समारोह में उनके घर पर मुलाकात हुई. जब मैंने दूसरी लड़की होने की बात न बताने पर नाराजगी दिखाई तो उनकी बेटी ने स्पष्ट कहा कि शायद मेरी दूसरी भी बेटी होने के “गम” में ये लोग डूबे हुये थे. अब आदमी खुद ही गम में डूबा हुआ हो तो दूसरों को कुछ भी बताने की स्थिति कहाँ होती है?
हम जब तक इस मानसिकता से पारिवारिक व सामाजिक रुप से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक साल में केवल एक दिन मनाये जाने वाला महिला दिवस सेमिनारों, भाषणों, शोधपत्रों व कुछ लोगों को महिला अधिकार के नाम पर सम्मानित करने की रस्म अदायगी से आगे नहीं बढ़ पायेगा. मात्र इससे महिलाओं की स्थिति में कोई क्रान्तिकारी बदलाव फिलहाल आने वाला नहीं है.

जगमोहन रौतेला
जगमोहन रौतेला वरिष्ठ पत्रकार हैं और हल्द्वानी में रहते हैं.
काफल ट्री वाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिये यहाँ क्लिक करें: वाट्सएप काफल ट्री
काफल ट्री की आर्थिक सहायता के लिये यहाँ क्लिक करें