जिस वक्त हम गाँव पहुँचे, धूप चोटियों पर फैलने के बाद उतरते-उतरते पहाड़ियों के खोलों में बैठने लगी थी. हवा अभी तपी नहीं थी, ठंडक थी उसमें- बल्कि, हल्का-सा जाड़ा था उसकी तासीर में.
(Story by Kshitij Sharma)
घोड़िया सड़क से उतरकर गाँव तक जा रही पगडंडी पर हम एक कतार में चले आ रहे थे. सबसे आगे थे प्रताप भैया और भाभी, उनके पीछे थीं यशोदा दीदो. मैं, चंदर और कमल साथ थे. श्याम थोड़ा पीछे रह गया था. वह बचपन में गाँव छोड़ने के बाद पहली बार आ रहा है, इसलिए ऊबड़-खाबड़ उतराई में उसे दिक्कत हो रही थी.
यशोदा दीदी बार-बार मुड़कर उसे देखती जा रही थीं. इशारों से, रास्ते की ऊँचाई-नीचाई के मुताबिक कदमों को सँभालने का तरीका बता रही थीं. उसकी हालत पर दीदी को तरस आ रहा था. बीच-बीच में ताज्जुब भी कर रही थी कि इतने वर्षों में वह कभी गाँव आया ही नहीं. एक बार भी नहीं! हमारी ओर देखकर सवाल-सा कर देती थीं.
गाँव को लेकर दीदी हमेशा एक भावुकता पाले रहती हैं. अनुराग तो हमें भी है, हमारी जन्मभूमि है, पर दीदी जितना पागलपन नहीं. उनके लिए यह अविश्वसनीय बात थी कि गाँव में जनमा आदमी, एक बार निकलने के बाद, कभी लौटकर वहाँ नहीं आया.
(Story by Kshitij Sharma)
हमारे बारे में वह जानती थीं-पढ़ाई के दिनों में छुट्टियाँ होते ही हम गाँव की ओर दौड़ आते थे. खेत, गधेरों और जंगल को रौंदते-रौंदते काफल-खबानी के पेड़ों पर की उछल-कूद में दीदी हमारी सहभागिनी होती थीं.
बाद में भी, ताऊजी के जीवित रहने तक, हमारे जेहन में बसा गाँव का मोह किसी-न-किसी बहाने हमें यहाँ खींच लाता था. यह मोह शायद गाँव का ही. नहीं था, ताऊजी के स्नेह-दुलार का भी था और उनकी मौजूदगी में शहर की. हदबंदियों से मुक्त विस्तृत फैलाव में रहने की स्वच्छंदता का भी था.
श्याम बचपन में बीमार अधिक रहा, इस कारण भी गांव नहीं आ पाया. चाची किसी भी हालत में उसे ऐसे स्थान पर भेजने को तैयार नहीं होती थीं जहाँ डॉक्टर और दवाइयां आसानी से न मिल पाएँ . दीदी ये सब बातें जानती थीं. पर उनका कहना था कि बड़ा होने पर तो आ ही सकता था. बाकी लोग भी तो आते रहे हैं. माना यह शहर में पला, वहीं पढ़ा, वहीं नौकरी कर ली, इसका मतलब यह तो नहीं कि गांव इसके संस्कारों में ही नहीं रहा. कोई वास्ता ही महसूस न होता हो. जड़-जमीन तो हमारी यहीं है. शहर में पहुँचे हैं डेढ़ पीढ़ी पहले . उसमें भी पूरी तरह शहर के कभी नहीं हो पाए.
वैसे गाँव अभी हमारे बच्चों ने भी नहीं देखा है. पर उनकी बात अलग है. हम ही उन्हें यहाँ नहीं ला पाए. वहीं से भूगोल समझाते रहे – रामगंगा गाँव से करीब डेढ़ मील नीचे छूट जाती है. सिद्ध मंदिर और डाक बंगले की आखिरी चोटियाँ मील-भर ऊपर रह जाती हैं. समुद्र-तल से इसकी ऊँचाई किसी ने मापी नहीं, फिर भी गाँव की धुर से हिमालय की श्वेत चोटियाँ हाथ पहुँचने के फासले पर लगती हैं. बाकी रचना आसान है. एक ओर चीड़ का जंगल है, शेष तीनों ओर खेत. ऊपर जहाँ खेती खत्म होती है, वहाँ से बाँज के झुरमुट फैलते-फैलते जंगल बन जाते हैं.
राज्य के नक्शे को छोड़, जिले के नक्शे में भी गाँव अंकित नहीं है. छोटा है, पंद्रह मवासों का – इसलिए हाकिमों ने अपनी सुविधा के लिए पता नहीं कब इसे एक बड़े गाँव के साथ जोड़ दिया. नाम हो गया-मौजा सिमार, लग्गा- तलकोट.
वैसे पीढ़ियाँ बढ़ने के साथ-साथ बाहर निकलने की मजबूरियाँ भी न बढ़ी होतीं तो अब तक यहाँ भी पचास-साठ मवासे हो गए होते. तब फैलाव इतना बढ़ जाता कि बाखलियों में मकानों की जगह नहीं बचती, धारों की ढलानों पर बढ़ना पड़ता.
इस समय सबके चेहरों पर एक बेबसी थी-अफसोस था. दीदी का अफसोस ज्यादा गहराता जा रहा था. उनकी आँखों से टपकता दर्द कह रहा थावह हमें माफ नहीं करेंगी. इस वक्त उनसे बात करना, उनको ही नहीं, अपने को भी कुरेद-कुरेदकर घावों के सैलाब में बदल देना था.
यहाँ पहुँचने से पहले, रास्ते-भर, मन में उत्साह था-एक उमंग थी, जो सालों बाद गाँव पहुँचने की खुशी को बचपन के करीब पहुँचने जैसा बना रही थी. वह उदासी में बदल गई थी.
घर के पटांगण में कदम रखते ही पाँव ठिठक गए थे. जैसे अपने का बियाबान जंगल के बीच खड़े ऐसे भूतहा मकान के सामने आ गए हो बदसूरत दीवारें ही नहीं आसपास के पेड़ पौधे भी भयानक शक्लें बनाकर जाने का डर पैदा कर रहे हों.
अनायास उग आई धारदार बाबिल घास और सिसौड़ के जहरीले पार पटांगण से उठते-उठते बदरंग दीवारों की अंधी ऊँचाई तक फैल गए थे. अपने लंबे-लंबे तनों से सफेदी और पलस्तर की मोटी परतों के उखड़ जाने से दीवारों पर उभरे कोढ़ को ढकने की नाकाम कोशिश कर रहे थे. इस झाड़-झंखाड के सामने मकान के विगत वैभव को बताना अपने को झूठा बनाना जैसा था.
वह जमाना ज्यादा पीछे नहीं गया, जब इस मकान के कारण इलाके-पड़ोस में हमारा सम्मान था. एक पहचान थी. वह ठुलकुड़ि (बड़ा मकान) के नाम से मशहूर था, हम ‘ठुलकुड़ि वाले’ नाम से.
जिस समय यह बना था, इसकी विशालता के आगे मीलों दूर तक के मकान बौने हो गए थे. चूने से पुती इसकी चिट्ट दीवारों और करीने से रंगे दरवाजों व खिड़कियों की चमक के आगे कमेटू और लाल मिट्टी से लीपे छोटे मकान फीके पड़ जाते थे.
तब गाँव की सारी चहल-पहल का केंद्र भी यही था. गाँव में आए साधु संन्यासी, पटवारी-तहसीलदार, लगान उगाई के लिए सयाने-मालगुजार सीधे यहीं आकर रुकते थे. पटांगण से लेकर सीढ़ियों तक भीड़ हो जाती थी. सर्दी की लंबी रातों में हुड़के की ताल पर रामी सूरदास के लोकगीतों और लोकगाथाओं को सुनने के लिए, गाँव-भर के बैठने लायक जगह हमारे चाख के अलावा और कहीं नहीं थी.
इसीलिए पटांगण में कदम रखते ही भ्रम हो गया था कि जिस मकान के कारण हम गद्गद होकर अपने को भरा-पूरा महसूस करते थे, यह वही मकान है. रात-भर बस में बैठे-बैठे जागते रहने के कारण पहले से ही भारी सिर, इतनी देर खड़े रहने से चकराने लगा था. आँखों में चुभन होने लगी थी. उतार का रास्ता वैसे ही पैरों को कँपकँपा देता है. अब थकान से तलवों में जलन होने लगी थी.
प्रताप भैया ने आँखों से इशारा किया पास आने को. नजदीक पहुँचने पर उन्होंने फाटक धकेलने के लिए धीमे से कहा कि उनकी आवाज खुद उन्हें भी सुनाई नहीं दी होगी. पर स्थिति की गंभीरता ने चेहरे के खिंचावों और आँखों के छोटे-बड़े होते आकारों को इतना मुखर कर दिया था कि शब्दों की जरूरत ही नहीं रह गई थी.
बारह-तेरह फुट ऊंचे भारी-भरकम दरवाजों को अंदर की तरफ धकेलने में की जोर लगाना पड़ा. सालों से बंद दरवाजों को चूलों में जमी मिट्टी ने उन्हें जाम कर दिया था. चरमराती आवाज के साथ आधे खुले दरवाजों से होकर बदबूदार गरम हवा का भबका मुंह पर थप्पड़ की तरह लगा, जैसे तपते तंदूर का मुंह खोल दिया हो. दरवाजे से ऊपर उठती सीढ़ियों पर जमी गर्द को फानने की हिम्मत नहीं हो रही थी, झांक लिया. दरवाजे के हो जालों के प्रतिरोधों के बीच, जहाँ तक नजर पहुँच सकती बाँक लिया. दीवारों और फर्श से उखड़ी मिट्टी की परतों से बने बदसूरत नक्शों और ढलवा छत की खपच्चियों से झड़ते गारे की सूखी डालियों को देखकर उदासी और बढ़ने लगी.
(Story by Kshitij Sharma)
खोई की दीवार पर बैठे हम अपने अतीत को ढूंढने लगे थे. पैतृक घर का मतलब दीवारों से घिरा, छत से ढका आवास ही नहीं होता. संस्कारों-विश्वासों को बनाने वाली पारिवारिक आस्थाओं और घटनाओं का निजी संसार भी होता है. पीढियों को जीवित रखने वाली स्मृतियों का इतिहास भी.
उसी संसार में इतिहास को ढूँढ़ते हुए हम उन घटनाओं से रूबरू हो गए जो इस मकान के कोने-कोने में खामोश दबी पड़ी थीं और हमारे कदमों को आहट से जागकर बोलने लगी थीं-आमा (दादी), बूबू (दादाजी) की आवाज में. ताई और ताऊजी के स्वर में. कभी रामी सूरदास के बोलों में.
पहले भी ये आवाजें जब कानों में गूंजने लगती थीं, हम अपने बच्चों को ब्यौरेवार इन घटनाओं को सुना देते थे.
हम ही नहीं, अपने अतीत के सुख को बार-बार स्मृति में दोहराने और गलतियों से सबक लेने का यही तरीका सबको पसंद है. संभवत: सारी कथाओं और उपदेशों के पीछे यही अवधारणा रही है.
मकान की दुर्दशा पर ज्यादा अफसोस यही था कि हमारे अवशेष मिटते दिखाई दे रहे थे. आज की हालत में वैसा भव्य मकान बनाना किसके बूते का है.
उस समय तो इसलिए बन गया था कि हमारे बूबू ओड़ (राज-मिस्त्री) थे. लाग कहते हैं-सागर ओड़ थे. इसका सही मतलब तो हमें नहीं मालूम, लेकिन अब महान से जरूर रहा है. इसका प्रमाण खुद यह मकान है.
सालों तो इसकी तैयारी में लग गए बताते हैं. रोजगार के घंटों के बाद बचे समय में, खेती-बाड़ी के साथ-साथ ठोक-बजाकर पत्थर छाँटने, उन्हें तराशकर इकट्ठा करने और लकड़ी जमाकर दार (चौखट, खिड़कियाँ आदि) बनाने में ही बूबू की आधी उस निकल गई.
उन्होंने अपनी सारी कला और मेहनत इसमें झोंक दी थी. सामने से यह काष्ठकला का उत्कृष्ट नमूना है. दरवाजे और खिड़कियों की पट्टियों को महज चौखट कह देना सरासर गलत होगा. डेढ़ से दो फुट की तिरछी चौड़ाई में जड़ी इन पट्टियों पर खुदे बेल-बूटे और देवी-देवता एक-दूसरे से ऐसे गुंथे हैं कि एक के मामूली से खिसक जाने पर पूरा इतिहास खंडित जान पड़ेगा. बहुत बाद में, जब हम पढ़-लिख गए, तब समझ पाए, बूबू महज ओड़ ही नहीं थे, इतिहास और संस्कृति के विद्वान् भी थे. इस कला-वैभव को बारीकी से देखें तो अनेक पौराणिक कथाएँ इन पट्टियों पर अंकित मिलेंगी.
दरवाजा छोटे-मोटे किले के प्रवेशद्वार से कम नहीं है. पटांगण से चाख तक सत्तरह सीढ़ियाँ और ऊँचाई ? सिर पर ताँबे का पूरी लंबाई वाला घड़ा लेकर चलो, सूत-भर भी नहीं झुकना पड़ेगा. छत्तीस हाथ लंबी अगली दीवार में पत्थरों की छाँट एकदम बराबर. ढलवाँ छत पर क्यबाड़ी के चौकोर पाथर, तोपों के जोड़ से सटे हुए.
आज, आठ दर नीचे और ऊपर लंबे-चौड़े चाख के पार चार कमरों वाले इस मकान को मकड़ी के जालों ने इस कदर घेर लिया है कि इन्हें तोड़ना चक्रव्यूह को भेदना जैसा ही हो गया है. जालों के महीन रेशों में फँसी मक्खियों पतंगों और धूल के कणों को रौंदती हुई मकड़ियाँ अभयारण्य में विचरती हुई-सी जान पड़ती हैं, जैसे बूबू की कला का उपहास कर रही हों.
सीढ़ियों के ऊपर गहन जालों को तोड़ने के बाद कपड़ों को झाड़ते हुए चाख तक पहुँचे. जालों का फैलाव देखने लायक था, जैसे एक ही रेशे से पूरे घर को बाँध रखा हो. इस चक्रव्यूह में शरीर को घुसाना तो दूर, नजर तक को आरपार जाने में दिक्कत हो रही थी. मकड़ी के इस साम्राज्य में जाना जंग फतह करके कब्जा करने जैसा था.
“क्या कुगत हो गई है घर की! कभी यहाँ मक्खी भी बैठने में डरती थी.” दीदी का गला भर्रा गया.
पड़ोस की हीरा ताई साथ में खड़ी थीं. दीदी को बेटी जैसी मानती हैं. आते-जाते के हाथ दीदी के लिए मौसम के हिसाब से भट, गहत और मडुवे का आटा आदि भेजती रहती हैं. हमारे आने के बाद अब तक गाँव के करीब-करीब सभी लोग मिल गए हैं, हीरा ताई तभी से साथ हैं. वह बोली, “छूटे मकान का क्या लगा रहे हो तुम? तीसरे दिन से ही कीड़े-पतंगों का राज हो जाता है. तुम्हारा तो ये सालों से छूटा ठहरा. तेरे बाबू के बाद लिपाई-पुताई, चूना-कमेटू भी किसने किया?”
‘सो तो ठहरा ही, ताई,’ दीदी ने हमारी ओर देखा, जैसे कह रही हों, इसके लिए तुम्हीं सब जिम्मेदार हो. उनकी आवाज में बेचारगी का स्वर था.
‘तुम लोगों ने गाँव के बारे में कभी नहीं सोचा,” दीदी की यह पुरानी शिकायत है.
गाँव के बारे में सोचा तो हमने बहुत बार है, हल कोई नहीं निकाल पाए. तो दीदी ने भी कभी नहीं सुझाया, शायद सूझा ही न हो. बस, एक मोह है वे बँधी हैं. दरअसल, गाँव से लंबा नाता उन्हीं का रहा है. हम थोड़ा बड़ा होने पर या होश सँभालते ही शहर आ गए थे, पढ़ने के लिए. दीदी से गाँव छूटा शादी के बाद. बाद में भी ताऊजी के जिंदा रहने तक वह बराबर गाँव आती जाती रहीं. इसलिए मायके का अर्थ उनके लिए गाँव ही है. शहर में प्रताप भैया और मेरा अपना मकान है. चंदर और कमल के पास सरकारी आवास. पर दीदी के लिए उनमें से किसी को भी मायका मान लेना वैसा ही है जैसे दूसरे के माँ बाप को अपना सगा मान लेना.
गाँव से लगाव किसको नहीं है ! दीदी जितनी भावुकता भले ही न हो, संस्कारों में तो इस तरह बसा है कि जब भी कोई पूछता है, “कहाँ के रहने वाले हो?” तो गाँव, खेत, जंगल और बहुत करीब से देखे चेहरों का बना एक बेहद पहचाना संसार दृष्टि के सामने आ जाता है. जान पड़ता है किसी ने हमारी पहचान पूछी है.
इतना लगाव इस शहर से कभी नहीं हुआ, जहाँ उम्र का बड़ा हिस्सा गुजर रहा है. रोजी-रोटी और भविष्य की संभावनाएँ दीख रही हैं.
अंतर इतना है, दीदी के पास रोष प्रकट करने का बहाना है. उनके सामने हम हैं. हमारे सामने कोई नहीं है, जिस पर अपना रोष लाद दें.
गाँव पहँचने के बाद, इतने दिनों से हम जालों की व्यूह-रचना को समझने में लगे हैं. इनके उदभव और विकास को देखते जा रहे हैं. कब, कहाँ से शुरू होकर ये जाले आदमियों के बनाए घेरों को तोड़कर, नए ब्रह्मांड रच देंगे, कहना कठिन है.
देखते-ही-देखते इनका फैलाव सीढ़ियों और चाख के उस भाग की तरफ बढ़ने लगा है जहाँ से परसों ही इन्हें उखाड़ फेंका था. इनकी तत्परता बताती है, ये पराजय मानने को तैयार नहीं हैं. इस दृढ़ संकल्प के पीछे यह भी कारण हो सकता है कि इस मकान पर ये हमसे ज्यादा अपना अधिकार मानते हैं. इसीलिए अपने आधिपत्य के बाद पहली बार किसी और के कदमों की आहट को इन्होंने चुनौती के रूप में लिया है.
इस मकान की बात तो कुछ समझ में आती है . मकड़ी के एकछत्र राज्य के लिए यह सुरक्षित किला है. लेकिन बाकी मकानों में तो लोग रहते हैं, उन्हें तो जालों से मुक्त करना चाहिए था. छूत की बीमारी होने पर जैसे गाँव को बाड दिया जाता है, जालों ने घरों को उसी तरह घेर रखा है. एक षढ़यंत्र की तरह इनका फैलाव एक घर से होकर, दूसरे को बेधता हुआ, सारे गाँव को अपनी परिधि में लपेटे हुए है.
टुकड़ों में बँटा गाँव जालों के माध्यम से जुड़ गया है. जालों के इस विराट में किसी भी मकान की अलग पहचान खोजना लगभग असंभव है.
खोई की दीवार पर खड़े होकर जिधर भी नजर उठती है जालों के पंजे हवा में झूलते दिखाई देते हैं. पेड़-पौधों की टहनियों से लेकर जड़ों तक गहरी पैठ बैठाए ये जाले लोगों के चेहरों पर भी फैल गए हैं . हीरा ताई, पार्वती काकी, बचीराय चाचा, जिसका भी चेहरा देखो, जालों से विकृत हो गया है.
आश्चर्य है, इन लोगों को जालों का अहसास ही नहीं हो रहा. क्या आँखों में देखने की सामर्थ्य नहीं रही? या दृष्टि इतना धुंधला गई है कि सामने की चीज भी दिखाई नहीं देती? चेहरों पर बेल की तरह उलझे जालों की जकड़न महसूस तो होनी चाहिए थी. उन्हें हटाने की कोशिश तो करनी चाहिए थी.
इनके चेहरों के जाले हमें कचोट रहे हैं. मन होता है, कपड़ा लेकर पोंछ दें. इन्हें बता दें-जालों का यों चेहरों पर रहना शुभ नहीं है. समाज के मृत होने का सूचक है. अपने को इतना दुर्बल तो न होने दो कि मकड़ी तक आक्रमण करने का साहस कर दे.
जालों से सबसे ज्यादा बेचैन श्याम है, उसे हर वक्त जाले जोंक की तरह बदन पर चिपटते लग रहे हैं. उनको छुटाने की कोशिश में कई बार कपड़ों तक को नोच देता है.
वह जालों को बास पहचानने लगा है. उसके सूंघने की शक्ति इतनी तेज हो गई है कि फलांग भर दूर के जालों को बता सकता है. भीतर-बाहर जहाँ कहीं बैठता है, नथुने सिकोड़ लेता है. यहाँ तक कि रोटी खाते-खाते उसे उबकाई आने लगती है. रोटी को सूंघकर किनारे कर देता है.
कमीज खोलकर सबको दिखाता फिरता है, “देखो, ये देखो, मेरे बदन को किस तरह खा रहे हैं जाले!”
दीदी उसे समझा देती हैं, “जाले-वाले कुछ नहीं लिपट रहे तेरे बदन पर. हवा-पानी के बदलाव से लाल पित्ती उठ गई है. सबको हो जाती है, पहली बार आने पर. एक-दो दिन में अपने-आप ठीक हो जाएगी .
उसे संतोष नहीं होता, उसकी आँखों में ‘बेकार की बात है’ वाला भाव रहता है. जैसे कह रहा हो – तुम्हारी ये हाय घर-हाय गाँव मेरी समझ में नहीं आ रहा. वहां शहर में ऐसी क्या कमी थी जिसको पाने के लिए बरसों से गाँव चलो, गाँव चलो चिल्ला रहे थे सब !
दीदी उसकी ओर ध्यान देने की बजाय हमारी ओर देखने लगती हैं. और हम नए सिरे से घर का निरीक्षण करने लगते हैं. जालों का हमारे घर से पुराना संबंध है.
जालों का हमारे घर से पुराना संबंध है, जब भी जाले लगे, माहौल भारी हो गया. एक डर व्याप गया सारे घर में. दीदी ऐसी घटनाओं की चश्मदीद गवाह हैं. हो सकता है उनकी भावुकता में कहीं यह डर भी छिपा हो.
बताते हैं, पहली बार जाले यहाँ तब लगे थे जब ताऊजी स्वतंत्रता आंदोलन पकड़े गए थे. हमारे जैसे दूर-दूराज के गाँव में यह अकेली घटना थी. इसलिए लोग समझ नहीं पाए, उनको क्यों पकड़ा गया है, कहाँ ले जाया गया है. तब घर की दीवारों तक में भय बैठ गया था.
ताज्जुब है, तब आदमियों से भरे घर में जाले इतनी जल्दी कैसे फैल गए. यही ताज्जुब आज इस गाँव के घरों को देखकर हो रहा है. हो सकता है, आदमियों के ठंडा पड़ते ही कीड़े-मकोड़ों की गति तेज हो जाती हो. यह भी हो सकता है, जालों के फैलने का कोई और अर्थ हो.
बचपन में हमें ऐसे विश्वासों की कई कहानियाँ सुनाई गई थीं-देखी हमने नहीं हैं. ये बातें हमारे पैदा होने से पहले की हैं. हमारा जन्म आजादी के बाद हुआ. उस समय तक घर में तीन ही बच्चे थे- यशोदा दीदी, प्रताप भैया और कांता दीदी. चाचाजी की तो शादी ही चव्वन-पचपन के आस-पास हुई.
हमारे होश सँभालने तक आमा और बूबू की मृत्यु हो चुकी थी. ताऊजी घर के मुखिया हो गए थे. वैसे भी घर में वही एक मर्द बचे थे. पिताजी शहर में नौकरी करते थे. चाचाजी को भी पढ़ने के लिए अपने पास बुला लिया था. इंटर के बाद नौकरी भी लगवा दी थी.
इसलिए बचपन की हमारी सारी यादें ताऊजी के साथ जुड़ी हैं. जब भी गांव का ध्यान आता है, इस विशालकाय मकान की खोई पर फरसी की लंबी नली पकड़े, खादी का कुर्ता-पाजामा-टोपी पहने, अधपकी नुकीली मूछों वाले एक व्यक्ति की आकृति सामने आ जाती है.
तब हम गुड्डे-गुडिया थे, ताऊजी चाबी घुमा देते थे, हम हरकत में आ जाते थे. मुंह खोलते थे बंद करते थे, ताली बजाते थे, ठुमक-ठुमक चलने लगते थे. हम से बड़े गड्डे-गुड़िया थे-पिताजी, चाचा, ताई, मां और चाची. चाबी भी ताऊजी को ही घुमानी होती थी. सब चाबी घूमने के इंतजार में रहते थे.
परिवार के भविष्य को लेकर ताऊजी के पास एक सपना था. अपर विश्वासों और मान्यताओं के दम पर एक सूत्र था. सब उसी सूत्र के अनशासन बँधे थे, लोग ही नहीं कीड़े-मकोड़े भी. तब बंदर-बाहर, गोठ-भीतर कहीं जाते नहीं होते थे. हो भी नहीं सकते थे. अनुशासन के विरुद्ध जाने का साहस किसमें था.
हमारा सामना उनसे सही में रात को लालटेन की रोशनी में होता था. दिन-भर की छूट, सूरज के सिद्ध मंदिर की आखिरी चोटी को लाँघने के साथ ही खत्म हो जाती थी.
गाय-बछियों के लौटने से थोड़ा पहले हमें खेल खत्म कर घर लौट आना होता था. माँ, ताई और चाची काम से लगभग रात ढल जाने के बाद ही लौटती थीं. क्रम यों था-माँ, ताई और चाची में से एक गोठ जाएगा, डंगरों को घासपात देने और दूध दुहने. दूसरा नौले से पानी लाएगा और तीसरा जाएगा सीधा चूल्हे की तरफ. चाय सुड़कने के बाद हम भाई-बहन लालटेन के इर्द-गिर्द सिमट जाते थे और ताऊजी बाराखड़ी से लेकर आधे, पौने, सवइया के पहाड़े रटाते थे. यह सिलसिला चलता था खाना पकने तक. वैसे इससे ज्यादा हम बैठ भी नहीं सकते थे, एक ड्योढ़ा ड्योढ़ा, दो ड्योढ़ा तीन कहते ही जीभ लड़खड़ाने लगती थी. नींद के झोंके में सिर लालटेन से जा टकराता था.
इस भरे-भरे घर का शोर धीरे-धीरे कब कम होता गया, किसी के पास ठीक हिसाव नहीं है. एक बार बाहर निकलने का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर थमा नहीं. पिताजी और चाचाजी के बाद प्रताप भैया निकले थे. उन्हें भी आठवीं पास करने के बाद पिताजी अपने साथ ले गए थे, पढ़ने को. मैं और कांता दीदी पाँचवीं पढ़कर गए थे. फिर एक-एक कर सभी बच्चों को लाया गया, अच्छी शिक्षा देने के लिए.
ताऊजी ने कोई आपत्ति नहीं की. उन्हें खुशी थी, बल्कि एक उत्साह था कि अगली पीढ़ी सुधर जाएगी. कुछ बनकर रहेगी. बाप-दादा, गाँव-इलाके का नाम रोशन करेगी. उन्हें पहला झटका तब लगा जब औरतों ने भी निकलना शुरू कर दिया. सबसे पहले माँ आई थीं. तर्क यह था कि इतने बच्चों की देखभाल करने और खाना पकाने को एक औरत यहाँ चाहिए. ताऊजी इसके पक्ष में नहीं थे. उनके स्वर में नाराजगी का पहला स्वर तभी देखा गया. पहली बार उन्हें बात के लिए तर्क करना पड़ा कि इस तरह तो खेती-बाड़ी, घर-जायदाद चौपट हो जाएगी. तीन औरतें नहीं संभाल पा रही हैं, बाद में क्या होगा?
इसके बाद चाची चली आई, श्याम की बीमारी के बहाने. गांव में रह गए ताई, ताऊजी और यशोदा दीदी. परिवार गाँव से ही नहीं टूटा, शहर में भी बिखर गया. चौथी श्रेणीवालों के लिये बने सरकारी क्वाटेर में सबका साथ रहना मुश्किल था. जगह थोड़ी थी. लिए चाचाजी को अलग इंतजाम करना पड़ा. नौकरी लगने के बाद प्रताप भैया ने भी अलग व्यवस्था कर ली.
ताऊजी इस पूरे प्रकरण में खामोश रहे. यशोदा दीदी बताती हैं- उन्हें इस बिखराव का दुख से गाँव के बेसहारा छूट जाने का डर था. उन्हें तक रहा.
उनका डर सही निकला. उनकी मौत के बाद गाँव का रिश्ता एक तरह से खत्म ही हो गया. पिताजी की असामयिक मृत्यु ताऊजी से पहले ही हो गई थी और चाचाजी थे दिल के मरीज. उनके लिए पहाड़ों पर आना वैसे ही खतरनाक था.
ताऊजी की तेरहवीं पर आखिरी बार गाँव में सब इकट्ठे हुए थे. तब भी यह सवाल उठा था-गाँव का क्या इंतजाम हो? उस समय चाचाजी ने समस्या हल कर दी थी कि वे रिटायरमेंट लेकर गाँव आ रहे हैं. सबको राहत महसूस हुई. लेकिन दो-तीन महीने बाद ही दिल का दौरा पड़ने से उनको कार्यक्रम रद्द करना पड़ा.
वही सवाल आज फिर खड़ा है, पहले से कहीं ज्यादा प्रखर रूप में.
जमीन की चिंता नहीं है. ताऊजी ही निकट कुटुंबियों को सौंप गए थे. उन्हीं का लिहाज है जो इन्होंने आज तक जमीन छोड़ी नहीं है. वरना यहाँ कौन किसकी जमीन जोतने को तैयार है. जहाँ पैदावार न के बराबर हो, वहाँ अपने ही खेत बोझ बन जाते हैं.
जमीन आबाद है, इसलिए हर बरसात में जो खेत टूट जाते हैं, उनकी मरम्मत होती रहती है. खेत पूरी लंबाई-चौड़ाई में सुरक्षित हैं. वरना जंगली काँटे और अनायास उग आए चीड़ के पेड़ खेतों में जड़ें फैलाकर उनके खेत होने के चिह्न मिटा देते.
समस्या मकान की है. उसी को लेकर चिंता है कि अगर इसी तरह लावारिस छोड़ दिया गया तो दो-चार साल और चलेगा, बस. सारी चर्चा मकान की व्यवस्था को लेकर है. यशोदा दीदी बार-बार रुआँसा हो जाती है. भैया गंभीर हैं, लगातार कुछ सोच रहे हैं.
एक व्यर्थ होती जा रही बहस में उलझे हम किसी नतीजे पर नहीं पर हैं और अंत में मौन साधकर चुप हो जाते हैं.
इस मौन को तोड़ते हुए प्रताप भैया ने कहा, “ऐसा करते हैं, एक बचीराम चाचाजी से बात कर लेते हैं. वे सुलझे हुए आदमी हैं, यहाँ के व्यवहार को हमसे बेहतर जानते हैं. उनसे बात करने से कोई रास्ता निकल सकता है.”
बात जंच गई. तय हुआ चाचाजी से बात करने के बाद ही आगे सोचेंगे. बात ठीक भी थी. इतनी देर से हम केवल इच्छाओं को ही व्यक्त कर रहे थे.
चंदर की इच्छा थी, “कुछ ऐसा हो जाए कि हमारा आना-जाना बना रहे.”
“हाँ, और जो दो-चार दिन के लिए आए, उसे असुविधा न हो, एक व्यवस्था बनी रहे,’ कमल का कहना था.
“यह तो तभी संभव है जब हममें से कोई स्थायी रूप से यहाँ रहे,’ प्रताप भैया ने कहा.
“पर फिलहाल स्थायी रूप से यहाँ रह कौन सकता है?” मेरी समझ में नहीं आया.
इस बीच श्याम बोल गया, “न होता हो कोई इंतजाम तो, बेकार हाय-हाय करने से क्या फायदा, बेच दो. हमारा यहाँ आनेवाला ही कौन है ? और हमें यहाँ से फायदा भी क्या हो रहा है?”
पता नहीं श्याम ने गंभीरता से कहा था या किसी नतीजे पर नहीं पहुँचने की खीझ में कह गया.
असल में, सवाल यहाँ से कोई लाभ होने, न होने का ही नहीं है, अपने मूल से जुड़े रहने का है. एक शहर से दूसरे शहर में तबादला होने पर पहले का अनावश्यक सामान बेचकर, दूसरे में नई स्फूर्ति से बस जाने और पैतृक स्थान को, निर्लिप्त होकर स्मृति से निकाल देने में अंतर होता है. यही अंतर जमीन से आदमी के रिश्ते को बनाता है. इस रिश्ते का जीवित रहना ही आदमी के जीवित रहने का पर्याय भी है. वरना घर, गाँव, शहर या देश का क्या अर्थ रह जाएगा. देश-प्रेम भी तो अपनी जमीन से जुड़े मोह का ही नाम है.
यह बहस रात ढलते वक्त चाय पीते-पीते हुई थी. प्रताप भैया तभी बचीराम चाचा के पास जाना चाहते थे, ताकि बात बन गई तो हमारे जाने तक औपचारिकताएं पूरी हो जाएँ. पर भाभी ने रोक दिया कि चाचाजी अभी-अभी बाजार से सामान लेकर आए हैं. थक गए होंगे. इस समय आराम करने दो, कल बात कर लेना.
सवेरे चाचाजी टहलते हुए खुद ही आ गए. प्रताप भैया मकान का सार्वजनिक उपयोग चाहते थे, उसी को ध्यान में रखकर बोले, “चाचाजी, हम चाहते हैं इतने बड़े मकान का कुछ उपयोग हो जाए. खाली पड़ा रहने से क्या फायदा!”
“बात तो ठीक है, क्या उपयोग चाहते हो?” इसी बावत तो आपसे बात करनी है.” चाचाजी ने ‘हूँऽऊ’ भर कहा और प्रताप भैया ने बात जारी रखी, “ऐसा है, हम देख रहे हैं, गाँव में स्कूल चाहें तो हमारे मकान में स्कूल खुल सकता है, टूट-फूट की मरम्मत हम देते हैं. सफाई, रंग-रोगन कर देते हैं. हमारा स्वार्थ सिर्फ इतना है कि अगर किसी को आपत्ति न हो तो स्कूल पर पिताजी का नाम डलवा दें.”
बचीराम चाचा पहले तो खामोश रहे. लगा, कुछ सोच रहे हैं. फिर धीरे-थके स्वर में बोले, “बात तो तेरी ठीक थी पर हालत ये है, गाँव से आधेपौने मील पर जो स्कूल है जिला परिषद् का, उसी का चलना मुश्किल हो गया है. तीन-चार गाँव के बच्चों को मिलाकर भी पैंतीस-चालीस से ऊपर नहीं हो रहे फर्जी नाम लिखवा रखे हैं. तुम लोग जो दिल्ली-लखनऊ रहते हो, तुम्हारे बच्चों के नाम भी यहाँ के स्कूल में दर्ज हैं. मास्टर इलाके के हैं, रजिस्टर में गिनती पूरी कर देते हैं. वरना स्कूल कब के रद्द हो गए होते. बच्चे तो तभी होंगे ना, जब लोग यहाँ रहेंगे. यहाँ हालत ऐसी है, मुर्दा उठाने को भी दो-तीन गाँवों से लोग इकट्ठे करने पड़ते हैं.” उन्होंने एक खोखली हँसी वाले अंदाज में मुँह को थोड़ा खोला, फिर खामोश हो गए. लेकिन उनकी खामोशी जो सवाल खड़ा कर गई, उसने हमें हिला दिया. उनसे बात करने से पहले हम थोड़ा उत्साहित थे. एक उम्मीद-सी बँध आई थी. उनकी बात सुनने के बाद अपने स्थान से जुड़े रहने का अहसास ज्यादा तकलीफदेह हो गया. एक बेहद निजी-सी लगने वाली चीज को जिसे हमारे पुरखों ने औलाद की तरह छाती से लगाए रखा, लावारिस कैसे छोड़ा जाए? ताऊजी एक हद तक शायद ठीक थे. उनका दुःख कुछ-कुछ समझ आ रहा है. हम, जिनका एक तरह से बहुत करीबी नाता नहीं है इस जमीन से, इस कदर बेचैनी महसूस कर रहे हैं. ताऊजी के तो खून से सनी थी यह मिट्टी. विवशता के घने दबाव में बच्चों को रोता-बिलखता छोडकर भागने की तैयारी कर रहे आदमी के आंतरिक कष्ट को उन्होंने देख लिया होगा.
(Story by Kshitij Sharma)
चाचाजी के जाने के बाद शाम तक फिर कोई बात नहीं हुई. रात ढलते समय हीरा ताई आई थीं, हमारे गाँव आने को लेकर भाभी के सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दे रही थी, “अपने परखों ली. आते-जाते रहना चाहिए.”
“पता नहीं ताई, दोबारा कब आना हो.” प्रताप भैया की आवाज में बेचारगी थी. उसे देखकर दु:ख हुआ. पैतृक संपत्ति भी कितना बडा बंधन ठहरा. इससे बँधे रहना भी कष्टकर है और छूट जाने की इच्छा करना भी. शारीरिक मुक्ति का तो कोई अर्थ ही नहीं होता. आदमी की सोच इस तरह प्रभावित हो जाती है कि कभी-कभी पूरी दुनिया बालिश्त-भर जगह में सिकुड़ जाती है.
“भाई साहब, इसमें इतना अफसोस करने की क्या बात है? नहीं कोई इंतजाम हो सका तो क्या कर सकते हैं. आज तक भी तो पड़ा हुआ था, आगे भी पड़ा रहने दो.”
“हूँऊँऊँ .’ उनका गंभीर मौन टूटा नहीं. लगा, इस समय उनमें ताऊजी अवतरित हो गए हैं. जब भी ताऊजी उनमें घुस जाते हैं, संवाद कठिन हो जाता है.
हीरा ताई काफी देर बैठकर गईं. तब ध्यान आया भाभी और दीदी को कि खाने का समय हो गया है. दीदी ने प्रताप भैया को खाने के लिए कहा, “भैया, उठो, खाना खा लो अब, क्या सोच रहे हो तब से?”
“सोच रहा था यशोदा कि अगर कोई यहाँ रहना चाहे तो मुश्किल भी नहीं है. कई तरह के काम हो सकते हैं . सोचता हूँ, दो-एक साल में रिटायरमेंट लेकर मैं ही आ जाऊँ.”
“हाँ, तुम आओगे यहाँ, बुढ़ापे में मरने को.” भाभी ने तत्काल टोक दिया, “रात-दिन की मेहनत के अलावा कुछ खाने-पीने को भी मिलता है यहाँ? चाय तक को दूध नहीं मिला. जब से आए हैं, काली चाय पी रहे हैं. जेब में पैसे हों भी तो लिये-लिये घूमते रहो, चीज तो कोई मिलेगी नहीं. मैं तो तुम्हें कभी नहीं रहने दूंगी ऐसे.”
भैया चुप हो गए. हो सकता है उन्होंने गंभीरता से न सोचा हो . एक खयाल ही आया हो कि ऐसा भी हो सकता है. पर भाभी उस खयाल को ही खत्म कर देना चाहती थीं.
एक खामोशी जो इस बंद घर की दीवारों से बँध गई थी, वह करीब-करीब सन्नाटे में बदल गई.
बाहर का मौन भीतर के कोलाहल का उत्तर नहीं हो सकता. ‘खाना तो खा लो,’ दीदी की थकी-थकी आवाज उस मौन में गूंजती हुई-सी लगी.
खाना खाकर, हाथ धोने, बाहर आते वक्त सिर बचाकर निकलना पड़ा. जाले सिर से उलझ गए थे. रोज ऐसे ही उलझ जाते हैं. लपेटा डालकर अपनी मौजदगी और ताकत को जता देते हैं. परसों जिस हिस्से से इन्हें तोड़ा था, आज वहाँ फिर बिछ गए हैं. छत की बल्लियों से उठते-उठते खिड़कियों को लाँघकर नीचे के कमरों तक पहुँच गए हैं.
एक मन करता है, दो दिन की मेहनत लगेगी, उखाड़ दें उन्हें. बिलकुल साफ कर दें. फिर हाथ रुक जाता है, एक खयाल आता है – किसी को तो रहना है यहाँ.
(Story by Kshitij Sharma)

15 मार्च 1950 को अल्मोड़ा के मानिला गाँव में जन्मे क्षितिज शर्मा की कहानी ‘किसी को तो रहना है यहाँ’ उनकी किताब ‘उत्तरांचल की कहानियां‘ से ली गयी है. भवानी के गाँव का बाघ, ताला बंद है, उकाव, समय कम है, पामू का घर, क्षितिज शर्मा की कुछ अन्य कृतियां हैं.
काफल ट्री वाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिये यहाँ क्लिक करें: वाट्सएप काफल ट्री
काफल ट्री की आर्थिक सहायता के लिये यहाँ क्लिक करें




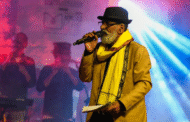

































4 Comments
विनोद
Bahut vadia h ji
प्रकृति कि गोद को नमस्कार
संजय कबीर
इन्सान नही तो जाले ही सही ।आखिर किसी को तो रहना है यहाँ …….एक बढ़िया कहानी ,खूबसूरत अंदाजे बयां
विनोद
सच में कोई नहीं रहना चाहता तो मैं रह सकता हु
मेरी दिली इच्छा है पहाड़ो में एकांत में शांति के साथ प्रकृति में रहने की
9896608150
विनोद कुमार यादव
रेवाड़ी हरियाणा
Kamal lakhera
क्षितिज शर्मा जी ने दिल को झकझोरती कहानी या कहूं कथा लिख दी, ‘ किसी को तो रहना है यहां ‘ लेकिन एक इंसान के तौर पर हमारी इच्छा शक्ति इतनी कमजोर हो गई है कि वो कहानी का ‘ किसी ‘ तो नहीं बनना चाहता । मम॑स्पर्शी ।