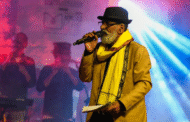आधुनिकता को अंग्रेजों के आगमन और उनकी भाषा के साथ आये ज्ञान-विज्ञान के साथ जोड़कर देखा जाता है. कुछ हद तक इस बात में सच्चाई हो सकती है, मगर जो नया समाज भारत में बना, उसके लिए सिर्फ यूरोपीय आधुनिकता को श्रेय देना निश्चय ही अधूरा सच है. यह कहना भी ठीक नहीं होगा कि भारतीय आधुनिकता इस देश में पहले से चले आ रहे ज्ञान-विज्ञान का विकास था; वास्तविकता यह है कि अंग्रेजों के आने से पहले शिक्षा का ऐसा ढाँचा था ही नहीं, जो समाज के हर वर्ग के लिए सहज उपलब्ध हो. कुछ खास लोगों को पढ़ने-लिखने की सुविधा प्राप्त थी, जिसे वे लोग अपने वर्गीय हितों को ध्यान में रखकर संकलित और सम्पादित करते थे. पिछली करीब दो-तीन सदियों में सारे संसार में एक नया समाज और उससे जुड़ी सोच का प्रादुर्भाव हुआ है, भारत उससे अछूता नहीं रहा है, मगर भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना इस प्रकार की रही है यहाँ अध्ययन-अध्यापन और चिंतन से जुड़ी उपलब्धियां कुछ खास जातियों को ही उपलब्ध रही हैं, यही कारण है कि उस आधुनिकता का प्रभाव शेष देशों की तरह का विकासशील नहीं रहा है.
उत्तराखंड का आधुनिक सांस्कृतिक ढाँचा अंग्रेजों की देन है, इसका बड़ा कारण यहाँ की भौगोलिक स्थिति है जो अंग्रेजों को अपने मूल देश के समान महसूस होने के कारण उन्हें ये इलाके अपने अन्तरंग लगते थे. जाहिर है कि उन्होंने यहाँ जो शिक्षण-संस्थाएं स्थापित कीं, वे उनके अपने बच्चों में शिक्षा के संस्कार पैदा करने के लिए थीं. उत्तराखंड के मसूरी, देहरादून, नैनीताल आदि स्थान इसी तरह के थे. इन जगहों के स्कूल विशेष सुविधाओं से युक्त थे, वहां से विभिन्न क्षेत्रों की बड़ी हस्तियों का जन्म हुआ. आज भी अलग-अलग क्षेत्रों की उन नामचीन राष्ट्रीय हस्तियों का जिक्र किया जाता है जिन्होंने अपने आरंभिक शिक्षा-संस्कार इन्हीं स्कूलों से प्राप्त किये.
यह बात कम आश्चर्य की नहीं है कि इन जगहों से राष्ट्रीय स्तर पर फैली प्रतिभाओं में से किसी ने भी राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भले ही खूब ख्याति अर्जित की हो, अपनी जड़ों से जुड़े क्षेत्र को लेकर काम नहीं किया. अंग्रेजों द्वारा स्थापित यहाँ के पब्लिक स्कूलों की ख्याति आज भी कम नहीं हुई है, मगर यह तथ्य अपनी जगह आज भी मौजूद है कि उत्तराखंड के पहाड़ी समाज को देश की मुख्यधारा के समाज के साथ जोड़ने का काम इन स्कूलों ने कभी नहीं किया.
निश्चय ही यह काम किया आजाद भारत की निर्वाचित सरकार के द्वारा स्थापित उच्च-शिक्षण संस्थाओं ने. जिन सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनितिक प्रतिभाओं ने इस कार्य में पहल की, हालाँकि उनका उदय आजादी से पहले हो गया था, मगर उनकी परिकल्पना को साकार रूप आजादी के बाद के वर्षों में ही मिला. खास बात यह है कि जिस व्यक्ति ने इस क्षेत्र में पहल की, वह कोई शिक्षा-शास्त्री या अध्ययन-अध्यापन से जुड़ा व्यक्ति नहीं था. एक पिछड़े इलाके का कल्पनाशील जंगलों का ठेकेदार था, जिसका अभ्युदय एक संयोग भी कहा जा सकता है.

वर्ष 1951 में जब अविभाजित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अल्मोड़ा के मूल निवासी गोविन्दबल्लभ पन्त थे, नेपाल-पिथोरागढ़ के एक पिछड़े गाँव के व्यापारी दानसिंह बिष्ट की आर्थिक हालत जब बेहतर हो गयी, उनके मन में विचार आया कि इलाके के लोगों में शिक्षा का प्रचार-प्रसार करके उन्हें मुख्यधारा के भारतीय समाज के साथ जोड़ने की दिशा में पहल की जाय. उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वो उत्तराखंड में एक उच्चशिक्षण संस्था की स्थापना के लिए भूमि और आरंभिक सुविधाएँ प्रदान करना चाहते हैं, जिसे एक उच्च-स्तरीय अकादमिक संस्था का रूप प्रदान करने में शासन मदद करे. मुख्यमंत्री पंत ने इसके लिए भरपूर सहयोग की पेशकश की और प्रदेश के शिक्षा विभाग को आदेश दिया कि इसके लिए तत्काल ढाँचा तैयार किया जाये. तत्काल प्रदेश के शिक्षा विभाग ने देश के सबसे बड़े प्रान्त (उत्तर प्रदेश) के दो छोरों – दक्षिण-पूर्व (ज्ञानपुर, वाराणसी) और उत्तर पूर्व (नैनीताल) में आदर्श महाविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की. नैनीताल की अयारपाटा पहाड़ी पर स्थित एक मशहूर मिशनरी स्कूल को खरीदकर दान सिंह बिष्ट ने पांच लाख रुपये का अनुदान भेंट किया और इस तरह अपने पिता ठाकुर देव सिंह बिष्ट के नाम से उत्तराखंड के पिछड़े इलाके में वर्ष 1951 में प्रदेश के पहले बड़े कॉलेज की आधारशिला रखी गयी. प्रदेश सरकार ने इस कॉलेज के प्राध्यापकों के लिए विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों से अधिक वेतन और सुविधाओं की पेशकश की जिस वजह से यहाँ देश के ख्यातिप्राप्त विद्वानों का आगमन हुआ.
यही वह अवसर था, जब उत्तराखंड में पहली बार आधुनिकता का प्रवेश हुआ. जिसे आज उत्तराखंड कहा जाता है और जिसके अंतर्गत कुमाऊँ और गढ़वाल मंडल आते हैं, उनके सुदूर अंचलों से लड़के और लड़कियाँ इस कॉलेज में आने लगे. जो लोग पहले सुदूर इलाहाबाद, लखनऊ और वाराणसी जाकर उच्च-शिक्षा प्राप्त करते थे, अपने क्षेत्र में ही नई आधुनिक शिक्षा को ग्रहण करने की सुविधा प्राप्त करने लगे और इस तरह अपनी जड़ों से जुड़कर, अध्ययन मनन का सिलसिला शुरू हो गया. इसलिए यह आज अनायास नहीं है कि उत्तराखंड के लोगों का आधुनिकता की धारा के साथ वास्तविक जुडाव, जो एक तरह से उनकी स्थानीयता को अंतर्राष्ट्रीयता के साथ जोड़ने की मुहिम की तरह सामने आया, पंडित गोविंदबल्लभ पन्त की प्रेरणा और ठाकुर दान सिंह बिष्ट की दानशीलता से सामने आया.

यद्यपि नए ज्ञान-विज्ञान के साथ परिचय की यह पहल कॉलेज के खुलने के साथ ही हो गयी थी, मगर इसका वास्तविक ढाँचा, जो इसकी जड़ों के जुड़ाव के साथ ज्ञान-विज्ञान के विस्तार को लेकर सामने आया, 1952 में भौतिकी के प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हुए डॉ. डी. डी. पन्त के बाद शुरू हुआ. यद्यपि डॉ. पन्त मुख्य रूप से शोध की दुनिया में जीने वाले एक एक भौतिक-विज्ञानी थे, मगर उनकी रुचि सिर्फ अपने विषय तक सीमित नहीं थी. वह अगले एक दशक तक देश के दूसरे स्थानों में भी भटकते रहे, अपनी कार्य योजना को लेकर चिंतन करते रहे, मगर अन्ततः जब वह 1963 में प्रधानाचार्य के रूप में इस कॉलेज में वापस आये, उन्हें अपनी कार्य-योजना को धरातल पर उजागर करने का वास्तविक मौका मिला. तब भी यद्यपि उन्होंने अपनी शोध की दुनिया को नहीं छोड़ा, मगर शिक्षा के वास्तविक दायित्व को विस्तार देते हुए उसे क्षेत्र की जरूरतों के साथ जोड़ने की पहल की. उनका आरम्भ से ही मानना था कि शिक्षा और शोध का वृक्ष कोरी हवा में खड़ा नहीं हो सकता, बिना जमीन के वह नहीं पनप सकता, जब तक कि उसे जमीं का टुकड़ा और खाद-पानी मुहय्या न हो.
एक अध्यापक और वैज्ञानिक के रूप में डॉ. पन्त ने इस मिथक को भी तोड़ा कि विज्ञान की पढ़ाई अंग्रेजी के बिना संभव नहीं है. उनकी हमेशा कोशिश रहती थी कि वे मातृभाषा में विद्यार्थियों तक अपनी बात पहुंचाएं, हालाँकि कठिन तकनीकी शब्दावली के पक्ष में वे कभी नहीं रहे. उनका मानना था कि जिस भाषा को विद्यार्थी आसानी से समझते हैं, उसी में उन्हें ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए. जब वह प्राचार्य थे, तब भी बी.एस-सी. के विद्यार्थियों की कक्षा कभी-कभी हिंदी में लेते थे जिसे सुनने के लिए दूसरे संकायों के विद्यार्थी भी बड़ी संख्या में उनकी कक्षा में शामिल होते थे. वो हमेशा मानते थे कि अध्यापक का काम विषय की कोरी जानकारी देना नहीं, अपने विद्यार्थियों में उसकी समझ पैदा करना है.
पाठ्यक्रम के अलावा ज्ञान के संस्कार पैदा करने को वह खास अहमियत देते थे, इसके लिए वह अपने समय में प्रचलित ज्ञान की अलग-अलग शाखाओं के साथ युवाओं के मन में जुड़ाव पैदा करने को विशेष महत्व देते थे. पाठ्यक्रम को रटकर उसे ग्रहण करने के वे कभी पक्षपाती नहीं रहे. अपने समय का ज्यादातर हिस्सा लैब में बिताने के बावजूद वे अलग-अलग मंचों के जरिए विज्ञान को समाज के बीच ले जाने की पैरवी करते थे. अपने भाषणों में तो हमेशा कहते ही थे, 1965 में डी. एस. बी. कॉलेज में उनके द्वारा स्थापित संस्था ‘द क्रैंक्स’ इसका अच्छा उदाहरण है. इस संस्था के वह अध्यक्ष थे और उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित विषयों पर उन्होंने विद्यार्थियों के दर्जनों सेमिनार-व्याख्यान आयोजित किये. संस्था में विज्ञान, कलाओं, साहित्य आदि से जुड़े तमाम विद्यार्थियों की अभिरुचियों को उन्होंने पाठ्यक्रम के विषयों की तरह महत्व दिया और उनकी प्रतिभा के सुषुप्त कपाटों को खोला.

1973 में जब डॉ. पन्त कुमाऊँ विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति नियुक्त हुए, उन्होंने सबसे पहले हिमालयी अध्ययन से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मलेन आयोजित किया और हिमालय, उसके मानव-भूगोल, पर्यावरण और संस्कृति के सभी जरूरी पक्षों को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों और चिंतकों के सरोकार उजागर किये. संस्कृति के प्रमुख संवाहक – साहित्यकार – के महत्व को स्वीकार करते हुए उन्होंने विवि के प्रथम दीक्षांत समारोह में दीक्षांत भाषण देने के लिए आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा को आमंत्रित किया. भारत के अनेक महत्वपूर्ण विचारकों, वैज्ञानिकों और साहित्यकारों के साथ विवि के विद्यार्थियों के बीच संवाद स्थापित किया.

1974 में भारत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जब कॉलेज में पहली बार प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों के लिए गाँधी के विचारों के परिचय की शृंखला आरंभ की. डॉ. पन्त को यू. जी. सी. ने यह कठिन काम सौंपा. उन्होंने उसी वर्ष हिंदी में (‘गाँधी सन्दर्भ’) और अंग्रेजी में (About Gandhi) के दो खण्डों में संकलन तैयार किये. इन संकलनों में संसार भर में गाँधी को लेकर जो भी काम हुआ है, डॉ. पन्त ने उसका संकलन और संपादन किया. भारतीय भाषाओँ में यह अपने ढंग का पहला काम है जिसे स्नातक स्तर के हरेक विद्यार्थी को पढाया जाता था, चाहे वह कला संकाय का हो, विज्ञान या वाणिज्य संकाय का. किताब के पहले खंड में लुई फिशर, गुन्नार मिर्डल, लेरी कॉलिंस, डोमीनीक लैपियर, रामनाथ सुमन, रोम्यां रोलां, जैनेन्द्र कुमार, चेस्टर बाउल्स और महात्मा गाँधी शामिल हैं; जब कि दूसरे खंड में अर्नेस्ट फ्रेडरिक शूमाकर, एरिक एरिकसन, होरेस एलेक्जेंडर, जयदेव सेठी, जे. बी. कृपलानी और निर्मल कुमार बोस शामिल किये गए हैं. लगभग आठ-दस वर्षों तक यह पाठ्यक्रम खासा लोकप्रिय हुआ, मगर जैसा कि होता आया है, बाद के कुलपतियों ने इसमें कोई रुचि नहीं ली और यह योजना भी अतीत की चीज बनकर रह गयी, लगभग उसी तरह जैसे डॉ. पन्त आज अतीत बनते जा रहे हैं.
शायद इसीलिए यह बात जरा भी गलत नहीं है कि वर्तमान परिस्थितियों में उत्तराखंड के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र में आज जो दयनीय हालत हो गयी है, उसे देखते हुए एकमात्र उम्मीद डॉ. डी. डी. पन्त के दिखाए रास्ते में ही दिखाई देती है.
यह वर्ष डॉ. पन्त का जन्म शताब्दी वर्ष है इसलिए इस गंदे-फूहड़ और डरावने माहौल में उन्हें याद करते रहने से शायद हम अपने और अपनी भावी पीढ़ियों के लिए ताकत अर्जित कर सकते हैं. इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता.

लक्ष्मण सिह बिष्ट ‘बटरोही‘ हिन्दी के जाने-माने उपन्यासकार-कहानीकार हैं. कुमाऊँ विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग के अध्यक्ष रह चुके बटरोही रामगढ़ स्थित महादेवी वर्मा सृजन पीठ के संस्थापक और भूतपूर्व निदेशक हैं. उनकी मुख्य कृतियों में ‘थोकदार किसी की नहीं सुनता’ ‘सड़क का भूगोल, ‘अनाथ मुहल्ले के ठुल दा’ और ‘महर ठाकुरों का गांव’ शामिल हैं. काफल ट्री में नियमित कॉलम.
काफल ट्री वाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिये यहाँ क्लिक करें: वाट्सएप काफल ट्री
काफल ट्री की आर्थिक सहायता के लिये यहाँ क्लिक करें