बचपन का धारचूला
गंगोत्री गर्ब्याल
जिस दिन कुंचा धारंचूला पहुंचता, उस दिन की खुशी का कोई पार नहीं. चित्त अति ही प्रफुल्लित होता. पटघार से धारचूला दिखता, मैना पक्षियों के झुण्ड ‘चिर-चिर’ शोर मचाते, चहचहाते. उनका चहचहाना लगभग छः सात महीने बाद सुनकर अजीब सा अपनत्व लगता, बड़ा सुहाता.
ब्यांस वालों के अपने-अपने खेड़े निश्चित हैं. ग्राम-कुटी (अन्तिम ग्राम) के कुटियाल कुटी खेड़ा में रहते हैं. रौंगकांग के ‘रौंगपा’ खेड़ा में रहते हैं. कुटी खेड़ा तथा रौंगकांग खेड़ा वर्तमान बस स्टेशन के निकट एक दूसरे से लगे हुए हैं. नाबी का नबियाल खेड़ा, रौंगकांग खेड़ा से कुछ दूर ढलान के पार है. नपलच्याल खेड़ा से लगा गुंजियाल खेड़ा है. इसी खेड़ा से लगे कुछ मकान बुदियाल एवं छांगरू (नेपाल) के हैं. कुछ चैदाँस वालों के मकान मल्ली बाजार में हैं.
इन सब खेड़ों से कुछ दूरी पर ग्यांग खेड़ा एक विस्तृत स्थान पर बसा हुआ है. गब्याँग गाँव के लोग ‘गर्ब्याल’ कहलाते हैं. गर्ब्याल खेड़ा के आगे मिशनरी वालों के घर, चर्च एवं बड़ा अहाता है. 1962 के बाद धारचूला की कायापलट हो गई है. खेड़े पूर्ववत हैं पर बाहर से पंजाबी, मुसलमान तथा अन्य व्यापारी आ गए हैं. कुछ व्यापारियों ने मकान भी बना लिये हैं.
हमें अपने बचपन का धारचूला विस्मृत नहीं होता. कुंचा पहुंचते ही हम बेर तोड़ने जाते. वर्तमान अस्पताल के पीछे बेर की झाड़ियां फैली थीं. कुछ गुलाबी, सुनहरे रंग लिये बेर हमें आकर्षित करते, बेर तोड़ने में कांटे की चुभन भी सहते, पर झगुली की जेब बेरों से भरी होती.
वर्तमान अस्पताल के पास एक बड़ा चिकना पत्थर था. हम बच्चे उस पत्थर पर किसी प्रकार चढ़ते व कभी सिर के बल फिसलते, कभी दो टांगें आगे बढ़ाकर फिसलते.
कहा जाता है कि वर्षों पूर्व पूर्वज अपने ग्रीष्मकालीन ग्रामों से घाम तापने धारचूला आया करते थे. दारमा घाटी के निवासी जौलजीवी, गलाती, गोठी व बलुआकोट में आते थे. गुंजियाल द्यौथला (नेपाल), तंतंती जाया करते थे. बुदियाल मिसलमथां एवं राइसौं (नेपाल) में रहा करते और कुछ गर्ब्याल परिवार भी थे. उनकी झोपड़ियां बनी थीं. कुछ पक्के मकान भी बने थे. 1962 के बाद लगभग सबको वहां छोड़कर भारत आना पड़ा. कुछ परिवार अब भी नेपाल में हैं पर उन्होंने नेपाली नागरिकता स्वीकार नहीं की, अतः वहां की जमीन-मकान उनके नाम पर नहीं हैं. धारचूला के पार दार्चुला-नेपाल में लगभग नब्बे परिवार ब्यांस (भारत) के हैं. उनको भारत में धीरे-धीरे बसाया जा रहा है. यह नयी बस्ती ‘खेतिला’ कहलाती है. दार्चुला में उनके मकान भूमि आदि उनके नाम चढ़ नहीं पाती.
उन दिनों धारचूला के खेड़ों में गिने-गिनाए पत्थर के मकान थे. दो कमरों के मकान के भीतर का कमरा बड़ा होता था और आगे खुला रहता. भखार (बुखार/काठ का बक्से नुमा) से कुछ घेरकर उसे कमरा सा बनाते. अधिकांश झोपेड़ियाँ ही बनी होतीं. किसको मालूम था कि एक दिन रंङ शौकों को यहीं दिन काटने पड़ेंगे.
लोग जंगल से निंगाल एवं बल्लियां काट लाते और लम्बी घास (खुयू) समिल से झोपडियां छाते थे. झोपड़ी में एक ही कमरा रहता- अपनी परम्परानुसार कमरे के बीचों-बीच चूल्हा बनाते, उसी में भोजन पकाते और आग तापते. आग के जलने से कमरा कुछ गर्म हो जाता.
तब लकड़ी काटने पर कोई प्रतिबंध नहीं था. लोग लकड़ी काट लाते व अपने जानवरों के लिये घास काटते. घास का लूटा (कुन्यू) बनाते थे. जिनके खच्चर, घोड़ेख् झप्पू, बैल अधिक संख्या में होते, वे उन्हें काली नदी के पार नेपाल-दार्चुला की घास वाली घाटियों में कुछ माह चराने ले जाते. रङ बोली में इसे ग्वार (खरक) ले जाना कहते हैं. घास खाकर जानवर पुष्ट हो जाते थे. उन दिनों शौंकों को अनाज कालीपार नेपाल से लाना पड़ता था. काली नदी भारत एवं नेपाल कीसीमा बनाती है. सुंड, मुण्ड, द्यौथला, दुमलिखू, असन्निबड़ा आदि ग्रामों को शौका अपने खच्चर, झप्पू, बैल एवं बकरियों पर ‘छा’ (नमक) लाद कर ले जाते थे और वहां से ‘छा’ के बदले में लाल चावल, गेहूं, मक्का, मडुवा, उड़द, मिर्च एवं हल्दी लाते.
एक लोकगीत इस प्रकार है
लूण मैले द्यौथला साँट्यो शौका, जामिर पानी
“शौका व्यापारी ने जामिरपानी (नेपाल) के पार द्यौथला जाकर नमक का बदला किया, यानी बदले में अनाज ले आया.”
दूसरा गीत है-
चावल भलौ आछाम को, लूण भलौ कुटी को
आछाम नेपाल के सुदूर क्षेत्र में स्थित है. वहां धान की फसल अच्छी होती है. कहा जाता है कि वहां का चावल अच्छा होता है तथा कुटी गांव (भारत) का नमक अच्छा समझा जाता है. अब स्थिति बिलकुल बदल गयी है. जो नेपाली शौका अनाज दिया करते थे, अब आबादी के बढ़ने से वे अनाज का अभाव महसूस करते हैं.
धारचूला, जौलजीवी, गलाती, कालिका, गोठी, बलुआकोट आदि सभी जगहें लगभग तीन हजार फीट की ऊंचाई पर घाटियों में स्थित हैं. शीतकाल में इन घाटियों में धूप बड़ी देर से निकलती है. हम बच्चे बेसब्री से धूप की प्रतीक्षा करते. ठण्ड के कारण अंगुलियां ठिठुर जातीं. ज्यों ही सूर्य की प्रारम्भिक किरणें प्रांगण में कुछ प्रकाश बिखरातीं, हम बच्चे एक स्वर में बोल पड़ते, उछलते- ‘निपिरायो, निपिरायो’ (नि-सूरज पिरा- आ गया, यो- हर्ष सूचक) ‘धूप आ गई हो.’ ‘धूप आ गई हो.’
अधिकांश पर्वतीय क्षेत्रों में अनचाही धूप होती है. धूप शीतकाल में देर से निकलती है, जल्दी अदृश्य हो जाती है, जबकि ग्रीष्मकाल में प्रातः काल से सायं तक रहती है.
कते ऊन का ताना-बाना ’चान’ कहलाता है. एक कतार में चान बुनती हुई महिलाएं अपने-अपने काम में बढ़ी व्यस्त, परन्तु प्रसन्नचित्त मालूम पड़ती थीं. मन ही मन उनमें स्पर्धा एवं प्रतियोगिता की भावना स्वतः ही जागृत होती. कभी वे हंसी-मजाक के फुहारे छोड़ अपनी थकान दूर करती थीं, उनका ऊनी कारोबार चालू रहता.
पुरुष व्यापार के लिए टनकपुर, दिल्ली एवं कलकत्ता भी पहुंच जाते थे. अधिकतर व्यापारी टनकपुर मण्डी में रहा करते थे, ऊन व सुहागा का व्यापार करते थे. उन दिनों स्वच्छता का बड़ा अभाव-सा था. चिकित्सा भी सीमित थी, अतः प्लेग, हैजा एवं चेचक का बड़ा प्रकोप छाया रहता था. कई शौका व्यापारी इन संक्रामक गगों के शिकार हो जाते थे. कहा करते थे कि टनकपुर की ओर से पत्र आने पर घरवाले किसी अशुभ समाचार की आशंका से मन ही मन डरे रहते थे. हमें याद है, चैत मास में ऊपरी शीतकालीन ग्रामों की ओर बढ़ता था जो हैजे ने कितने ही परिवारों को मौत के घाट उतार दिया होता था. बलिहारी, चिकित्सा विज्ञान की अब उन संक्रामक रोगों पर नियंत्रण पा लिया गया है.
उन दिनों गांवों में स्वच्छता नहीं के बराबर थी. शिक्षा का अभाव था. यातायात की सुविधा नहीं थी. जीवन का तीन-चैथाई भाग पैदल चलने में ही व्यतीत हो जाया करता था. अब भी इसमें प्रगति नहीं हो पायी है.
सायंकाल ‘मुछंग’ (छयूला) फाड़ते थे. मुछंग में लीसा का अंश रहता है. उसे डंठा (छ्यूलास्टैंड) में जलाया करते थे. उसी के प्रकाश में घर का काम होता व बच्चे भी उस प्रकाश में थोड़ा पढ़ा करते. मुछंग की कालिख से कापी-किताब व वस्त्र भी बच नहीं पाते.
हर ग्राम की यही कहानी हुआ करती थी. अब भी है. अब बिजली का जमाना आ गया है. पर नाम भर के लिये. कहूं तो अतिरंजित नहीं. सुदूर गांवों में बिजली की यहीं दशा है कि ‘अभी आई व अभी गयी’.
वर्तमान बस-स्टेशन से तहसील के अन्त तक खेत ही खेत थे, खेतों की मेडें थीं. सायंकाल इन्हीं खेतों में घुड़दौड़ हुआ करती थी. शौका व्यापारी ताकलाकोट मण्डी (तिब्बत) से घोड़े पर सायंकाल गब्यांग पहुंचते थे, ताकलाकोट से गब्याँग लगभग चालीस-पैंतालिस किलोमीटर की दूरी पर है.
घुड़दौड़ में काफी लोग भाग लेते थे. कुछ लोग तो इसमें बड़े माहिर होते थे. बड़ी रौनक रहती. एक प्रकार से घुड़दौड़ की प्रतियोगिता समझिए. चारों ओर दर्शकों की अच्छी-खासी भीड़ जमा रहती.
धारचूला से दार्चुला (नेपाल) जाने के लिए लकड़ी की बल्लियों का कच्चा पुल बनाया जाता था. चैत मास में जब पहाड़ों पर पड़ा हिम पिघलता तो काली नदी का पानी बढ़ता जाता, यहां तक कि वह कच्चा पुल बह जाता और लोगों को आर-पार जाने में बड़ी कठिनाई होती थी. तब लोग काली नदी के आर-पार सुरक्षित स्थान पर बड़ी मजबूत बल्लियाँ गाड देते तथा पक्का-मजबूत रस्सा, जैसे ‘रस्साकसी’ में प्रयोग में लाते हैं, बल्लियों के ऊपरी भाग में कसकर बाँघ देते, जिसके सहारे हिंडोल को आर-पार खींचते. हिंडोल में बच्चों और औरतों को पहले बिठाते थे. कुछ साहसी व्यक्ति, जो तैराक भी होते, वे अपनी कमर पर काठ का अर्द्धगोलाकारनुमा बांध लेते, उसे झुंगोला (रोपवे) पर अटकाकर कलात्मक ढंग से अपने पैरों की हरकत से पार चले जाते. ‘झुंगोला’ एक प्रकार से अविकसित सा रज्जुमार्ग था.
सबसे दुःखदायी दृश्य जानवरों का होता था, जानवरों को एक-एक करके काली नदी में हांकते थे, बलिष्ठ जानवर को अगुवा बनाते थे. जानवर काली नदी के बर्फीले थपेड़ों से जुझते, संघर्ष करते हुए धारचूला के किनारे पहुंचते. जानवरों के मालिक और अन्य लोग जानवरों को प्रोत्साहित करते, कहते थे- ‘ले’, ‘ले’, ‘आ जाओ बा’ आदि. ¬अब यह अभिशाप दूर हो चुका कुछ वर्ष पूर्व भारत सरकार की ओर से काली नदी पर लोहे का पक्का पुल बन गया है.

स्व. श्रीमती गंगोत्री गर्ब्याल तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ
यह लेख सबसे पहले ‘पहाड़’ में छपा था. इसे वहीं से साभार लिया गया है.
वाट्सएप में काफल ट्री की पोस्ट पाने के लिये यहाँ क्लिक करें. वाट्सएप काफल ट्री
काफल ट्री के फेसबुक पेज को लाइक करें : Kafal Tree Online
काफल ट्री वाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिये यहाँ क्लिक करें: वाट्सएप काफल ट्री
काफल ट्री की आर्थिक सहायता के लिये यहाँ क्लिक करें






























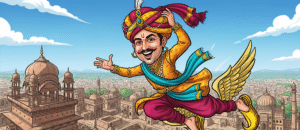






1 Comments
Sudhan Chandra Chandola
गंगोत्री बहन एक बिलक्षणं ब्यक्तित्त्व। उनके तथा बेरीनाग ग्राम स्वराज मंडल के श्री सदन मिश्र के साथ वर्ष 1982 में धारचूला के अनेक गावों में शराब- विरोधी पद यात्राओं में भागीदारी करने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त है। बहन को प्रणाम।