मुझे आजकल लगता है कि मैं कोई जमाने से यहीं खड़ा, हवा चले न चले सिर पटकता पेड़ हूं. या कोई धूल से अटी पिचके टायर वाली जीप हूं जिसके स्टीयरिंग का पाइप काटकर मेरे गांव छोकरे लोहार से कट्टा बनवाने की सोच रहे होंगे. या कोई हिरन हूं जिसकी सींगों को तराश कर, भुस भर दिया गया है और जिसकी कांच की आंखों में उजबकपन के सिवा कोई और भाव नहीं है.
कभी लगता है कि बीमार, मोटे, थुलथुल, सनकी, भयभीत और ताकत के नशे मे चूर लोगों से भरे एक जिम में हूं. पसीने और परफ्यूम की बासी गंध के बीच मुझे एक ऐसी मशीन पर खड़ा कर दिया गया है जिस पर समय लंबे पट्टे की तरह बिछा हुआ है. मैं उस पर दौड़ रहा हूं, पसीने-पसीने हूं, हांफ रहा हूं लेकिन वहीं का वहीं हूं. कहीं नहीं पहुंचा, एक जमाना हुआ. समय का पट्टा मुझसे भी तेज भाग रहा है. अगर मैं उसके साथ नहीं चला तो मशीन से छिटक कर गिर पड़ूंगा और कोई और मेरी जगह ले लेगा. मैं थक रहा हूं यानि समय जरूर कहीं न कहीं पहुंच रहा है. मैं लोगों को चलने का भ्रम देता आदमी का एनीमेशन हूं (यह सिर्फ मुझे पता है.)
जमाना हुआ, मैं कहीं गया ही नहीं. कई बार सपनों में बेहद तेज हूक उठी लेकिन वह नींद में ही मर गई.
आखिरी बार मैं शायद रिपोर्टरी के धंधे के चलते शायद जबलपुर गया था एक राजनीतिक पार्टी का सम्मेलन कवर करने. लेकिन वह जाना इतना प्रायोजित, समय का पाबंद, वातानुकूलित, अल्कोहलमय था कि कुछ महसूस ही नहीं हुआ. यहां तक कि आधीरात को भेड़ाघाट का धुआंधार और आधारताल में ज्ञानरंजन महाशय का घर खोजने की असफल कोशिश में भी कुछ नहीं था. सड़के, सड़क जैसी थी, बत्तियां बत्तियों जैसी और वहां के आदमी यहां के आदमियों जैसे और क्या? वह नमक के एक बोरे का रेलगाड़ी पर लदकर जबलपुर जाना और आना था. रास्ते में जिनसे बात हुई उन सबने इसे थोड़ा-थोड़ा चखा और कहा कोई खास बात नहीं नमक जैसा ही लगता है.
दुर्गा दादा में भी यह अम्ल बहुत था. नसों में बहता और मुंह से भभकता सलफ्यूरिक एसिड. उन दिनों थकी कम्यूनिस्ट पार्टी की कराहती किताबों की दुकान चलाते थे. दिन भर वही भभकेः जमाना खराब, दुनिया खराब, लोग हरामजादे मक्कार, संसद सुअरबाड़ा, पार्टी के नेता सब उसी की नौकरी बजा रहे हैं. चाची भी चार बात सुनाती हैं, बच्चे भी ढंग से बात नहीं करते. सारे अच्छे लोग गुजर गए. हियां अब जी घबराता है, अनिल निकालो हमको यहां से ले चलो कहीं जहां आदमी और आदमी की जात से मुलाकात न हो.
दुर्गा मिसिर की एक खास बात. सारे दिन काउंटर पर बैठे-बैठे अपने मरे कामरेडों और दोस्तों की लिस्ट बनाया करते थे और शाम को शटर गिराते समय फाड़ कर फेंक देते थे. कुल उनसठ नाम-कभी अंग्रेजी में कभी एकाध चेहरे का चेहरा या फूल भी, अक्सर उलझी रेखाओं की गोंजागोंजी. मुझमें भी नकार ही भरा था दुनिया के लिए. यही शायद साठ पार के दुर्गा से मेरी दोस्ती का धागा रहा होगा.
दुर्गा दादा एक दिन घर से अपना गांधी आश्रम वाला पुराना गाउन उठा लाए और दोपहर में पहन कर दुकान में खड़े हुए. एक हाथ से पकड़ कर दूसरे को सिर तक उठाया और उकताकट से फटती आवाज में बोले, बच्चा अब यहां से कहीं चलो.
सबसे पहले हम लोग आंख का आपरेशन करा कर अस्पताल मे पड़े महात्मा हरगोविंद के यहां गए. देखने का बहाना था. हालचाल नहीं चाभी लेने. केदारनाथ के रास्ते में झोसी गांव में उनका दो कमरों का एक घर था जिस पर शायद अब भी पत्रकार आश्रम की तख्ती लगी होगी. उनको मरे दो साल हो रहे हैं. कभी आजादी के मूल्यों के पतन से क्षुब्ध महात्मा वहां रहकर अध्यात्म की सस्ती, उपयोगी किताबें लिखते थे, खुद गुलाब के कलाकंद और अपना च्यवनप्राश बनाते थे और गाय-बकरियां चराते हुए कच्चे अखरोट फोड़कर चबाने वाले बच्चों से बतियाते थे.
चाभी मिलने के बाद किराया जुटाने की बात आई. किताब की दुकान पर आने वाले दोस्तों से बिना मकसद बताए चंदा बटोरा गया और इसी बीच अखबार के दफ्तर से तनख्वाह भी मिल गई. रिजरर्वेशन हो गया और हम लोग एक दिन दो झोले और कुछ किताबें लेकर चल पड़े. निकलते समय मैने गौर किया दुर्गा दादा बेहद हड़बड़ी में थे. डिब्बे में घुसने के लिए अपना बैग घसीटते हुए इतना झटके से भागे कि गिर पड़े, उठे और बैग वहीं छोड़कर डिब्बे में घुस गए. पता नहीं क्या सोचकर फिर उतरे और अपना बैग उठाया. दरअसल हम लोग कहीं घूमने नहीं जा रहे थे. यह दुनिया के शोर, कमीनगी और धूसरपन से छूटने की यात्रा थी. हमें निविड़ एकांत में जाकर महसूस करने की बेहद जल्दी थी कि इसी दुनिया में इतने सालों से बेमन से रहते-रहते हम कितने बचे रह गए हैं. वहां ऊपर पहाड़ के निर्जन में हमारा एक टेस्ट होना था और उसमें मिले नंबरों के आधार पर जीवन आगे चलना या नहीं चलना था.
अपनी बर्थ पर बैठने के दस मिनट बाद, अपने पड़ोसी यात्री से उन्होने राधा छाप तमाखू की पुडि़या फड़वा कर अपनी हथेली पर रखवाई और फांकने के बाद लगभग घोषित कर दिया अब पब्लिक पूरी तरह नानपोलिटिकल हो चुकी है. पहले ट्रेन, बस वगैर जो सफरी बहस का माहौल था वह मंडल-मंदिर यानि जाति-धर्म की पार्टियों और उनके चाकर मीडिया ने साजिशन खत्म कर डाला है. अब कुछ बचा नहीं है.
ये लोग आदमी हैं, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के खिलौने नहीं कि कामरेड माओ खटका दबाएंगे और खट-खट बहस शुरू हो जाएगी.- मैने चिढ़कर कहा.
डिब्बे में बेहद भीड़ थी, बस एक चालीस वाट का पीला लट्टू था. इसके सिवा कुछ नहीं था. रहा भी होगा तो हम देखना नहीं चाहते थे. ट्रेन बहुत धीरे चल रही थी. हम तेज चल रहे थे. अपने भीतर न जाने कहां-कहां गए और पस्त होकर सो गए.
अगले दिन ऋषिकेश के बस स्टैंड से क्षितिज पर पहाड़ की झिलमिली दिखी तो दुर्गा दादा फिर उफनाए जो पहिली बस मिले निकल लो अब यहां के चूतिया-चर्खे में फंसने का कोई काम नहीं है.
(क्रमशः अगली पोस्ट का लिंक)

अनेक मीडिया संस्थानों में महत्वपूर्ण पदों पर अपने काम का लोहा मनवा चुके वरिष्ठ पत्रकार अनिल यादव बीबीसी के ऑनलाइन हिन्दी संस्करण के लिए नियमित लिखते हैं. अनिल भारत में सर्वाधिक पढ़े जाने वाले स्तंभकारों में से एक हैं. यात्रा से संबंधित अनिल की पुस्तक ‘वह भी कोई देश है महराज’ एक कल्ट यात्रा वृतांत हैं. अनिल की दो अन्य पुस्तकें भी प्रकाशित हैं.
काफल ट्री वाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिये यहाँ क्लिक करें: वाट्सएप काफल ट्री
काफल ट्री की आर्थिक सहायता के लिये यहाँ क्लिक करें




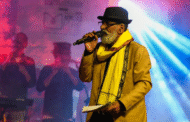

































1 Comments
suraj p. singh
अनिल जी के इस यात्रा विवरण के सत्य में कभी-कभी लगता है कुछ हमारा भी हिस्सा है… धन्यवाद काफल ट्री!