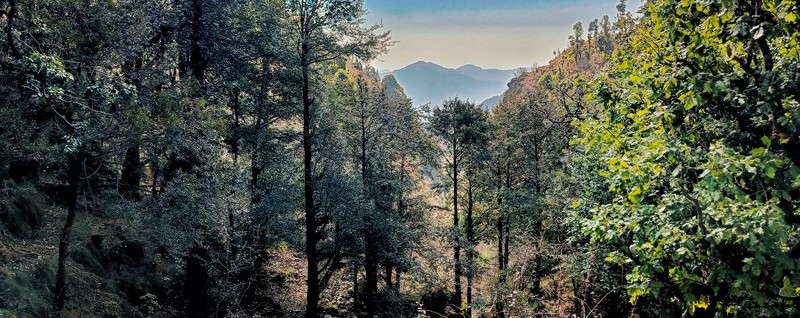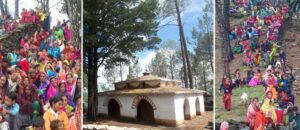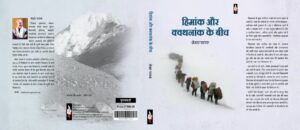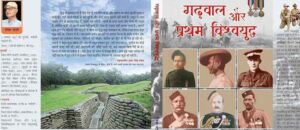रामगंगा घाटी की स्थानीय बोली में आभूषणों को ‘हतकान’ कहा जाता है, इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन समय में यहाँ के लोग कान और हाथों के आभूषणों से ही परिचित थे। इन दोनों अंगों को अलंकृत करने वाले आभूषण स्त्री-पुरुष दोनों धारण करते थे। कालान्तर में जागरुकता के प्रादुर्भाव से अनेक आभरणों ने यहाँ के लोकजीवन में प्रवेश किया। नारी वर्ग के प्रत्येक अंग के लिए आभूषणों का निर्माण होने लगा। निम्न-मध्यम वर्गीय पुरुषों के आभरण हतकान तक ही सीमित रहे, किन्तु कुछ सम्भ्रान्त परिवारों के पुरुष कण्ठाभरण भी धारण करने लगे। यहाँ के स्थानीयजनों द्वारा धारण किए जाने वाले आभूषणों को भी तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है- शिुशु वर्गीय आभूषण, पुरुष वर्गीय आभूषण एवं नारी वर्गीय आभूषण। (Traditional jewelery Western Ramganga valley)
शिशु वर्गीय आभूषण
प्राचीन समय से ही यहाँ शिशुओं को नामकरण के अवसर पर चाँदी के अलंकरणों से अलंकृत करने की परम्परा रही है। परम्परानुसार शिशु के नैनीहाल से चाँदी का सुत (हंसुली), धागुल (कड़े), कमरज्योड़ी/करधनी (चाँदी की पतली जंजीर जिसमें संयोजक में घुँघरू भी लगे रहते थे) तथा कन्याओं के लिए पायल भेंटस्वरूप लाये जाते थे। यह परम्परा पर्वतीय अंचलों में वर्तमान में भी जीवन्त है। इसके अतिरिक्त घर के बड़े-बुजुर्ग शिशुओं को नकारात्मक कुप्रभावों से सुरक्षित रखने के लिए उनके कण्ठ में सीपों तथा कौड़ियों की माला तथा शेर/बाघ के दांत अथवा नाखूनयुक्त ताबीज बांधा करते थे, सुलभता के अभाव में अब यह परम्परा लुप्तप्राय है।
पुरुष वर्गीय आभरण
पुरुष वर्ग यद्यपि आभूषणप्रियता की श्रेणी में नहीं आता तथापि हमारे पुरातन साहित्य एवं गुहाचित्रों में पुरुषों के हस्ताभरणों (रत्नजड़ित अंगूठी तथा भुजबन्ध), कर्णाभरणों (केयूर कुण्डल) एवं कण्ठाभरणों (मुक्ताहार) आदि के दर्शन होते हैं। घाटी के पुरुष वर्ग में अत्यधिक प्रयुक्त होने वाले आभूषण अंगूठी एवं गोरख थे, जो सामान्यतया व्यक्ति को विवाह के अवसर पर ससुराल पक्ष से भेंटस्वरूप दिए जाते थे। यह सहूलियत के अनुसार सोने, चाँदी, ताँबा, गिलट आदि के होते थे। यह रत्नजड़ित भी हो सकते थे और सामान्य भी। अंगूठी तो अभी भी शादी-ब्याह में भेंट की जाती है, परन्तु गोरख आधुनिकता की भेंट चढ़ चुका है। पुरातन समय में सम्पन्न लोग कानों में सोने के मुनड़े/मुर्खिया/मुर्खले भी पहनते थे। कईं देवताओं के पुजारी अथवा डंगरिये, जिनमें देवता अवतरित होते थे, भी कानों में मुनड़े/बुजनी एवं हाथ में बिना घुंडी वाला चाँदी का कड़ा धारण करते थे।
नारी वर्गीय आभूषण
यह सर्वविदित तथ्य है कि आभूषणों तथा सौन्दर्य प्रसाधन का सम्बन्ध मूलतः नारी वर्ग से रहा है। इस अभावग्रस्त पर्वतीय क्षेत्र में वस्त्राभूषणों का स्वरूप अत्यन्त सीमित हुआ करता था। लोक साहित्य के माध्यम से हमें जिन आभूषणों का परिचय मिलता है, उनमें प्रमुख थे- नाक की नथुली, माथे की बिन्दूली, बुलाक, सुता, झुमके, बाली, मुनड़े, हाथ के धागुले, गले में चाँदी के सिक्कों की हार, तुंगल, चाँदी की लड़ीदार जंजीर, मूंगे की माला, मुनड़ी/मुद्रिका, पैरों की झांवर, मुरकौल, उतरौला, कलाइयों की पंहुचियाँ, बिछुवे, हिरौदा, ठ्वाक इत्यादि। कुछ प्रमुख आभूषणों का विवरण इस प्रकार है-
शीर्षाभरण
शीर्षाभरणों में राजसी और सम्पन्न परिवार की महिलाएं शीशफूल धारण करती थी, जिसे जूड़े पर लगाया जाता था। साधरण वर्गीय महिलाओं में इस आभरण का सर्वथा अभाव पाया जाता था, क्योंकि यहाँ की निम्न-मध्यमवर्गीय नारी कृषि एवं पशुचारण के कार्यों की पूर्ति हेतु सिर में घास, लकड़ी, पानी आदि का बोझ उठाती थी। अतः सिर पर कोई आभरण अलंकृत करना न तो सम्भव था, न ही उनके अभावग्रस्त जीवन में इसकी उपलब्धता होती थी।
मस्तकाभरण
बिन्दुली/बिन्दिया- मस्तकाभरणों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान बिन्दिया का था। यह चमकदार काँच की बनती थी। यह बहुरंगी, बहुकोणीय, एवं गोलाकार हुआ करती थी, जिसे लीसे (चीड़ की गोंद) से चिपकाया जाता था। यह नारी के मुखमंडल में सौन्दर्य अभिवृद्धि के साथ ही सौभाग्य का प्रतीक भी मानी जाती थी। इसे केवल सुहागिन स्त्रियाँ ही धारण कर सकती थी।
टीका- टीका परम्परागत रूप से पर्वतीय आभूषणों में स्थान नहीं रखता था। बाहरी लोगों के आगमन ने इस नवागत आभूषण को यहाँ की नारियों के आभरणों की सूची में स्थान दिला दिया। यह आधुनिकतम सुवर्णाभूषण सुहागिन स्त्री ही धारण कर सकती है। इसकी आकृति गोल अथवा लम्बोत्तर हुआ करती है। निचले भाग में छोटे-छोटे मोती या सोने के घुंघरू लगाए जाते हैं। इस पर एक जंजीर लगी होती है, जिसके ऊपरी सिरे पर उसे बालों में अटकाने के लिए एक कांटा लगा होता है। इसी रूपाकृति वाला एक चाँदी की जंजीर से निर्मित आभूषण होता है, जो बैणीफूल कहलाता है।
नासाभरण
फूली- यह बाम नासापुट में पहना जाने वाला एक छोटा सा गोलाकार अथवा चन्द्राकार आभूषण है, जो सोने, चाँदी अथवा गिलट धातु में रत्न लगा हुआ होता था।
बुलाक/बुलांग- यह परम्परागत नासाभरण मुख्यतः नेपाली महिलाओं का आभूषण था, किन्तु नेपाल से लगने वाले कुमाऊँ के सीमान्त क्षेत्रों में संस्कृतियों के आदान-प्रदान स्वरूप यहां की महिलाओं ने भी इसे अपना लिया। यह सुवर्णाभरण नासापुटों की बीच की डंडी में छेद करके पहना जाता था, जो सादा भी हो सकता था, और पेण्डुलमयुक्त लटकने वाला भी।
नथ/नथुली- प्राचीन साहित्य में इसका उल्लेख न मिलने से इसे मुस्लिम सम्पर्क की देन माना जाता है। प्रचलन में आने के बाद से ही इसे नारी का सौभाग्याभरण माना जाने लगा, जिसे पाणिग्रहण संस्कार से लेकर पति के जीवनपर्यन्त पहना जाता है। यह सोने की तार से निर्मित गोलाकृतिक आभूषण है, जिसे बाम नासापुट में छिद्र करके पहना जाता है। सजावट के लिए सामर्थ्यानुसार रंग-बिरंगे नगों से बने एक से लेकर तीन तक चन्द्रक लगाये जाते हैं, तथा इसके एक सिरे पर बनी घुंटी को दूसरे सिरे में बने पुंअर में फंसाकर अटकाया जाता है। सौभाग्य का प्रतीक होने के कारण यहां की नारियाँ सभी मांगलिक कार्यों तथा उत्सव के अवसर पर अनिवार्य रूप से इसे धारण किया करती हैं।
कर्णाभरण
झुपझुपी/झुमके- यह कानों में पहना जाने वाला चाँदी का त्रिभुजाकार आभूषण होता था। इसमें नीचे की ओर लटकी हुई 5-6 पतली-पतली जंजीरें होती थी, जिनके सिरों पर घुंघरू लगे होते थे, तथा ऊपर की ओर कानों में फंसाने के लिए मुड़ा हुआ एक हुक लगा होता था। भारी होने के कारण इन्हें सहारा देने के लिए दोनों कानों की झुपझुपी की घुंटियों पर डोरी बांधी जाती थी, जिसे सिर के पीछे अटका दिया जाता था।
मुर्खली/मुनड़े तथा बालियाँ- मुर्खली अथवा मुनड़े कानों में पहना जाने वाला सुवर्णाभूषण होता था। अतः निम्न-मध्यमवर्गीय नारियाँ इसे बहुत कम धारण कर पाती थी। जनसाधारण में मुनड़ी के स्थान पर चाँदी की बालियाँ अधिक प्रचलित थी। ये वर्तुलाकार छोटी, बड़ी, मध्यम सभी आकारों में बनाई जाती थी, जबकी मुर्खली शंक्वाकार तथा गोलाकार होती थी।
कर्णफूल/कनफूल- ये पुष्पाकृतिक आभरण अधिकत्तर सोने के बने होते थे। इनके बीच में एक खोखली कील लगी होती थी, जिसे कान के पीछे से पेंच लगाकर रोका जाता था, और आगे से उस कील में नग लगा दिया जाता था।
कण्ठाभरण
सुत/हंसुली- उत्तराखण्डी नारियों में बहुप्रचलित इस कण्ठाभरण को हंसुली कहने का कारण, इसका गले की हंसली अस्थि के समान्तर पहना जाना था। यह चाँदी का प्राचीनत्तम कण्ठाभरण था, जिसका भार 200 ग्राम से एक किलो तक होता था। इसकी रूपाकृति मध्य में चपटी तथा मोटी और छोरों पर मुड़ी हुई घुंडियों से युक्त संकरी होती थी, बीच वाले भाग में वर्गाकार खानों पर फूल-पत्तियाँ बनी होती थी।
दुबड़ा/सुतिया- यह सुत का ही लघु रूप होता था। इसका स्वरूप सुत से पतला होता था तथा इसमें कोई सजावट भी नहीं की जाती थी। साधारणतया निर्धन परिवार की महिलाओं का कण्ठाभरण यही हुआ करता था।
ताबीज/लॉकेट- प्राचीनकाल में यह चाँदी का वर्गाकार आभूषण होता था, इसके दोनों सिरों पर कुंडे बने होते थे, जिससे यह डोरी में पिरोया जाता था। भीतर के खोखले भाग में मोम अथवा लाख भर दी जाती थी। ऊपर से अलंकरण के लिए मूंगे और रत्ती के दाने जड़े जाते थे। कालान्तर में यह आभूषण सोने में बनने लगा।
चरेऊ- काले मूंगे की एकाधिक लड़ियों में पिरोये गये इस कण्ठाभरण को धारण करना कुमाऊँ-गढ़वाल की सुहागिन नारी के लिए परमावश्यक माना जाता है। पुरातनकाल में इसके विखण्डन होने पर भी टूटने के स्थान पर मौलना शब्द का प्रयोग किया जाता था और बिना चरेऊ के नारी के लिए चौखट लांघना एवं पानी पीना वर्जित होता था। आधुनिककाल में इसके मध्य में सोने की लॉकेट भी पिरोई जाने लगी है।
गुलबन्द/गलोबन्द- गुलबन्द सुत के समान कण्ठ से सटाकर पहना जाने वाला, समृद्ध परिवार की नारियों का सुवर्णाभरण है, जो कुछ दशक पूर्व ही प्रचलन में आया है। यह मखमल अथवा सनील की पट्टी पर चतुष्कोणीय सोने की टिकिया को टांके से जोड़कर बनाया जाता है। इन टिक्कियों की संख्या 5 से 9 तक होती है। किनारे की दो टिक्कियाँ परस्पर कुण्डों से जुड़ी होती हैं, जिन्हें कपड़े पर सिला जाता है। दोनों सिरों को डोरी से जोड़ा जाता है।
दुबज्योड़- यह लाल रंग की जनेऊ के समान डोरी होती थी, जिसे सौभाग्याभरण के रूप में विवाह के समय दुल्हन को अनिवार्य रूप से पहनाया जाता था।
वक्षाभरण
चाँदी की जंजीर- यह कण्ठ से नाभि तक लटकने वाला भारी-भरकम आभूषण होता था। इसमें प्रयुक्त चाँदी की लड़ियों के अनुरूप इसे पंचलड़, सतलड़ अथवा नौलड़ कहा जाता था। इसका निर्माण चाँदी की चपटी तार को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर बनाये गए कुण्डों को परस्पर श्रृंखलाबद्ध करके किया जाता था। गर्दन के पास एक गोलाकार कुण्डे से अथवा शंक्वाकार चाँदी की पत्ती से लड़ियों के दोनों सिरों को संयुक्त कर दिया जाता था। कभी-कभी बीच में भी चौकोर या गोल पत्तियों से संयुक्त किया जाता था।
हमेल- चाँदी के सिक्कों (चवन्नी-अठन्नी) से बना आभरण हमेल कहलाता था। धागे की मोटी डोरी में कुंडे लगे चाँदी के सिक्कों को पिरोकर इस आभूषण का निर्माण किया जाता था, जिसे सम्पन्न परिवार की महिलाएं ही धारण कर पाती थी। वर्तमान में यह केवल संग्रहालय की वस्तु बन चुकी है।
चम्पाकली- कुछ दशक पूर्व से कुमाऊँ में चांदी के जेवरों का स्थान सुवर्णाभूषणों ने ले लिया है। चम्पाकली भी उनमें से एक है। स्वर्ण को चम्पक की आकृति में गढ़कर मोटी डोरी में पिरोया जाता है। यह समृद्ध परिवार की नारियों का प्रिय आभूषण हुआ करता है।
मटरमाला/जौमाला- सोने से जौ और मटर के दानों का खांका तैयार करके काले मूंगे के दानों के साथ इन्हें पिरोया जाता है। कभी-कभी इसके साथ लॉकेट भी संयुक्त कर दिया जाता है।
मंगलसूत्र- यह चरेऊ का ही नवीन स्वरूप है। जहाँ चरेऊ कण्ठ से सटा हुआ होता था, वहीं मंगलसूत्र कण्ठ से वक्ष तक लटका रहता है। सुवर्ण के गोलाकृतिक अथवा लम्बोत्तर दानों को परम्परागत काले मूंगे के दानों के साथ ग्रसित कर मध्य में सुवर्ण का लॉकेट लगाया जाता है। इसे भी वधू को पाणिग्रहण के अवसर पर पहनाया जाता है।
हस्ताभरण
धागुले- पश्चिमी रामगंगा घाटी सहित सम्पूर्ण उत्तराखण्ड के परम्परागत हस्ताभरणों में धागुलों का अनन्यत्तम स्थान रहा है। ठोस चांदी से बनाये जाने वाले ये कड़े दोनों सिरों पर शंक्वाकार होते थे। सजावट के लिए उनमें नक्काशी भी की जाती थी। वर्तमान में सोने-चांदी के कंगन इन्हीं का परिष्कृत रूप हैं।
ठ्वाक- चाँदी की मोटी चादर पर बनाया जाने वाला यह हस्ताभरण कुछ दशक पूर्व तक पर्वतीय समाज में बहुप्रचलित था। यह दो भागों में विभक्त होता था। दोनों भागों के सिरों पर कब्जे बनाये जाते थे, जिन्हें चाँदी की कील फंसाकर संयुक्त किया जाता था। संपूर्ण कलाई को ढ़क लेने वाला यह गिलासनुमा आभूषण नीचे से संकरा तथा ऊपर से चौड़ा होता था, जिसे अलंकृत करने के लिए उस पर किंगरियाँ एवं धारियाँ बनाई जाती थी।
पौंची/पंहुची- यह गुलबन्द की भांति ही चाँदी के घुंडीयुक्त शंक्वाकार दानों को सनील या मखमल की पट्टी पर 3-4 पंक्तियों में पिरोह कर बनाए जाने वाला एक आभूषण था। सम्भवतः हाथ की पौंची (कलाई) में पहने जाने के कारण इसे पौंची कहा जाता था। प्राचीनकाल में यह आभूषण चांदी से ही बनाया जाता था, जिनके दानों की आकृति ठोस व नोकदार होती थी। वर्तमान में सोने के पौंची प्रचलन में आ गए हैं, जिनके दाने गोल होने के साथ ही अन्दर से खोखले होते हैं, इसलिए उनमें लाख भरी जाती है।
मुनड़ी/अंगूठी/मुद्रिका- इसका निर्माण सोने, चाँदी, ताँबा, पीतल, गिलट आदि धातुओं में रत्न जड़ित करके भी किया जाता है, और साधारण रूप में भी। वैवाहिक बन्धन सम्बन्धी प्रक्रिया में स्थान प्राप्त करने से इसके सांस्कृतिक महत्व में और अधिक वृद्धि हुई।
पादाभरण
झांवर/झांझर- यह चाँदी अथवा गिलट के कड़ों के समान होता था, जो अन्दर से खोखला हुआ करता था। इसके अन्दर चाँदी के छोटे-छोटे टुकड़े अथवा पत्थर के छोटे-छोटे कंकड़ डाल दिए जाते थे, जो चलते समय छन-छन की मधुर ध्वनि किया करते थे।
अमर्तीतार- यह भी चाँदी से निर्मित पादाभरण होता था। चाँदी के तीन तारों को एक साथ बटकर गोल रिंग का आकार दे दिया जाता था, जिन्हें ऐसे ही एकाधिक संख्या में पैरों में डाल लिया जाता था।
पैरे- यह चाँदी अथवा गिलट से बनने वाला चपटा, चौड़ा तथा बीच में भीतर की ओर दबा हुआ, 50 तोले तक का भारी पादाभरण होता था। इसके ऊपर अलंकरण के लिए बेल-बूटे बनाये जाते थे।
पायजेब- यह चाँदी की अनेक लड़ियों से गठित पैर के टखनों पर पहना जाने वाला आभूषण था, पिछली पीढ़ी की महिलाओं के पास यह अभी भी देखा जा सकता है। इसमें नीचे की ओर अनिवार्य रूप से छोटे-छोटे घुंघरू लगे होते थे, जो चलते समय मोहक ध्वनि उत्पन्न करते थे। इसके दोनों सिरों को पेंच द्वारा संयुक्त किया जाता था। वर्तमान में प्रचलित पायल इसी का लघुरूप है, जिसमें घुंघरू होना अनिवार्य नहीं है।
इसे भी पढ़ें : गायब हो गए हैं उत्तराखण्ड से बच्चों के परम्परागत बाल परिधान
चैनपट्टी- ग्रामीण अंचलों में वर्तमान में भी प्रचलित इस पादाभरण को चाँदी के छोटे-छोटे गोल अथवा चौकोर दानों को परस्पर संयुक्त कर एक चौड़ी पट्टी के रूप में तैयार किया जाता था।
पुरातन समय में आभूषणों में स्वर्ण आभूषण यहाँ के लोगों के लिए प्रायः दुर्लभ ही थे। अधिकांशतया आभूषणों के निर्माण हेतु चाँदी ही प्रयोग में लाई जाती थी। कुछ सम्भ्रांत लोग स्वर्णाभूषण भी पहनते थे, तो कुछ अत्यन्त वंचित वर्ग के लोग गिलट के आभूषण पहना करते थे। ज्यों-ज्यों क्षेत्र में लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा, त्यों-त्यों आभूषणों की धातु एवं स्वरूप में भी परिवर्तन आने लगा। वर्तमान में शुभ अवसरों पर अधिकांशतया लोग स्वर्ण आभूषण पहने हुए देखे जा सकते हैं। बाजार में स्वर्णाभूषणों के प्रतिरूप भी उपलब्ध हैं, जिन लोगों के पास वास्तविक स्वर्ण से निर्मित आभूषण नहीं होते हैं अथवा जिनके पास होते भी हैं तो वह भी उनकी सुरक्षा हेतु इन प्रतिरूप आभूषणों को प्राथमिकता देते हैं। इनके साथ ही विभिन्न धातुओं एवं रत्नों से सुसज्जित आभूषण भी खूब चलन में हैं। आधुनिकता की दौड़ में पुरातन आभूषणों में से अनेक आभरण विस्मृति के गर्त में विलीन हो चले हैं। (Traditional jewelery Western Ramganga valley)

मूल रूप से मासी, चौखुटिया की रहने वाली भावना जुयाल हाल-फिलहाल राजकीय इंटर कॉलेज, गैरखेत में राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता हैं और कुमाऊँ विश्वविद्यालय से इतिहास की शोध छात्रा भी.
हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें: Kafal Tree Online
काफल ट्री वाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिये यहाँ क्लिक करें: वाट्सएप काफल ट्री
काफल ट्री की आर्थिक सहायता के लिये यहाँ क्लिक करें