गाँव के अपने घर से निकल कर मंदिर की ओर का रास्ता लेता हूँ . वापिस देहरादून लौटने के पहले एक बार अपने ईष्टदेव के दर्शनों के लिए. मगर एक और लालच खींच लिए जा रहा था. बचपन के अपने पाँवों के कितने ही निशान, अब भी क्या पता वहीं कहीं पड़े मिल जाएँ. किसी कोने मे, किसी फ़लक, पर क्या पता अब भी कुछ निशानियाँ शेष हो. ये उम्मीदें भी न! इतने वर्षों में बदला भी क्या?
(Memoirs of Bairaskund)
मंदिर के आँगन के वे देवदार के वृक्ष और बौने हो गए हैं. आसमान की नीली थाली पर सूरज का तेज अभी वैसा ही दमकता है, जैसा कांसे की थाली में डंगरिया के गीतों पर आरती का थाल चमकता है. गाँव की सुबहो-शाम बिना ज्यादा शोर किए उदासी में अब भी डूबती है. किनारे के खेतों में हहकारते हलवाहे की पुकार भले ही थोड़ा-थोड़ा उस वक्त अटपटाती है, जब सड़क से कोई वाहन गुजरता है. यह शोर यहाँ की जिंदगी का हिस्सा अभी नहीं बन पाया है, बस गूँजकर खामोश हो जाता है अथवा दूर कहीं पहाड़ी ढलानों में विलीन हो जाता है. जीवन की आपाधापी का शोर थोड़ा सा वे वाहन लाते हैं जो कभी-कभार सामने की सड़क पर आ रुकते हैं. उन पर सवार होकर ही समय यहाँ तक पहूँच सकता है. अन्यथा, समय बीतने का कोई चिन्ह नहीं.

हमारे ईष्ट का मंदिर यहीं एक समतल मैदान के बीचों-बीच बना है. कहते हैं, रावण ने अपने दसों शीश यहीं चढ़ाये थे. इसके आगे एक कुंड बना है. पवित्रता का पूरा भावलोक यहाँ रचा गया मालूम पड़ता है. दोपहर की उमगाई धूप यहाँ कुंड के ऊपर जलछाया में विचरण करती है. किसी-किसी पल आने वाले श्रद्धालुओं के घंटा-नाद से मन की एकाग्रता भंग होती है. यज्ञ-मंडप की छतों पर उल्लिखित निर्वाण-दशक शंकर-स्तोत्र की पंक्तियां बरबस ध्यान खींचती हैं –
न शुक्लं न कृष्णं न रक्तं न पीतं,
तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम्॥
मंदिर के पास ही किसी ग्राम घर में देवताओं को औतराया जा रहा है उसकी धुन में पूरा प्रांत मानो किसी मध्यकालीन महक को जी रहा है. फ़ानी दुनिया में वैसे भी यहाँ कुछ बदला ही कहाँ है! अब भी भरथरी और गोरखवाणी प्रकाश तले मंदिर के दिए जगमगाते हैं.
सवारियों के लिए आखिरी पुकार लगाते कंडक्टर की आवाज में बड़ा सब्र होता है. इसके बाद कोई दूसरा वाहन नंदप्रयाग तक नहीं जाने वाला. एक-एक सवारी की कीमत है, वक्त कि उतनी नहीं. हमें जल्दी जल्दी नीचे उतरकर गाड़ी तक पहुँचना होगा.
पहाड़ की चढ़ाई और ढलान – दोनों ही, पूरी जीवट का नाप लेती है. साँसों तक को हलक में अटका देती है. तब उन ढलानों पर खेतों के किनारे से होते, कैसे हमारे बाप-दादा यहाँ तक आते जाते रहे होंगे? अपना घर तो अपना घर ही होता है. शहर की आपाधापी के बीच खंडहर हो चुकी किसी इमारत की सबसे ऊँची छत पर बना मधुमक्खियों का छत्ता उनके लिए तो उनका घर ही होता है, जहाँ जीवन के तार बुने जाते हैं. मेरे पुरखों ने भी तो वही देशना यहाँ महसूस की होगी. देस के लिए सहज अनुराग पाया होगा. बरसों पहले, पता नहीं कैसे और किन हवाओं पर सवार हमारे पूर्वजों का पहला कारवां यहाँ उतरा होगा.
देश के किसी समतल भाग से, ट्रेन की पटरियों के बीच से सरपट गुजरकर, पहाड़ों पर दौड़ती बसों की खिडकियों से भीतर झाँकते पर्वत-शिखरों को पीछे धकेलने के बाद जीप या ट्रैकर के लटके-झटके सहन करने के बाद पगडंडियों से ऊपर चढ़ने के क्रम मे सिर पर छा रखे घने बादलों में छुप रखे इन पहाड़ों पर चढ़ते हुये, मुझे बारम्बार यही ख्याल आता रहा कि बरसों पहले उन पुरखों को भी वही अनुभूति रही होगी, जो पेड़ की सबसे ऊँची डाल पर अपने छत्ते की तरफ जाते हुये किसी मधुमक्खी को होती होगी. वहाँ तक मधुमक्खी बड़ी जतन से जाती है.
मेरे पुरखों ने भी, ऊँचाई की ओर चढ़ते हुये, पैरों को सीने पर धरकर आगे बढ़ते हुए बरसाती बादल, गाड़-गधेरों, उमस भरी चढ़ानों या फिसलन भरी ढलानों को यों ही एकाग्रता से छुआ होगा – और तब वे इस अगम ऊँचाई तक पहुँचे होंगे. मेरी आँखों के आगे जैसे कोई फिल्मी रील धुँधली सी नाचने लगती है – जब इस कठिन परीक्षा के बाद कोई अपना यहाँ पहुँचता होगा, तब उन चार घरों की हलचल को महसूस कर सकता हूँ. इस स्थान की पवित्र तन्मयता थोड़ी उस पल भंग हुई होगी, और इन चार घरों की हलचल उत्साह मे बदली होगी. बदरंग कपड़ों मे ठंड को उलझाये हुये बालकों के फटे गालों की रूमानियत थोड़ा और बढ़ी होगी. अपनी दुविधाओं का भी उत्सव मनाता यह पर्वतीय समाज मेलापक खुदेड़ गीतों को यों ही शिरोधार्य नहीं करता, इसके पीछे यही उमगाती दोपहरियाँ और खामोश शामें महका करती हैं. और यही वे पल होते हैं, जो अभी एक दशक पहले तक भी इस समाज का आईना थे.
महसूस कर सकता हूँ, यहीं कहीं किसी पत्थर पर बैठे मेरे दादाजी (ईश्वर उन्हें सद्गति दे, मैंने उन्हें कभी देखा नहीं) के हुक्के की गुडगुड़ी थम गई होगी, जब दूर से किसी को आते हुए देखा होगा. उन आँखों के आह्लाद और जिगर की खुदबुदाहट की कल्पना भी नहीं की जा सकती है जो औलाद को यों अचानक सामने पाकर उन्हें हुई होगी. वर्ना उनकी शामें चूल्हे के आगे बैठकर सजल आँखों से भरथरी और गोपीचन्द के गीतों को गाते बीता करतीं.
माता रोये जनम- जनम को,बहन रोये छै मासा
भाई भतीजा कुटुम घनेरू, अंत माँ कुई ना तेरू
झूठू ये सब जग जंजाल, मोह माया कू घेरू
सुन ले बेटा गोपीचन्द तू, बात सुनो चित लाई
झूठी सारी माया-ममता,जीव-जगत भरमाई
झुककर अब बैठा नहीं जाता. कै होती है. खाना पचता नहीं. शरीर किसी जंग लगी धातु सा छीजता जा रहा है. भौतिक पदार्थ की अपनी सीमायें उसे जड़ता के कोने तक खींचे लिए जा रही है और उसके परे चेतना का अविलंब सहारा – यह मन, है कि मानता नहीं. गेहूं में जैसे उलार आती हो, ऐसी ही उलार उनके चेहरे पर देख सकता हूँ. ईश्वर ने मुझे मन की आँखें दी है.
ढलानों से उतरते हुये, अपने आँगन की चौहद्दी की वह छत मुझे बहुत खींचती है – बुलाती है. छत टूट चुकी है, लगभग ढहने को है. उसका उजाड़ बहुत खलता है. वह मेरे पितरों की निशानी है. बहुत नीचे तक आने के बाद भी दूर से मुझे वहीं कहीं पर पित्र हो चुके अपने दादाजी बैठे दिखाई देते हैं. हुक्का हाथ में लिए, गुडगुड़ाते हुये. मैंने सच मे उन्हें कभी नहीं देखा. मगर फिर भी वे दिखाई देते हैं – उसी चौपथ पर गुड़गुड़ी लिए, पुरानी बाट पर, खेत खलिहान में, और सबसे विस्मयकारी तो उस छत के आगे बने कोने वाली जगह में, जहाँ वे (मैंने सुना है) अक्सर बैठा करते थे.
ढलुवाँ खेतों से नीचे उतरते हुए, खामोशी में बैठे उस जीव की आभा मुझे झलकती है. मेरी कल्पनाओं में सत्तर के दशक के वे अंतिम वर्ष जीवंत होने लगते हैं. आँगन में दादा उकड़ूँ बैठे हैं. कै हो रही है. उनके पीछे पिताजी उन्हें पानी दे रहे हैं. एक खेत और नीचे उतर आया हूँ. जैसे खुद ही से एक सीढ़ी और एक पीढ़ी नीचे खिसक कर दूर हो गया हूँ.
एक खेत और नीचे उतर कर मानो अगाध और अनंत शून्य के सागर में डूब रखे किसी शहर की ओर बढ़ता जा रहा हूँ – और गहरे, और गहरे. उधर ऊँचाई पर एक ठौर है, जो बाहर से दिखता है – मेरा घर, मेरी पित्रकुड़ी. और आंगन में दो-चार जीव है. उसी शाम जब वहाँ जब किसी ने दम तोड़ा, उस गहन उदासी में. शाम थोड़ा और गहरा गई. कुछ महीनों बाद उसी आँगन के आगे गौशाला में एक बालक ने किलकारी भरी. वही बालक आज एक-एक सीढ़ी नीचे उतरकर गहराई के शोर मे डूबने को जा रहा है. तल मे जहाँ पानी का शोर है और एक चक्की निरंतर उसकी तन्मयता को भंग कर रही है. मगर मेरे कानों मे जैसे अब भी कोई गा रहा है, दुखी उदास स्वर मे, कहीं चूल्हे के पास बैठा-
ना घर तेरा, ना घर मेरा, चिड़िया रैन-बसेरा
हाथी घोडा कुटुम कबीला रे,चला-चली का फेरा
सुन ले बेटा गोपीचन्द तू, बात सुनो चित लाई
झूठी सारी माया-ममता,जीव-जगत भरमाई
सदा अमर यां धरती नि रैयी,मेघ पड़े टूट जाई
अमर नि रैन्दा चंद सुरीज यां, गरण लगे छूट जाई
कागज-पत्री हर कोई बांचे, करम न बांचे कोई
राज महल को राज कुंवर जी, करमन जोग लिखाई.
मंदिर की उपत्यका में बैठकर जीवन का अंतिम सोपान गढ़ते उस जोगी की माया याद आती है, जो संयोग से मेरे ही कुटुंब में दूर के रिश्ते से कोई नातेदार थे. लोभ-मोह की मैली चादर के दाग वाली कमली में ठिठुरते अपने स्वजनों की अनोखी बेरहम उदासीनता के घूँट भरते हुए भी, मोह के धागे में लिपटे पड़े थे. हमें देखकर जोगी के भीतर का गृहस्थ बाहर आ गया. आत्मीयता नाच उठी. बड़ी आत्मीयता से मिले. जाते हुए अनायास मेरी जाकेट पर हाथ फेर कर कहने लगे, “जाड़ा बहुत लगता है, अगली बार ऐसी ही एक फतूही मेरे लिए भी लेते आना.“ उस समय इतना साहस न था कि जैकेट उतार कर दे देता. न ही वह आशय मेरी समझ मे आया. मगर वादा जरूर किया कि अवश्य लेता आऊँगा. और अगले साल जब गया, तो वो पहाड़ वहीं था, मंदिर भी था, कुंड भी, और वह पत्थर भी वहीं था, मगर वह जोगी नहीं थे. इन्हीं धाराओं के पानी में, कहीं उनकी राख न जाने तब तक बहकर गंगा सागर पहुँच गयी हो, किसे पता ! पीछे केवल मोह-तृष्णा, अपनापन और खुदेड गीत.
इन्द्रेश प्रसाद पुरोहित ‘मिहिर’ गोचर महाविद्यालय रामपुर मनिहारान, सहारनपुर में अंग्रेजी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं.
‘मुनस्यारी हाउस’ इस तरह पहाड़ी उत्पादों का सबसे विश्वसनीय ब्रांड बना
हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें : Kafal Tree Online
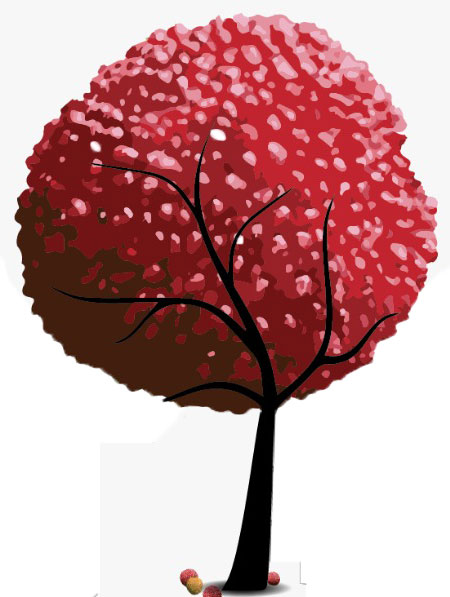
Support Kafal Tree
.
काफल ट्री वाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिये यहाँ क्लिक करें: वाट्सएप काफल ट्री
काफल ट्री की आर्थिक सहायता के लिये यहाँ क्लिक करें







































