कहो देबी, कथा कहो – 39
पिछली कड़ी- कहो देबी, कथा कहो – 38
तो, परिवार को साल भर के लिए लखनऊ में अकेला छोड़ कर मैं दिल्ली आ गया. समय के साथ कितनी बदल गई थी दिल्ली! पहली बार सन् 1958 में उसे तब देखा था, जब मैं अपने सहपाठियों के साथ दिल्ली के शैक्षिक टूर पर आया था. उसके आठ साल बाद अपनी पहली नौकरी करने दिल्ली पहुंचा और तीन साल बाद दिल्ली को अलविदा कह कर चला गया था. और अब, उसके उन्नीस साल बाद बैंक की नौकरी में एक बार फिर दिल्ली आ गया. कहां वह तीस साल पहले की दिल्ली, जब मैंने चौदह साल की उम्र में कुतुबमीनार के टॉप में खड़े होकर उसे देखा था और तीन मूर्ति भवन में सहपाठियों के साथ प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू जी से मिला था. कहां वह दिल्ली जिसके कॉफी हाउस, टी-हाउस में साहित्यकारों का जमावाड़ा लगा रहता था और मैं इंद्रपुरी से तालकटोरा गार्डन के तरण ताल तक तैरने के लिए बिना किसी ट्रैफिक जाम के साइकिल से आया करता था! तब से आज तीस साल बाद कितनी बदल गई है दिल्ली! दिन-रात सड़कों पर दौड़ती लाखों मोटरगाड़ियां, कानों के पर्दे को झनझना देने वाला हॉर्नों का कर्कश शोर और दमघोंट देने वाली जहरीली हवा, दिन-रात न जाने कहां की तेजी में भागते लाखों लोग.
कहां गई वह दिल्ली? बहरहाल, अब तो इसी दिल्ली महानगर में था मेरा आबोदाना. इसी में खुद को चलाना और खपाना था. ब्रीफकेस में यों ही दो-चार कपड़े, शेविंग का सामान और टूथ ब्रश रख कर चला आया था यह सोच कर कि जब रहने को घर मिल जाएगा तो लखनऊ जाकर ले आवूंगा. लखनऊ से दिल्ली की ओर चला तो ट्रेन में सोचता रहा कि घर मिलने तक आखिर रहूंगा कहां? कुछ पुराने साथी याद आए. वह दोस्त भी याद आया जिसे मैंने बीस साल पहले पूसा इंस्टिट्यूट की अपनी मक्का प्रजनन योजना में ही एक अस्थाई नौकरी के लिए बंगलौर से बुला लिया था. सोचा था, एक बार यहां पैर टिकाने की जगह मिल गई तो कल अनुभव हो जाने पर स्थाई नौकरी भी मिल जाएगी. वह नैनीताल डी एस बी कालेज में मुझसे दो साल जूनियर था. दिल्ली आने के बाद वह दो माह हमारे ही साथ रहा था और अब पूसा इंस्टिट्यूट में वैज्ञानिक की स्थाई नौकरी में था. पता मेरे पास था, मुझे लगा, उसी के पास जाना ठीक रहेगा. इसलिए मैं उसका पता खोजते-खोजते लारेंस रोड में उसके घर पहुंच गया. देख कर दोस्त खुश हुआ. मैंने उससे कहा, कुछ दिनों के भीतर रहने के लिए घर मिल जाएगा. हम लोग पुराने परिचित थे इसलिए मैं भी घर के सदस्य के रूप में साथ रहने लगा. मेरे ऑफिस भीखाएजी कामा प्लेस पहुंचने के लिए उसने मुझे डी टी सी की बसों का रूट समझा दिया.
दिल्ली में पहले दिन सुबह सात बजे घर से ब्रीफकेस लेकर रिंगरोड की बस पकड़ने के लिए वजीरपुर स्टॉप पर पहुंचा. जो भी बस आती, भरी हुई होती. ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, इसलिए हिम्मत करके एक बस में घुसा. धक्के लगते-लगते बीच में पहुंच गया. बस में तिल रखने की भी जगह नहीं थी. हाथों-हाथ टिकट के पैसे दिए जा रहे थे और हवा में ही हाथों-हाथ टिकट मिल रहा था. पहले दिन की पहली बस यात्रा में टिकट के लिए जेब से पैसे निकाल ही रहा था कि दो रूपए का नोट नीचे गिर गया. झुक कर उठाने की कोशिश कर ही रहा था कि बगल में खड़े आदमी ने वह नोट उठा कर मुझे देते हुए राय दी कि कुछ पैसे नीचे गिर जाएं तो उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. इतनी देर में कोई आपकी जेब काट सकता है. ये तो आपके ही पैसे थे, कई बार जेब कतरे खुद पैसे गिरा कर कहते हैं- आपके पैसे गिर गए! उठाने तक जेब से बटुआ गायब कर देते हैं. उसकी यह राय मैंने गांठ बांध दी.
खचाखच भरी बस में देर शाम लौटते समय भी दो-चार दिन बाद एक किस्सा हो गया. बस में चढ़ा और भीड़ में किसी तरह आगे खिसकते-खिसकते एक हाथ से डंडा पकड़ कर खड़ा हो गया. ब्रीफकेस सीट के पास नीचे रखा ही था कि वहां बैठे सज्जन ने तल्ख आवाज़ में कहा, “उठाओ, इसे उठाओ. मेरे पैरों से टकरा रहा है. मैंने चुपचाप ब्रीफकेस उठा लिया. लेकिन, उसका बोलना बंद नहीं हुआ. वह बोलता रहा, “आ जाते हैं न जाने कहां से? बस इन्हें दिखाना होता है कि इनके पास कितना काम है. उसे घर भी ले जाते हैं. क्या जरूरत है इस दिखावे की?” वह मुझसे पूछ रहा था. मैं चुप रहा. उसके पास बैठे दो-एक लोगों ने कहा भी, “वे तो चुपचाप खड़े हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं. आपको क्या परेशानी है?”
“परेशानी है, ऐसे दिखावा करने वाले लोगों से. क्या बस इन्हीं के पास काम है?” उसने और भी भड़क कर कहा. मैं फिर भी चुपचाप खड़ा रहा. उसे क्या बताता कि ब्रीफकेस में रात को पहनने के लिए मेरा पैजामा-कुर्ता है, रेजर, ब्लेड, टूथब्रश और टूथपेस्ट है. लोगों के समझाने से वह शांत तो हुआ लेकिन मेरी ओर क्रोध भरी आंखों से घूरता भी रहा. अगर मेरा ब्रीफकेस उससे छू भी जाता तो विस्फोट हो जाता. इसलिए मैंने ब्रीफकेस अपने पैरों के बीच दबा लिया.
हर रोज सुबह भीड़ भरी बस में किसी तरह दक्षिण दिल्ली में भीखाएजी कामा प्लेस के अपने दफ्तर तक पहुंचता. मुझे क्लास्ट्राफोबिया था और भीड़ में मेरा दम घुटने लगता. मैं बदहवास होने लगता. लेकिन, दफ्तर पहुंचने का और कोई साधन भी नहीं था. दिन भर साथियों से आसपास घर ढूंढ देने की बात करता रहता, लेकिन इतनी आसानी से कहां घर मिलना था. दो-चार प्रापर्टी डीलरों से भी बात की लेकिन बात बनी नहीं. कुछ जगह ‘मुंडा अकेला है जी. कहता है साल भर बाद फेमली लाऊंगा’ के शक-शुब्हे ने बात नहीं बनने दी. दो-एक सप्ताह बाद दोस्त भी बेचैन दिखाई देने लगा. रोज शाम को पूछ लेता, “मिला कहीं घर?”

भीखाएजी कामा प्लेस के पास ट्रेफिक. फोटो गूगल से साभार
“नहीं, अभी नहीं मिल पाया है. साथी लोग खोजने की कोशिश कर रहे हैं,” मैंने कहा.
“अरे, घर मिलने में ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. खुद कोशिश करनी पड़ती है. प्रापर्टी डीलर पच्चीस घर दिखा देंगे. कल इतवार है, मेरे साथ चलो.”
“चलूंगा,” मैंने कहा.
अगले दिन हम धौलाकुआं के पास सत्य निकेतन पहुंचे. सड़क के सामने ही प्रापर्टी डीलर का बोर्ड दिखाई दिया. दोस्त के साथ भीतर गया. वहां दो शोहदे टाइप के नौजवान मेज पर जूतों सहित पैर रख कर आराम फरमा रहे थे. हमारे आने से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा. कमरे की बात की तो बोले, “कई कमरे हैं. लड़का अभी दिखा देगा, लेकिन दिखाने के लिए पहले पच्चीस रूपया एडवांस दो.”
दिए पच्चीस रूपए और उन्होंने एक आदमी हमारे साथ भेज दिया. उसने हमें दो-तीन कमरे दिखाए लेकिन वे परिवार सहित रहने लायक बिल्कुल नहीं थे. छात्रों या पेइंग गेस्ट के लायक थे. लौट कर दोस्त ने उनसे कहा, “हमने परिवार के लायक घर दिखाने को कहा था. इनमें से तो कोई कमरा इस लायक नहीं है.”
वे बोले, “तो हम क्या करें? हमारे पास यही कमरे हैं.”
दोस्त ने नाराजगी से कहा, “ये क्या बात हुई? पैसे वापस करो.”
“कैसे पैसे? पैसे वापस नहीं करते हम. कमरे दिखा दिए हैं. नहीं पसंद आए तो हम क्या करें? अब निकलो यहां से,” यह कह कर उन्होंने अपने आदमी को पैसे थमा कर कहा, “जा भाग कर दो बीयर ले आ.” हम निराश लौट आए.
महीना भर समय तो लगा लेकिन फिर साथी अनिल की मदद से आफिस के पास ही सफदरजंग इंक्लेव से लगे कृष्णानगर की गली नंबर पांच में पहली मंजिल पर घर मिल गया. कर्नल सूरी का घर था. वे उत्तर-पूर्व में नियुक्त थे. भूतल पर उनके बड़े भाई डा. सूरी का परिवार रहता था. घर तो मिल गया लेकिन मेरे पास अभी बिस्तर नहीं था. वापस दोस्त की ओर भी नहीं जाना चाहता था क्योंकि वहां माह भर रह चुका था. इसलिए घर में आया और फर्श पर अखबार बिछा कर दो-एक रातें बिताईं. खाना ढाबे पर मिल जाता था.
आफिस के करीब घर होने के कारण मैं अधिक से अधिक समय आफिस में दे सकता था, और दिया. मोटरसाइकिल अभी लखनऊ में ही थी इसलिए बस और आटो से ही काम के लिए निकलता था. हेड आफिस के अपने विभाग में पहुंच कर मैंने ड्यूटी ज्वाइन की और काम में लग गया. धीरे-धीरे आफिस का माहौल भी समझ में आने लगा. मुखिया एक महिला थीं जिनका मैं बहुत आदर करता था. इतना कि पहले तीन-चार माह तक उन्हें ‘सर’ कह कर ही संबोधित करता रहा. आफिस के तीन पुराने साथी उनके बहुत करीबी थे. बात-व्यवहार से धीरे-धीरे यह स्पष्ट हो गया कि यहां मुझे चुपचाप काम करना है और काबू में रहना है. शायद इस बात पर ध्यान दिया जा रहा था कि कहीं परिंदे के पर न उग आएं! किसी भी काम के लिए ना-नुकर न कर सके. मैं भी अच्छी तरह जानता था कि मेरी कोई और पहचान तो है नहीं, सिर्फ काम से ही मुझे अपनी पहचान बनानी है लिहाजा काम में ही लगा रहता.
माह में मुश्किल से एक या दो बार परिवार से मिलने लखनऊ जा पाता था. एक बार वहां जाने पर मैंने मोटरसाइकिल ट्रेन से दिल्ली के लिए बुक कर दी. मोटरसाइकिल दिल्ली पहुंचने पर मैं रेलवे स्टेशन गया, मोटरसाइकिल ली और किक मार कर दिल्ली की सड़कों पर पहली बार उसे चलाते हुए सुरक्षित घर तक ले आया. मोटरसाइकिल आ जाने के बाद आवाजाही की काफी सुविधा हो गई. हेड आफिस में अधिकांश समय नए तरह के कामों को सीखने में ही लग जाता था. कई आदेश मेरे लिए परीक्षा की घड़ी साबित होते लेकिन मुझे पता था, इसी तरह मैं ये सारे काम सीख सकूंगा. बैंक के चेयरमैन कई बार दूसरे देशों की यात्रा पर जाते. एक बार वे लातीनी अमेरिका के किसी देश की यात्रा पर जा रहे थे. आदेश हुआ कि वहां देने के लिए भारत की कुछ सुरुचिपूर्ण सौगातों की व्यवस्था की जाए. मुखिया ने मुझसे सौगातें खरीद कर लाने को कहा. मैंने पूछा किस तरह की सौगातें और कहां से खरीदनी होंगी.
“यू शुड नो ऑल दिस. आप जाइए और अपनी पसंद से खरीद कर लाइए.”
“क्या मैं एक साथी को अपने साथ ले जाऊं?”
“नहीं, किसलिए? इस काम में दो लोगों की क्या जरूरत है?”
गया मैं, अपनी मोटरसाइकिल से गया. चेयरमैन का मामला था, इसलिए विभिन्न प्रदेशों के इंपोरियम याद आए. वहां जाकर कुछ स्कार्फ, वुड पेंटिंग, अलंकृत डिब्बियां, बातिक पेंटिंग जैसी कई चीजें खरीदीं. कुछ चीजें मोटरसाइकिल के साइड में लगे डिब्बे में डालीं और बची हुई चीजें कंधे का झोला खरीद कर उसमें रखीं. कृषि भवन के पास से आगे बढ़ा ही था कि कंधे में लटके झोले की चीजें संभालना मुश्किल हो गया. कड़ी धूप थी और मैं बहुत तनाव में था. मोटरसाइकिल किनारे रोकी. अचानक खुशबू का एक झौंका आया. मुझे लगा, जैसे मेरे गांव के जंगल में बकरलदी की झाड़ी पर फूलों की बहार आ गई है और उसकी वह भीनी-भीनी खुशबू मेरे पास तक पहुंच रही है. मैं अपनी मजबूरी पर फफक कर रो पड़ा. एक साथी और होता तो वह सामान पकड़ने में मेरी मदद कर सकता था. खैर किसी तरह साइड के बक्से और झोले का सामान संभालते हुए हेड आफिस तक आया. वे चीजें लेकर मुखिया एक साथी के साथ चेयरमैन को दिखाने गईं. उन्हें चीजें काफी पसंद आईं.
उन्हीं दिनों सभी अंचलों में अखिल भारतीय सांस्कृतिक तथा नाटकों की प्रतियोगिता की तैयारियां शुरू हुईं. दिल्ली अंचल से कोई नाटक तैयार नहीं किया जा रहा था. मुझे और मेरे विभाग के साथी अरूण मरवाह को लगा कि हम इस मौके का लाभ उठा सकते हैं. अगर हम डाक्टर शंकर शेष के दो पात्रों का नाटक ‘आधी रात के बाद’ तैयार कर लें तो उसे प्रतियोगिता में प्रस्तुत कर सकते हैं. मेरे घर और उसकी छत पर रिहर्सल के लिए बहुत जगह मिल सकती थी. हम बहुत उत्साहित होकर मुखिया के पास गए. मैंने उनसे कहा, “मैम, हम दिल्ली अंचल के लिए डाक्टर शंकर शेष का दो पात्रों का नाटक तैयार करना चाहते हैं. इससे हमारे विभाग का भी नाम होगा. आपकी अनुमति हो तो हम इस नाटक की रिहर्सल शुरू कर दें.”
उन्होंने तल्ख आवाज में जवाब दिया, “मिस्टर मेवाड़ी, इफ यू थिंक आइ विल परमिट यू टु पार्टिसिपेट इन द प्ले, यू आर मिसटेकन. आइ विल नेवर परमिट यू.”
मैंने कहा, “लेकिन मैम, हम तो यह रिहर्सल आफिस टाइम के बाद करेंगे?”
“नो बडी शुड ट्राई टू कंविंस मी. आप लोग जा सकते हैं.”
हम दोनों बाहर निकले और निराशा में हंसते हुए एक-दूसरे की ओर देखा. हम जानते थे कि अनुमति मिलना कठिन होगा, फिर भी सोचा कि पूछ लेने में क्या हर्ज है. लेकिन, इतने रूखे उत्तर की आशा नहीं थी. उस दिन मैंने संकल्प किया कि मैं रिटायर होने से पहले बैंक के नाटकों में जरूर भाग लूंगा, मौका चाहे जब भी मिले.
घर में साल भर के एकांतवास की तपस्या के बाद मैं लखनऊ जाकर परिवार को ले आया. मई माह समाप्त हो रहा था. अब सबसे बड़ी समस्या थी- बच्चों का एडमिशन. दिल्ली में मार्च में ही एडमिशन हो जाते हैं जबकि उत्तर प्रदेश में जुलाई के प्रारंभ में एडमिशन किए जाते हैं. दोनों छोटे बच्चों का कक्षा दो तथा कक्षा चार में एडमिशन होना था. घर के पास ही सेंट मेरी पब्लिक स्कूल में जाकर पता किया. उन्होंने कहा कि बच्चों की परीक्षा लेंगे. परीक्षा ली और बच्चे पास हो गए. हम खुश हो गए कि चलो एडमिशन हो जाएगा. तभी उन्होंने मिलने को बुलाया और कहा कि बीस हजार रूपया डोनेशन देना होगा. हमारा तभी तबादला हुआ था और आवाजाही में एक-एक पैसा खर्च हो चुका था. मैंने उन्हें अपनी मजबूरी बताई और प्रार्थना की कि बच्चों का एडमिशन कर लिया जाए. मैं हर माह किस्तों में यह पैसा चुका दूंगा. लेकिन, उन्होंने साफ मना कर दिया और पास होने के बावजूद बच्चों का एडमिशन नहीं हो सका.
फिर हम पंचशील पार्क के मानव भारती स्कूल में गए. वहां भी बच्चों की परीक्षा ली गई. बच्चे पास हो गए और उन्होंने फीस का पैसा जमा करने को कहा. पता लगा, उनके स्कूल की कोई बस सफदरजंग इंक्लेव में नहीं आती है. इसलिए बच्चे चार्टर्ड बस से भेजने होंगे. दिल्ली की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में हमारे लिए बच्चों को चार्टर्ड बस से स्कूल भेजना और वापस बुलाना संभव नहीं था. हम बहुत डर गए थे कि अगर कहीं बच्चे बस में इधर-उधर हो गए या बस छूट गई तो फिर क्या होगा? हम तो किसी को जानते भी नहीं. इसलिए हमने वहां एडमिशन नहीं कराया.

उसी बीच प्रधानमंत्री कार्यालय की सुरक्षा से जुड़े मेरे एक पुराने सहपाठी सपरिवार मिलने आए. उन्होंने बच्चों के एडमिशन की बात सुनी तो कहा, “आप अर्जी लिख कर मुझे दे दें. केन्द्रीय विद्यालय में एडमिशन हो जाएगा.” इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी? मैंने उन्हें अर्जी लिख कर दी और बच्चों के एडमिशन की चिट्ठी का इंतजार करने लगा. दिन बीतते गए लेकिन चिट्ठी नहीं आई. मेरा मानसिक तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था, इतना कि मैं कई बार सोचता- यह नौकरी में किसके लिए कर रहा हूं? अगर मैं अपने बच्चे भी नहीं पढ़ा सकता तो यहां इस दिल्ली शहर में मेरे लिए नौकरी करने का क्या मतलब है. इससे तो पहाड़ ही अच्छा था जहां बच्चों का एडमिशन तो कम से कम हो जाता है. दिन भर दफ्तर में काम करके थका-मांदा देर शाम या कई बार देर रात घर पर आता और सोने के बाद अचानक बड़बड़ाता हुआ उठ बैठता. पत्नी से पूछता, “बच्चों के एडमिशन की चिट्ठी आ गई? मुझे दिखाई नहीं?”
पत्नी मुझे समझाती. पानी पीने को देती. सिर पर भीगा तौलिया रखतीं और कहतीं, “तुमने सपने में देखा होगा.”
“हां मैंने देखा, रजिस्ट्री से एडमिशन की चिट्ठी आई है. इसका मतलब वह सपना था.”
नींद उचट जाती और बुरे-बुरे ख्याल आते रहते. आखिर दो महीने हो गए लेकिन सहपाठी के आश्वासन के बावजूद एडमिशन की कोई सूचना नहीं आई. एक बार मैंने फिर सहपाठी से संपर्क किया और पूछा, तो उसने बाद में फोन पर बताया कि मानव संसाधन मंत्रालय के जिस आदमी को मार्क करके आपकी अर्जी दी थी, वह डेढ़ माह पहले किसी पार्टी में गया था और स्कूटर से लौटते समय किसी गाड़ी से टकरा गया. वह अस्पताल में है. हाथ-पैरों में फ्रैक्चर है.
मेरी निराशा और अधिक बढ़ गई. अब क्या करूं? ‘रविवारी जनसत्ता’ में उन दिनों मैं काफी लिख रहा था. एक दिन लेख देने के लिए मंगलेश डबराल जी के पास गया. उन्होंने पूछा, “आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है?”
मैंने उन्हें पूरी बात बता दी. तभी उनका एक साथी पत्रकार माचिस खोजते हुए हाथ में सिगरेट लेकर आया तो मंगलेश जी ने उससे मेरा परिचय कराया, “मेवाड़ी जी, यह आलोक तोमर हैं. यह आपकी मदद कर सकते हैं.” उन्होंने मेरी परेशानी आलोक जी को समझाई. पूरी बात सुन कर उन्होंने कहा, “क्या शाम को आप गोल मार्केट में मेरे घर पर आ सकते हैं?”
मैंने कहा, “जी मैं जरूर आ सकता हूं.” उन्होंने घर का पता देकर समय बताया. मैं शाम को ठीक उस समय उनके पास पहुंच गया. वे अपने किसी दोस्त के साथ खाना बना रहे थे. मुझे बैठा कर उन्होंने फोन उठाया और नंबर घुमा कर बोले, “कौन, पंडित जी?”
उधर से किसी ने कुछ पूछा तो आलोक जी ने कहा, “मेरा नाम आलोक तोमर है.”
उधर से किसी ने फिर कुछ पूछा तो आलोक बोले, “क्या सुनाई नहीं देता? कान में तेल डाला करो. मेरा नाम आलोक तोमर है. भीतर जाकर पंडित जी को बताओ.”
फोन बजा. आलोक जी ने फोन उठा कर कहा, “नमस्कार, क्या आप आराम कर रहे थे? आपके आदमी को साफ सुनाई नहीं देता. उससे मैंने कहा है, कान में तेल डाला करे. अच्छा, आपसे एक जरूरी काम है. हमारे एक साथी हैं देवेंद्र मेवाड़ी. उनके दो बच्चों का एडमिशन होना है केन्द्रीय विद्यालय, सेक्टर-2, आर. के. पुरम में. हमारा इतना काम तो आप कर ही देंगे ना?”
दूसरी ओर से फोन पर कुछ कहा गया. आलोक बोले, “ये ठीक साढ़े नौ बजे अर्जी लेकर आपके पास पहुंच जाएंगे. नाम एक बार फिर सुन लीजिए- देवेंद्र मेवाड़ी.”
फिर आलोक जी ने मुझसे कहा, “आपका काम हो जाएगा. मैंने शिक्षा मंत्री एल. पी. साही से बात कर ली है. कल सुबह साढ़े नौ बजे आपको अर्जी के साथ उनकी कोठी पर पहुंचना है.”
मैंने हाथ जोड़ कर उन्हें तहेदिल से धन्यवाद दिया और कहा, “आपका यह अहसान में कभी नहीं भूलूंगा. कल सुबह मैं सही समय पर उनकी कोठी पर पहुंच जाऊंगा.”
वे बोले, “इसमें अहसान की कोई बात नहीं है. आपका काम हो जाए, वही बहुत है.”
सुबह मैं साढ़े नौ बजे से पहले ही साही जी की कोठी पर पहुंच गया. गार्डों ने रोक कर पूछ-ताछ की. मैंने उन्हें बताया कि साही जी ने मिलने के लिए बुलाया है मुझे. भीतर जाते ही साही जी के व्यक्तिगत सहायक परशुराम मिले. मैंने उन्हें नाम बताया तो वे बोले, “साहेब ने बताया है मुझे कि आप आने वाले हैं.” परशुराम मुझे मुख्य बैठक से लगे हुए दूसरे कमरे में ले गए. पानी पिलाया और चाय के लिए पूछा. मैंने मना करते हुए कहा कि अभी पीकर आ रहा हूं. मेरे लिए तो सबसे जरूरी एडमिशन था. इसलिए कहा, “बच्चों का एडमिशन हो जाए, बस इतनी ही प्रार्थना है.”
“एडमिशन तो हुआ ही समझिए. साहेब ने कहा है कि आपसे अर्जी लेकर मैं उनको दूं. वे अभी पूजा कर रहे हैं, थोड़ा कसरत करके स्नान करेंगे. आप उनसे मिल कर जाइए. यह काम तो हुआ ही समझिए.”
मुझे लगा मंत्री जी को काफी समय लगेगा. अर्जी परशुराम जी को दे ही दी थी इसलिए सोचा कि पहले जाकर भाई आलोक तोमर को बताऊं कि मैंने ठीक साढ़े नौ बजे उनके व्यक्तिगत सहायक परशुराम को अर्जी दे दी है. यह बताना ज्यादा जरूरी था. इसलिए मैं परशुराम जी को धन्यवाद देकर बाहर आया और मोटरसाइकिल से दफ्तर की ओर भागा. वहां से आलोक भाई को फोन करके पूरी जानकारी दी.
अब फिर एडमिशन की सूचना का इंतजार करने लगा. कुछ दिनों के बाद पता लगा कि जिन बच्चों का मंत्री कोटे में एडमिशन के लिए चयन हो जाता है, उनका नाम मानव संसाधन मंत्रालय में सूची में देखा जा सकता है. मैं सूची में नाम देखने के लिए गया तो उस भीड़ में मुझे अपने बच्चों के नाम मिल गए. हम भाग कर केन्द्रीय विद्यालय, सेक्टर-2, आर.के. पुरम पहुंचे और प्रिसिंपल राव साहब से मिले. उन्होंने सूची में नाम की बात सुनते ही सख्ती से कहा, “आप लोग मंत्रालय से एडमिशन के लिए बच्चों का नाम पास करा लेते हैं लेकिन मेरे स्कूल में एडमिशन तभी होगा जब बच्चे परीक्षा पास कर लेंगे.”
हमने कहा, “ठीक है सर.” उसके बाद उन्होंने बच्चों की परीक्षा ली और हमें बुला कर कहा, “आपके बच्चे परीक्षा में पास हो गए हैं.” साथ ही यह भी कहा कि ये अच्छे बच्चे हैं. यह हमारे लिए बड़ी राहत की बात थी. इस तरह दोनों बच्चों का केन्द्रीय विद्यालय में एडमिशन हो गया और मेरा मानसिक तनाव धीरे-धीरे कम हुआ. सरोजनी नगर के स्कूल में मंझली बेटी के बारहवीं कक्षा में एडमिशन के लिए प्रधानाचार्य एम. एस. रावत जी ने बड़ी मदद की.
“चलो, परेशानी तो बहुत हुई लेकिन बच्चों का एडमिशन हो गया?”
“आप ठीक कह रहे हैं. कई बार तो सोचता हूं कि उस भयानक तनाव के दौर में मैं न जाने कैसे बच गया. तनाव के कारण तो कई और भी थे लेकिन एक थिरेपी से शायद मेरा इलाज भी हो रहा था.”
“कौन-सी थिरेपी?”
“सुनाता हूं, ओं कहो,”
“ओं”

वरिष्ठ लेखक देवेन्द्र मेवाड़ी के संस्मरण और यात्रा वृत्तान्त आप काफल ट्री पर लगातार पढ़ते रहे हैं. पहाड़ पर बिताए अपने बचपन को उन्होंने अपनी चर्चित किताब ‘मेरी यादों का पहाड़’ में बेहतरीन शैली में पिरोया है. ‘मेरी यादों का पहाड़’ से आगे की कथा उन्होंने विशेष रूप से काफल ट्री के पाठकों के लिए लिखना शुरू किया है.
वाट्सएप में काफल ट्री की पोस्ट पाने के लिये यहाँ क्लिक करें. वाट्सएप काफल ट्री
काफल ट्री वाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिये यहाँ क्लिक करें: वाट्सएप काफल ट्री
काफल ट्री की आर्थिक सहायता के लिये यहाँ क्लिक करें




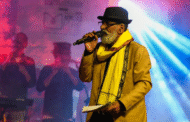

































1 Comments
मृगेश पाण्डे
वाह. संघर्षों भरे लम्हे.