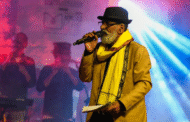खुद को अभिव्यक्त करने का सलीका मैंने अपने दौर के वरिष्ठ और चर्चित लेखक शैलेश मटियानी से सीखा. और यह सीखना अपने भावों को व्यक्त करने के लिए सटीक शब्दों के चयन की प्रक्रिया की तरह का नहीं था, इस रूप में था कि शैलेश मटियानी की अभिव्यक्ति में मुझे पहली बार अपने समाज के दर्शन हुए. भाषा मेरे लिए साध्य कभी नहीं रही, वह खुद को और अपने परिवेश को व्यक्त करने का माध्यम मात्र थी. बाद के दिनों में औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब मैंने देखा कि पंडितों के द्वारा परिवेश के बदले सिर्फ शब्दों-ध्वनियों को ही महत्व दिया जा रहा है तो मुझे बहुत निराशा हुई. मैंने जब देखा कि उच्च वर्ण के मेरे कई बुजुर्ग शब्द-ज्ञान के जरिए उनके साथ खेलते और चमत्कार प्रदर्शित करता हैं, मुझे लगा, मेरा यह निर्णय गलत नहीं था क्योंकि बुजुर्गों के रास्ते में चलकर मेरा संपर्क अपने परिवेश से छूटता चला जा रहा था. (Importance of Mother Tongue Batrohi)
शैलेश मटियानी की कहानियाँ हमारी जिंदगी से जुड़ी धरती और उसमें रहने वाले लोगों के सपनों को हू-ब-हू उसी रूप में उजागर कर देती थीं, जिस रूप में हम महसूस करते थे. वह एक समानांतर दुनिया की रचना थी, जिसके अन्दर प्रवेश करने के बाद हम भूल जाते थे कि इनमें से कौन-सी दुनिया वास्तविक है और कौन-सी प्रतिकृति. हालाँकि तब इस संसार को बनाने वाले के बारे में सोचने का विवेक नहीं था, मगर उस कच्ची उम्र में भी मुझे इस संसार को बनाने वाले (जिसे हम भगवान कहते थे) और शैलेश मटियानी में कोई फर्क नहीं महसूस होता था. बाद की जिंदगी में, साहित्य का सैद्धांतिक अध्ययन करने के बाद हमने पाया कि ग्रामीण जीवन की भाषा-शैली को लेकर लिखने वाले लेखकों में आभिजात्य हिंदी का दबाव पैदा हुआ और आंचलिक लेखन की चर्चा हिंदी के प्रतिष्ठित समीक्षकों-आलोचकों के बीच गायब होती चली गयी. इसका परिणाम यह हुआ कि हिंदी के अधिकांश आंचलिक कथाकार साहित्यिक चर्चा से गायब हो गए. यह दौर ‘नई कहानी’ आन्दोलन का था, जब सिर्फ मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेन्द्र यादव, मन्नू भंडारी और निर्मल वर्मा की कहानियाँ मानक समझी जाती थीं. (Importance of Mother Tongue Batrohi)

हो सकता है, यह कारण न रहा हो, इन्हीं दिनों मुझे लगा कि हिंदी कथा-साहित्य में भाषा-बोलियों की जो अनगढ़ सहजता थी, गायब होती चली गयी और उसके स्थान पर विशिष्ट वर्ग की भाषाओँ – संस्कृत, फारसी और हिंदी – के व्याकरण और मुहावरे का दबाव बढ़ा. हिंदी समीक्षा में यूरोप के औजार तेजी से आयात किये जाने लगे और भारतीय जीवन की सहज अभिव्यक्ति, गाँवों-कस्बों की अपनी पहचान, हाशिए में चली गयी. इसका सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि हिंदी प्रदेश की मातृभाषाएं धीरे-धीरे अपना वजूद खोती चली गईं; खुद को पढ़ा-लिखा और शिक्षित सिद्ध करने के लिए लोग न केवल स्थानीय भूगोल से पलायन करने लगे, स्थानीय अभिव्यक्ति से भी किनारा काटने लगे. स्थानीयता का इस्तेमाल लेखकगण अपने समाज की सापेक्षिकता में नहीं, अपने शब्द-ज्ञान और बौद्धिक चमत्कार के लिए करने लगे. हिंदी लेखन के आम हिंदी भाषी से कटने का सिलसिला भी यहीं से शुरू हुआ. (Importance of Mother Tongue Batrohi)
इन्हीं दिनों मेरे प्रिय लेखक शैलेश मटियानी में भी यह दबाव बढ़ा और और वे अपनी कहानियों और उपन्यासों का पुनर्लेखन करने लगे. वे हिंदी के उन विरले लेखकों में थे जिनकी आजीविका लेखन पर ही आश्रित थी, इस तरह का पुनर्लेखन करते हुए हुए उन्हें हिंदी के शिष्ट समाज में स्वीकृति का छद्म अहसास भी हो जाता था. बहरहाल, इससे उन्हें जो भी फायदा हुआ हो, मुझ जैसे उनके भक्त लेखकों का आधार खिसक गया और हम वैचारिक दृष्टि से त्रिशंकु बन गए.
हो सकता है, यह मेरा पूर्वाग्रह हो, मगर मेरी इस आपबीती को सुनकर शायद आप मेरा पक्ष जान सकें. सन 2000 में नए राज्य का गठन होने के बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अपना अलग पाठ्यक्रम निर्मित किया. पाठ्यक्रम निर्माण समिति का एक सदस्य मैं भी था. अविभाजित उत्तर प्रदेश के परीक्षा पाठ्यक्रम में फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास ‘मैला आँचल’ था, मैंने सुझाव दिया कि हमें अपने पाठ्यक्रम में ऐसे उपन्यास को शामिल करना चाहिए जो उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़ा हो. मैं इस काम में सफल भी हो गया और शैलेश मटियानी का लोकगाथा परक उपन्यास ‘मुख सरोवर के हंस’ पाठ्यक्रम में रख दिया गया.
उस वक़्त हिंदी पाठ्यक्रम समिति की संयोजक डॉ. सुधा पांडेय थीं, जिन्होंने सहज उत्साहवश कुमाऊँ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापक मटियानी जी की बेटी शुभा को उसी रात सूचना दी कि नए राज्य बनने के उपलक्ष्य में वो प्रदेश की संस्कृति का सर्वोत्कृष्ट दस्तावेज मटियानीजी का उपन्यास पाठ्यक्रम में रखकर उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहती हैं. सुधाजी की उम्मीद के विपरीत शुभा गुस्से में बोली कि वो जानती हैं, इसके पीछे आप लोगों की मंशा क्या है! हम सब लोग उनके पिता के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे है. हम लोग शैलेश मटियानी की छवि एक क्षेत्रीय लेखक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जब कि वो राष्ट्रीय स्तर के लेखक हैं. बिना प्रसंग जाने उन्होंने धमकी दी कि अगर उन्होंने यह उपन्यास कोर्स में रख दिया तो वह उन्हें कोर्ट में घसीटेगी. अपेक्षा के विपरीत प्रतिक्रिया सुनकर सुधाजी घबरा गईं और तत्काल उन्होंने मुझे फोन किया. मैंने बताया कि समिति में जो एक बार स्वीकृत हो चुका है, उसे बदला नहीं जा सकता, मगर सरल मना डॉ. पाण्डेय घबरा गईं और उन्होंने फिर शुभा को फोन किया कि वो खुद बताएं, उनका कौन-सा उपन्यास कोर्स में रक्खा जाये? शुभा ने उनके इस उपन्यास को किसी भी हालत में कोर्स में शामिल न करके किसी और राष्ट्रीय स्तर के उपन्यास को लेने की बात की. बाद में उसने बहुत ही मामूली उपन्यास ‘छोटे-छोटे पक्षी’ को रखने की जिद की जिसका उत्तराखंड के परिवेश से कोई सम्बन्ध नहीं है. मजेदार बात यह है कि यह उपन्यास आज भी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पाठ्यक्रम में स्वीकृत है.
मां की सिखाई ज़बान भूल जाने वाला बेटा मर जाता है
जिन लोगों ने पूर्व-सोवियत संघ के छोटे से देश की पहाड़ी भाषा ‘अवार’ में लिखने वाले कवि रसूल हमज़ातोव की विश्व प्रसिद्ध किताब ‘मेरा दागिस्तान’ पढ़ी है, केवल वही जान सकते हैं कि आदमी के जीवन में मातृभाषा का क्या महत्व है? संसार की लगभग सभी प्रमुख भाषाओँ में अनूदित इस बेस्ट-सेलर किताब में हमज़ातोव ने अपने क्षेत्र की भाषा ‘अवार’ को ‘माँ’ कहा है, जिसने उसे जन्म दिया, और पूरे देश में बोली जाने वाली भाषा ‘रूसी’ को ‘धाय माँ’, जिसने उसका पोषण किया. लेखक बार-बार इस बात का उत्तर तलाशता है कि इन दोनों माँओं में से किसको अधिक महत्व दिया जाये, मगर पूरी किताब में वह कहीं भी इसका उत्तर नहीं खोज पाता. (Importance of Mother Tongue Batrohi)

क्या इसका कोई जवाब हो सकता है?
इस सन्दर्भ में लेखक ने अपनी किताब में एक मार्मिक अनुभव का जिक्र किया है:
“एक बार पेरिस में एक दागिस्तानी चित्रकार से मेरी भेंट हुई. क्रांति के कुछ ही समय बाद वह पढ़ने के लिए इटली गया था, वहीँ एक इतालवी लड़की से उसने शादी कर ली और अपने घर नहीं लौटा. पहाड़ों के नियमों के अभ्यस्त इस दागिस्तानी के लिए अपने को नई मातृभूमि के अनुरूप ढलना मुश्किल था. वह देश-देश में घूमता रहा, उसने दूर-दराज़ के अजनवी मुल्कों की राजधानियां देखीं, मगर जहाँ भी गया, सभी जगह उसे घर की याद सताती रही.
“मैंने यह देखना चाहा कि रंगों के रूप में यह याद कैसे व्यक्त हुई है. इसलिए मैंने चित्रकार से अपने चित्र दिखाने का अनुरोध किया.
“एक चित्र का नाम ही था – ‘मातृभूमि की याद’. चित्र में इतालवी औरत (उसकी पत्नी) पुरानी अवार पोषाक में दिखाई दे रही थी. वह होत्सातल के मशहूर कारीगरों की नक्काशी वाली चाँदी की गागर लिए एक पहाड़ी चश्मे के पास खड़ी थी. पहाड़ी ढाल पर पत्थरों के घरों वाला उदास-सा अवार गाँव दिखाया गया था और गाँव के ऊपर पहाड़ तो और भी ज्यादा उदास-से लग रहे थे. पहाड़ी चोटियाँ कुहासे से लिपटी हुई थीं.
“पहाड़ों के आँसू ही कुहासा है’, चित्रकार ने कहा, ‘वह जब ढालों को ढक देता है, तो चट्टानों की झुर्रियों पर उजली बूँदें बहने लगती हैं. मैं कुहासा ही हूँ.’
“दूसरे चित्र में मैंने कंटीली जंगली झाड़ी में बैठा हुआ एक पक्षी देखा. झाड़ी नंगे पत्थरों के बीच उगी हुई थी. पक्षी गाता हुआ दिखाया गया था और पहाड़ी घर की खिड़की से एक उदास पहाड़िन उसकी तरफ देख रही थी. चित्र में मेरी दिलचस्पी देखकर चित्रकार ने स्पष्ट किया – ‘यह चित्र पुरानी अवार किंवदंती के आधार पर बनाया गया है.’ (Importance of Mother Tongue Batrohi)
“किस किंवदंती के आधार पर?’
“एक पक्षी को पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया गया. बंदी पक्षी दिन-रात एक ही रट लगाए रहता मातृभूमि, मेरी मातृभूमि, मातृभूमि, मातृभूमि, मातृभूमि… बिलकुल वैसे ही, जैसे कि इन तमाम सालों के दौरान मैं भी यही रटता रहा हूँ… पक्षी के मालिक ने सोचा, जाने कैसी है उसकी मातृभूमि, कहाँ है, अवश्य ही वह कोई फलता-फूलता हुआ बहुत ही सुन्दर देश होगा, जिसमें स्वर्गिक वृक्ष और स्वर्गिक पक्षी होंगे. तो मैं इस परिंदे को आज़ाद कर देता हूँ. और फिर यह देखूंगा कि वह किधर उड़कर जाता है. इस तरह वह मुझे उस अद्भुत देश का रास्ता दिखा देगा.’ उसने पिंजरा खोल दिया और पक्षी बाहर उड़ गया. दसेक कदम की दूरी तक उड़कर वह नंगे पत्थरों के बीच उगी जंगली झाड़ी में जा बैठा. इस झाड़ी की शाखाओं पर उसका घोंसला था… अपनी मातृभूमि को मैं भी अपने पिंजरे की खिड़की से ही देखता हूँ.’ चित्रकार ने अपनी बात खत्म की.
“तो आप लौटना क्यों नहीं चाहते?’
“देर हो चुकी है. कभी मैं अपनी मातृभूमि से जवान और जोशीला दिल लेकर आया था. अब मैं उसे सिर्फ बूढ़ी हड्डियाँ कैसे लौटा सकता हूँ!
“पेरिस से घर लौटकर मैंने चित्रकार के सगे-सम्बन्धियों को खोज निकाला. मुझे इस बात की बड़ी हैरानी हुई कि उसकी बूढ़ी माँ अभी तक जिन्दा थी. अपनी मातृभूमि को छोड़ देने और विदेश में जा बसने वाले बेटे के बारे में उसके सगे-सम्बन्धियों ने उदास होते हुए मेरी बातें सुनी. ऐसा लगता था कि उन्होंने मानो उसे माफ़ कर दिया था और इस बात से खुश थे कि वह जिन्दा तो है! पर तभी उसकी माँ पूछ बैठी, ‘तुम दोनों ने अवार भाषा में बातचीत की?’
“नहीं, हमारी बातचीत दुभाषिये के जरिए हुई. मैं रूसी बोलता था और तुम्हारा बेटा फ्रांसीसी.’
“माँ ने काले दुपट्टे से मुँह ढक लिया, जैसा कि बेटे की मौत की खबर मिलने पर किया जाता है. पहाड़ी घर की छत पर बारिश पटापट ताल दे रही थी. हम अवारिस्तान में बैठे थे. अपनी मातृभूमि को त्याग देने वाला दागिस्तान का बेटा भी शायद पृथ्वी के दूसरे छोर पर, पेरिस में बारिश का राग सुन रहा था. बहुत देर तक चुप रहने के बाद चित्रकार की माँ ने कहा, ‘तुम्हें ग़लतफ़हमी हुई है, रसूल, मेरा बेटा तो कभी का मर चुका. वह मेरा बेटा नहीं था. मेरा बेटा वह ज़बान नहीं भूल सकता था, जो उसे मैंने, अवार माँ ने सिखाई थी.’”
फिर से शैलेश मटियानी
एक और रोचक उदाहरण. करीब सात-आठ साल पहले केन्द्रीय साहित्य अकादेमी और नेशनल बुक ट्रस्ट ने मुझे मटियानी जी के साहित्य का संचयन तैयार करने का काम सौंपा. मैंने दो वर्ष की मेहनत के बाद अकादमी के लिए 400 और ट्रस्ट के लिए 250 पृष्ठों की किताबें तैयार कीं, मगर जब प्रकाशन की अनुमति के लिए प्रकाशकों ने उनके बेटे राकेश को लिखा तो उसने दोनों प्रकाशकों को लिखा कि जिस व्यक्ति से वे लोग पुस्तकें तैयार करवा रहे हैं, वो वर्षों से उनके पिता की छवि ख़राब करने में तुले हैं. वे कॉपी राईट की अनुमति तभी देंगे, जब या तो संचयनकर्ता बदले जाएँ या पुस्तक पहले उन्हें पढ़ने के लिए दी जाए. प्रकाशकों ने जब बताया कि वे लोग पुस्तकों को देश के शीर्षस्थ विद्वानों से रिव्यू करा चुके हैं, मगर उनके पुत्र ने अनुमति देने से मना कर दिया. (Importance of Mother Tongue Batrohi)
इस प्रसंग से मटियानी जी का जो अहित हुआ वह तो है ही, मेरा भी सारा परिश्रम बेकार गया. यह पहला मौका था जब शैलेश मटियानी कि किताबें देश के इन शीर्षस्थ प्रकाशकों से छप रही थीं.
कुमाऊनी के लिए लखटकिया सम्मान
एक और प्रसंग. यह मामला थोड़ा अलग है, मगर प्रकृति सबकी समान है. केन्द्रीय साहित्य अकादमी ने भारत की लोक भाषाओँ के लिए एक लाख रुपये का सम्मान घोषित किया, जिसे 2016 में कुमाऊनी को दिया जाना तय किया गया. निर्णायक मंडल में साहित्य अकादमी ने विद्वान कवि-आलोचक रमेशचंद्र शाह, मुझे और हिंदी अकादमी, दिल्ली के तत्कालीन सचिव कथाकार हरिसुमन बिष्ट को नामित किया. हम लोगों ने उत्साह के साथ काम शुरू किया.
लोक भाषाओँ की अभिव्यक्ति को लेकर मेरे दिमाग में कुछ निश्चित विचार हैं. मेरा मानना है कि लोक भाषाओँ के समाज की संरचना को जाने बगैर उसकी अभिव्यक्ति के स्वरूप को नहीं समझा जा सकता. उसके पाठक और श्रोता वर्ग की अपेक्षाएं प्रतिष्ठित भाषाओँ के पाठक से भिन्न होती हैं.
हो सकता है कि मेरी ऐप्रोच पूर्वाग्रहग्रस्त दिखाई दे, मैंने अपने वोट के रूप में कुमाऊँ के एक लोकप्रिय गीतकार-कवि हीरा सिंह राणा को चुना और उस बहाने बहस के लिए अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निवेदन किया. शाह जी ने शुरू में ही आपत्ति की, आरोप लगाया कि अपना आलेख सुनाकर निर्णायकों को प्रभावित करने का यह एक परोक्ष तरीका है; लेकिन जब मैंने इसे अपने वोट के रूप में लेने की बात की तो उन्होंने कहा कि राणाजी कवि नहीं हैं, मेले-ठेलों में लोकप्रिय गायक हैं. मेरे वोट का जब हरिसुमन बिष्ट ने भी समर्थन किया, शाह जी ने कहा कि कविता एक लिखित साहित्य की विधा है, उसका स्तर इतना नहीं गिराया जाना चाहिए.
शाहजी के तर्क का प्रभाव अकादमी के प्रतिनिधि उनके सचिव-सदस्य पर पड़ना ही था, उसी वर्ष उन्हें हिंदी के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, इसलिए हम दोनों बहुमत में होते हुए भी अल्पमत में आ गए. अकादमी के रुख को देखकर हरिसुमन ने बीच का रास्ता निकाला, ‘अच्छा हो इसे दो लोगों में बाँट दिया जाये.’ उन्होंने जो नाम सुझाये, हीरासिंह वहां भी शामिल थे, जिस पर शाहजी राजी नहीं हुए. शाहजी ने जो नाम सुझाये, उनसे मैं सहमत नहीं था, अंततः अकादमी के सचिव ने बीच का रास्ता निकाला, ‘देखिये, ये सम्मान भारत की सभी भाषाओँ के लिए साल में एक बार दिया जाता है; इसके बाद कुमाऊनी का नंबर पता नहीं कब आ पाता है, इसलिए इस बार यह सम्मान कुमाऊनी के सबसे बुजुर्ग कवि को दे दिया जाये.’ इस प्रस्ताव का सबने स्वागत किया और अंत में 94 वर्षीय बुजुर्ग कुमाऊनी कवि चारू चन्द्र पांडे पर सभी सहमत हो गए, फिर भी शाहजी के सुझाव पर एक अन्य कवि को पचास हजार का आधा सम्मान प्रदान करने में अकादमी को सफलता मिल ही गई. (Importance of Mother Tongue Batrohi)
हम लोग अपनी जड़ों की चिंताओं को लेकर पुनर्विचार करें
दिल्ली सरकार के द्वारा कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी भाषाओँ के लिए एक स्वतंत्र अकादमी स्थापित करने के निर्णय के सन्दर्भ में इतनी लंबी भूमिका को पढ़कर कुछ लोगों को खीझ हो सकती है, मगर मुझे यह चिंता इसलिए जरूरी लगी कि हम लोग अपनी जड़ों की चिंताओं को लेकर पुनर्विचार करें! अपनी जड़ों को हम केवल अतीत की भावुकता या नोस्टेल्जिया के रूप में न देखें.
यह ठीक है कि जिस दौर में हम जी रहे है, वह राजनीति से प्रेरित और संचालित समाज है, लेकिन हमारा समाज और उसकी परम्पराएँ, उसकी चेतना और धडकनें तो वही हैं, जो हमारे पुरखों के ज़माने में थीं. इस रूप में हमारी भारतीयता और स्थानीयता के बीच भी बहुत फर्क नहीं है. अगर ऐसा है तो हम क्यों बार-बार अपनी जड़ों को लेकर हमेशा इतने भावुक हो जाते हैं?
दरअसल, हम अपनी जड़ों को लेकर कभी तो इतने भावुक हो जाते हैं कि सिर्फ अतीत और स्मृतियों में खो जाना चाहते हैं (नराई!, खुद!!) या फिर इतने व्यावहारिक बन जाते हैं कि अपने अतीत को आज के लोकप्रिय फैशन के अनुरूप तत्काल ढाल देना चाहते हैं. नई पोषाक, नए वाद्य, नई थिरकन, नई ध्वनियाँ, नई बीट… मानो इनके बिना भी भला क्या आधुनिक हुआ जा सकता है, मानो परम्परा और आधुनिकता दो परस्पर विरोधी ध्रुवांत हों.
उत्तराखंड की लोक भाषाओँ को मंच प्रदान करने का जो काम इस प्रदेश की सरकार को करना चाहिए था, उसे देश की केंद्र सरकार कर रही है, इससे अधिक सम्मान की बात और क्या हो सकती है? और सबसे बड़ी बात यह कि अकादमी के उपाध्यक्ष का चयन राजनीतिक नहीं, शुद्ध कलात्मक मानदंडों पर आधारित है. उत्तराखंड की वर्तमान बीजेपी सरकार से पहले कांग्रेस सरकार के ज़माने में भी ‘उत्तराखंड साहित्य, कला एवं संस्कृति परिषद्’ का गठन किया गया था; पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश के राज्यगीत की रचना के लिए उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया था, दोनों ही जगह प्रदेश के हर क्षेत्र के प्रतिनिधि कलाकारों को प्रतिनिधित्व दिया गया था, मगर प्रदेश की जनता ने ही उसका कितना स्वागत किया? अपनी जड़ों को हमने अपने राजनीतिक छल-छद्मों से इतना ढक दिया है कि उससे हमारी पहचान और जड़ें इतनी दब गयी हैं कि उनके पुनः-अंकुरण और प्रजनन की संभावना ही नष्ट कर दी गयी है.
दुनिया जितनी तेजी से सिमटती और एकरूप होती जा रही है, उसमें अपनी स्वायत्त अस्मिता को बचाए रख पाना आसान नहीं है. बार-बार ऐसे दबावों के भार के बीच हम घुटन महसूस कर रहे हैं, बार-बार उससे मुक्ति पाना हमारी ताकत से परे होता जा रहा है, मगर हम हैं कि उसी घुटन के बीच खुशियाँ तलाश रहे हैं. ख़ुशी से चीखना चाह रहे हैं, हमें आनंद आ रहा है और हम समझ रहे हैं कि हम अपनी आदिवासी पहचान से मुक्त होकर सभ्य और आधुनिक बनते जा रहे हैं.
राजनीति की नहीं कला की नींव चाहिए
इसलिए, हमारे अपने हाथों न सही, हमारे दूसरे समानधर्मा शुभ-चिंतकों के द्वारा हमारी चिंताओं का जो विस्तार किया जा रहा है, उसका तो हमें स्वागत करना ही चाहिए. हम सब जानते हैं कि आज की राजनीति सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थों की चिंताओं के बीच सिमटी रहती है, उसे अपने समाज और परिवेश की चिंताओं से कोई सरोकार नहीं है.
ऐसे में अपने समाज को परिभाषित करने का काम सिर्फ और सिर्फ अपनी जड़ों से जुड़ा समाज ही कर सकता है, बशर्ते कि वह समाज कलाओं की नींव पर खड़ा हो, राजनीति की नींव पर बना नहीं. संयोग से अभी उत्तराखंडी समाज की परंपरागत जड़ें अभी मुरझाई नहीं हैं, वे आज भी कला और संवेदना की नींव पर अंकुरित हुई बहुत साफ दिखाई दे रही हैं. (Importance of Mother Tongue Batrohi)
हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें: Kafal Tree Online

लक्ष्मण सिह बिष्ट ‘बटरोही‘ हिन्दी के जाने-माने उपन्यासकार-कहानीकार हैं. कुमाऊँ विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग के अध्यक्ष रह चुके बटरोही रामगढ़ स्थित महादेवी वर्मा सृजन पीठ के संस्थापक और भूतपूर्व निदेशक हैं. उनकी मुख्य कृतियों में ‘थोकदार किसी की नहीं सुनता’ ‘सड़क का भूगोल, ‘अनाथ मुहल्ले के ठुल दा’ और ‘महर ठाकुरों का गांव’ शामिल हैं. काफल ट्री के लिए नियमित लेखन. टेलीफोन : 9412084322
काफल ट्री वाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिये यहाँ क्लिक करें: वाट्सएप काफल ट्री
काफल ट्री की आर्थिक सहायता के लिये यहाँ क्लिक करें