आज से 60-70 वर्ष पूर्व हमारी पीढ़ी के लोगों ने कुमाऊँ की पावन भूमि के जिस सांस्कृतिक वातावरण में प्रथम श्वास ली थी तथा किंचित् होश संभालने के साथ ही जिन परम्परागत सांस्कृतिक तत्त्वों को अपने संस्कारों में आत्मसात् किया था हिमालय के उन्नत शिखरों के समान अनन्तकाल से पुंजीभूत तथा भागीरथी के प्रवाह के समान अनन्तकाल से प्रवहमान वे तत्त्व आज नवयुग के ताप से पिघलते व सूखते जा रहे हैं. महानगरों के विशाल मंचों तथा कलागृहों में कुमाऊंनी के सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा कला प्रदर्शनियों के आयोजक केवल इन मंचों तथा प्रदर्शनियों तक सीमित रूपों के आधार पर इसके संरक्षण की बात कहकर भले ही आत्म संतोष कर ले, किन्तु उसकी अपनी आधार भूमि पर उसका जिस तीव्र गति से क्षरण हो रहा है वह किसी भी संवेदनशील कुमाऊंनी से छिपा हुआ नहीं. उसे एक महान सांस्कृतिक जागरण के बिना इन इक्के-दुक्के रंगीन टल्लों के माध्यम से सुरक्षित रख पाना सम्भव नहीं. यदि क्षरण तथा विध्वंश की इस गति का किसी सशक्त रुप में अवरोधन नहीं हुआ तो वह दिन दूर न होगा जब कि पुरातन विनष्ट संस्कृतियों के समान ही कुमाऊंनी संस्कृति भी किसी कला संग्रहालय में रखी हुई एक प्रदर्शनीय वस्तु मात्र बनकर रह जायेगी.
(Cultural Change Article)
दुर्भाग्य से हमारी नई पीढ़ी ने भौतिक समृद्धि को सांस्कृतिक निधि के साथ समीकृत कर डाला है जिससे हमारी सांस्कृतिक परम्पराओं का तथा मूल्यों का निरन्तर हास होता जा रहा है. इस भूमि को अपना आवास बनाने वाले हमारे समाज के कर्णधारों ने अपने पीढ़ी दर पीढ़ी के संचित अनुभवों के आधार पर जन कल्याण की भावना से प्रेरित होकर यहां के सामाजिक जीवन को जिस ढांचे में ढाला था उसकी आधार भित्ति की शिलाएं अब निरन्तर खिसकती जा रही हैं. सांस्कृतिक भूकम्प के इन झटकों की विपरिणति अन्ततोगत्वा किस रूप में होगी अभी यह कह पाना तो कठिन है, किन्तु इस समय सांस्कृतिक संक्रमण का जो रुप सामने आ रहा है वह पुरानी पीढ़ी के लोगों को अवश्य ही स्तम्भित व विचलित करने वाला है.
आज नव सांस्कृतिक उत्थान, सामाजिक समानता, शहरीकरण एवं आधुनिकता के नाम पर जो कुछ हो रहा है उससे आधुनिक युग की चकाचौंध में चकित सामान्य जन मानस को भले ही सन्तोष हो रहा हो, किन्तु कुमाऊंनी संस्कृति के प्रति संवेदनशील एवं इसके दूरगामी दुष्परिणामों के प्रति सचेत मानस अवश्य ही व्यथित होंगे ऐसा मैं समझता हूँ. सम्भव है आज मेरे इन विचारों से सहमति प्रकट करने वाले लोग कम ही मिलें, क्योंकि प्रगतिवाद का झंडा उठाने वालों को तो इनमें रुढ़िवादिता की ही गन्ध आयेगी.
यह किसी से छिपा हुआ नहीं कि आज अनेक परम्पराओं का पालन करने वाले भी केवल एक लकीर ही पीट रहे हैं. उनके प्रति न उनकी आस्था है और न उनके महत्त्वों से वे परिचित ही हैं. उनके महत्त्व को उजागर करने वाली परम्पराएं ही लुप्त हो चली है एवं तथाकथित वैज्ञानिकता के दृष्टिकोण ने उन्हें पिछड़ेपन के अवशेषों का नाम देकर उनके प्रति अनास्था एवं उपेक्षा उत्पन्न कर दी है. यहाँ तक कि अतीत में बड़े उत्साह से सम्पन्न किये जाने वाले पर्व, पूजन एवं सामाजिक संस्कार अब या तो उपेक्षा के पात्र बन गये हैं या केवल एक परम्परा का पालन मात्र बनकर रह गये हैं, उनके रूपों एवं रंगों में बहुत अन्तर आ गया है. अनेक ऋतु उत्सव अब केवल स्मृति शेष रह गये हैं. विशेष उत्सवों अथवा मेलों में होने वाले नृत्य, गीत, भटगान आदि अब कहाँ? जिन्होंने उन्हें देखा या सुना है उन्हें उनकी स्मृति अब भी आत्मविभोर अवश्य करती होगी. शहरी जीवन को ही सब कुछ समझने वाले लोगों के मन में तो शायद इनकी धूमिल छाया भी कभी नहीं पड़ी होगी.
(Cultural Change Article)
इससे भी बड़ी विडम्बना तो यह है कि कुमाऊंनी लोग जहाँ एक ओर अपनी पुरातन परम्पराओं के प्रति बढ़ती हुई अनास्था के कारण उन्हें छोड़ते जा रहे हैं वहीं दूसरी ओर अन्य प्रदेशों में प्रचलित उन अनेक परम्पराओं को अपनाते जा रहे हैं जो हमारी संस्कृति के प्रतिकूल है तथा हमारे समाज के लिए अकल्याणकारी भी. उदाहरणार्थ, विवाह को ही लीजिए. सुरसा के मुख की भांति निरन्तर बढ़ता हुआ दहेज का राक्षस तो समाज को ग्रसता ही जा रहा था पर साथ में और भी अनेक कुरीतियाँ जो कि हमारी संस्कृति से बिल्कुल भी मेल नहीं खातीं, अपने पैर इस क्षेत्र में पूरी तरह पसार चुकी हैं. विवाह के अवसर पर सुरा का खुला अनियंत्रित प्रयोग तो इसका अभिन्न अंग बन ही चुका था पर अब एक भौंडे प्रकार का नृत्य जिसे डिस्को, ट्विस्ट आदि के नाम से अभिहित किया जा रहा है वह भी इसमें सम्मिलित हो गया है. हैरानी की बात तो यह है कि अब धीरे-धीरे पुरुषों के साथ स्त्रियाँ भी इसमें भाग लेने लगी हैं. (स्मर्तव्य है कि कुमाऊं में स्त्रियाँ वर यात्रा में तथा शवयात्रा में भाग नहीं लेती थीं). वर यात्रा के साथ किया जाने वाला परम्परागत छोलिया नृत्य तो अब कभी दूरदर्शन पर ही देखने को मिल सकता है.
इसी प्रकार परम्परागत वादनों- ढोल, नगाड़े, तूरी, शंख, मशक बीन का स्थान अब बैंड के नाम को बदनाम करने वाले टटपूजिया किस्म के बेसुरे, बेमेल बाजों की ढम ढम व तू-तू ने ले लिया है और तो और अब तो विवाहों में धूलि अर्घ्य का कार्य दिन के 12 बजे तथा ध्रुवदर्शन की विधि दिन के 1 बजे सम्पन्न की जा रही है. स्मर्तव्य है कि दिवसीय विवाह का जो कार्य आतंकवाद से पीड़ित क्षेत्रों में विवशता वश प्रारम्भ किया गया था उसे यहाँ पर इस प्रकार की कोई विवशता न होने पर भी अपना लिया गया है जो कि विवाह जैसे पवित्र संस्कार के प्रति लोगों की बढ़ती हुई अनास्था का द्योतन करता है. उनके लिए सम्भवतः विवाह अब कोई पवित्र संस्कार न रहकर स्त्री-पुरुष के गृहस्थ जीवन को प्रारम्भ करने की सामाजिक स्वीकृति मात्र रह गया है. यही कारण है कि शगुनाक्षरों व मांगलिक संस्कार गीतों के स्थान पर भरे रिकार्डेड गीत बजाये जाते हैं और विवाह सम्बन्धी लोकगीतों के नाम पर जो गीत गाये जाते हैं वे भी अपनी धुनों तथा शब्दावली में मात्र सिने गीतों की भद्दी नकल होते हैं.
इसी प्रकार कुमाऊंनी संस्कृति के प्रतीक विशिष्ट प्रकार के वस्त्राभूषण तो अब कभी-कभी किन्हीं परिवारों में मात्र मांगलिक कार्यों तक ही सीमित रह गये हैं. पहले विवाहित नारियाँ विशेषकर जब विशेष अवसरों पर मन्दिरों में पूजा-अर्चना के लिए जाती थीं तो अपनी परम्परागत वेशभूषा में ही सुसज्जित होकर जाती थीं, जो स्वयं में एक सांस्कृतिक झांकी प्रस्तुत किया करती थी. किन्तु अब वह सब कुछ धीरे-धीरे अतीत की वस्तु बनती जा रही है. शेष रह गयी है नकली धागों से बनी साड़ियाँ जो चाहने पर भी कुमाऊंनी नारी द्वारा सिर ढकने की सांस्कृतिक परम्परा का निर्वाह कर पाने में भी असमर्थ है, पुरुषों ने तो अपनी सांस्कृतिक परम्पराओं को पहले ही एक ओर रख दिया था, पर स्त्रियाँ इसकी संरक्षिका बन कर इसे सुरक्षित रखे हुए थीं, किन्तु अब वह आशा भी दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है. शहरों में ही नहीं, ग्रामीण अंचलों में भी स्त्रियाँ अपनी नागरिक बहिनों का अनुकरण करके आधुनिकता की धुन में अपनी परम्परागत वेश भूषा को त्यागती जा रही हैं, उन्हें यह ज्ञात नहीं कि उष्ण प्रदेशों के लिए अनुकूल साड़ी, ब्लाउज़ जैसे वस्त्रों को अपनाकर वे इन शीत प्रधान क्षेत्रों में अपने लिए कितने रोगों को आमंत्रित कर रही हैं. घरों के अन्दर रहने वाली स्त्रियों के स्वास्थ्य पर भले ही इन वस्त्रों का उतना दुष्प्रभाव न पड़ता हो किन्तु शीत, वर्षा में खेतों व वनों में काम करने वाली स्त्रियों के स्वास्थ्य पर इन हल्के फुल्के वस्त्रों का कितना घातक प्रभाव हो रहा है इसे ग्रामीण अंचलों में नये-नये प्रकार के बढ़ते हुए स्त्री रोगों में देखा जा सकता है.
(Cultural Change Article)
बताने की आवश्यकता नहीं कि इन शीत प्रधान क्षेत्रों में घरों से बाहर काम करने वाली स्त्रियों के लिए परम्परागत घाघरा, आंगड़ा, धोती रक्षा कवच का काम करता था. ये उनके शरीरांगों को शीत के दुष्प्रभावों से बचाये रखते थे. कमर में बंधा हुआ पट्टू न केवल भार वाहन में उनकी रीढ़ की हड्डी को स्थिर रखता था, अपितु उनके उदर को भी अनावश्यक वृद्धि से बचाता था. आधुनिकतम अनुसन्धानों से पता चलता है कि जो लोग कमर पर पट्टू या चौड़ी पेटी बाँधते हैं ये कमर-दर्द के शिकार नहीं होते. आज गाँव की नारियों में भी सामान्य रुप से कमर दर्द, प्रसूत, हाथ पैरों में सूजन आदि की जो शिकायत पायी जाती है उसका एक कारण इस परम्परागत वेश भूषा का परित्याग है. हमारे पूर्वजों ने क्षेत्र विशेष की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही यहाँ के निवासियों के लिए इस प्रकार के परिधानों का विधान किया होगा.
इसी प्रकार हमारे पूर्वजों ने अपने संचित अनुभवों के आधार पर हमारे भोजन में विशेष-विशेष प्रकार के खाद्य पदार्थों का समावेश किया था. जो कि यहाँ की जलवायु के अनुकूल स्वास्थ्यवर्धक तो थे ही रोग परिहारक भी थे. किन्तु आज का कुमाऊंनी वर्ग उन्हें पिछड़ेपन तथा निर्धनता की निशानी समझ कर त्यागता जा रहा है और उसके स्थान पर आयातित भोजन पद्धति को अपनाता जा रहा है. फलत: विशेष कर हमारे बच्चों का स्वास्थ्य विकृत होता जा रहा है और हमारी कमाई का एक बहुत बड़ा भाग अंग्रेजी दवा निर्माताओं की जेब में जा रहा है. आर्थिक समृद्धि का होना तो अच्छा है किन्तु वह धन घर में हानिकारक वस्तुओं के आयातन का आधार बने यह वाञ्छनीय नहीं. हमें विवेकपूर्ण ढंग से उसका सदुपयोग इस रुप में करना चाहिए जो कि हमारी सभ्यता, संस्कृति एवं क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुकूल हो.
उदाहरणार्थ, सम्पन्नता का एक रुप पहाड़ों में बनने वाले पक्के लैंटर वाले भवनों के रुप में देखा जा सकता है. इनके भीतर के सीमेण्ट के फर्श व प्लास्टर की हुई दीवारें देखने में सुन्दर तथा सुदृढ़ अवश्य होती हैं किन्तु शीत प्रधान क्षेत्रों में इस प्रकार के घरों का उनमें रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर क्या दुष्प्रभाव होता है इसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता. यहाँ पर भी मुझे फिर वही बात दुहरानी पड़ती है कि हमारे पूर्वजों ने क्षेत्र विशेष की जलवायु को देखते हुए अपने परम्परागत संचित अनुभवों के आधार पर इसके अनुकूल रहन- सहन की जिस पद्धति को अपनाया था हम उसे भूलते जा रहे हैं और उसके स्थान पर मैदानी क्षेत्रों का अन्धानुकरण करते जा रहे हैं. इसका भयंकर दुष्परिणाम हम अभी गत वर्ष के गढ़वाल के भूकम्प में देख चुके हैं जिसमें सारे पक्के लेंटर वाले मकान ध्वस्त हो गये और उनके नीचे दब कर सैकड़ों जीवन दीप बुझ गये. जब कि परम्परागत ढंग से बने घरों की न तो हानि हुई और न उनके भार से दबे लोगों की जीवन ज्योति ही बुझी. हमारे समाज के गठन व व्यवस्थाओं के स्तर पर जो आमूल-चूल परिवर्तन आ रहे हैं उनका सम्यक् आंकलन तो एक वृहत् शोध प्रबन्ध के द्वारा ही हो सकता है, किन्तु यहाँ पर बानगी के रुप में कतिपय रुपों की ओर संकेत किया जा सकता है.
यथा-यहाँ की अभिवादन प्रत्यभिवादन की शब्दावली को ही लीजिए शहरों में उसका ऐसा समतलीकरण हो रहा है कि उससे कुमाऊंनी के उस परम्परागत सामाजिक ढांचे का आभास तक नहीं हो पाता जो कि पहले बहुत स्पष्ट एवं पूर्ण रुप से व्यवस्थित था. अर्थात् अभिवादनात्मक शब्दावली से ही अभिवादक एवं प्रत्यभिवादक की जाति, वर्ग एवं सामाजिक स्वर की स्पष्ट अभिव्यक्ति हो जाया करती थी. उसके उस परम्परानुमोदित रुप का अनुपालन न करना सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टियों से अवांछनीय समझा जाता था, किन्तु अब इस स्वातन्त्र्य युग में ऐसा सामाजिक बन्धन न किसी को स्वीकार्य है और न किसी को इसका अनुपालन करने के लिए विवश ही किया जा सकता है. दूर दराज के ग्रामीण अंचलों में भले ही इसके अवशेष देखने को मिल जायें.
ऐसे ही सांस्कृतिक धरोहर समझी जाने वाली बन्धुत्ववाची शब्दावली, विशेषकर वैवाहिक सम्बन्धों से सम्बद्ध सम्बोधन परक शब्दावली, तो संक्रमण के उस दौर से गुजर रही है जिसमें कि उसका अस्तित्व ही समाप्त होने की आशंका बढ़ती जा रही है, पति-पत्नी के द्वारा अपने वैवाहिक सहयोगी के निकटतम सम्बन्धियों को सम्बोधित करने वाली शब्दावली दोनों ही ओर से एक रुप होती जा रही है. अर्थात् पति के माता-पिता, चाचा-चाची, ताऊ-ताई, भाई-भाभी, दीदी- जीजा, मामा-मामी आदि को अब नवीन प्रवृत्ति के अनुसार पत्नी द्वारा इन्हीं सम्बन्धों की सम्बोधक शब्दावली में सम्बोधित किया जाने लगा है. यही स्थिति पत्नी के सम्बन्धियों के विषय में भी पायी जाती है. इस संक्रान्ति के फलस्वरुप सास-ससुर ज्यू, सौर्ज्यू जैसे शब्दों का तो सर्वथा बहिष्कार हो ही रहा है और इसके साथ ही इन शब्दों के साथ सम्बद्ध बन्धुत्ववाची सांस्कृतिक गरिमा का भी जो कि अन्यथा इनके साथ सम्बद्ध हुआ करती थी.
फलत: जब कोई स्त्री चाचा जी, मामा जी या भाई साहब आये थे कहती हैं तो यह भेद कर पाना कठिन हो जाता है कि उसके अपने चाचा आदि आये थे या उसके चचिया, ममिया श्वसुर व जेठ जी आये थे. पति के भाई को जेठजी, उसकी बड़ी बहिन को नानिज्यू या पौंणी कहने में जो एक विशेष कोटि की सांस्कृतिक गरिमा व्यक्त होती है वह भाई साहब व दीदी कहने में नहीं, उनकी भी अपनी गरिमा है किन्तु भिन्न सन्दर्भ में. कुमाऊंनी के अन्य बन्धुत्ववाची शब्दों पर होने वाला हिन्दी का आक्रमण भी चिन्तनीय है. यथा ज्येष्ठ पिता (ज्याठ् बाबु), के लिए ताऊ, ज्येष्ठ माता (जेड़जा) के लिए ताई, मातृष्वसा (कैंजा) के लिए मौसी, पितृष्वसा (बुबु) के लिए बुआ आदि, नाते रिश्तों को मटियामेट करने की रही सही कसर को पूरा कर दिया अंग्रेजी की जूठन अंकल और आंटी ने जोकि सारे धान ढाई पसेरी की कहावत को भली भांति चरितार्थ कर रहा है. उपर्युक्त तथ्य मात्र दिशा निर्देशक हैं. उस सांस्कृतिक क्रान्ति के जो कि कुमाऊंनी समाज में बड़े जोरों से आ रही है.
(Cultural Change Article)
प्रो. डी. डी. शर्मा
प्रो. डी. डी. शर्मा का यह लेख ‘श्री लक्ष्मी भंडार हुक्का क्लब, अल्मोड़ा’ द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पत्रिका पुरवासी के 1993 के अंक में छपा था. काफल ट्री में यह लेख पुरवासी पत्रिका से साभार लिया गया है.
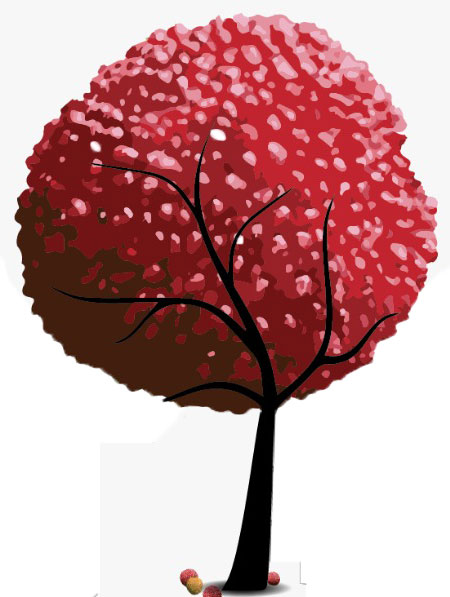
Support Kafal Tree
.
काफल ट्री वाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिये यहाँ क्लिक करें: वाट्सएप काफल ट्री
काफल ट्री की आर्थिक सहायता के लिये यहाँ क्लिक करें








































