अनुवाद पढ़कर बनता है गंभीर और स्थायी पाठक
भारत जैसे महादेश में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं, उन्हें देखते हुए कोई भी अनुमान लगा सकता है कि यहाँ के लोग कितनी तो भाषाएँ जानते होंगे. मगर वास्तविकता एकदम उलटी है. अपनी पडौसी भाषा के साथ एक आम भारतीय ईर्ष्यालु पडौसी का-सा व्यवहार करता है. मानो वह कह रहा हो, मेरा वश चले तो मैं पूरे देश में अपनी ही भाषा फैला दूँ.
काश, एक औसत भारतीय ऐसा होता!
भाषा और ज्ञान को लेकर हमसे अधिक कंजूस शायद ही कोई दूसरा समाज हो. ‘अतिथि देवो भव’ और ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ वाले इस कथित महा-समाज में ज्ञान को लेकर यह मनोवृत्ति कब पैदा हुई, कहना मुश्किल है; हालाँकि जाति और वर्ण के नाम पर छली जाने वाली ‘एकलव्य और कर्ण-वादी’ व्यवस्था अब भी यहाँ मौजूद हैं.
आज हम एक नए, उदार और वैश्विक समाज के अंग हैं फिर भी बहुत बड़ी संख्या में हमारे ही बीच ऐसे लोग हैं जो अपनी जुड़वाँ भाषा को ‘म्लेच्छ की भाषा’ कहकर दुत्कारते हैं और अपने अकेले क्षणों में भले ही उसे घंटों गुनगुनाते हों, सार्वजनिक रूप से उसे जुबान पर लाना तक नहीं चाहते. वास्तविकता तो यही है कि इस महादेश की भाषाओं के प्रति अगर यहाँ के लोगों का सम्मान-भाव होता तो हम संसार की महा-भाषा-शक्ति होते.
एक-दूसरे के साथ जुड़ने और भावनात्मक साझीदार बनने का भाषा से बड़ा सहारा और कुछ नहीं है. भाषाओँ से ही समाज बनते हैं उसी के विस्तार के साथ समाजों का विस्तार होता है. बिना भाषा के क्या एक जीवित समाज की कल्पना की जा सकती है?
दूसरी ओर यह भी सत्य है कि भाषाओँ का विस्तार समाजों के परस्पर मिलने से होता है, हालाँकि समाजों का विस्तार भी भाषाओँ के परस्पर आदान-प्रदान से ही संभव है. भाषाविहीन समाज एक गूंगा समाज ही तो है और निश्चय ही ऐसे समाज की उम्र बहुत नहीं होती.
छपाई की मशीन के आविष्कार के बाद आदमी दूर-दूर के समाजों के साथ जुड़ा, हालाँकि भाषा पहले भी उसके पास थी और अपने ‘अकेले’ समाजों में उसने बड़ी मात्रा में साहित्य सृजन किया. फिर भी उसकी पहुँच की सीमाएँ तो थी ही; जहाँ तक वह भौतिक रूप में पहुँच सका, या उसका श्रोता पहुँच सका, उसकी बात तथा उसका समाज भी पहुँचा, मगर श्रोता की भाषा के साथ उस तक पहुँचने का असर ही कुछ और होता है. अपने तरीके से यात्री-यायावर और साधु-महात्मा दूसरे समाजों में अनादि काल से मिलते आ रहे हैं, उनकी मिश्रित भाषाएँ निर्मित भी हुईं हैं मगर यह संवाद बहुत-कुछ इकतरफा ही रहा है.
+++++
 भारत का नया हिंदी समाज अनुवाद की ही देन है. वह उन्नीसवीं सदी का भारतीय पुनर्जागरण था, जिसने कमोवेश पूरे संसार को बदला. ‘हिंदी समाज’ नामक अवधारणा तो इससे पूर्व थी भी नहीं. इस सदी ने ज्ञान और तकनीक के अनेक दरवाजे खोले जिनमें छपाई की मशीन और किताब का प्रकाशन इस क्रांति के बड़े औजार थे. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यों तो अनेक जगहों में घूमी मगर चेतना का जो स्वरूप उसने बंगाल के समाज के साथ मिलकर इस देश के लिए तैयार किया, निस्संदेह वही सच्ची वैचारिक क्रांति और भारतीय नव-ज्ञानोदय था. यही कारण है कि उन्नीसवीं सदी के भारतीय ज्ञानोदय और बंगाली समाज को एक-दूसरे का पर्याय कहें तो इसमें जरा भी अतिशयोक्ति नहीं होगी. यही कारण है कि यह बात हैरान करती है कि भारत के सामान्य जन की भाषा (ज्ञान की भाषा भी) हिंदी और अंग्रेजी के स्थान पर बांग्ला क्यों नहीं बन पाई; मगर दूसरी ओर यह जानकर संतोष तो होता है कि बंगाल के बौद्धिक समाज ने एक स्वर में हिंदी को एकमात्र भारतीय संपर्क भाषा बनाने की पैरवी की. यह बंगाली समाज का बड़प्पन था. कमी अगर कहीं थी तो शायद हिंदी समाज की ओर से ही थी क्योंकि उन्होंने हिंदी को राजनीति की भाषा बना दिया.
भारत का नया हिंदी समाज अनुवाद की ही देन है. वह उन्नीसवीं सदी का भारतीय पुनर्जागरण था, जिसने कमोवेश पूरे संसार को बदला. ‘हिंदी समाज’ नामक अवधारणा तो इससे पूर्व थी भी नहीं. इस सदी ने ज्ञान और तकनीक के अनेक दरवाजे खोले जिनमें छपाई की मशीन और किताब का प्रकाशन इस क्रांति के बड़े औजार थे. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यों तो अनेक जगहों में घूमी मगर चेतना का जो स्वरूप उसने बंगाल के समाज के साथ मिलकर इस देश के लिए तैयार किया, निस्संदेह वही सच्ची वैचारिक क्रांति और भारतीय नव-ज्ञानोदय था. यही कारण है कि उन्नीसवीं सदी के भारतीय ज्ञानोदय और बंगाली समाज को एक-दूसरे का पर्याय कहें तो इसमें जरा भी अतिशयोक्ति नहीं होगी. यही कारण है कि यह बात हैरान करती है कि भारत के सामान्य जन की भाषा (ज्ञान की भाषा भी) हिंदी और अंग्रेजी के स्थान पर बांग्ला क्यों नहीं बन पाई; मगर दूसरी ओर यह जानकर संतोष तो होता है कि बंगाल के बौद्धिक समाज ने एक स्वर में हिंदी को एकमात्र भारतीय संपर्क भाषा बनाने की पैरवी की. यह बंगाली समाज का बड़प्पन था. कमी अगर कहीं थी तो शायद हिंदी समाज की ओर से ही थी क्योंकि उन्होंने हिंदी को राजनीति की भाषा बना दिया.
इसलिए यह सहज ही था कि हिंदी समाज के प्रकाशित साहित्य पर सबसे पहला और बड़ा असर बंगाल का ही पड़ा. आधुनिक हिंदी के सबसे पहले प्रयोग भी बंगाल से, और उसके बाद, प्रवासी बंगालियों के पहले-गढ़ काशी और प्रयाग से हुए. बंगाल की तरह हिंदी के सबसे पहले अनुवाद भी अंग्रेजी से, और बाद में बांग्ला से हुए. यह बात इस रूप में भी उल्लेखनीय है कि हिंदी के आरंभिक लेखकों का संकीर्ण राष्ट्रवाद (हिंदी, हिन्दू, हिंदूस्थान-‘ब्राह्मण’–प्रतापनारायण मिश्र) टैगोर और बंकिम के यहाँ ‘मानवतावादी राष्ट्रवाद’ बना. हिंदी समाज तो धर्म और कर्मकांड से जुड़ा समाज था, शायद यही कारण था कि इस समाज ने ज्ञान के साहित्य को धर्म के साथ जोड़ दिया. हिंदी की दुनिया में तो अनुवाद के साहित्य के प्रवेश के बाद ही नया तर्कमूलक समाज पैदा हुआ.
 यद्यपि आज हम अनुवाद की दृष्टि से बहुत समृद्ध हैं, मगर उन दिनों की कल्पना कीजिये जब हिंदी प्रदेशों में लिखित पांडुलिपियों को ‘ईश्वर की किताब’ माना और उन्हें पूजा जाता था. उन दिनों हिंदी समाज के दो ही बड़े नायक थे, राम और कृष्ण, और इनकी छवि हिंदी समाज में धार्मिक नेताओं की थी.
यद्यपि आज हम अनुवाद की दृष्टि से बहुत समृद्ध हैं, मगर उन दिनों की कल्पना कीजिये जब हिंदी प्रदेशों में लिखित पांडुलिपियों को ‘ईश्वर की किताब’ माना और उन्हें पूजा जाता था. उन दिनों हिंदी समाज के दो ही बड़े नायक थे, राम और कृष्ण, और इनकी छवि हिंदी समाज में धार्मिक नेताओं की थी.
आज तो हम सभी यह बात जानते हैं कि हिंदी क्षेत्र के नायकों की छवि को लेकर बड़ा परिवर्तन तब आया जब भारत में पश्चिम से साहित्य की नवीन विधा उपन्यास के रूप में आई. यह विधा पश्चिम से पहले बांग्ला के, फिर अन्य भारतीय भाषाओँ, और फिर हिंदी में आई. जिस दौर में उपन्यास भारत में आया, हिंदी में तिलस्मी और जासूसी उपन्यास खूब लोकप्रिय थे, जिन्हें सिर्फ मनोरंजन के लिए पढ़ा जाता था. ऐसी हालत में पढ़ा-लिखा प्रबुद्ध समाज अपने लिए भी साहित्य के रूप में गंभीर उपन्यास जैसी विधा चाहता था. इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए हिंदी के उपन्यासकार और प्रबुद्ध रचनाकार देशी और विदेशी भाषाओँ से अनुवाद प्रस्तुत करने लगे. जाहिर है कि पहले प्रयास भारतीय भाषाओँ से हुए और सबसे पहले बांग्ला रचनाओं को अनुवाद के लिए चुना गया. इसी कोशिश ने सामाजिक, ऐतिहासिक और पारिवारिक समस्याओं से जुड़े उपन्यासों की रचना का मार्ग प्रशस्त किया. सबसे पहले  बांग्ला से अनूदित उपन्यासों में जो अनुवाद सामने आए, उनमें प्रमुख उपन्यास ये थे : भारतेंदु का ‘राजसिंह’, राधाकृष्ण का ‘स्वर्णलता’, पतिप्राणा अबला का ‘राधारानी’, गदाधर सिंह के ‘दुर्गेश नंदिनी’ और ‘बंगविजेता’; किशोरीलाल गोस्वामी के ‘दीप निर्वाण’ और बिरजा’; बालमुकुंद गुप्त का ‘मडेलभगिनी’ (चार भाग), रामशंकर व्यास के ‘मधुमालती’ और ‘मधुमती’, विजयानंद त्रिपाठी का ‘सच्चा सपना’, राधिकानाथ वंद्योपाध्याय का ‘स्वर्णबाई’, उदितनारायण लाल वर्मा का ‘दीपनिर्वाण’, प्रतापनारायण मिश्र के ‘युगलांगुरीय’ और ‘कपालकुंडला’, अयोध्यासिंह उपाध्याय ‘हरिऔध’ के ‘कृष्णकांत का दानपत्र’ और ‘राधारानी’, कार्तिकप्रसाद खत्री के ‘कुलटा’, ‘मधुमालती’, और ‘दलित कुसुम’ आदि. इन अनेक उपन्यासों के प्रकाशन से स्पष्ट हो जाता है कि बांग्ला उपन्यासों ने हिंदी समाज में आधुनिक चेतना को जगाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इस दौरान इन्हीं जागरूक लेखकों के द्वारा अंग्रेजी के साथ-साथ मराठी और गुजराती उपन्यासों के भी बड़ी मात्रा में अनुवाद किये. जाहिर है कि इन अनुवादों के माध्यम से हिंदी समाज में गंभीर और व्यापक पाठकीय अभिरुचि का जन्म हुआ.
बांग्ला से अनूदित उपन्यासों में जो अनुवाद सामने आए, उनमें प्रमुख उपन्यास ये थे : भारतेंदु का ‘राजसिंह’, राधाकृष्ण का ‘स्वर्णलता’, पतिप्राणा अबला का ‘राधारानी’, गदाधर सिंह के ‘दुर्गेश नंदिनी’ और ‘बंगविजेता’; किशोरीलाल गोस्वामी के ‘दीप निर्वाण’ और बिरजा’; बालमुकुंद गुप्त का ‘मडेलभगिनी’ (चार भाग), रामशंकर व्यास के ‘मधुमालती’ और ‘मधुमती’, विजयानंद त्रिपाठी का ‘सच्चा सपना’, राधिकानाथ वंद्योपाध्याय का ‘स्वर्णबाई’, उदितनारायण लाल वर्मा का ‘दीपनिर्वाण’, प्रतापनारायण मिश्र के ‘युगलांगुरीय’ और ‘कपालकुंडला’, अयोध्यासिंह उपाध्याय ‘हरिऔध’ के ‘कृष्णकांत का दानपत्र’ और ‘राधारानी’, कार्तिकप्रसाद खत्री के ‘कुलटा’, ‘मधुमालती’, और ‘दलित कुसुम’ आदि. इन अनेक उपन्यासों के प्रकाशन से स्पष्ट हो जाता है कि बांग्ला उपन्यासों ने हिंदी समाज में आधुनिक चेतना को जगाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इस दौरान इन्हीं जागरूक लेखकों के द्वारा अंग्रेजी के साथ-साथ मराठी और गुजराती उपन्यासों के भी बड़ी मात्रा में अनुवाद किये. जाहिर है कि इन अनुवादों के माध्यम से हिंदी समाज में गंभीर और व्यापक पाठकीय अभिरुचि का जन्म हुआ.
अनुवादों के द्वारा सामाजिक तथा सांस्कृतिक अभिरुचि पैदा करने की दिशा में बीसवीं सदी का बहुत बड़ा योगदान रहा. यह दौर आजादी की लड़ाई का था, जब अधिकांश पुरुष वर्ग आजादी की चेतना जगाने में सक्रिय था. स्त्रियाँ अपने ढंग से इस काम में हाथ बंटा रही थी, और इस चेतना को लेकर भारत में अनेक उपन्यास और कहानियाँ लिखी जा रही थीं. बंगाली समाज का प्रबुद्ध वर्ग दोनों स्तरों पर कार्यरत था – सांस्कृतिक जागृति के कामों में सीधे हिस्सा लेकर तथा इस जागृति को अपने लेखन में उतारकर. इसी दौर में बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय जैसी असाधारण प्रतिभा का उदय हुआ, जिनका ‘वन्दे मातरम्’ भारतीय राष्ट्रवादी चेतना का निर्विवाद स्वर बना. उसके कुछ ही समय बाद कालजयी रचनाकार रवीन्द्रनाथ टैगौर और शरतचंद्र चट्टोपाध्याय का उदय हुआ जो अपने अनुवादों के माध्यम से समूचे देश की आवाज बने. शरत तो हिंदी समाज में इतने लोकप्रिय हुए और स्त्री समाज में पाठकीय अभिरुचि जगाने में उनका इतना बड़ा योगदान है कि यह काम हिंदी के लेखक अपने समाज में कभी नहीं कर पाए. रवीन्द्र के कालजयी चरित्र गोरा, काबुलीवाला और शरत के उपन्यासों की नायिकाएं पुनर्जागरणकालीन भारतीय समाज की केन्द्रीय संवेदना के साक्षात् प्रतीक बन गए. बाद की पीढ़ियों में भी बांग्ला उपन्यासकारों, विशेष रूप से शंकर, विभूतिभूषण वंद्योपाध्याय, विमल मित्र, ताराशंकर आदि की हिंदी समाज में लोकप्रियता किसी भी लेखक-समाज के लिए ईर्ष्या का विषय हो सकती है.
अंग्रेजी के समृद्ध साहित्य के अनुवाद ने तो हिंदी समाज को ही नहीं, समूचे भारतीय लेखन को प्रभावित और विकसित किया. इस दौर में अंग्रेजी के माध्यम से, और कहीं-कहीं सीधे अनुवाद के माध्यम से संसार भर की भाषाओँ का हिंदी में अनुवाद हुआ जो खूब लोकप्रिय हुआ. हिंदी समाज में अन्तरंग पाठकीय अभिरुचि उत्पन्न करने में इन अनुवादों ने जो भूमिका निभाई, उसे अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है.
उर्दू के साथ हिंदी का जो सम्बन्ध है उसके आधार पर जन सामान्य के मन में भी इनकी छवि दो भाषाओँ की नहीं है. अनेक बार लिपि परिवर्तन के साथ इन्हें एक ही भाषा के रूप में पढ़ा जा सकता है और कई बार दूसरी भारतीय भाषाओँ के रचनाकार भी इतने अधिक हिंदी में पढ़े जाते हैं कि वे हिंदी के ही लगते हैं. कहने की आवश्यकता नहीं है कि आज भी कई लोग अमृता प्रीतम और कृष्ण चंदर-जैसे कितने ही कथाकारों को हिंदी का ही लेखक समझते हैं. ऐसे और भी अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने हिंदी की पाठकीय अभिरुचि उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
आजादी के बाद तो एक प्रकार से अनुवाद ने हिंदी पाठकों में एक क्रांति ही ला दी. स्वतंत्र भारत का हर प्रबुद्ध पाठक हिंदी की अपेक्षा अंग्रेजी में अधिक सिद्धहस्त था, इसलिए उसका परिचय संसार भर के साहित्य के साथ हुआ, यह बात अलग है कि इस क्रम में हिंदी का लेखन हाशिए में जाता दिखाई दिया. इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, यह बता पाना तो कठिन है, तथापि हिंदी लेखन को लेकर सवाल तो उठाये ही जाते रहे हैं. सवाल उठता रहा कि हिंदी लेखक अपने मौलिक लेखन के द्वारा अपने पाठक-प्रशंसक क्यों नहीं जुटा सके.
 इसी बीच हिंदी क्षेत्र में एक ऐसा लेखक मुख्यधारा में आया जिसकी प्रथम भाषा अंग्रेजी थी. ऐसे लेखकों के बीच से ही एक ओर भारतीय अंग्रेजी लेखन का उदय हुआ और दूसरी ओर अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषाओँ का प्रभाव ग्रहण कर हिंदी में लिखा जाने लगा. इस प्रवृत्ति का एक अच्छा परिणाम यह सामने आया कि हिंदी में विविधता भरा साहित्य और नवीन साहित्यिक विधाओं का जन्म हुआ, मगर एक सीमा यह सामने आई कि लेखक अपनी जड़ों से कटता चला गया. नई सदी के उदय के साथ नए इलेक्ट्रोनिक माध्यमों ने पाठक की पहचान बदली और किताब हाशिए में जाती दिखाई दी. ई-पुस्तक प्रकाश में आई, जिसने पाठक और किताब के परंपरागत रिश्तों को एकदम बदल डाला. हालाँकि पाठक की अभिरुचि पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा फिर भी भाषाओँ, सामाजिक पृष्ठभूमि, अभिरुचि तथा ज्ञान से जुड़ी वरीयताओं को लेकर सवाल उठने लगे. बार-बार यह बहस उठने लगी कि क्या किताब का परंपरागत पाठक अब अतीत की वस्तु रह जाएगा?
इसी बीच हिंदी क्षेत्र में एक ऐसा लेखक मुख्यधारा में आया जिसकी प्रथम भाषा अंग्रेजी थी. ऐसे लेखकों के बीच से ही एक ओर भारतीय अंग्रेजी लेखन का उदय हुआ और दूसरी ओर अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषाओँ का प्रभाव ग्रहण कर हिंदी में लिखा जाने लगा. इस प्रवृत्ति का एक अच्छा परिणाम यह सामने आया कि हिंदी में विविधता भरा साहित्य और नवीन साहित्यिक विधाओं का जन्म हुआ, मगर एक सीमा यह सामने आई कि लेखक अपनी जड़ों से कटता चला गया. नई सदी के उदय के साथ नए इलेक्ट्रोनिक माध्यमों ने पाठक की पहचान बदली और किताब हाशिए में जाती दिखाई दी. ई-पुस्तक प्रकाश में आई, जिसने पाठक और किताब के परंपरागत रिश्तों को एकदम बदल डाला. हालाँकि पाठक की अभिरुचि पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा फिर भी भाषाओँ, सामाजिक पृष्ठभूमि, अभिरुचि तथा ज्ञान से जुड़ी वरीयताओं को लेकर सवाल उठने लगे. बार-बार यह बहस उठने लगी कि क्या किताब का परंपरागत पाठक अब अतीत की वस्तु रह जाएगा?
निश्चय ही पाठक और अनुवाद को लेकर जो पुरानी धारणा समाज में मौजूद थी, आजादी के बाद विकसित हुए समाज ने साहित्य को लेकर उनकी आस्था को खंडित किया और वह खुद को ऐसे दुराहे पर ला खड़ा अनुभव करने लगा, जहाँ उसकी समझ में नहीं आ पा रहा था कि वो इन दोनों में से किसी एक रास्ते को अपनाये भी या नहीं. वह जानता था कि यह रास्ता उसे भटकाएगा नहीं लेकिन यह भरोसा मन में नहीं था कि वो मंजिल तक पहुँच भी पायेगा. इस सब के बावजूद इस प्रक्रिया में उसके पास जो संभावनाएं थीं, उसे भरोसा था कि वे उसे भटकायेंगी नहीं. तो भी यह भ्रम तो बना ही रहा कि वह अपनी जड़ों से कटता चला जा रहा है.
भारत के जैसे अर्धविकसित समाज में अनुवाद के द्वारा घुसपैठ किये जाने के बाद दोनों तरह के खतरों की संभावना हो सकती है. अनुवाद का समाज एक पराया समाज होता है, जहाँ अर्थ और आशय के बीच हमेशा दुविधा और संशय पसरा रहता है. कलाएँ अंततः अर्थ और आशय के बीच कलात्मक समन्वय पैदा करने का काम करती हैं.
 ऐसे में लेखक और लेखन की जड़ें पाठक की मदद करती हैं. शब्द का अनुवाद तो हो सकता है, मगर आशय का अनुवाद कैसे हो? यही कारण है कि रचनात्मक लेखन के सन्दर्भ में अनुवादक की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है.
ऐसे में लेखक और लेखन की जड़ें पाठक की मदद करती हैं. शब्द का अनुवाद तो हो सकता है, मगर आशय का अनुवाद कैसे हो? यही कारण है कि रचनात्मक लेखन के सन्दर्भ में अनुवादक की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है.
देखा जाये तो मनुष्य सभ्यता के विकास के मूल में पहली चीज अनुवाद ही है. सभ्यता के विकास और विस्तार के साथ ही मनुष्य के सामने नई चुनौतियाँ बढ़ी हैं, इन चुनौतियों का सावधानी से सामना कर पाना ही अभिव्यक्ति की सफलता है. सामान्य रूप से भावनाओं को यथावत व्यक्त करने के लिए मनुष्य के पास अनेक संकेत-माध्यम हैं, जिनके द्वारा वह जैसे-तैसे अपनी बात को संप्रेषित कर ही देता है. मगर साहित्य के पास सिर्फ शब्द हैं और उसका अर्थ.
मनुष्य सभ्यता के विकास के साथ साहित्य के अनेक अनुशासनों (विधाओं) का जन्म हुआ है और ये विधाएँ एक तरह से अनुवाद की मदद करती हैं. इसीलिए एक अनुवादक से यह अपेक्षा रहती है कि वह रचनाकार के भावबोध के साथ-साथ भावक की संवेदना को भी गहराई से महसूस करता हो. ज्यों-ज्यों हमारी संस्कृति विकसित होती जाएगी, इसीलिए अनुवाद की चुनौती भी बढ़ती चली जाएगी. चूंकि मनुष्य समाज की अभिव्यक्ति से जुड़ी यह पहली वरीयता है इसलिए इसका रास्ता भी मनुष्य अंततः खोज ही लेगा.
(जारी)
पिछली क़िस्त का लिंक: इतने विशाल हिंदी समाज में सिर्फ डेढ़ यार : आठवीं क़िस्त

फ़ोटो: मृगेश पाण्डे
लक्ष्मण सिह बिष्ट ‘बटरोही‘ हिन्दी के जाने-माने उपन्यासकार-कहानीकार हैं. कुमाऊँ विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग के अध्यक्ष रह चुके बटरोही रामगढ़ स्थित महादेवी वर्मा सृजन पीठ के संस्थापक और भूतपूर्व निदेशक हैं. उनकी मुख्य कृतियों में ‘थोकदार किसी की नहीं सुनता’ ‘सड़क का भूगोल, ‘अनाथ मुहल्ले के ठुल दा’ और ‘महर ठाकुरों का गांव’ शामिल हैं. काफल ट्री के लिए नियमित लेखन करेंगे.
काफल ट्री वाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिये यहाँ क्लिक करें: वाट्सएप काफल ट्री
काफल ट्री की आर्थिक सहायता के लिये यहाँ क्लिक करें




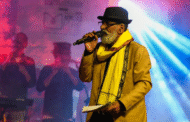

































1 Comments
Anonymous
बटरोही जी की नौवीं किस्त में बंग्ला के राजभाषा न बनने के विषय में उल्लेख किया गया है। मैंने निराला जी का लेख कहीं पढ़ा था जिसमें कहा गया है कि,” बंग्ला के लिए बहुत प्रयत्न किये गये थे।” इस सम्बंध में निराला जी नेहरु जी से मिले भी थे। निराला जी बंग्ला भी अच्छी तरह जानते थे। शायद उनकी किताब “परिमल” में इसका उल्लेख है। हिन्दी किसी क्षेत्र विशेष की भाषा नहीं होते हुए भी, उसे क्षेत्र विशेष की भाषा मानकर राजनीति की जाती है।
महेश रौतेला,
[email protected]