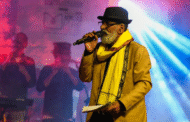असंख्य पाठ्यपुस्तकों के बीच अदृश्य हिंदी पाठक
अगर आप देश-विदेशों में हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या पर जायेंगे तो जरूर चकरा जायेंगे. बीते कुछ सालों से हिंदी पढ़ने का फैशन कम होता जा रहा है, फिर भी कई कारणों से हिंदी पढ़ना-पढ़ाना आज भी मजबूरी है. हमारे छुटपन के ज़माने तक कबीर, रहीम आदि के नीतिपरक दोहे बच्चों को रटाये जाते थे, उसी तरह जैसे पहाड़े और बाराखड़ी. अब तो बच्चों के लिए ये अजनवी चीजें हो गयी है. बहुत वक़्त नहीं बीता है, जब भाषा और साहित्य का पठन-पाठन भी अतीत की चीज बनता जा रहा है. भारत की प्रांतीय भाषाएँ इस मार को बहुत पहले झेल चुकी हैं, हिंदी इसे हाल के वर्षों में बेरहमी से झेल रही है.
 पाठ्य-पुस्तकें अब पहले की तरह मूल किताबों के रूप में नहीं पढ़ी जातीं, अलबत्ता छोटी कक्षाओं में उनकी ‘वर्क-बुक’ और बड़ी कक्षाओं में कुंजियाँ इस कदर फ़ैल गयी हैं कि हिंदी का अठानवे प्रतिशत छात्र आज अपनी मूल किताबों के नाम तक नहीं जानता, उनके लेखकों के बारे में जानना तो दूर की कौड़ी है. यह हालत कमोवेश प्रत्येक विषय की पाठ्य-पुस्तकों के बारे में कही जा सकती है, हिंदी में हालत ज्यादा ही दयनीय है. न सही दयनीय, उपहासास्पद-जैसी तो हो ही गयी है.
पाठ्य-पुस्तकें अब पहले की तरह मूल किताबों के रूप में नहीं पढ़ी जातीं, अलबत्ता छोटी कक्षाओं में उनकी ‘वर्क-बुक’ और बड़ी कक्षाओं में कुंजियाँ इस कदर फ़ैल गयी हैं कि हिंदी का अठानवे प्रतिशत छात्र आज अपनी मूल किताबों के नाम तक नहीं जानता, उनके लेखकों के बारे में जानना तो दूर की कौड़ी है. यह हालत कमोवेश प्रत्येक विषय की पाठ्य-पुस्तकों के बारे में कही जा सकती है, हिंदी में हालत ज्यादा ही दयनीय है. न सही दयनीय, उपहासास्पद-जैसी तो हो ही गयी है.
बहुत दूर न जाकर अपनी जिंदगी के अनुभवों के आधार पर बातें करूँ तो लगता है, सारी जिन्दगी ऐसी भाषा और पाठ्यक्रम के पीछे भागता रहा जिसे न तो मैं अपनी जरूरत बना सका और न अपनी भाषा को अपने समाज के लिए रोल मॉडल बना सका. इस प्रक्रिया में खुद से लगातार सवाल पूछता रहा कि साहित्य के अंतर्गत जो सामग्री विद्यार्थी पढ़ता था, उसका मेरे विद्यार्थियों की जिंदगी के साथ क्या सम्बन्ध है?
पिछले पचास सालों में मैं जो पढ़ाता रहा, उसकी एक बानगी देखिये. (हमारे देश में पाठ्यक्रम-रचना का अधिकार अध्यापक को नहीं है, उसे तैयार-शुदा सामग्री दी जाती है जिसे उसे अपनी अगली पीढ़ी तक उसी रूप में पहुँचाना होता है!)
कॉलेज की पृष्ठभूमि (जिसे इंटरमीडिएट कहा जाता है) के रूप में हिंदी भाषा और साहित्य को अनेक स्तरों पर बांटा गया है: इसमें भाषा की निम्नलिखित छवियाँ शामिल हैं –
राजभाषा, राष्ट्रभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, कृत्रिम भाषा, कूट भाषा, व्यावसायिक भाषा, अपभाषा, बोली, भाषा की स्वायत्तता, ऐतिहासिकता, जीवन्तता, मानकीकरण और फिर संसार की भाषाओँ के साथ हिंदी का सम्बन्ध.
हिंदी क्षेत्र, हिंदी की बोलियाँ, हिंदी की शैलियाँ; हिंदी, उर्दू, हिन्दुस्तानी, कामकाजी हिंदी, मानक हिंदी; हिंदी उच्चारण, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण, उच्चारण विषयक अशुद्धियाँ, वर्तनी, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, वर्तनी की अशुद्धियाँ, वर्तनी-विश्लेषण.
हिंदी शब्दसमूह, पर्यायवाची, समानाभास या समध्वनीय भिन्नार्थक शब्द, विलोम, अनेकार्थी, ऊनार्थक, समूहवाची, ध्वन्यात्मक या अनुकरणमूलक, शब्दों का वर्गीकरण.
संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाच्य-परिवर्तन, क्रियापद व्याख्या, अविकारी शब्द, क्रिया-विशेषण, सम्बन्ध सूचक, विस्मयबोधक, अव्ययों के प्रयोग.
वाक्य, भाषा प्रयोग, विरामचिह्न, अशुद्धियाँ और उनका शोधन.
भाषा-पाठ्यक्रम का एक दूसरा हिस्सा भी है जिसमें पत्रलेखन, टिप्पणी लेखन, सरकारी व गैर सरकारी पत्र, संक्षेपण, विस्तारण, अपठित, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद, मुहावरे और कहावतें, निविदा-विज्ञापन सूचनाएँ, पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक शब्दावली, मानविकी शब्दावली, वैज्ञानिक शब्दावली और भाषा वैज्ञानिक शब्दावली.
हिंदी पाठ्यक्रम का दूसरा भाग है साहित्य; जिसके अंतर्गत हिंदी साहित्य का काल-विभाजन और विभिन्न कालों की प्रवृत्तियां, रचनाकार और उनकी कृतियों का अध्ययन शामिल है. ज्यों-ज्यों कक्षाएं बढ़ती जाती हैं, पाठ्यक्रम में रचनाकारों और साहित्यिक विधाओं का विस्तार होता जाता है.
इस विवरण को प्रस्तुत करने के पीछे मेरा आशय हिंदी की कक्षाएं लेना नहीं, इस विडंबना की जानकारी देना है कि साहित्य की जिस जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए मुझे हमेशा पहली रात को तैयारी करनी पड़ती थी, आज के विद्यार्थी न जाने किस जादू से इन प्रश्नपत्रों में अस्सी-नब्बे प्रतिशत अंक ले आ रहे हैं. इसके दो ही संकेत हैं; या तो हमारे विद्यार्थी-काल में बच्चों का मानसिक स्तर घटिया होता था, या आज एकाएक हिंदी के प्रबुद्ध बच्चों की नस्ल पैदा होने लगी है. यह भी संभव है कि आज मूल्यांकन पद्धति ही पूरी तरह बदल चुकी है.
आश्चर्य तब और अधिक होता है, जब हम देखते है कि जो पब्लिक स्कूली बच्चे व्यावहारिक जीवन में हिंदी ठीक-से बोल या लिख नहीं पाते, परीक्षा कक्ष में आते ही फर्राटे की हिंदी लिख-पढ़ लेते हैं. इसका प्रमाण यह है कि लिखित-मौखिक परीक्षा में वही बच्चे अस्सी प्रतिशत से अधिक अंक ले आते हैं. हमारे समय में तो हिंदी में इतने अंक प्राप्त कर सकने की कल्पना तक नहीं की जा सकती थी.
+++++
 अब जरा स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों के बारे में सुनिए. पचास-साठ के दशक में, जब हम विद्यार्थी थे, बीए के दो वर्षों में हिंदी साहित्य के चारों कालखंडों में से दो महाकाव्य, दो खंड काव्य, लगभग दर्जन भर कवि और कहानीकार, दो उपन्यास, दो नाटक, आठ-दस एकांकी और गद्य की नवीन विधाओं से जुड़ी अनेक रचनाएं पढ़ते हैं. ये सभी रचनाएँ कुछ विस्तार और बढ़े हुए स्तर के साथ एमए में पढ़ाई जाती थीं और आज भी पाठ्यपुस्तकों के फेरबदल के साथ आज भी लागू हैं.
अब जरा स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों के बारे में सुनिए. पचास-साठ के दशक में, जब हम विद्यार्थी थे, बीए के दो वर्षों में हिंदी साहित्य के चारों कालखंडों में से दो महाकाव्य, दो खंड काव्य, लगभग दर्जन भर कवि और कहानीकार, दो उपन्यास, दो नाटक, आठ-दस एकांकी और गद्य की नवीन विधाओं से जुड़ी अनेक रचनाएं पढ़ते हैं. ये सभी रचनाएँ कुछ विस्तार और बढ़े हुए स्तर के साथ एमए में पढ़ाई जाती थीं और आज भी पाठ्यपुस्तकों के फेरबदल के साथ आज भी लागू हैं.
यह तिलिस्म भी मेरी समझ से बाहर है कि 1951 में आरम्भ हुए हमारे विभाग में एमए का पहला प्रथम श्रेणी विद्यार्थी 1966 में आया था, वह भी कुल 60.75% अंकों के साथ. आज केवल इसी कालेज में नहीं, दूर-दराज के कस्बों-गाँवों में हाल के वर्षों में खुले विभाग में एक से अधिक, कहीं-कहीं आठ-दस प्रथम श्रेणी विद्यार्थी तक सुनाई देते हैं. इसके पीछे विद्यार्थियों की प्रतिभा का विस्फोट है या कोई शार्टकट, कहा नहीं जा सकता. मैं नई पीढ़ी की प्रतिभा पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा, अपने इस अनुभव के आधार पर बात कर रहा हूँ कि मौखिक परीक्षा के वक़्त जब ऐसे विद्यार्थियों से एकदम मामूली सवाल पूछे जाते हैं तो कई विद्यार्थियों का कहना होता है कि इन्हें फलां उपन्यास/कहानी संग्रह या नाटक/एकांकी संग्रह बहुत खोजने पर भी कहीं नहीं मिला, बड़े विश्वास के साथ वो बताते हैं कि उस किताब की उन्होंने आज तक शक्ल भी नहीं देखी है, तब फिर आप लोग कहाँ से पढ़ते हैं, इसके जवाब में उनका कहना होता है कि बाजार में रेडीमेड गाइड खूब मिल जाते हैं. उनकी सारी तैयारी उन्हीं किताबों से होती है.
मुझे याद है, सत्तर-अस्सी के दशक तक भी कई विद्यार्थी, जिन्हें मूल पुस्तक उपलब्ध नहीं हो पाती थी, कभी जरूरत के कारण या कभी शौक के कारण आसपास के बड़े शहरों या नामी विश्वविद्यालयों के हिंदी विभाग का चक्कर लगाते थे और जिन प्राध्यापकों की उन्होंने चर्चा सुनी होती थी, उनकी कक्षाओं में शामिल हो आते थे. आज ऐसा कुछ नहीं होता, हालाँकि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि आज भी अपवाद स्वरुप ऐसे विद्यार्थी मौजूद होंगे. दूसरी ओर, जो उत्तर पुस्तिकाएं हमें देखने को मिलती हैं, उनमें से अगर दो-चार प्रतिशत को छोड़ दिया जाये तो किसी में भी ऐसा नहीं लगता कि किताबें मूल रूप में पढ़ी गयी हैं; यहाँ तक कि बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को लेखक का नाम भी नहीं मालूम होता. (ऐसे भी छात्र मिलते हैं जो लेखक का नाम पूछने पर गाइड-लेखक का नाम बता देते हैं.)
हालाँकि हिंदी साहित्य की पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित आलोचना और पाठ्यपुस्तकीय समीक्षा-आलोचना में फर्क होना स्वाभाविक है, अंततः बीस-बाईस साल के विद्यार्थी और पेशेवर लेखक में फर्क तो होगा ही; मगर जितने विश्वास के साथ आज का अधिकांश विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में उल्टा-सीधा जवाब लिख देता है उसे देखकर कभी-कभी तो यही लगता है कि अपने पाठ्यक्रम को आज का छात्र कितने गैर-जिम्मेदाराना अंदाज में ले रहा है. और यह बात सिर्फ एक कॉलेज या विश्वविद्यालय की नहीं है, कमोबेश सभी जगहों का यही हाल है.
 यह सब लिखने का आशय यह भी नहीं है कि हिंदी पाठ्यक्रम-संसार में सब जगह धांधली हो रही है. पिछले अनेक वर्षों में भारतीय और प्रादेशिक प्रशासनिक सेवाओं की हिंदी की कापियां जांचने का मुझे मौका मिला; निश्चय ही कई ऐसे उत्तर देखने को मिले जिनसे परीक्षकों को भी नई दृष्टि मिलती है, मगर ऐसी कापियां वहां भी उँगलियों पर गिनी जा सकती हैं. परीक्षा की कापियों को देखते हुए, यों भी, कोई परीक्षक उसका साहित्यिक मूल्यांकन नहीं कर रहा होता; इसे वह समझ रहा होता है कि विद्यार्थी के उत्तर में अगर कुछ भी अंतर्दृष्टि और परिश्रम दिखाई देता है तो हर जागरूक परीक्षक उससे प्रभावित होता है और अच्छे अंक देता है. परीक्षक यह जानता है कि एक विद्यार्थी, वह कितना भी परिपक्व दृष्टि का क्यों न हो, त्रुटिहीन नहीं हो सकता. और साहित्यिक कृतियों का मूल्यांकन तो विविधतापूर्ण होगा ही, वह विज्ञान या समाज- विज्ञानों की तरह सर्वथा सहमतिमूलक हो ही नहीं सकता, अगर कहीं ऐसा है भी तो ऐसा शायद ही कोई परीक्षक होगा जो उसे 98-99% अंक दे देगा (जैसा कि इन दिनों दसवीं-बारहवीं की परीक्षाओं या कभी-कभी डिग्री कक्षाओं में भी) देखने को मिलता है.
यह सब लिखने का आशय यह भी नहीं है कि हिंदी पाठ्यक्रम-संसार में सब जगह धांधली हो रही है. पिछले अनेक वर्षों में भारतीय और प्रादेशिक प्रशासनिक सेवाओं की हिंदी की कापियां जांचने का मुझे मौका मिला; निश्चय ही कई ऐसे उत्तर देखने को मिले जिनसे परीक्षकों को भी नई दृष्टि मिलती है, मगर ऐसी कापियां वहां भी उँगलियों पर गिनी जा सकती हैं. परीक्षा की कापियों को देखते हुए, यों भी, कोई परीक्षक उसका साहित्यिक मूल्यांकन नहीं कर रहा होता; इसे वह समझ रहा होता है कि विद्यार्थी के उत्तर में अगर कुछ भी अंतर्दृष्टि और परिश्रम दिखाई देता है तो हर जागरूक परीक्षक उससे प्रभावित होता है और अच्छे अंक देता है. परीक्षक यह जानता है कि एक विद्यार्थी, वह कितना भी परिपक्व दृष्टि का क्यों न हो, त्रुटिहीन नहीं हो सकता. और साहित्यिक कृतियों का मूल्यांकन तो विविधतापूर्ण होगा ही, वह विज्ञान या समाज- विज्ञानों की तरह सर्वथा सहमतिमूलक हो ही नहीं सकता, अगर कहीं ऐसा है भी तो ऐसा शायद ही कोई परीक्षक होगा जो उसे 98-99% अंक दे देगा (जैसा कि इन दिनों दसवीं-बारहवीं की परीक्षाओं या कभी-कभी डिग्री कक्षाओं में भी) देखने को मिलता है.
व्यावहारिक जीवन में हम एक सामान्य हिंदी पाठक की जो छवि देखते हैं, वह कुछ अपवादों को छोड़कर बहुत निराशाजनक देखने को मिलती है. सवाल यह है कि इस स्थिति के लिए किसे दोषी ठहराया जाये?
कुछ वर्षों से स्कूलों और महाविद्यालयों में छात्रों की मदद के लिए पाठ्यपुस्तकों के बुक-बैंकों की स्थापना की गई है. इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम में शामिल उपन्यासों, महाकाव्यों, नाटकों, खंडकाव्यों, कहानी-कविता संग्रहों को बहुत बड़ी संख्या में खरीदा जाता है ताकि जरूरतमंद विद्यार्थी मूल पुस्तकों को पढ़ सके.. इसके बावजूद हाल के वर्षों में देखने को मिला कि जो विद्यार्थी यह शिकायत करते थे कि उन्हें पाठ्यपुस्तक उपलब्ध ही नहीं है, ऐसे लोगों ने ही बुक-बैंक पुस्तकालय से एक भी किताब अपने नाम इशू नहीं कराई. देखा गया कि उन्होंने बाजार से कुंजी या ‘गाइड’ खरीदकर पढ़ा और मजेदार बात कि प्रथम या अच्छी द्वितीय श्रेणी के अंक प्राप्त किये. इसी मनोवृत्ति की अगली कड़ी यह थी कि कई जगह, जहाँ ऐसे विद्यार्थियों का दबदबा है, वहाँ ‘बुक-बैंकों’ में कुंजियाँ और ‘गाइड’ ख़रीदे जाने लगे हैं. पहले अपवाद स्वरुप ऐसे विद्यार्थी होते थे, अब तो यह संख्या लगातार बढ़ रही है. छात्र यूनियनें भी ऐसी किताबों को पुस्तकालय में खरीदने का दबाव बनती हैं.
अपने अध्यापन से जुड़े पचास सालों के बाद इस तरह की शिकायत का ढोल पीटना किसी को भी नागवार गुजार सकता है. कहा जा सकता है कि इस ओर मैंने अपने अधिकारियों और व्यवस्था का ध्यान क्यों आकर्षित नहीं किया? इसे अपना स्पष्टीकरण तो नहीं कहूँगा, अपने ही जीवन से जुड़ी एक घटना का यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ.
सत्तर के दशक की घटना है, मुझे अपने ही विश्वविद्यालय की बीए हिंदी भाषा की कापियाँ मूल्यांकन के लिए दी गयी थी. मैं नया-नया अध्यापक बना था और बड़े उत्साह और बारीकी के साथ मैंने मूल्यांकन किया. अधिकांश विद्यार्थी फेल हो गए थे. यह कोई खास बात नहीं थी; मगर कुछ ही दिनों के बाद मेरे पास विश्वविद्यालय का पात्र आया कि मैं कुलपति से मिलूँ. कुलपति कार्यालय में पहुँचा ती मेरे विभागाध्यक्ष वहाँ पहले से मौजूद थे. उनके आगे कापियों का एक पुलिंदा था. बैठ चुकने के बाद मैंने देखा कि कुलपति के सामने मेरे द्वारा जांची गयी कापियां थी. कुलपति मेरे प्रशंसक थे, इसलिए मेरे दिमाग में यह बात नहीं आई कि सारा प्रकरण मेरे बारे में की गयी शिकायत को लेकर है.
मुझे लेकर जो शिकायत की गई थी, उसका सार यह था कि जिस केंद्र के विद्यार्थियों को मैंने दस से बीस प्रतिशत के बीच अंक दिए हैं, उसी केंद्र के विद्यार्थियों को मेरे विभागाध्यक्ष ने अस्सी से नब्बे प्रतिशत तक अंक दिए थे. कुलपति की समझ में भी यह बात नहीं आई थी इसलिए उन्होंने हम दोनों को आमने-सामने बुलाकर समस्या को समझना चाहा था. मैंने अपना पक्ष रखा और बुजुर्ग विभागाध्यक्ष ने अपना. विभागाध्यक्ष एक चोट खाए बुजुर्गवार थे जो हर बात पर न्यायालय की शरण में जाने की बात करते थे. वे किसी को भी फेल करने के खिलाफ थे, और जब तक कि कॉपी एकदम ब्लेंक न हो, उनका कहना था कि किसी न किसी तरीके से उसे पास कर देना चाहिए. इसका एक कारण तो यह था कि विद्यार्थियों के एक निश्चित प्रतिशत से कम पास होने पर सम्बंधित अध्यापक की वेतनवृद्धि रोक दी जाती थी, वैसे भी पास प्रतिशत अगर तैतीस है तो अठाईस से तीस प्रतिशत अंक लाने वाले को खींच-तान पर पास कर देना चाहिए.
 भौतिक विज्ञान के प्राध्यापक रहे कुलपति के सामने मैंने अपना पक्ष रखा; वो मुझसे सहमत थे, मगर अध्यक्ष जी किसी भी हालत में समझौते के लिए तैयार नहीं हुए.
भौतिक विज्ञान के प्राध्यापक रहे कुलपति के सामने मैंने अपना पक्ष रखा; वो मुझसे सहमत थे, मगर अध्यक्ष जी किसी भी हालत में समझौते के लिए तैयार नहीं हुए.
हुआ यह था कि भाषा का परचा होने के कारण मैंने शब्दावली और वर्तनी की अशुद्धियों पर नंबर काटे थे. उदाहरण के लिए पर्यायवाची शब्दों में अगर पांच शब्द पूछे गए थे, तो दो या तीन शब्द लिखने वाले छात्र को मैंने शून्य दिया था जब कि अध्यक्ष जी ने दो शब्द लिखने पर भी उसे 2/5 अंक दिए. इसी प्रकार ‘अंधकार’ के विलोम ‘प्रकाश’ को ‘परकास’ लिखने पर मैंने शून्य दिया था, जबकि उन्होंने पूरे अंक दिए थे. उनका कहना था कि छात्र अर्थ जानता था, जरा-सी कलम की असावधानी पर क्या उसे आपको क़त्ल कर देना चाहिए? उनके अनुसार एक अध्यापक को इतना निर्मम नहीं होना चाहिए. बात-बात में वो धमकी देते कि लड़का अगर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा तो पक्का जीत जाएगा और आपको हर्जाना देना पड़ेगा सो अलग; यूनिवर्सिटी की बदनामी तो होगी ही.
कुलपति मेरे तर्कों से सहमत तो थे, इसके बावजूद उनका कहना था कि विद्यार्थी का मूल्यांकन एक साहित्यकार की तरह नहीं किया जाना चाहिए. आखिर हमारा बच्चा ही है, उसे हम सहारा नहीं देंगे तो भला और कौन देगा!
+++++
हिंदी इस महादेश की एकमात्र संपर्क भाषा है. दुर्भाग्य से इसकी ताकत को इसी के शुद्धतावादियों ने कैद कर रखा है और वही इसके फलने-फूलने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बने हुए हैं. हिंदी की स्थति टैगोर की किशोर नायिकाओं की तरह है जो अपने किशोरपन को भरपूर जीना चाहती है, भरपूर शरारत करना चाहती है और पूरे देश की युवा धड़कन बनना चाहती है, मगर उसी के परिवार के सयाने लोग उसके अल्हड किशोरपन को नष्ट करने पर तुले हुए हैं. हिंदी इस रूप में भी चिर-किशोरी है कि वह हर समाज, हर भाषा-भाषी और हर उम्र के लोगों के साथ चुटकी में घुलमिल जाती है. इसके बावजूद वह अपनी अल्हड़ता बचाए रखती है. आज भी वह उसी रूप में जिन्दा है और अपना अस्तित्व बनाए हुए है. उसे आज भी अपने ठेट रूप में पहचाना जा सकता है, सिर्फ उसे पंडिताऊ कैदखाने से दूर रखने की जरूरत है. अपने लाल बुझक्कड़ों से बचाए रखना है.
हर समाज में ज्ञान की भाषा और बोलचाल की भाषा को अलग-अलग करके देखा जाता है और आदर्श भाषा वही होती है जिसमें इन दोनों भाषाओँ का समन्वय होता है. जिस दिन हिंदी अपने वर्तमान रूप में ज्ञान की भाषा बन जाएगी, संसार भर में फैलने में उसे कोई नहीं रोक सकता. रोड़ा कोई बनेगा तो हमारा ही शुद्धतावादी.
(जारी)
पिछली क़िस्त का लिंक: इतने विशाल हिंदी समाज में सिर्फ डेढ़ यार : सातवीं क़िस्त

फ़ोटो: मृगेश पाण्डे
लक्ष्मण सिह बिष्ट ‘बटरोही‘ हिन्दी के जाने-माने उपन्यासकार-कहानीकार हैं. कुमाऊँ विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग के अध्यक्ष रह चुके बटरोही रामगढ़ स्थित महादेवी वर्मा सृजन पीठ के संस्थापक और भूतपूर्व निदेशक हैं. उनकी मुख्य कृतियों में ‘थोकदार किसी की नहीं सुनता’ ‘सड़क का भूगोल, ‘अनाथ मुहल्ले के ठुल दा’ और ‘महर ठाकुरों का गांव’ शामिल हैं. काफल ट्री के लिए नियमित लेखन करेंगे.
काफल ट्री वाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिये यहाँ क्लिक करें: वाट्सएप काफल ट्री
काफल ट्री की आर्थिक सहायता के लिये यहाँ क्लिक करें