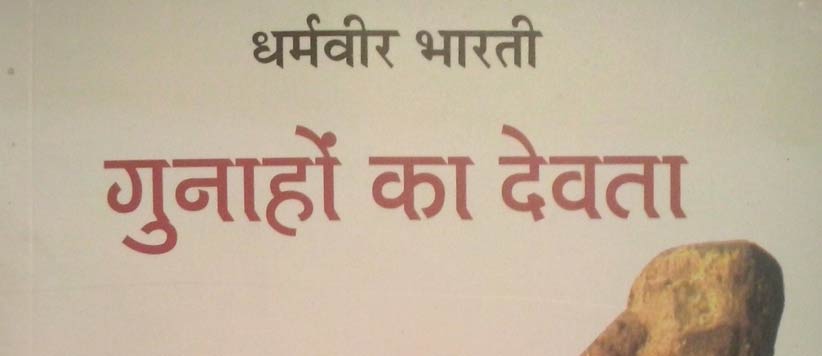हिंदी में लुगदी, पेशेवर और श्रेष्ठ साहित्य का विभाजन
थोड़ा-सा चर्चित हो जाने के बाद हिंदी का लेखक बहुत तेजी-से अपने खोल में घुस जाता है. उसकी दुनिया बन जाती है: वो खुद, उसके हमप्याला दोस्त और बहुत हुआ तो हमकौफी और हमचाय मित्रगण! पहले ऐसा नहीं था. साठ-सत्तर के दशक के बाद यह प्रवृत्ति खास तौर पर दिखाई दी है. पहले भी साहित्यकारों की टोलियाँ हुआ करती थीं, मगर उनके बीच एक-दूसरे से बचने का भाव नहीं रहता था, आपस में दृष्टि और कथाभूमि का जरूर फर्क होता था, मगर एक दूसरे के साथ मेल-मुलाकात और अधिक-से-अधिक संपर्क की कोशिश दिखाई देती थी. हिंदी के विरोधी-से दिखाई देने वाले जो बड़े ‘स्कूल’ (घराने) आज दिखाई देते हैं, प्रेमचंद और प्रसाद, उनके बीच आपस में कितनी मेल-मुलाकात थी, इसे दुहराने की जरूरत नहीं है.
यह भी दुहराने की जरूरत नहीं है कि पिछले अनेक वर्षों में साहित्यकारों के आपसी कंसर्न रचनात्मक मुद्दों के बजाय निजी रुचियों में सिमट आये हैं. कुछ वर्षों से, खासकर रंगीन पत्रिकाओं के प्रकाशन के बाद तो एक अजीब बात देखने में आई है कि जो लेखक अधिक लिखता है या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में प्रकाशित होता है, उसे जाने क्यों कम गंभीर लेखक समझ लिया जाता है. यही नहीं, साहित्यिक और गैर-साहित्यिक लेखक का बंटवारा इस बात से किया जाने लगा है कि बाज़ार में उसकी मांग होने का मतलब है कि वो ‘बाजारू’ लेखक बनने की प्रक्रिया में है. यह बात भी सामने आई थी कि लेखक को बौद्धिक बहसें खड़ी करनी चाहिए और बहुत आसानी से समझ में आने वाला लेखक खास उल्लेखनीय नहीं होता. चर्चित होने का अर्थ दोस्तों के बीच चर्चित होना है, न कि पाठकों के बीच.
इसी से मिलती-जुलती यह धारणा भी सामने आई है कि हिंदी का आम पाठक कमतर बौद्धिक स्तर का होता है. हालाँकि आलोचकों और चर्चाकारों की आकांक्षा अधिक-से-अधिक पाठकों के बीच पहुँचाना होता है मगर पश्चिमी लेखकों की चर्चा और उनकी अति-बौद्धिकता का इतना आतंक होता है कि सभी लोग उसी हवा में बहने लगते हैं. एक दौर तो ऐसा भी आया था कि आलोचकों और समीक्षकों में यह होड़ रहती थी कौन यूरोप के नवीनतम आदोलन का जिक्र करता है (दूसरे को पछाड़ता है). रचना और कथाभूमि के बीच दिखाई देने वाले इस अंतर और दूरी ने हिंदी के लेखकों में एक अजीब-सी ग्रंथि पैदा की है कि अधिक लिखना लेखक की संवेदना को बाधित करता है. इसका एक दुखद परिणाम यह सामने आया है कि लेखन को जीविका के रूप में अपनाने वाले लेखकों की जमात एकदम गायब हो गयी है. जो हैं भी, वे पेशेवर लेखक हैं.
असल में शब्द की जीविका करने वाले व्यक्ति की पूँजी उसका परिवेश और उसके बीच तैरने वाली अभिव्यक्ति है, जिसका माध्यम है भाषा. कोई भी आदमी भाषा के वजूद पर अलग से ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे लगता है कि साँस और भोजन की तरह उसे ग्रहण करने में कोई अतिरिक्त कोशिश नहीं करनी पड़ती. भाषा के कारण ही तो उसका अस्तित्व है. अभिव्यक्ति है तो भाषा होगी ही. और इस बात में सच्चाई भी है.
इसके बावजूद, हिंदी भाषी क्षेत्रों में भाषा का मसला थोड़ा अलग है. सभी भाषाओँ में ज्ञान की भाषा और बोलचाल की भाषा में फर्क होता ही है, हिंदी में यह फर्क इसलिए अलग है क्योंकि वहां की अधिकांश जनसंख्या के लिए ज्ञान की भाषा हमेशा से दूर की कौड़ी रही है. जाहिर है कि भाषा के इन दोनों रूपों ने इस समाज में वर्ग-भेद पैदा कर दिए हैं. संस्कृत और अंग्रेजी विशिष्ट लोगों की भाषा आज भी है, मुग़ल काल में तो मुहावरा ही प्रचलित था. ‘पढ़े फारसी बेचे तेल.’
इसी ग्रंथि ने हिंदी और उसकी बोलियों का प्रयोग करने वालों को मुख्यधारा के विशिष्ट समाज से काट दिया और उसमें अपनी अभिव्यक्ति और भाषा के प्रति हीनता का भाव पैदा कर दिया. गद्य साहित्य के विकास के माध्यम से इस मनोग्रंथि को आसानी से समझा जा सकता है, खासकर कथा-साहित्य के जरिए.
संभव है, इस मनोवृत्ति के पीछे एक कारण यह भी हो कि गद्य की विधाएँ पश्चिम से सीधे हिंदी में आईं, मगर ऐसा तो भारत की सभी भाषाओँ के साथ हुआ है. संस्कृत रचनाओं में जिस प्रकार कुलीन पात्रों की भाषा अलग होती थी और सेवकों की अलग (अपभ्रंश), अंग्रेजी के प्रचार-प्रसार के बाद विशिष्ट लोगों की भाषा में अंग्रेजी की शब्दावली शामिल होती चली गई; यह भी स्वाभाविक था, बुरा यह हुआ कि अंग्रेजी पढ़े-लिखे और विशिष्टों की भाषा बन गयी और हिंदी अपढ़ों की.
सच्चाई यह भी है कि संसार की सभी भाषाओँ में शिष्ट साहित्य और पेशेवर साहित्य का प्रचलन साथ-साथ चलता रहा है. मगर ऐसा कहीं नहीं है कि कम बिकने वाले लेखकों को श्रेष्ठ और अधिक बिकने वाले को ‘लुगदी’ समझ लिया जाये. यह अपने आप में एक तिलिस्म से कम नहीं है.
मुझे लगता है, इस तिलिस्म को समझने के लिए हमें हिंदी उपन्यासों की पृष्ठभूमि की ओर लौटना होगा.
शुरू में ही हिंदी उपन्यासों का लेखन चार सामानांतर धाराओं के रूप में हुआ : तिलस्मी-ऐयारी उपन्यास, जासूसी उपन्यास, ऐतिहासिक और सामाजिक उपन्यास. इन चारों धाराओं के लेखक अपने दौर में बेहद लोकप्रिय थे; खासकर ऐसे दौर के लिए यह छोटी बात नहीं है, जब हिंदी गद्य में पाठकीय अभिरुचि थी ही नहीं. देवकीनंदन खत्री के तिलिस्मी उपन्यासों के बारे में तो कहा ही जाता है कि बनारस के लहरी प्रेस से जब उनके उपन्यासों के फर्मे छपकर दुकान तक लाये जा रहे होते थे, उनमें से अधिकांश रास्ते में ही बिक जाया करते थे. यही हालत उनके समकालीन जासूसी उपन्यासकार गोपालराम गहमरी के बारे में भी कही जाती है.
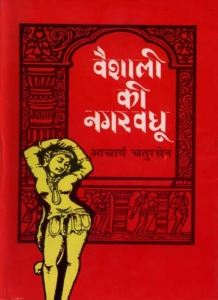 यह दौर उन्नीसवीं सदी के अंतिम और बीसवीं की शुरुआत का था, मगर ऐसा कैसे हुआ कि आधी सदी के बीतते ही तिलस्मी और जासूसी उपन्यासों की छवि गैर-साहित्यिक रचनाओं की बन गई. हिंदी उपन्यास की रचना-यात्रा इसकी गवाह है. इस तरह के सवाल हिंदी के शीर्षस्थ उपन्यासकार प्रेमचंद के उपन्यासों को लेकर भी उठाये गए, और बाद में वृन्दावनलाल वर्मा, आचार्य चतुरसेन, भगवतीचरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, यज्ञदत्त शर्मा आदि दर्जनों लेखकों के बारे में भी. मगर केवल इस आधार पर यह फतवा देना कि अधिक लिखने वाला अनिवार्य रूप से अगंभीर लेखक हैं सही नहीं ठहराया जा सकता.
यह दौर उन्नीसवीं सदी के अंतिम और बीसवीं की शुरुआत का था, मगर ऐसा कैसे हुआ कि आधी सदी के बीतते ही तिलस्मी और जासूसी उपन्यासों की छवि गैर-साहित्यिक रचनाओं की बन गई. हिंदी उपन्यास की रचना-यात्रा इसकी गवाह है. इस तरह के सवाल हिंदी के शीर्षस्थ उपन्यासकार प्रेमचंद के उपन्यासों को लेकर भी उठाये गए, और बाद में वृन्दावनलाल वर्मा, आचार्य चतुरसेन, भगवतीचरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, यज्ञदत्त शर्मा आदि दर्जनों लेखकों के बारे में भी. मगर केवल इस आधार पर यह फतवा देना कि अधिक लिखने वाला अनिवार्य रूप से अगंभीर लेखक हैं सही नहीं ठहराया जा सकता.
लेखन की मात्रा को साहित्यिकता का पैमाना मानना तो खैर, गलत है ही, एक ही लेखक की ऐसी रचना, जिसकी मांग बहुत बढ़ गयी हो, को सस्ता लेखन मानना और उसी की दूसरी रचना को स्तरीय कहना समझ में तो आता है; यह संभव भी है, मगर यह कैसे संभव है कि रातों-रात एक लुगदी लेखक उच्च कोटि की रचनाएँ लिखने लगे. आजादी के बाद के लेखकों में डॉ. धर्मवीर भारती के लेखन को लेकर यह बात कही जाती रही है. उनका पहला उपन्यास ‘गुनाहों का देवता’ अपने प्रकाशन के साथ बहुत लोकप्रिय और चर्चित हुआ अपने दौर के लेखकों की अपेक्षा इस किताब के सर्वाधिक संस्करण भी प्रकाशित हुए, मगर जिन समीक्षकों आलोचकों को हिंदी लेखन में गंभीरता से लिया जाता रहा है, उनकी चर्चा में इस उपन्यास का उल्लेख नदारत है. वहीं, उनके दूसरे उपन्यास ‘सूरज का सातवाँ घोड़ा’ और नाटक ‘अंधा युग’ की परम्परा-स्थापक कृतियों के रूप में खूब चर्चा हुई है. इसी दौर की एक और महत्वपूर्ण उपन्यासकार शिवानी को तो मानो हिंदी समीक्षा-आलोचना में अछूत मान लिया गया. शिवानी ने मात्रा में भी पर्याप्त लिखा है, पाठकों के बीच वह अपने दौर में सबसे अधिक लोकप्रिय भी रही हैं, उनके उपन्यासों के जितने संस्करण प्रकाशित हुए हैं, वो किसी भी लेखक के लिए ईर्ष्या का विषय हो सकती हैं; यहाँ तक कि भाषा, शिल्प और कथन भंगिमा में भी वो अपने दौर में सर्वथा अलग हैं, फिर भी शिवानी पर मुख्यधारा के चर्चाकारों ने एक शब्द भी नहीं लिखा है. हिंदी में पाठकों और आलोचकों के बीच दिखाई देने वाली दृष्टि के इस अंतर को समझ पाना सचमुच कठिन है. ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं मगर हिंदी के अभिजात वर्ग के जिन गिने-चुने कथित प्रबुद्ध चर्चाकारों का हिंदी की दुनिया में आतंक है, अधिकांश चर्चाएँ उन्हीं के इर्द-गिर्द घूमती दिखाई देती हैं.
***
लुगदी साहित्य का अर्थ है वो साहित्य, जो एक बार के पढ़ने के लिए होता है. पढ़ा, मनोरंजन किया (मजा लिया) और फैंक दिया. यात्रा पर, वक़्त काटने के लिए ख़रीदा जाने वाला साहित्य. मतलब ये कि तात्कालिक उपयोगिता के सिवा उसका कोई महत्व नहीं. मेरा आशय इस चर्चा के जरिए यह बहस खड़ी करना नहीं है कि लुगदी साहित्य की भी साहित्यिक गुणवत्ता हो सकती है और साहित्य के नाम पर कुछ लोग लुगदी साहित्य लिखते हैं; दोनों तरह के लेखन को मैं एक-दूसरे का विरोधी ठहराना भी नहीं चाहता, सिर्फ इस शंका को उठाना है कि एक ही तरह की भाषा और रचनात्मक दृष्टि (अपेक्षाओं) से लिखे साहित्य में यह अंतर क्यों? अगर इसके पीछे कोई साहित्यिक तर्क मौजूद हैं तो उसकी चर्चा होनी चाहिए. स्पष्ट है कि इस चर्चा में उन लेखकों और किताबों का उल्लेख करना होगा जिनसे चर्चाकार परहेज करना कहते हैं और जो उनकी छवि की पोल खोल सकता है. वे ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनकी छवि हिंदी समाज के बीच ‘जागरूक’ लेखक की नहीं रह जाएगी.
जिसे आज लुगदी साहित्य कहा जाता है, हिंदी में तो शुरुआत के सालों से ही उसे खूब लिखा जाता रहा है, उत्तेजक, वर्जनाओं का चित्रण करने वाला लेखन हिंदी गद्य के आरंभिक वर्षों से ही खूब बिकता रहा है मगर उसे लेकर किसी किस्म की भ्रान्ति नहीं होती थी; न पाठक में, न लेखक में. ऐसी किताबों की कोई सार्वजनिक चर्चा भी नहीं करता था, कह सकते हैं कि इन्हें निजी आनंद के लिए पढ़ा जाता था, इनमे स्तर-भेद भी हो सकता था, मगर मुख्य विषय-वस्तु को लेकर कोई बहस नहीं उठाता था. ऐसे में एक ही लेखक की एक रचना को ‘लुगदी’ और दूसरी को ‘साहित्य’ का दर्जा देना असमंजस में तो डालता ही है.
एक अन्य बात, जिसका प्रसंग शुरू में ही उठाया गया था, जासूसी, ऐयारी, तिलस्मी और ऐतिहासिक उपन्यासों को गंभीर साहित्य के अंतर्गत न मानने का दुराग्रह है. संसार भर की भाषाओँ में इस कोटि की रचनाओं की पर्याप्त चर्चा होती रही है, उनके स्तरभेद को लेकर बहस हो सकती है, मगर एक ही विधा की होते हुए भी उनके प्रति अछूत का-सा व्यवहार समझ में नहीं आता. समीक्षक और चर्चाकार की रुचियाँ अलग-अलग हो सकती हैं, मगर बिना तर्क दिए, किसी रचना का नकार किसी भी रूप में समझ में नहीं आ सकता. इसे दुराग्रह नहीं तो क्या कहेंगे!
 हिंदी चर्चाकारों में एक और विसंगति धर्म को लेकर देखने को मिलती है. पिछली किसी कड़ी में मैंने पंडित प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका ‘ब्राह्मण’ का हवाला देते हुए लिखा था कि इस पत्रिका का ‘लोगो’ ‘हिंदी. हिन्दू, हिन्दुस्थान’ था जो हिंदी समाज के बीच खासा लोकप्रिय हुआ था. भाषा को धर्म और राष्ट्रवाद के साथ जोड़ने का यह बेहद खतरनाक प्रस्थान-बिंदु था. हिंदी गद्य के आरंभिक काल में, स्वाभाविक रूप से, धर्म से जुड़ी पुस्तकें लिखी गईं, हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसी किताबों की चर्चा भी साहित्यिक विधाओं के खांचे में रखकर की गई. आरंभिक गद्यकारों – लल्लूजी लाल, सदासुखलाल नियाज, सदल मिश्र, श्रद्धाराम फुल्लोरी आदि की अनेकानेक किताबों/रचनाओं की चर्चा इस सन्दर्भ में की जाती रही है. आर्यसमाजी प्रचारक श्रद्धाराम फुल्लोरी की किताब ‘भाग्यवती’ की चर्चा तो हिंदी के अनेक वरिष्ठ इतिहासकारों ने (आचार्य रामचंद्र शुक्ल समेत) हिंदी के प्रथम उपन्यास के रूप में की है.
हिंदी चर्चाकारों में एक और विसंगति धर्म को लेकर देखने को मिलती है. पिछली किसी कड़ी में मैंने पंडित प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका ‘ब्राह्मण’ का हवाला देते हुए लिखा था कि इस पत्रिका का ‘लोगो’ ‘हिंदी. हिन्दू, हिन्दुस्थान’ था जो हिंदी समाज के बीच खासा लोकप्रिय हुआ था. भाषा को धर्म और राष्ट्रवाद के साथ जोड़ने का यह बेहद खतरनाक प्रस्थान-बिंदु था. हिंदी गद्य के आरंभिक काल में, स्वाभाविक रूप से, धर्म से जुड़ी पुस्तकें लिखी गईं, हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसी किताबों की चर्चा भी साहित्यिक विधाओं के खांचे में रखकर की गई. आरंभिक गद्यकारों – लल्लूजी लाल, सदासुखलाल नियाज, सदल मिश्र, श्रद्धाराम फुल्लोरी आदि की अनेकानेक किताबों/रचनाओं की चर्चा इस सन्दर्भ में की जाती रही है. आर्यसमाजी प्रचारक श्रद्धाराम फुल्लोरी की किताब ‘भाग्यवती’ की चर्चा तो हिंदी के अनेक वरिष्ठ इतिहासकारों ने (आचार्य रामचंद्र शुक्ल समेत) हिंदी के प्रथम उपन्यास के रूप में की है.
आम आदमी के बीच इस प्रकार की चर्चा स्वाभाविक है; हिंदी में यह प्रवृत्ति खतरनाक इसलिए है क्योंकि एक ओर तो कुछ रचनाओं को नैतिकता के मानदंड के आधार पर बहुत घटिया मान लिया जाता है, जब कि हिन्दू धर्म से जुड़े प्रसंग प्रशंसा के विषय बन जाते हैं. हालाँकि ऐसा सायास नहीं है, फिर भी हिंदी समाज के शैक्षिक परिवेश में या एक भयावह समस्या के रूप में उभरी है. हिंदी की पाठ्यपुस्तकों और दूसरी भाषा सिखाने वाली किताबों में लगभग सभी स्थानों पर लड़कों के नाम ‘राम’, ‘मोहन’ आदि और लड़कियों के ‘रमा’, ‘सीता’ ‘मोहिनी’ आदि मिलते हैं; यह बात अलग है कि पिछले कुछ समय से इस तरह के संज्ञा नामों में व्यापक परिवर्तन हुआ है. हिंदी समाज में राजनीति का दखल इतना अधिक है कि सत्ताधारी दल के माध्यम से भाषा और संस्कृति सम्बन्धी नीतियों का निर्धारण होता है. इस सन्दर्भ में हद तो तब हो गई जब कुछ वर्ष पहले पाठ्यक्रम में से धर्म से जुड़े चरित्रों को निकाल बाहर करने का मुहीम चला. स्थानों, शहरों के नाम मनमाने ढंग से बदलने का काम तो आज भी जारी है.
भाषा पर अंकुश का सम्बन्ध अभिव्यक्ति की आजादी के साथ है. प्रत्येक समाज में अनिवार्य रूप से भाषा के दो पार्श्व होते है: ज्ञान की भाषा और संपर्क की भाषा. पहले तरह की भाषा समाज का शिक्षित वर्ग बनाता है और दूसरी आम लोगों की बोलचाल से विकसित होती है. इसी प्रक्रिया में ज्ञान की भाषा को सम्मानजनक समझा जाता है और बोलचाल की भाषा की बनावट पर किसी का ध्यान नहीं जाता. निश्चय ही इन दोनों से अलग एक तीसरी भाषा भी होती है, रचनाकारों की भाषा, जिसे कलाकार अपनी विधा के आधार पर आकार देते है. इस भाषा का निर्माता रचनाकार ही होता है और एक अच्छा लेखक कभी भी किसी के दबाव में आकर अपनी भाषा को लेकर कोई समझौता नहीं करता. यही कारण है कि इस भाषा को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और समाज का हर संवेदनशील व्यक्ति अपनी भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति के लिए इसी का सहारा लेना चाहता है. और शायद यही कारण है कि भाषा और अभिव्यक्ति को लेकर किसी भी तरह की छेड़छाड़ को सबसे पहले रचनाकार ही अनुभव करता है और ऐसी मनोवृत्ति का तत्काल प्रतिरोध करता है.
किताबों को लेकर ‘रचनाशील’, ‘पेशेवर’ और ‘लुगदी’ विभाजन भी शब्द की अपनी विशिष्ट संवेदना के आधार पर ही किया गया है. यह विभाजन किसी भी रूप में गलत नहीं है, गलत वह तब बन बैठता है जब एक परिवेश की अभिव्यक्ति की शर्तें दूसरे परिवेश के आधार पर, जिसका उसके साथ कोई लेना-देना नहीं है, निर्धारित की जाने लगती हैं.
(जारी)

फ़ोटो: मृगेश पाण्डे
लक्ष्मण सिह बिष्ट ‘बटरोही‘ हिन्दी के जाने-माने उपन्यासकार-कहानीकार हैं. कुमाऊँ विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग के अध्यक्ष रह चुके बटरोही रामगढ़ स्थित महादेवी वर्मा सृजन पीठ के संस्थापक और भूतपूर्व निदेशक हैं. उनकी मुख्य कृतियों में ‘थोकदार किसी की नहीं सुनता’ ‘सड़क का भूगोल, ‘अनाथ मुहल्ले के ठुल दा’ और ‘महर ठाकुरों का गांव’ शामिल हैं. काफल ट्री के लिए नियमित लेखन करेंगे.
काफल ट्री वाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिये यहाँ क्लिक करें: वाट्सएप काफल ट्री
काफल ट्री की आर्थिक सहायता के लिये यहाँ क्लिक करें