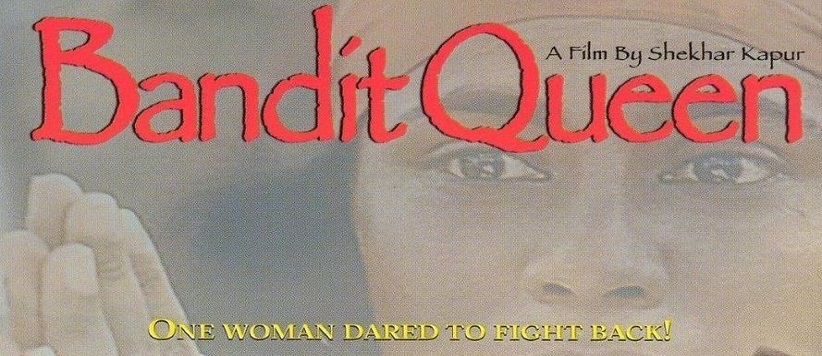पंडित प्रतापनारायण मिश्र के ‘ब्राह्मण’ और डकैत फूलन देवी के ‘ठाकुर’
पिछली बार हमारा किस्सा इस बात के जिक्र पर ख़त्म हुआ था कि साहित्य और भाषा की चाल में कोई यूटर्न नहीं होता. इसका मतलब यह है कि ‘जिस रास्ते पर समाज का श्रेष्ठ-जन (महाजन) चल पड़ता है जरूरी नहीं कि वही रास्ता आने वाले समाज की भाषा और साहित्य का सांस्कृतिक रास्ता बन जाता हो! (महाजनो येन गतो सो पन्थाः) अगर ऐसा होता तो राजा-महाराजाओं और विद्वानों की भाषा और आम आदमी की भाषा में कोई फर्क नहीं होता.
***
फूलन देवी जब 1994 में जेल से छूटी थी, उसी समय दो फ्रांसीसी पत्रकारों – पॉल रांब्ली और मारी तेरेस क्युनी ने फूलन से उनके जीवन को लेकर एक विस्तृत इन्टरव्यू लिया था, जिसके आधार पर उन्होंने बाद में एक किताब लिखी – ‘मुअ फूलन देवी : रैं दे बांदि’ (मैं फूलन देवी : डाकुओं की रानी). मूल रूप से फ्रेंच भाषा में लिखी गई यह किताब 1996 में पेरिस के एक प्रकाशक ने छापी थी. (बाद में शेखर कपूर की इसी थीम पर आधारित फिल्म ‘बैंडिट क्वीन’ हिंदी समाज में खासी हिट हुई. फूलन की यह जीवनी पश्चिमी देशों में इतनी लोकप्रिय हुई कि इंग्लैंड के ‘हाउस ऑफ़ कॉमन्स’ की एक सदस्या ने तो फूलन की इस करुणा भरी दास्तान को सुनकर उन्हें सम्मानित करने का प्रस्ताव रखा और उसके एक के बाद दूसरे देशों की भाषाओँ में अनुवाद होने लगे. संसार की श्रेष्ठतम भाषाओँ के अनुवाद के बाद इस किताब का फूलन की भाषा हिंदी में भी अनुवाद हुआ.
1998 में जब हंगरी के केन्द्रीय विश्वविद्यालय के इंडोलौजी विभाग में इसका हंगेरियन अनुवाद हो रहा था, फूलन की हिंदी, खासकर उसकी गालियों के अनुवाद को लेकर मुझसे परामर्श लिया गया. हिंदी समाज का हिस्सा होने के नाते इस सारे प्रकरण को लेकर मुझे अजीब-सी असुविधा महसूस हो रही थी. मैं विदेश में था और एक उच्च पद पर. (मेरा वेतन भारतीय विदेश सेवा के प्रथम सचिव के बराबर था और एक तरह से मैं हंगरी में भारत का सांस्कृतिक प्रतिनिधि था.)
मेरे विभाग के प्राध्यापक गहरी जिज्ञासा के साथ फूलन की ठेठ देसी गाली का फिकरा मेरे कानों में फेंकते और जब तक मैं उसका आशय स्पष्ट करने की कोशिश करता, खीझ भरे स्वर में कोई कहता, पहले इसका शाब्दिक अर्थ तो बताइए. मुझे उलझन में देखकर उनमें से कोई एक मेज ठोकते हुए कहता, ‘अच्छा, ये बताइए, इस शब्द को बोलते हुए फूलन के चेहरे पे कैसा भाव आता होगा, उसे आप अपने चेहरे पर लाइए.’
मैं उनकी जिज्ञासा और उलझन को समझ रहा था, मगर दूसरे ही पल मानो मैं कुछ छिपाने लगता था और वे इसे भाँप जाते. कई शब्दों का चयन करके वो लोग नोट करते और उनमें से पता नहीं किस शब्द का चयन करते. मुझे इतनी हंगेरियन नहीं आती थी कि मैं उन्हें सटीक शब्द बता पाता. बहरहाल, कुछ महीनों के बाद जब मैंने शहर के सबसे बड़े बुक स्टॉल पर उस किताब को सलमान रुश्दी, अरुंधती राय वगैरह की किताबों के साथ सजा हुआ देखा तो पता नहीं कैसा अनुभव हुआ… मानो मैं ऐसे देश का दर्शक हूँ, जो अपने घर को ही नहीं पहचानता, वहां की ठेठ देसी भाषा का उच्चारण नहीं कर पा रहा. इसके बाद लम्बे समय तक मैं इस बात को लेकर परेशान रहा कि फूलन के साथ मेरा क्या रिश्ता है? वो किसकी जुबान है जिसे वह धड़ल्ले से बोलती है और जिसका मैं न तो उच्चारण कर पाता और न अर्थ समझा पाता…
***
आखिर किसी भी समाज की जातीय भाषा कौन-सी होती है? ऐसा क्यों होता है कि हम अपनी जातीय भाषा को अपने समाज के साथ गंभीर विचार-विमर्श में शेयर नहीं कर पाते. भाषा का ऐसा दोगलापन क्यों अपनाते हैं हम? ऐसी मनोवृत्ति हिंदीभाषियों में ही पाई जाती है या ऐसा सभी भाषा-समाजों में होता है! हंगरी मध्य-पूर्वी यूरोप का, अनेक समृद्ध भाषाओँ वाले देशों से घिरा छोटा-सा देश है, आकार में शायद उत्तराखंड से भी छोटा, मगर सांस्कृतिक दृष्टि से संसार के समृद्ध देशों में उसकी गणना की जाती है. एक आम हंगेरियन कम-से-कम तीन-चार भाषाएँ जानता है, जिनमें अंगेजी शामिल नहीं होती, मगर आपस में वे लोग हंगेरियन में ही बातें करते हैं और उनकी शिक्षा का माध्यम भी हंगेरियन है, जातीय भाषा के इस घपले के बारे में सोचते हुए हम हिन्दीभाषी अगर डेढ़ सदी पहले लौटें, जो हिंदी गद्य निर्माण के शुरुआती साल थे, तो पाते हैं कि हिंदी समाज में यह विरोधाभास नया नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं.
हिंदी गद्य के आरंभिक निर्माताओं में अनिवार्य रूप से तीन लोगों का जिक्र किया जाता है – भारतेंदु हरिश्चंद्र (1850-1885), पंडित बालकृष्ण भट्ट (1844-1914) और पंडित प्रतापनारायण मिश्र (1856-1895). ध्यान देने की बात है कि इन तीनों में भारतेंदु की स्थिति अजीब दिखाई देती है. हिंदी के पंडितों ने उनके नाम से आधुनिक हिंदी युग का नामकरण करने की इजाजत तो दे दी, मगर उन्हें ‘पंडित’ नहीं माना. एक और झूठ हिंदी समाज में यह फैलाया जाता रहा है कि आधुनिक हिंदी का जन्म संस्कृत के गर्भ में से हुआ है. एक ओर हम हिंदी की उप-भाषाओँ और बोलियों के अंतर्गत हिंदी समाज में बोली जाने वाली बोलचाल की भाषाओँ का उल्लेख करते हैं, दूसरी ओर हिंदी भाषा को संस्कृत के गर्भ में से उत्पन्न मानते हैं; जब कि वास्तविकता यह है कि बोलचाल की इन भाषाओँ ने संस्कृत के वर्चस्व के खिलाफ लम्बा संघर्ष किया है.
वर्ष 1882 में ब्रिटिश हुकूमत ने प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीयों की परम्परागत शिक्षा प्रणाली तथा माध्यम-भाषा का पता लगाने के लिए एक कमीशन का गठन किया: “कमीशन ऑफ़ इंडियन एजुकेशन, 1882”. इस आयोग ने भारत के कुछ चुने हुए प्रबुद्ध व्यक्तियों से तत्कालीन परंपरागत शिक्षा-प्रणाली और अंग्रेजों के द्वारा दी जा रही नई शिक्षा-व्यवस्था के सम्बन्ध में विचार आमंत्रित किये. अंग्रेजी में लिखी गयी 70 प्रश्नों की इस वृहत प्रश्नावली का भारतेंदु के द्वारा अंग्रेजी में ही लगभग सौ पृष्ठों का विस्तृत उत्तर दिया गया. अपने उत्तर में भारतेंदु ने अंग्रेजों की नई शिक्षा पद्धति की बेहद तारीफ की है. मगर हिंदी से जुड़े शुद्धतावादियों को यह बात रास नहीं आई और इस बात को लेकर उनके देश-प्रेम की भावना पर सवाल उठाये गए. (यह एक लम्बी बहस है; जो लोग विस्तार से जानना चाहते हैं, इतिहासकार रामगोपाल की किताब “स्वतंत्रता-पूर्व हिंदी के संघर्ष का इतिहास” (1964, प्रकाशक: हिंदी साहित्य सम्मलेन, प्रयाग) देख सकते हैं. भाषाओँ को धर्म के साथ जोड़ने का यह झूठ आज भारत में बाक़ायदा जड़ें जमा चुका है, मगर इसकी जड़ें अंग्रेजों के शासनकाल में ही जम चुकी थी, हैरान करने वाली बात यह है कि इन जड़ों को रोपा हमारे ही देशवासियों ने. यह अनायास नहीं है कि हिंदी में ‘विद्वान’ के लिए प्रयोग किया जाने वाला ‘पंडित’ शब्द ब्राह्मणों के लिए प्रयुक्त होने लगा, और कालांतर में यह जातिसूचक बन गया. मजेदार बात है कि हिंदी के आरंभिक उन्नायकों की त्रिमूर्ति में प्रतापनारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट के नाम के साथ ‘पंडित’ शब्द का प्रयोग किया जाता है जब कि हरिश्चंद्र के साथ ‘भारतेंदु’ या ‘बाबू’ शब्द का. यह भी अनायास नहीं है कि आज तक भी संस्कृत के अधिकांश विद्यार्थी ब्राह्मण ही होते रहे हैं. आरम्भ में तो संस्कृत की कक्षा में निम्न वर्ण के लोगों तथा स्त्रियों को प्रवेश नहीं दिया जाता था. (कवयित्री महादेवी वर्मा ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में संस्कृत विषय में उन्हें इसलिए प्रवेश नहीं दिया गया कि वो द्विज नहीं थीं और स्त्री थीं.) भारतीय शिक्षा-संस्थानों में हिंदी विषय की डिग्री प्राप्त करने के लिए संस्कृत की जानकारी अनिवार्य होती थी. हिंदी का कोई भी अध्यापक संस्कृत के प्रमाणपत्र के बिना नियुक्त नहीं हो सकता था.
प्रतापनारायण मिश्र ने 15 मार्च, 1883 को कानपुर से एक मासिक पत्रिका ‘ब्राह्मण’ का प्रकाशन शुरू किया जो 1894 ईस्वी तक चली. पत्रिका के मुखपृष्ठ पर इसके नाम के साथ ही ‘लोगो’ की तरह ही छपा रहता था, ‘हिंदी, हिन्दू, हिंदुस्तान’. यह प्रतीक-वाक्य हिंदी समाज में बेहद लोकप्रिय हुआ और इसी नारे का असर था कि हिंदी को हिन्दुओं के साथ उसी प्रकार जोड़ दिया गया, जैसे आज की राजनीतिक भाषा में उर्दू को मुसलमानों के साथ जोड़ दिया जाता है. भाषा को किसी मजहब या जाति के साथ जोड़ने की यह प्रवृत्ति शायद ही किसी अन्य समाज में देखने को मिलती हो. शायद यह भी अनायास नहीं है कि संस्कृत की तरह हिंदी भी आम लोगों की भाषा नहीं बन पाई; वह हिंदी जो हिंदी क्षेत्र के आम जन की भाषा थी. यह भी अकारण नहीं है कि आमफहम की भाषा होने के बावजूद आज शुद्ध हिंदी का अर्थ संस्कृतनिष्ठ हिंदी समझा जाता है है, जिस पर पहले की तरह हिन्दू सवर्णों का आधिपत्य है. आजादी के बाद तो, तमाम बड़े प्रभावशाली नेताओं की कोशिश के बावजूद, हिंदी अपनी इसी शुद्धतावादी प्रकृति की गिरफ्त में अधिकाधिक आती चली गयी. जिसे आज हम शुद्ध हिंदी कहते वह न तो बोलचाल की भाषा रह गयी है और न संस्कृत की तरह ज्ञान की भाषा. हिंदी की तकनीकी भाषा, अनुवाद की भाषा और शिष्ट भाषा का स्वरूप एक ऐसी उलझी, आकाशीय भाषा का रूप ग्रहण करता चला गया जो न आम आदमी की भाषा है और न पढ़े-लिखे लोगों की भाषा. सरकारी भाषा के रूप में भी हिंदी एक नपुंसक, निर्जीव भाषा के रूप में विकसित हुई जो संस्कृत और अंग्रेजी की अपेक्षा कहीं अधिक कठिन और क्लिष्ट है. ऐसे में सरकारी नोट लिखते हुए हाकिमों के लिए अंग्रेजी और दूसरी भारतीय भाषाएँ तो सहज लगती हैं, जब कि ऐसी हिंदी के लिए पग-पग पर शब्दकोष देखने की जरूरत पड़ती है. आज हालत यह है कि हिंदी की उपभाषाएं और बोलियाँ तो हमारे लिए दुरूह हो ही गयी हैं, ऐसी शुद्ध हिंदी भी समझ से बाहर हो गयी है. जिस समाज में भाषा ही दुरूह हो तो ज्ञान संभव कैसे होगा. शायद यह भी एक कारण है कि हिंदी समाज खुद हिंदी से अपना पल्ला झाड़ रहा है और थोडा अतिरिक्त प्रयत्न के बाद अंततः अंग्रेजी की शरण में जाना अधिक पसंद कर रहा है. एक पढ़े-लिखे समाज के लिए यह सोचना स्वाभाविक है कि यदि अनुवाद से ही काम चलाना है तो हिंदी के अनुवाद के बदले अंग्रेजी का अनुवाद निश्चय ही फायदेमंद है क्योंकि वह एक भारतीय को न केवल राष्ट्रीय, वरन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ता है.
***
क्या हिंदी समाज की जातीय भाषा फूलन देवी की भाषा है? अगर ऐसा है तो हिंदी समाज का पढ़ा-लिखा वर्ग उसकी भाषा के उच्चारण में असुविधा क्यों महसूस करता है? क्यों फूलन की भाषा को अंग्रेजीदा हिंदी समाज ‘स्लैंग’ कहता है? क्या स्लैंग असभ्यों की भाषा होती है? कहीं इसके पीछे यह तर्क तो नहीं है कि फूलन की हिंदी से हम इसलिए बचना चाहते हैं कि क्योंकि हम असभ्य कहलाने से बचना चाहते है. मगर आज के राजनीतिक सन्दर्भों में फूलन तो असभ्य नहीं है. वो अपनी जाति के इलाके से शानदार बहुमत से विजयी हुई थी और एक सांसद के रूप में भी उसे खासी सफलता मिली थी. उसकी जीवनगाथा सुनकर उसे कितने ही अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने पुरस्कृत किया था और नारीवादियों के लिए वह आदर्श बन गयी थी.
क्या फूलन देवी इसलिए असभ्य और असामाजिक थी क्योंकि उसने दर्जन भर सवर्ण ठाकुरों को एक कतार में खड़ा करके गोलियों से भून डाला था. अगर वो असभ्य और उसकी भाषा अशालीन थी तो उन ठाकुरों को हम कैसे सभ्य और शालीन कहेंगे जिन्होंने फूलन और उसकी परिजनों के साथ दरिंदगी की थी. खुले आम उसे नंगा करके लोगों को दिखा-दिखाकर उसके साथ सम्भोग किया था.
और अगर फूलन और उसकी बिरादरी के साथ बलात्कार करने वाले ठाकुरों की सजा वही है जो फूलन ने उन्हें दी, तो उन ‘पंडितों’ की क्या सजा होनी चाहिए जिन्होंने पीढ़ी-दर-पीढ़ी अपने वंशजों को बिना योग्यता के विद्वत्ता का उपहार दे दिया और अपने ही समाज के बाकी मानव समूह को दिमागी तौर पर नपुंसक बना डाला. वास्तविकता यह भी नहीं है कि वह समाज, जिसका नेतृत्व पंडित करते हैं, पहले इसलिए मूढ़ था क्योंकि उसे ज्ञान की भाषा के उच्चारण का अधिकार नहीं था, अब इसलिए मूढ़ हैं क्योंकि जो नई हिंदी उसके समाज में अंकुरित हो रही है, उसकी छवि इतनी अशिष्ट और गलीज बना दी गयी है कि उसका समाज खुद ही उसका उच्चारण नहीं करना चाहता. क्या फूलन की भाषा का उच्चारण करने में उसी का समाज आज सुविधा का अनुभव करता है!
मेरे नए रचनाकार दोस्तो!
आप लोग हिंदी समाज के नए-नए अंग बने हैं, आपने अभी लम्बी यात्रा तय करनी है. आपके प्रयत्नों से ही हिंदी समाज का खाका निर्मित होना है.
दो सदी पूर्व हमारे पुरखों ने जो यात्रा शुरू की थी, आज यह अंदाज लगा पाना कठिन है कि उन्हें कितनी और किस तरह की परेशानियों को तब झेलना पड़ा था. तब अभिव्यक्ति की भाषा के रूप में हिंदी का कोई वजूद नहीं था, जो था, उसे महाज्ञानी पंडित भाषा मानने के लिए तैयार नहीं थे. इन दो सौ वर्षों में हमारे पुरखों ने खूब संघर्ष किया, मगर उसका सिफर समाधान निकला. उन लोगों में से कुछ शुद्धतावादियों ने, हिंदी को जाति और धर्म के साथ जोड़कर इतना इकहरा और अपंग बना डाला है कि उसे भाषा के रूप में कोई भी अपनाने के लिए तैयार ही नहीं है. हिंदी आज ऐसी मुद्रा बन गयी है जो दूसरों को तो दिल खोलकर दौलत लुटा रही है, मगर उसी दौलत से उसका खुद का वजूद नष्ट हो रहा है.
हम देख रहे हैं कि आप लोग अपने समाज की नई भाषा गढ़ रहे हैं, हमारे प्रतिभाशाली कथाकारों ने यह कोशिश काफी पहले शुरू कर दी थी, मगर शुद्धतावादियों ने ‘हिंग्लिश’ नाम देकर उसका मजाक भी कम नहीं उड़ाया और उसे मुख्यधारा से बेदखल करने की भरपूर कोशिश की. इसलिए आपके लिए यह कहीं अधिक कठिन और चुनौतीपूर्ण दौर है.
अगर समाज जिन्दा होगा तभी भाषा जिन्दा रहेगी. समाज ही दो-फाड़ हो जाएगा तो उसकी भाषा कैसे बची रह सकती है. हाँ, जो नई भाषा बनेगी, वह अपना आत्मीय समाज बना ही लेगी,
(जारी)

फ़ोटो: मृगेश पाण्डे
लक्ष्मण सिह बिष्ट ‘बटरोही‘ हिन्दी के जाने-माने उपन्यासकार-कहानीकार हैं. कुमाऊँ विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग के अध्यक्ष रह चुके बटरोही रामगढ़ स्थित महादेवी वर्मा सृजन पीठ के संस्थापक और भूतपूर्व निदेशक हैं. उनकी मुख्य कृतियों में ‘थोकदार किसी की नहीं सुनता’ ‘सड़क का भूगोल, ‘अनाथ मुहल्ले के ठुल दा’ और ‘महर ठाकुरों का गांव’ शामिल हैं. काफल ट्री के लिए नियमित लेखन करेंगे.
काफल ट्री वाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिये यहाँ क्लिक करें: वाट्सएप काफल ट्री
काफल ट्री की आर्थिक सहायता के लिये यहाँ क्लिक करें