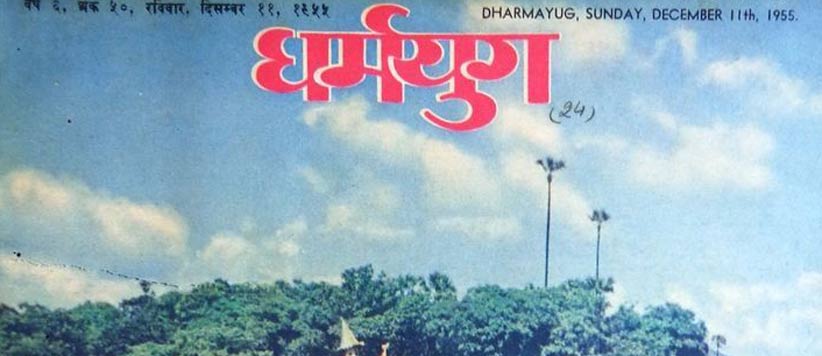हिंदी की नई पौध के लिए एक चिट्ठी : नसीहत नहीं, ‘हलो’
मेरे नए रचनाकार दोस्तो!
आज से करीब पचपन साल पहले मैंने हिंदी लेखकों की दुनिया में प्रवेश किया था. वो पिछली सदी के साठ के दशक का आरंभिक दौर था और हिंदी में रंग-विरंगी पत्रिकाओं के प्रकाशन की शुरुआत हो रही थी. हालाँकि पत्रिकाएं पहले भी छपती थीं मगर कहानी, कथात्मक गद्य और समाचार फीचर आदि नई विधाएँ एकदम भिन्न साज-सज्जा के साथ पत्र-पत्रिकाओं में दिखाई देने लगी थी. कविता की जगह कहानी साहित्य की मुख्य विधा के रूप में स्थापित हो रही थी. पत्रिकाएं एकदम अलग तेवर के साथ बाजार में दिखाई देने लगी थीं, पहली बार साहित्य बाजार के आकर्षण के साथ हिन्दीभाषी मध्यवर्गीय समाज की जरूरत बनने लगा था. शुद्धतावाद का नकाब उतर रहा था और नौजवान पीढ़ी उसे अपनी जरूरत के मुहावरे के अनुसार ढाल रही थी. कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि साहित्यिक अभिरुचि देश के बड़े व्यवसाइयों का ध्यान आकर्षित करेगी और साहित्य और संस्कृति के बड़े घराने देश में व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बन जाएंगे.
1950 में टाइम्स ऑफ़ इंडिया प्रकाशन-समूह ने ‘जोशी बंधुओं’ (डॉ. हेमचन्द्र और इलाचंद्र जोशी) के संपादन में ‘धर्मयुग’ का प्रकाशन आरम्भ किया तो लेखकों और साहित्यकर्मियों ने उसे हाथों-हाथ लिया. उन्हीं दिनों इसी तरह के कलेवर में भारत का दूसरा बड़ा प्रकाशन-समूह हिंदुस्तान टाइम्स ‘साप्ताहिक हिंदुस्तान’ नाम से पत्रिका निकाल चुका था. इन दोनों पत्रिकाओं और प्रकाशन समूहों ने हिन्दीभाषी लेखकों और संस्कृतिकर्मियों की एक नई छवि भारतीय युवाओं के सामने प्रस्तुत की. अब वह होरी-धनिया-गोबर-झुनिया-मेहता-मालती-नुमा पुराने शुद्धतावादी विश्वासों को लेकर क्रांति की पहल करने वाला नौजवान नहीं था, उसमें से बहुत स्पष्ट रूप में आने वाले हिंदी समाज के हरिशंकर परसाई, राही मासूम रजा, उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी, शानी, श्रीलाल शुक्ल आदि के एकदम ताज़ा चेहरे अंकुरित होने लगे थे. हिंदी मध्यवर्गीय युवाओं की एक नई आकर्षक आर्थिकी जन्म लेने जा रही थी.
मगर हिंदी समाज के स्थाई संस्कार पुराने ही चल रहे थे; कह सकते हैं कि राजनीति के वाम और दक्षिण पंथों के जबरदस्त दखल के कारण साहित्यिक अभिरुचि में पूरा बदलाव तो संभव नहीं था, फिर भी शुद्धतावादियों के बीच से एक रेडिकल किस्म के नव-शुद्धतावादी का जन्म हो रहा था, जो विचारधारा से तो वामपंथी था, मगर व्यवहार में दक्षिणपंथी शुद्धतावादी. इसी की देखादेखी साहित्यिक अभिरुचि में एक बड़ा फर्क आया. लोकप्रियता और ग्लैमर को गैर-साहित्यिक मूल्य की छवि प्रदान कर दी गई और लेखन में ‘साड़ी बनाम धोती’-नुमा विभाजन करके पत्रिकाओं की एक नई प्रजाति – लघुपत्रिका – का जन्म हुआ. जैसा कि होना ही था, लघुपत्रिका आर्थिक उदारीकरण के दौर की जिंस होने के कारण इसने पत्रिका के कलेवर और प्रबंध-तंत्र में व्यापक परिवर्तन ला दिया. कम पूँजी और सस्ते न्यूज़प्रिंट में छपी पत्रिका ‘लघुपत्रिका’ मान ली गयी और महंगे कागज में रंगीन छपाई वाली पत्रिका को ‘व्यावसायिक’ पत्रिका का ख़िताब मिला. लघुपत्रिका का संपादक प्रतिस्पर्धा से नहीं, मित्र-मंडली के बीच से नियुक्त होने लगा. इतना ही नहीं, यह भी मान लिया गया कि शुद्ध साहित्य केवल लघुपत्रिका में ही प्रकाशित हो सकता है और व्यावसायिक पत्रिकाएं गैर-साहित्यिक होती हैं. मजेदार बात यह कि दोनों के बीच की प्रतिस्पर्धा कला की कसौटी पर नहीं, मित्र-मंडली की रुचि और विदेशी साहित्य के अध्ययन के आतंक आधार पर तय होने लगा.
युवा साथियों, इसी बीच हिंदी गद्य की सबसे लोकप्रिय विधा ‘कहानी’ के गर्भ में से एक ‘अखबारी-कहानी’ का जन्म हुआ जिसका प्रत्यावर्तन ‘आवरण-कथा’ (कवर स्टोरी) के रूप में हुआ. व्यावसायिकता के दबाव ने साहित्य की अनेक अन्तर्धाराओं को जन्म दिया. एक नए तरह के पाठकीय जनतंत्र का जन्म हुआ; पढ़े-लिखे मध्यवर्ग के उदय के साथ ही पाठकीय अभिरुचि के मूल्य लेखक, पत्रकार और साहित्यिक महंत नहीं, आम पाठक तय करने लगे.
आजादी के बाद भारतीय समाज में सामने आये व्यापक परिवर्तनों में सबसे बड़ा था, गाँवों का कस्बों और कस्बों का शहरों के रूप में परिवर्तन. यह सिर्फ भौगोलिक सीमाओं का बँटवारा नहीं था, परम्परागत समाज-व्यवस्था का नितांत नया चिह्नीकरण था. इसी कड़ी में ग्रामांचलों पर लिखने वाले ‘आंचलिक’ कथाकारों का बेहद आकर्षक वर्ग सामने आया. 1954 में राजकमल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित बिहार के पूर्णिया जिले के ग्रामांचल के ठेठ आंचलिक मुहावरे को प्रस्तुत करने वाले उपन्यास ‘मैला आँचल’ को खुद इसके लेखक फणीश्वरनाथ रेणु ने ‘आंचलिक’ नाम दिया : “यह है मैला आँचल. एक आंचलिक उपन्यास… इसमें फूल भी हैं शूल भी, धूल भी है, गुलाब भी, कीचड़ भी है, चंदन भी, सुन्दरता भी है, कुरूपता भी,.. मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया… कथा की सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ साहित्य की दहलीज पर आ खड़ा हुआ हूँ; पता नहीं अच्छा किया या बुरा…” (रेणु, 9 अगस्त, 1954; ‘मैला आँचल’ की भूमिका)
हिंदी उपन्यास-साहित्य में ‘गोदान’ के बाद जिस उपन्यास की सबसे अधिक चर्चा हुई वो ‘मैला आँचल’ ही है, यद्यपि हिंदी के बेहतरीन जातीय उपन्यासों की एक लम्बी सूची इन दोनों उपन्यासों के बीच मौजूद है.
आज, यानी इक्कीसवीं सदी के दूसरे दशक में, हिंदी भाषा और साहित्य भारतीय समाज की मुख्यधारा नहीं रहा. आज यह बात सुनने में अविश्वसनीय लगती है, मगर सिर्फ एक सदी पहले, जब हिंदी गद्य का जन्म हुआ था, हालत यह नहीं थी. कह सकते हैं कि करीब-करीब इसके विपरीत थी. आज हिंदी क्षेत्र की चर्चा होने पर इसके अंतर्गत उत्तर-मध्य भारत का इलाका आता है, मगर तब भी दक्षिण भारत समेत पूरा देश हिंदी के जरिए एक सूत्र में जुड़ता था.
एक और विरोधाभासी बात इन दिनों सुनने में आती है कि बोलचाल की संपर्क भाषा के रूप में तो हिंदी पूरे देश की भाषा है मगर ज्ञान की भाषा इस देश में सिर्फ अंग्रेजी है. इस बात से एक अजीब निष्कर्ष निकलता है कि अंग्रेजी के आने से पहले भारत एक ज्ञानहीन देश था, जहाँ यद्यपि विभिन्न क्षेत्रों में काम चलाने वाली अनेक बोलियाँ थीं, मगर पढ़े-लिखे लोगों की कोई भाषा नहीं थी.
इस तरह के निष्कर्ष पर पहुँचते ही हमारे ध्यान में फ़ौरन संस्कृत, पालि आदि भाषाएँ आती हैं और लगता है कि ज्ञान की भाषाओँ के रूप में भले ही हमारे पास प्राचीन भाषाएँ थीं, मगर आम आदमी के पास ऐसी कोई भाषा नहीं थी जिसके माध्यम से ज्ञान से सम्बंधित विषयों की जानकारी प्राप्त कर सके. कुछ पुराने शुद्धतावादियों के दिमाग में जरूर ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली और राजस्थानी आदि भाषाएँ और उनमें लिखा गया साहित्य तैरता हैं लेकिन यहाँ भी विगत दो-तीन सौ वर्षों में यहाँ की स्थानीय भाषाओँ के लिए अंग्रेजों के द्वारा दिये गए ‘वर्नाक्युलर’ शब्द ने अपनी स्थानीय भाषाओँ के प्रति अजीब-सा हीनता बोध पैदा कर दिया है. यही कारण है कि भारतवासी अपनी भाषाओँ को ‘ज्ञानसम्पन्न’ भाषा के रूप में स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते.
***
आज से पचास साल पहले जब मैंने प्रेमचंद-पूर्व कथा-साहित्य पर शोध कार्य शुरू किया था, लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, खासकर जब मैं श्रद्धाराम फुल्लोरी, श्रीनिवासदास. देवकीनंदन खत्री, ब्रजनंदन सहाय, किशोरीलाल गोस्वामी, गोपालराम गहमरी आदि की कथात्मक-गद्यकार के रूप में चर्चा करता था. मैं प्रयाग विश्वविद्यालय से शोधकार्य कर रहा था और उन दिनों इलाहाबाद हिंदी साहित्य के गढ़ के रूप में पांव जमा रहा था. भारत के एकमात्र ज्ञान-केंद्र के रूप में स्थापित वाराणसी का रुतबा ढीला पड़ रहा था और हिंदी के बुद्धिजीवी काशी के स्थान पर प्रयाग में बसना पसंद करने लगे थे. मगर नए ज्ञान-विज्ञान से संपन्न होने के बावजूद नई पीढ़ी के लेखकों में उन्नीसवीं सदी के कथा-गद्यकारों को पुनर्जागरण के प्रतिनिधि स्वीकार करने की हिम्मत नहीं दिखाई देती थी. शायद इसके पीछे यह कारण था कि संस्कृत के आभामंडल से आतंकित पढ़ा-लिखा समाज हिंदी को ज्ञान की भाषा मानने के लिए तैयार नहीं था. एक और दबाव था, जिसने इस ग्रंथि को ताकत दी… यह कि इसी दौर में पश्चिम का तैयार ज्ञान-विज्ञान मध्यवर्गीय पढ़े-लिखे समाज का हिस्सा बन चुका था. उस ज्ञान के माध्यम से देश का युवा अंतर्राष्ट्रीय फलक के साथ जुड़ रहा था, इसलिए भी क्लासिकल बनाम वर्नाक्युलर की बहस छेड़ने का अवसर किसी के पास नहीं था.
अपने शोध के दौरान जिस बात ने मुझे चौंकाया था, ये कि उन्नीसवीं सदी में हिंदी का केंद्र आज का कथित हिंदी क्षेत्र न होकर इस क्षेत्र के धुर पूर्व और पश्चिम के ऐसे हिस्से थे, जिन्हें किसी भी रूप में हिंदी प्रदेश तो नहीं कहा जा सकता. न तब और न आज. ये हिस्से थे पूरब का हिस्सा कलकत्ता और पश्चिम का बम्बई.
अगर उन्नीसवीं सदी की भाषा-साहित्य सम्बन्धी बहसों में जायेंगे तो आपकी नजर सबसे पहले दो बहुपठित पत्रिकाओं पर टिकेगी – कलकत्ता से प्रकाशित मासिक ‘भारतमित्र’ (मासिक; संपादक : पंडित रुद्रदत्त) और बम्बई से प्रकाशित ‘श्रीबैंकटेश्वर समाचार’ (साप्ताहिक; संपादक : मेहता लज्जाराम शर्मा). इसी दौर की दो अन्य पत्रिकाओं का भी उल्लेख आवश्यक होगा, ‘सदादर्श’ और ‘सुदर्शन’. ये दोनों मासिक पत्रिकाएँ दिल्ली से प्रकाशित होती थीं, मगर ये दोनों इस रूप में ऐतिहासिक महत्व की हैं क्योंकि प्रथम के संपादक कलकत्ता के तत्कालीन मजिस्ट्रेट और हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास ‘परीक्षागुरू’ के लेखक श्रीनिवासदास तथा द्वितीय के प्रकाशक हिंदी के प्रथम लोकप्रिय उपन्यास ‘चंद्रकांता संतति’ के लेखक देवकीनंदन खत्री. आशय यह कि हिंदी क्षेत्र के हाशिए में रहने वाले इन लोगों ने हिंदी को जन-सामान्य तक पहुँचाने का जो ऐतिहासिक काम किया, वह काम हिंदी की मुख्यधारा के केन्द्रों के लेखक नहीं कर पाए.
यहीं पर यह जिज्ञासा पैदा होती है कि हिंदी साहित्य, विशेष रूप से गद्य-साहित्य की जो परंपरा हिंदी प्रदेश के हाशिए के केन्द्रों में शुरू हुई थी, अगर उसी रूप में विकसित होती तो समकालीन हिंदी साहित्य का परिदृश्य आज शायद कुछ और ही होता.
लेकिन आज हालत वश में नहीं रह गयी है, साहित्य और भाषाओँ में यू टर्न नहीं होता, और भाषा-अभिव्यक्ति का वेग पहाड़ी जल-प्रपात से कहीं अधिक वेगमयी होता है. ठहरकर उस पर विचार करने का मतलब है कि हम तो अपने ही वर्तमान में उलझे रह जायेंगे मगर हमारा परिवेश तब तक भविष्य बन चुका होगा.
जो हो चुका है, उसे लौटाया तो नहीं जा सकता है, मगर आज की नौजवान पीढ़ी के भाषा-साहित्य विषयक सरोकारों को लेकर अपनी चिंता तो व्यक्त की ही जा सकती है जिसे हम अगली कड़ी में साझा करेंगे.
(जारी)

फ़ोटो: मृगेश पाण्डे
लक्ष्मण सिह बिष्ट ‘बटरोही‘ हिन्दी के जाने-माने उपन्यासकार-कहानीकार हैं. कुमाऊँ विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग के अध्यक्ष रह चुके बटरोही रामगढ़ स्थित महादेवी वर्मा सृजन पीठ के संस्थापक और भूतपूर्व निदेशक हैं. उनकी मुख्य कृतियों में ‘थोकदार किसी की नहीं सुनता’ ‘सड़क का भूगोल, ‘अनाथ मुहल्ले के ठुल दा’ और ‘महर ठाकुरों का गांव’ शामिल हैं. काफल ट्री के लिए नियमित लेखन करेंगे.
काफल ट्री वाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिये यहाँ क्लिक करें: वाट्सएप काफल ट्री
काफल ट्री की आर्थिक सहायता के लिये यहाँ क्लिक करें