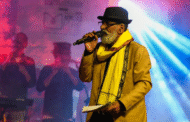खेती के इतिहास का सभ्यता के विकास के साथ अटूट सम्बन्ध है. इसी के आधार पर मनुष्य अपने समाज की संरचना कर पाया. परन्तु दुर्भाग्यवश इतिहासकारों का ध्यान भारतीय खेती के इतिहास, विशेषकर हिमालयी खेती की ओर अधिक नहीं गया है. खेती का इतिहास लिखना जटिल कार्य है और हमें अपनी सीमाओं का पूरा भान है. फिर भी इस आशा के साथ यह प्रयास किया जा रहा है कि शोधार्थी भविष्य में इसमें सुधार कर सकेंगे.
(Agriculture in Uttarakhand History)
खेती के इतिहास का प्रारम्भ पश्चिम एशिया में दजला-फराद की घाटियों में पाषाण युग में माना जा सकता है. तदुपरान्त सिन्धु सभ्यता में भी खेती के पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं. भारतीय खेती पर बौद्ध धर्म ग्रन्थों के अतिरिक्त मैगस्थनीज (300 ई.पू.), फाह्यान (300-345 ई.पू.), ह्वेनसांग (629-641 ई.) तथा अलबरूनी (1031 ई.) के यात्रा वृतान्तों से जानकारी मिलती है. कृषि पराशर (950-1000 ई.) तथा कृषि सूक्ति (1000 ई.) में भी एक क्रमिक वर्णन प्राप्त होता है. कौटिल्य के अर्थशास्त्र (300 ई.पू.) में भी भारतीय खेती की व्यवस्था का वर्णन है.
उत्तराखण्ड का उन्नत शिखरों तथा गहन घाटियों से परिपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र तराई से जुड़ा है. राजनैतिक उथल-पुथल के कारण उत्तराखण्ड का अनेक बार पुनर्गठन किया गया. 1815 में जिला कुमाऊं, टिहरी रियासत तथा देहरादून बने. सरकार द्वारा कुमाऊं को भी दो जिलों में बाँट दिया गया. कुमाऊं तथा ब्रिटिश गढ़वाल. कालान्तर में इसमें एक जिला तराई नाम से बना दिया गया. पुनः कुमाऊं व तराई के स्थान पर अलमोड़ा तथा नैनीताल जिले बनाये गये. स्वाधीनता के बाद अलमोड़ा जिले से सोर क्षेत्र को पृथक करके पिथौरागढ़, अपर गढ़वाल को चमोली तथा टिहरी के ऊपरी हिस्से को उत्तरकाशी जिला बनाया गया. उत्तराखण्ड क्षेत्रफल तथा जनसंख्या में संयुक्त राष्ट्रसंघ के अनेक सदस्य राष्ट्रों से बड़ा है.
किसी भी देश अथवा क्षेत्र की खेती का इतिहास लिखने हेतु वहाँ के सामाजिक तथा राजनैतिक इतिहास का अध्ययन किया जाना चाहिये. इसीलिये आवश्यक है कि उत्तराखण्ड के खेती के इतिहास को इस क्षेत्र की ऐतिहासिक घटनाओं के परिपेक्ष्य में देखा जाये. यहाँ की खेतिहर अर्थव्यवस्था सम्बन्धी विशेषताओं की समीक्षा करने से हिमालय क्षेत्र की पर्यावरण सम्बन्धी समस्याओं पर प्रकाश पड़ेगा तथा समाधानों के दिशा संकेत प्राप्त हो सकेंगे.
(Agriculture in Uttarakhand History)
उत्तराखण्ड के निवासी विभिन्न प्रजातीय समूहों का सम्मिश्रण हैं, जिनकी एक सम्पन्न सांस्कृतिक विरासत है परन्तु फिलहाल जिनके क्रमिक इतिहास का अभाव है. आर्यों के आगमन से पूर्व संभवतः कोल, किरात, नाग तथा खस जातियाँ यहाँ निवास करती थी. यहाँ के मूल आदिवासियों में कुछ पशु चारण और खेती के कार्य में संलग्न थे. पर्वतीय खेती में अत्यधिक श्रम तथा दक्षता की आवश्यकता होती है. सीड़ीदार खेतों को पुरातन यंत्रों से जोतना एक कठिन कार्य है. यद्यपि बाढ़ तथा सूखा जैसे प्राकृतिक प्रकोपों से सामान्यतः यह क्षेत्र मुक्त रहा था. परन्तु भूमि के कटाव तथा भूस्खनल जैसी समस्यायें उठती रही. 1868 के महादुर्भिक्ष में यह क्षेत्र इस प्रकोप से मुक्त रहा और मैदानी क्षेत्रों को यहाँ से अनाज भेजा गया. कमिश्नर रामजे ने लिखा- पहाड़ी किसान की तुलना भारत के श्रेष्ठतम किसानों से की जा सकती है, क्योंकि ये सदियों से पर्यावरण के साथ समन्वय बनाये हुये है. ऐसा प्रतीत होता है कि हिमालय क्षेत्र की खेतिहर अर्थव्यवस्था 1910 तक ज्यों की त्यों बनी रही.
प्रारम्भ में किसान असुरक्षा के कारण अस्थिर तथा घुमक्कड़ थे. कुछ समय तक एक स्थान पर खेती करने के बाद दूसरे स्थान की तलाश में निकल जाते थे. फसल परिवर्तन की परम्परागत व्यवस्था इस क्षेत्र के लिये अत्यन्त उपयुक्त थी, बशर्ते भूमि की उर्वरता बनी रहे. ऊंची ढलानों में पैदावार कम होती थी जबकि घाटियों की भूमि अत्यन्त उपजाऊ थी, जहाँ भूमि का छोटे से छोटा भाग भी श्रम पूर्वक जोता जाता था. एटकिन्सन ने सोमेश्वर व भीमताल की घाटियों को सम्पूर्ण एशिया में सुन्दरतम व उर्वरतम बताया है. खस जाति के लोग, जो पश्चिमी एशिया से आये थे, मुख्यतः पशुपालन करते थे और अपने पशुओं को चराने के लिये उन्होंने पर्वतों की तलहटी में बसना श्रेयस्कर समझा. बाद में उन्होंने पशुचारण के साथ खेती को भी स्वीकार किया.
पर्वतीय क्षेत्र की सम्पन्नता को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि मैदानों से अनाज आयात करने का कोई संकेत नहीं मिलता उल्टे मैदानों को अनेक वस्तुयें निर्यात की जाती थी. जैसे हल्दी, अदरख, लाल मिर्च, घी, शहद, अखरोट, चाय, भेड़, बकरी, तिब्बती घोड़े इत्यादि. इसके अतिरिक्त अनेक कृषि वानिकी उत्पाद जैसे लकड़ी, रंग- रोगन, तारपीन, गोंद, मसाले, मादक द्रव्य, कस्तूरी, जड़ी-बूटी इत्यादि – भी निर्यात किये जाते थे. सन् 1872 में इस में 2490 कुन्तल ऊन का आयात किया गया और 1883 में लगभग 24966 कुन्तल गेहूँ तथा जौ तिब्बत को निर्यात किया गया.
(Agriculture in Uttarakhand History)
कुमाऊं में विभिन्न राजवंशों ने राज्य किया. विभिन्न जनजातियों के बीच निरन्तर युद्धों से खेती पर असर पड़ा और भूमि की उर्वरता क्षीण होती चली गयी. चीनी यात्री ह्वेनसांग, जो हर्ष के काल में भारत आया था, ने पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को देखकर लिखा कि यह अत्यन्त सम्पन्न है, भूमि उर्वर है तथा मुख्य फसलें है मोटा गेहूं, जौ, उवा तथा फाफर. लोग भेड़ व घोड़े पालते हैं तथा उनके प्रमुख व्यवसाय पशुपालन तथा युद्ध है. तराई क्षेत्र में भैंस की अर्नी जाति पाई जाती थी.
उत्तराखण्ड वासियों का धर्म बौद्ध एवं ब्राह्मण धर्म का एक विचित्र सम्मिश्रण है. अनेक स्थानीय ईष्ट देवी-देवताओं की उपासना की जाती रही है. जैसे खेतों में बीजों के अंकुरण तथा फसलों की रक्षा हेतु खेतों का देवता भूमिया (क्षेत्रपाल), वनों के संरक्षण का देवता सैम, पशुधन में वृद्धि का देवता चौमू, बधाण, कलबिष्ट इत्यादि.
यद्यपि भौगोलिक कारणों से पहाड़ों पर खेती योग्य भूमि अत्यन्त सीमित है (19 प्रतिशत) पर भूमि के आकर-प्रकार से संबंधित अनेक नामों से संकेत मिलता है कि यहाँ काफी पहले से खेती की एक नियमित व्यवस्था थी. निचले भागों की सिंचित भूमि को तलाऊं, ऊपरी भागों की असिचिंत भूमि को ‘उपजाऊ’, दलदली भूमि को ‘सिमार’, उर्वर घाटी को ‘गैर’, बंजर भूमि को ‘बॉज’, कृषि योग्य तीखे ढलानों को ‘रेलों’, भेड़ रखने के स्थान को ‘खोड़’ तथा अन्य पशुओं को रखने के स्थान को ‘गोठ’ कहा जाता है. भूमि को नापने की ईकाई ‘नाली’ (अर्थात दो किलो बीज को बोने के लिये आवश्यक स्थान लगभग 240 वर्ग गज) तथा ‘बिस्सी’ (एक एकड़ से 40 वर्ग गज कम) थे, जो कि एक वैज्ञानिक कृषि व्यवस्था का आभास देते हैं.
(Agriculture in Uttarakhand History)
उत्तराखण्ड प्रमुख फसलें वहीं हैं जो उत्तरी भारत के मैदानों की. अन्तर केवल इतना है कि ऊंचाई में होने वाली फसलें जल्दी तैयार नहीं होती हैं और कुछ मोटे दाने की होती हैं. प्रमुख फसल चावल है जिसकी अनेक किस्मों का वर्णन मिलता है. बासमती हंसराज, तिमिल, जमाल, अंजन, रोतुवा, कत्यूरी, धनिया, किरमुली, मोतिया, जोगियाना, चुनकुली, सालम, पलिया. गेहूँ की चार किस्मों का उल्लेख मिलता है. मोटे अनाज में कोटू, कौणि, मडुवा, मादिरा इत्यादि उगाये जाते हैं. इनके अतिरिक्त विभिन्न दालों तथा तिलहन की खेती भी होती है. एक और फसल उपल च्यूँडा का औषधिक महत्व है.
तिब्बत की सीमा से लगा हुआ विशाल हिमाच्छादित क्षेत्र भोट कहलाता है, जिसकी प्रमुख घाटियाँ हैं ब्यॉस, जोहार, दारमा, नीती और माणा इत्यादि. यहाँ केवल संकरी घाटियाँ कृषि योग्य हैं. शेष भाग चट्टानों, वनों तथा हिम से आच्छादित है. शौका (भोटिया ) मंगोलाई मूल उद्यमी लोग हैं, जिनका तिब्बत व नेपाल के साथ व्यापार पर एकाधिकार रहा है. ये लोग खेती की अपेक्षा व्यापार में अधिक रुचि रखते हैं. वर्ष में केवल एक ही मुख्य फसल उगाई जाती है तथा उपज भी साधारण रहती है. मुख्य फसलें हैं – मोटा गेहूँ, चूआ, भोटिया गेहूँ या नपल, जौ, जई, जंगली जई, फाफर इत्यादि. तूफानी हवाओं तथा हिमस्खलनों से बचने के लिये शौका गाँव ऐसे स्थानों पर बसे हैं, जहां पहाड़ों तथा चट्टानों की ओट हो. अपने पशुओं को चराने हेतु वे ऊंचे चरागाहों (बुग्याल) में ले जाते हैं. इतनी ऊंचाई में रहने वाले पशुओं के बाल बहुत होते हैं, जिनसे शौका पशमीना और ऊन के सामान बनाते और फिर इन वस्तुओं का निर्यात करते थे. 1909 में 4800 कुन्तल ऊन कुमाऊं से मैदानों को निर्यात किया गया था.
(Agriculture in Uttarakhand History)
कुमाऊं के दक्षिणी छोर पर पहाड़ों की तलहटी पर बसा तराई तथा भाबर का विशाल क्षेत्र है. भाबर जल रहित बन क्षेत्र हे, जो हाल तक कृषि के लिये अयोग्य समझा जाता था. इसके विपरीत तराई अत्यन्त नम एवं उपजाऊ भूमि वाला क्षेत्र है. पशुपालन तथा वनों के बीच खेती करने के लिये यह क्षेत्र अत्यन्त उपयुक्त थे परन्तु अनेक कारणों से लोग यहाँ रहने में हिचकिचाते थे. जैसे- बीहड़ वन, मलेरिया का प्रकोप, जंगली जानवरों तथा डकैतों का आतंक यहाँ सबसे पहले बसने वाले लोग संभवतः थारू व बोक्सा थे. वन सम्पदा से लालायित होकर अनेक बार मैदानी क्षेत्र के शक्तिशाली जमीदारों ने इस क्षेत्र पर अधिकार करने का प्रयास किया. अन्ततः ब्रिटिश सरकार ने यह निर्णय लिया कि इस क्षेत्र में खेती करने का अधिकार केवल पर्वतीय लोगों का हो.
कमिश्नर ट्रेल ने लिखा कि यदि मैदान का किसान इस क्षेत्र में पहाड़ी किसान के बराबर श्रम कर सकता है, तभी पहाड़ी किसान मैदानी किसान लिये स्थान छोड़े. एटकिन्सन के अनुसार तराई के कुछ वन अमेरिका के श्रेष्ठतम वनों से मुकाबला कर सकते थे. 1861 में सिंचाई के लिये एक व्यापक योजना बनाई गई. भूमि की उर्वरता के बावजूद खेती का तरीका पारम्परिक ही था. प्रमुख फसल चावल थी, जिसकी वर्ष में तीन किस्में बोई जाती थी – गांजा (अप्रैल-मई), बिझुरा (जून) तथा रसौता (जुलाई ).
कुमाऊं के अधिकांश शासक खेती के विकास के प्रति उदासीन थे. अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि भूमि की व्यवस्था सर्वप्रथम 1518 ई. में सोर के राजा भीमराज द्वारा की गई. सुविधा की दृष्टि से कुमाऊं के कृषि प्रशासन को विभिन्न शासकों के अन्तर्गत अपनाई गई नीतियों से मूल्यांकित किया जा सकता है.
(Agriculture in Uttarakhand History)
खेतिहर समुदाय विभिन्न वर्गों में बंटा था जैसे – थातवान (जमींदार), खैकर (कास्तकार), सिरतान (भूराजस्व का नकद भुगतान करने वाले) इत्यादि. सभी के अधिकार पृथक थे. भू-राजस्व के भुगतान के 36 तरीके थे. जैसे- नकद, अनाज, भेंट, बेगार आदि और इन्हें वसूलने के लिए दलाल होते थे. इसके अतिरिक्त वाणिज्य, वन उत्पाद तथा दुधारू पशुओं पर भी (घी-कर) कर देना पड़ता था. कुल मिलाकर किसानों को 68 प्रकार के कर देने होते थे – 32 शुल्क (बत्तीस कलम) और 36 प्रकार के राजस्व (छत्तीस रकम), जिसके फलस्वरूप उनके पास अपने लिये बहुत कम बचता था. साधारण भूमि पर फसल का 1/3 तथा उपजाऊ भूमि पर 1/2 भू राजस्व के रूप में देना पड़ता था.
उत्तराखण्ड पर मुसलमान शासकों का आधिपत्य नहीं रहा (केवल 1743 ई. में कुछ माह रुहेलों का शासन रहा जिन्होंने लूटमार और तबाही मचाई.) फरिस्ता (1623) लिखता है कि कुमाऊं का क्षेत्र उत्तर में तिब्बत से लेकर दक्षिण में सम्भल तक फैला हुआ था और यहाँ स्वर्ण व तांबे की प्रचुरता थी उत्तराखण्ड में गोरखों का शासनकाल (1790-1815) अत्यन्त क्रूर तथा निर्मम रहा. भू-राजस्व के परम्परागत नियमों को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया गया तथा करों को और भी बढा दिया गया. अत्याचारों से पीड़ित अनेक किसानों ने अपने गाँव छोड़ दिये और भूमि बिना जोती रह गई. इसके फलस्वरूप कृषि उत्पादन में अत्यधिक हास हुआ और राजस्व में भी कमी हुई. जिस समय एक छोटे घोड़े का दाम रु. 250 था उस समय गोरखे गुलामों को 10 से 150 रु. के बीच में बेच रहे थे. गोरखों के शासन काल में अत्यधिक करारोपण से बचने के लिये ग्रामीणों ने छत के ऊपर खेती प्रारम्भ कर दी.
(Agriculture in Uttarakhand History)
ब्रिटिश सरकार ने 1815 में गोरखों को हराकर कुमाऊं पर अधिकार कर लिया. (वैसे निचले हिस्सों को तो वह 1805 में ही गोरखों के आतंक से मुक्त कर चुकी थी.) यहीं से खेती के क्रमिक विकास का काल प्रारम्भ होता है. ट्रेल, बैटन व रामजे जैसे कुशल प्रशासकों ने खेती को समुचित वरीयता दी. सम्पूर्ण भूमि की पैमाइश व मूल्यांकन का कार्य नक्शों की सहायता से अत्यन्त सूक्ष्मता से किया गया. भूमि का वर्गीकरण किया गया. जैसे खेती योग्य, उजाड़, वन इत्यादि. ब्रिटिश सरकार ने किसानों में स्थिरता एवं सुरक्षा की भावना पैदा की. सिंचाई के लिये नहरों का निर्माण किया तथा जंगलों में बाघों के आतंक को कम किया गया. (1860 से 1888 के बीच कुमाऊं में 624 बाघों को मारा गया). फलस्वरूप भाबर व तराई के क्षेत्र अभिन्न रूप से पहाड़ों से जुड़ गये, जहाँ पहाड़ी किसान जाड़ों में खेती के साथ अपने पशु भी चरा सकते थे.
परन्तु इन सुधारों के कारण भूमि का दाम भी अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया. इसीलिये अधिक बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के प्रयास प्रारम्भ हुये. कृषि योग्य भूमि को पुनः वर्गीकृत किया गया जैसे – सिंचित, शुष्क (प्रथम श्रेणी), शुष्क (द्वितीय श्रेणी) इत्यादि. निर्धारण के लिये सिंचित भूमि की उपज, द्वितीय श्रेणी शुष्क की उपज की दोगुनी के बराबर मानी जाती थी. इसी प्रकार प्रथम श्रेणी शुष्क भूमि की उपज द्वितीय श्रेणी उपज से 1/3 मानी जाती थी. नियमों को ऐसा बनाया गया जो उस भौगोलिक स्थिति के निवासियों के लिये उपयुक्त हो. यद्यपि इससे भू-राजस्व में 81.43 प्रतिशत की वृद्धि अवश्य हुई. साथ ही साथ इस काल में अनाज का मूल्य कम हो गया और उत्पादन में वृद्धि हुई. अभिलेखों के अनुसार 55 कुन्तल गेहूँ, 45 कुन्तल धान, 3 कुन्तल मडुवा तथा 2 कुन्तल उरद प्रति एकड़ की उपज होने लगी. ब्रिटिश सरकार ने कुमाऊं को छोटी-छोटी इकाईयों में बाँट दिया. कुछ ग्रामों के एक समूह को पट्टी और पट्टियों के समूह को परगना कहा गया. भूमि के अधिकारों से सम्बन्धित नियमों में भी परिवर्तन किया गया. बाहर की फसल उगायी जाने लगी तथा पशुओं के मिश्रित प्रजनन के कार्यक्रम भी प्रारम्भ किये गये. 1840 के आस-पास चाय की खेती प्रारम्भ की गई. तथा 1880 में 3342 एकड़ भूमि पर 9000 कुन्तल उत्तम चाय का उत्पादन हुआ. उल्लेखनीय है कि 1800 में ईस्ट इण्डिया कम्पनी इस क्षेत्र में भाँग की खेती की संभावनाओं की ओर संकेत किया था, जिससे उच्च स्तर के रेशे प्राप्त हों. सन् 1882 में कृषि उत्पादों से दस लाख लीटर अच्छे किस्म की मदिरा (एल, वियर, पोर्टर आदि) का उत्पादन इस क्षेत्र में आर्थिक संभावनाओं को इंगित करते हैं.
(Agriculture in Uttarakhand History)
उत्तराखण्ड के रेशम का उपयोग आठवीं सदी में प्रारम्भ किया गया था. चीन से रेशम के कीड़े, तिब्बत व नेपाल के रास्ते मंगवाये गये थे. 1856 के कैप्टन हटन ने पर्वतीय क्षेत्र में रेशम उद्योग को बढ़ावा देने का सुझाव दिया परन्तु इस दिशा में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं हो सका. उत्तराखण्ड में चाय, रेशम, रेशा आदि मुनाफे वाली खेती का कैसे लोप हो गया इस विषय पर कृषि वैज्ञानिकों को पड़ताल करनी चाहिए.
अंग्रेज सरकार द्वारा उत्तराखण्ड की वन सम्पदा के दोहन के विरुद्ध 1911-17 के बीच विद्रोह उठ खड़ा हुआ. इसी के साथ कुली बेगार आन्दोलन प्रारम्भ हुआ जो कालान्तर में राष्ट्रीय आन्दोलन की मुख्य धारा में विलीन हो गया. ये दोनों किसानों के आन्दोलन थे. स्वतंत्र्योत्तर काल में खेती के विकास के मुख्य आधार बने जमीदारी प्रथा का अन्त एवं तराई भाबर क्षेत्रों में खेती का मशीनीकरण, जिसका श्रेय पंडित पंत को भी जाता है
उत्तराखण्ड में खेती के इतिहास की इस समीक्षा से स्पष्ट होता है कि हरित एवं श्वेत क्रांतियों का इस क्षेत्र के लिये कोई विशेष महत्व नहीं है. इसके पीछे अनेक कारण हैं जैसे – सामाजिक, राजनैतिक परिवर्तन, कृषि के मशीनीकरण में कठिनाई, छोटे-छोटे खेतों का बँटवारा, वन क्षेत्र में कमी, जनसंख्या में वृद्धि व पशुपालन (चारण) हेतु बुग्यालों में जाने की परम्परा समाप्त हो जाने से निचले पर्वतीय चारागाहों पर दुगुना बोझ पड़ा है. जिससे पर्यावरण असन्तुलन का संकट आ खड़ा हुआ है. भारत चीन युद्ध के बाद उत्तराखण्ड से तिब्बत व्यापार का बन्द हो जाना भी ऐसी घटना है जिससे यहाँ कृषि अर्थव्यवस्था एवं व्यापार पर निश्चित विपरीत प्रभाव पड़ा है.
(Agriculture in Uttarakhand History)
-भगवत जोशी
भगवत जोशी का यह लेख पहाड़ पत्रिका 1992 से साभार लिया गया है. पहाड़ हिमालयी समाज,संस्कृति, इतिहास और पर्यावरण पर केन्द्रित भारत की सबसे महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में है जिसका सम्पादन मशहूर पर्यावरणविद और इतिहासकार प्रोफ़ेसर शेखर पाठक द्वारा किया जाता है.
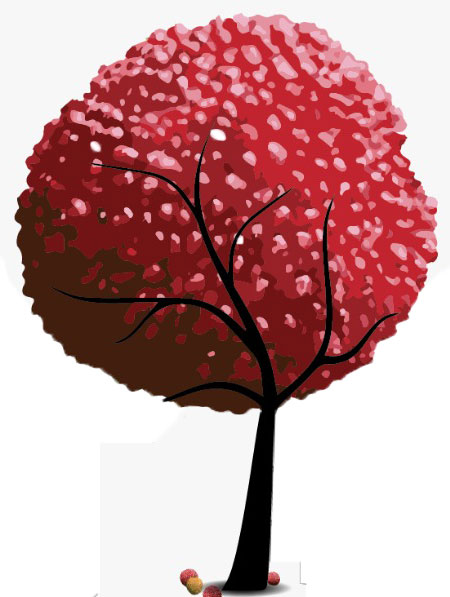
Support Kafal Tree
.
काफल ट्री वाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिये यहाँ क्लिक करें: वाट्सएप काफल ट्री
काफल ट्री की आर्थिक सहायता के लिये यहाँ क्लिक करें