इतिहास का विषय बन चुकी हैं उत्तराखण्ड के पर्वतीय अंचलों की पारम्परिक पोशाकें
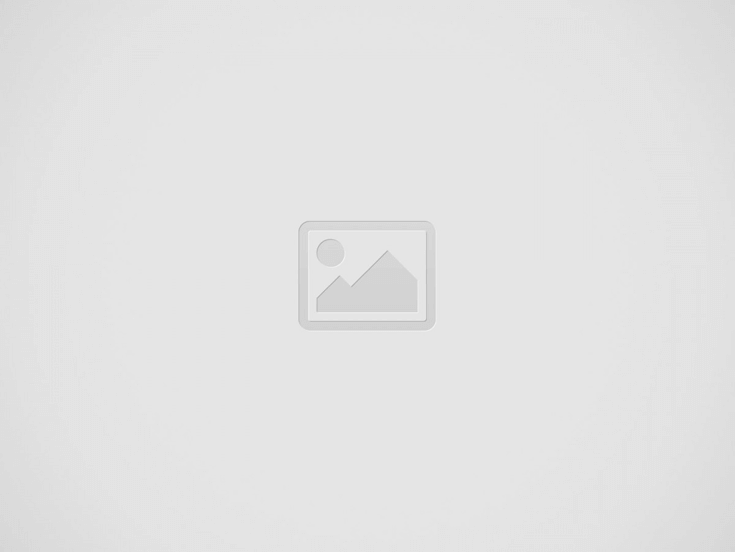

फोटो : स्व. कमल जोशी
विश्व के अन्य भागों की भाँति ही उत्तराखण्ड की संस्कृति भी अपने आप में समृद्ध रही है, परन्तु आधुनिकता की चकाचौंध में दिन-प्रतिदिन इसकी चमक धूमिल होती जा रही है. शिक्षा और जागरुकता का प्रभाव यहाँ के निवासियों को अपनी सांस्कृतिक विरासत से दूर ले जाने लगा है. परम्परागत वस्त्रों को पहनना तो दूर आज हम इनके विषय में जानते तक नहीं. ये पारम्परिक पोशाकें न केवल हमारी शीलता को बनाए रखती थीं, वरन् यहाँ कि जलवायु के अनुकूल कम साधनों में सुखी जीवन जीने में भी सहायक होती थीं. क्या आज की युवा पीढ़ी का दायित्व नहीं है कि वे अपनी जिम्मेदारियों को समझे और अपनी समृद्ध संस्कृति के अभिव्यंजक तत्वों को पुनर्जागृत करने का प्रयास करें? आइए जानते हैं इसी समृद्ध संस्कृति के पारम्परिक वत्राभरणों की कुछ रोचक जानकारियाँ—
(Traditional Dresses Uttarakhand History)
उत्तराखण्ड का उत्तरी सीमान्त क्षेत्र एक शीतप्रधान भूभाग होने के कारण, यहाँ के लोगों के परिधानों में ऊनी आवरणों एवं शीर्षावरणों का आवश्यक रूप से प्रयोग होता था. निर्धन जनता द्वारा स्थानीय स्तर पर प्राप्त प्राकृतिक संसाधनों से ही वस्त्र निर्माण किया जाता था. लोग भेड़ों से प्राप्त ऊन, जानवरों की खाल, पेड़ों की छाल, कपास से निकलने वाली रूई अथवा भांग के रेशों को कातकर वस्त्रों का निर्माण किया करते थे, जो पूर्णतः शुद्ध और प्राकृतिक होते थे. सामान्यतः पर्वतीय अंचलों में पुरुषों अथवा महिलाओं का परम्परागत परिधान लावा होता था, जो जाड़े में एक कंबलनुमा ऊनी कपड़े से सिर से पैर तक ढक लेने वाला एक शरीरावरण होता था, जिसे सूई-संगल से बांधे रखा जाता था. गर्मियों में सूती लावा (एक काली चादर) पहना जाता था. कालान्तर में पुरुष वर्ग में इसका स्थान लंगोट और मिरजई ने तथा महिला वर्ग में घाघरी व आंगड़ी ने ले लिया.
इसे भी पढ़ें : गायब हो गए हैं उत्तराखण्ड से बच्चों के परम्परागत बाल परिधान
पुरुष परिधान
पुरुषों के शरीरावरणों में मुख्यतया लावा, गाती, धोती, मिरजई, फतुही, लंगोट, सुराव, पजामा, जांघि, कमरिया, पगड़ी/टांका/साफा, टोपी इत्यादि हुआ करते थे. कुछ मुख्य पोशाकों की रूपाकृतियां इस प्रकार हुआ करती थी—
गाती
गाती ऊन अथवा भांग के रेशों को बुनकर बनायी जाने वाली चादर के समान होती थी, जिसे शीतप्रधान क्षेत्रों के निम्न-मध्यम वर्गीय पुरुष शरीरावरण के रूप में धारण करते थे. गाती को इस प्रकार ओढ़ा जाता था कि वह पूरे शरीर को ढक ले, अन्त में उसके दोनों सिरों को कन्घे पर बांस अथवा लोहे की सूईयों से अटकाया जाता था. ‘उत्तराखण्ड का लोकजीवन एवं लोकसंस्कृति’ नामक पुस्तक में प्रो. डी. डी. शर्मा कहते हैं कि कुमाऊँ में अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ क्षेत्रों के ’कुथलिया बोरा’ कहलाए जाने वाले लोग भंगेले की गाती पहनते थे. यह बड़ी मजबूत होती थी. प्रायः महिला-पुरुष दोनों इसे धारण करते थे.
धोती
यह लगभग 5 गज लम्बा बिना सिला हुआ एक आयताकार सफेद रंग का सूती कपड़ा होता था, जिसे अधिकांशतया उच्च वर्गीय ब्राह्मण एवं कुछ सम्भ्रांत लोग ही पहना करते थे. पूजा-पाठ, विवाह, नामकरण संस्कार, सामूहिक भोज आदि शुभ अवसरों पर अनिवार्य रूप से इसे पहना जाता था.
मिरजै या मिरजई
यह एक प्रकार का अंगरखा था, जो पूरी बांहो वाला तथा घुटनों तक लम्बा होता था. सामने से बन्द करने के लिए दोनों पल्लों पर दो-दो तनियाँ लगी रहती थी, जिन्हें आपस में कसकर बांध दिया जाता था. कहीं-कहीं इसे ‘कमरिया’ भी कहा जाता था. राजसी और समृद्ध परिवार के लोग पजामें के ऊपर इसे पहना करते थे, जो जामा कहलाता था.
फतुही या भोटू
फतुही उत्तराखण्डी पुरुषों का सबसे पसन्दीदा वक्षावरण था. इसे भोटी अथवा भोटुवा भी कहा जाता था. बिना बांहों वाला वास्कट फतुही का ही परिष्कृत रूप है, परन्तु फतुही को सामने से बन्द करने के लिए बटनों के स्थान पर कपड़े की घुंडियों का प्रयोग होता था.
लंगोट एवं सुराव या सुराल (पजामा)
पराम्परागत रूप से कुमाऊँनी लोग मिरजई अथवा गाती के साथ लंगोट पहना करते थे. धीरे-धीरे इसका स्थान सुराल अर्थात पजामे ने ले लिया. यह घुटनों तक ढीली तथा उसके नीचे एड़ी तक तंग होता था, ऊपर से नेफा मोड़कर नाड़े (इजारबन्द) से बांधा जाता था. इसका स्वरूप आधुनिक चूड़ीदार पजामे जैसा होता था. नीचे से तंग होने के कारण यह पैरों को ठण्ड से बचाये रखता था. पिछली पीढ़ी के लोगों के वस्त्राभरणों में अभी भी इसकी झलक देखी जा सकती है.
शीर्षावरण
हिमालय की तलहटी में बसा उत्तराखण्ड शीतप्रधान भूभाग होने से यहाँ के लोगों में शीर्षावरण का विशेष महत्व था. जहाँ एक ओर यह ठण्ड से बचाव के लिए आवश्यक था, वहीं दूसरी ओर इन्हें पुरुष की मान-मर्यादा का प्रतीक भी माना जाता था. सम्भ्रान्त लोग पगड़ी, टांका, साफा आदि बांधा करते थे, तथा साधारण जनसमुदाय टोपी का प्रयोग किया करता था. कोई भी व्यक्ति बिना शिरोवस्त्र के घर से बाहर नहीं निकलता था.
नारी परिधान
प्राचीनकाल में निर्मित नारी मूर्तियों को दृष्टिगत करने से ज्ञात होता है कि कत्यूरी शासनकाल में महिलाएं कंचुक (पूरी बांहों की कमर तक लम्बी अंगिया), खनुवा आंगड़ी अथवा चोली (केवल वक्षस्थल को आवृत करने वाली चोली), शॉल या दुपट्टा एवं शाटिका (साड़ी) को अंगीकृत करती थी. मध्यकाल में साड़ी का स्थान लहंगे अथवा घाघरे ने ले लिया. प्राचीन समय में यहाँ की नारी के परिधानों का स्वरूप कुछ इस प्रकार हुआ करता था-
घाघरा
घाघरा पर्वतीय नारी का अनन्य परिधान था, जिसे गजनिया (काला गाढ़ा अथवा छींट) से बनाया जाता था. आमतौर पर नौ पाट (पट्टियां) का घाघरा पहना जाता था, परन्तु समृद्ध परिवार की महिलाएं बारह पाट का घाघरा भी पहनती थी. इसमें नीचे की ओर 3-4 अंगुल की गोट लगाई जाती थी, जिसे लावण कहा जाता था. ऊपर की ओर इजारबन्द डालने के लिए नेफा/संजाप लगाया जाता था. इसका निर्माण स्थानीय दर्जी ही किया करते थे. वर्तमान में ‘घाघरा’ सिलने वाले कुशल दर्जी या तो नहीं रहे या अब वे सिलने में समर्थ नहीं हैं. प्रचलन में नहीं होने से अधिकांस दर्जी यह कला सीखने में रुचि नहीं रखते. मात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ही इस अप्रतिम परिधान की झलकियाँ शेष रह गई हैं, परन्तु बागेश्वर के दानपुर क्षेत्र की बुजुर्ग महिलाओं की पहली पसन्द आज भी यही घाघरा है. जौनसार-भावर में भी इसके परम्परागत स्वरूप को अभी भी देखा जा सकता है.
आंगड़ी अथवा चोली
घाघरे के साथ ऊर्ध्वांग में पहने जाने वाले वस्त्रावरण को आंगड़ी के नाम से जाना जाता था. प्रारम्भिककाल में यह खनुआ आंगड़ी अथवा खानड़ी कहलाता था, जो केवल वक्षावरण करने वाला होता था, तथा पीछे तनियों से बांधा जाता था. 19वीं शताब्दी के पश्चात् इसके स्वरूप में परिवर्तन आ गया और यह पूरी बाहों का कमर से गर्दन तक लम्बा बनने लगा, जिसमें अन्दर से अस्तर लगा होता था. सामने की ओर से बन्द करने के लिए बटन लगाए जाते थे. दोनों बाजुओं के कफ खुले रहते थे, उन्हें बन्द करने के लिए उन पर भी बटन लगते थे. सामने से दो जेबें होती थी. सामान्यतः निम्न-मध्यमवर्गीय महिलाएं मोटे कपड़े में, जबकि सम्भ्रान्त परिवारों की नारियाँ मखमल, सनील अथवा ऊन के आंगड़े बनवाती थी. शीतप्रधान क्षेत्रों में इससे शरीर भली भांति कसकर ढ़का रहता था, और अस्तर लगे मोटे कपड़े से बने होने के कारण ठण्ड से बचाव भी होता था. शुभ कार्यों के अवसर पर इसे मांगलिक परिधान माना जाता था.
धोती
धीरे-धीरे घाघरे के स्थान पर पुरुषों की भाँति महिलाओं द्वारा भी धोती का प्रयोग होने लगा, परन्तु दोनों की धोतियों में धारण शैली और रूपाकृति का अन्तर होता था. महिलाओं की धोतियाँ सूती अथवा मारकीन की रंग-बिरंगी कलाकृतियों वाली होती थी, जिसे वर्तमान साड़ी की भाँति पहना जाता था, परन्तु काम करने में सुविधा हेतु चुन्नटें निकालकर पल्ले को कमर पर इस प्रकार बाँधा जाता था कि पीछे का हिस्सा सिर पर रखा जा सके. कई महिलाएं इसे घाघरे के ऊपर सिर्फ कमर पर बाँधकर सिर पर भी रखा करती थी. समय बदला और धोती का स्थान विभिन्न प्रकार के कृत्रिम रेशे से बनी साड़ियों ने ले लिया. अब तो शुद्ध सूती कपड़े की बनी धोतियाँ विरले ही देखने को मिलती हैं.
पिछौड़ा या पिछौड़ी
समूचे कुमाऊँ में शुभ अवसरों पर महिलाएं तेज पीले रंग पर गहरे लाल रंग से रंगी ओढ़नी पहने देखी जा सकती हैं, जो रंगाई पिछौड़ा अथवा रंगवाली पिछौड़ी कहलाती है. इसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है. प्राचीनकाल में जब वस्त्राभरण सुगमता से उपलब्ध नहीं होते थे, तब पिछौड़े का निर्माण घर पर ही किया जाता था. इसके लिए रंगों का निर्माण भी लोग गृहोपयोगी संसाधनों से घर पर ही कर लिया करते थे. पीला रंग किलमोड़े की जड़ को पीसकर अथवा हल्दी से तैयार किया जाता था. लाल रंग बनाने के लिए महिलाएं कच्ची हल्दी में सुहागा और नींबू निचोड़कर दो-तीन दिन के लिए रख छोड़ती थी, तत्पश्चात उस मिश्रण को नींबू के रस के साथ पका लिया जाता था. इस प्रकार लाल रंग भी तैयार हो जाता था. लगभग तीन मीटर लम्बा और सवा मीटर चौड़ा सफेद सूती कपड़ा लेकर उसे गहरे पीले रंग में रंग लिया जाता था. रंगने के बाद उस वस्त्र को छाया में सुखा लेते थे. रंगांकन के लिए कपड़े के बीच में केन्द्र स्थापित कर खोरिया अथवा स्वास्तिक चिन्ह बनाया जाता था. इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता था कि स्वास्तिक एकदम बीचोंबीच बने, अन्यथा सम्पूर्ण रंगांकन खराब हो सकता था. अतः कुशल महिलाओं द्वारा ही रंगांकन कार्य किया जाता था. इसके चारों कोनों पर सूर्य, चन्द्रमा, शंख, घंटा आदि अलंकृत किए जाते, तदुपरान्त ताँबें अथवा चाँदी के सिक्के पर कपड़ा लपेटकर बांध लिया जाता तथा उसे लाल रंग में डुबोकर निश्चित दूरी पर वृत्तों का निर्माण किया जाता था. वर्तमान में औद्योगीकरण के प्रभाव के चलते मशीनों में कृत्रिम रंगों द्वारा बने पिछौड़ों से उत्तराखण्ड के बाजार पटे पड़े हैं और घर पर पिछौड़ा रंगने की कला धीरे-धीरे दुनियाँ से विदा लेती उत्कृष्ट पीढ़ी के साथ ही समाज से विदा लेने लगी है.
मूल रूप से मासी, चौखुटिया की रहने वाली भावना जुयाल हाल-फिलहाल राजकीय इंटर कॉलेज, पटलगाँव में राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता हैं और कुमाऊँ विश्वविद्यालय से इतिहास की शोध छात्रा भी.
हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें: Kafal Tree Online
काफल ट्री वाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिये यहाँ क्लिक करें: वाट्सएप काफल ट्री
काफल ट्री की आर्थिक सहायता के लिये यहाँ क्लिक करें
Recent Posts
पहाड़ से निकलकर बास्केटबॉल में देश का नाम रोशन करने कैप्टन हरि दत्त कापड़ी का निधन
हरि दत्त कापड़ी का जन्म पिथौरागढ़ के मुवानी कस्बे के पास चिड़ियाखान (भंडारी गांव) में…
डी एस बी के अतीत में ‘मैं’
तेरा इश्क मैं कैसे छोड़ दूँ? मेरे उम्र भर की तलाश है... ठाकुर देव सिंह…
शराब की बहस ने कौसानी को दो ध्रुवों में तब्दील किया
प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत की जन्म स्थली कौसानी,आजादी आंदोलन का गवाह रहा कौसानी,…
अब मानव निर्मित आपदाएं ज्यादा देखने को मिल रही हैं : प्रोफ़ेसर शेखर पाठक
मशहूर पर्यावरणविद और इतिहासकार प्रोफ़ेसर शेखर पाठक की यह टिप्पणी डाउन टू अर्थ पत्रिका के…
शराब से मोहब्बत, शराबी से घृणा?
इन दिनों उत्तराखंड के मिनी स्विट्जरलैंड कौसानी की शांत वादियां शराब की सरकारी दुकान खोलने…
वीर गढ़ू सुम्याल और सती सरू कुमैण की गाथा
कहानी शुरू होती है बहुत पुराने जमाने से, जब रुद्र राउत मल्ली खिमसारी का थोकदार…


