कलबिष्ट : खसिया कुलदेवता
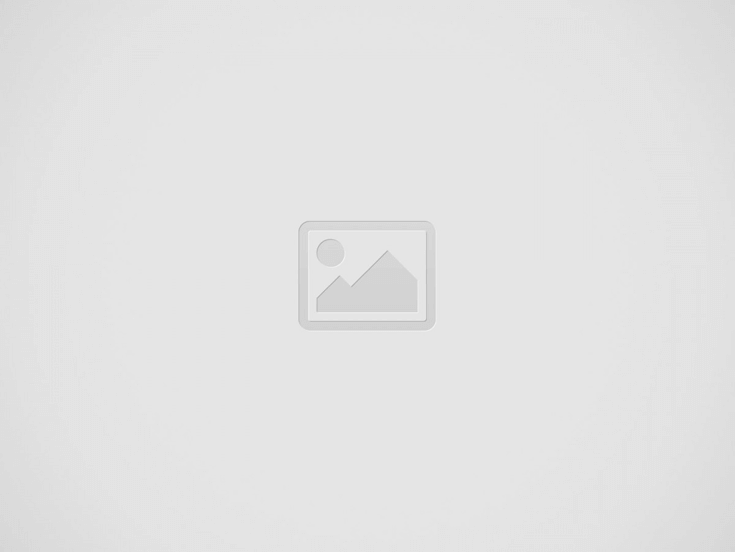
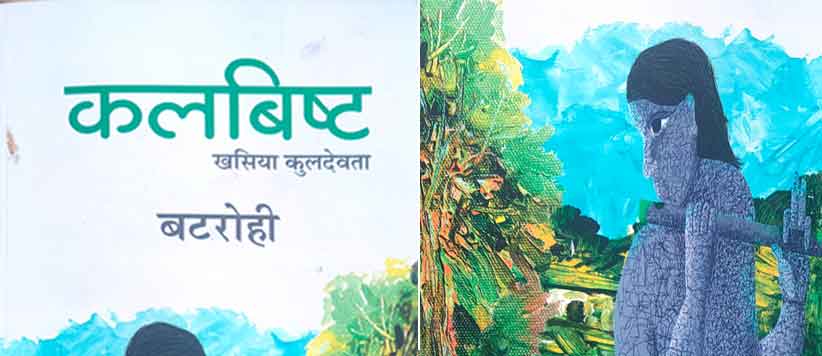
किताब की पैकिंग खुली तो आकर्षक सा मुखपन्ना था, नीले से पहाड़ पर सफेदी के स्ट्रोक, गाढ़े हरे पीले बसंती रंग के साथ लालिमा लिया अधेड़ सा एक पेड़ और उसके बगल में देवालय. इस परिदृश्य से उभरती हुई हाथों में बंसी थामे नील वर्ण मूरत जिसकी देह प्रस्तर शिला सी खुरदरी है. वक़्त के थपेड़ों ने उसकी त्वचा को खुरदरा भोंतरा बना डाला है.
(Kalbisht Khasiya Kuldevta Book Review)
कहानी की यह शुरुवात है जिसने लिखी उसके अवचेतन में धंसी. जिसकी रहस्यमय बातें पूर्वजों के मुंह से सुनी और उन बातों को अपने परिजनों के व्यवहार में तलाशने का जतन भी किया. साथ-साथ अपने पूर्वजों-खशों को लेकर उठाये गए संदेह और जिज्ञासाएँ, जिनकी संकल्पना वह अपने पुरखों को भूत-प्रेत-चुड़ैल जैसी अति मानवीय ताकतों के रूप में करते भी आए.
“कभी अतीत में मेरा एक पुरखा कलबिष्ट भी जन्मा था. इन्हीं जड़ों में से, जिसकी एक शाखा के रूप में मेरा भी अस्तित्व सामने आया था. कलबिष्ट तो ग्वाला था जो अपनी सदाशयता के कारण देवता बन गया… एक अभिशप्त देवता, मगर मेरी विडंबना यह थी कि मुझे ऐसे परिचय के साथ जोड़ दिया गया जिसकी अपनी कोई पहचान ही नहीं बन पाई.”
लोकदेवता के बहाने उत्तराखंड का सांस्कृतिक आख्यान रचते उनकी स्वीकारोक्ति है कि ‘यह इतिहास नहीं है… निजी और सामूहिक स्मृति के माध्यम से अपने समय और समाज को समझने का प्रयास भर है. यह आत्मकथा नहीं है, फिक्शन भी नहीं, हालांकि इसे रचने में आत्मकथा और फिक्शन की मदद ली गई है….
घुटा हुआ सिर और उसके बीचों-बीच खिचड़ी बालों की चुटिया, माथे पर रोली -चन्दन का त्रिपुण्ड, बाएँ कंधे पर लटकी तीन पल्ले की जनेऊ और दाहिने हाथ की कलाई पर रंगीन धागे का रक्षा सूत्र.ऐसे वस्त्र विन्यास में लक्षमण सिंह बिष्ट ‘बटरोही’ को देख मित्र परिचित पूछते हैं तो वह चेहरा लटकाये हड़बड़ाहट से हकलाते जवाब देते हैं – बहुत पुराने जमाने की दादी थीं, चल बसीं.
नहीं मालूम कि वह कब मरी, कभी न कभी तो मरी होंगी. हरिद्वार के कुशाघाट पर उनके संस्कार के लिए बिरादरों के साथ खड़े, उभरते कई अनुत्तरित सवालों का दंश झेलते वह सम्बोधन रह रह उभरने लगता जिसे बचपन से अभी तक न जाने कितने बार सुना.सुन कर हंसी में टाल दिया, मुस्कुराते हुए सह लिया. यह शब्द जो गुस्से और व्यंग में, गाली और उपेक्षा में और कभी कभी अप्रत्याशित प्रशंसा में कान से टकराता.
यह शब्द था “खसिया”.
बच्चा था कोई गलती होती तो सयाने मुझे मूढ़-बौड़म सिद्ध करने के लिए कह डालते खसिया, जवान होने लगा गुस्से में अपने से ज्यादा ताकतवर को पटक डालने में प्रशंसा से कहा गया कि ये है पक्का खसिया. ऐसी औलाद जो शेर सी ताकत रखे पर दिमाग से हो पैदल.
दस पीढ़ी पूर्व की दिवंगत दादी का हाल में संपन्न अंतिम संस्कार. आज अपने ही घर के लोग इस शब्द से संबोधित करते लगे एहसास हुआ कि मेरी जड़ों में से ही मेरे एक प्रतिरूप का अंकुर फूट आया है. कभी अतीत में जो मैं ही था, मगर आज नहीं हूँ. बहुत प्रयास के बाद इससे मुक्त हुआ. एक नई जमीन पर खड़ा हुआ, नई पहचान के साथ. मैं एक विसंगति का हिस्सा बन चुका था जो मेरी वास्तविकता तो थी और जिससे मैं मुक्त हो जाना चाहता था. जन्म के साथ मिली मेरी यह पहचान मुझसे लिपटी ही रही. आज इस प्रशंसा भरी छवि के साथ जो व्यंगात्मक परछाई मेरे साथ चल रही है, चाहूँ-न चाहूँ मुझे स्वीकार तो करनी ही पड़ी. खसिया यानी खसों की संतति वह चेतना संपन्न प्राणी क्या मेरा प्रतिरूप है? जिनकी पहचान के लिए मैं व्याकुल हो रहा. क्या मैं उन्हीं वीर खशौं की संतान हूँ जो दुनिया की श्रेष्ठ वीर जातियों में शुमार है?
(Kalbisht Khasiya Kuldevta Book Review)
महाभारत के सभा पर्व में ‘खश’ का उल्लेख है अन्यत्र इन्हें ‘खस’, खष’, ‘कश’, ‘कुश’ भी कहा गया. शोध के अनुसार ‘खश’ अवैदिक आर्यभाषा का शब्द रहा जिससे तात्पर्य ‘मुख’, ‘विशिष्ट’, ‘राजा’, ‘प्रतिष्टित’, ‘महतो’ जैसा होना संभव है. फ़ारसी का जो ‘खास’ शब्द है वह इन लोगों की पदवी ‘खश ‘ से निकला. खश मेहनती, व्यवहारकुशल, राज्य प्रबंध में कुशल, वीर व लड़ाकू माने गए, तभी यह जाति जहाँ गई विजय व वैभव अर्जित करती रही, अपने नाम की मुहर लगाती चली. पूरा मध्य ऐसिया तब ‘खशगढ़’ कहलाता था.
‘खश’ जो मूलतः आर्यों के ही रक्त बांधव थे, वैदिक विधियों, अनुष्ठान व पुरोहित वर्ग के प्रति आस्था न रखने के कारण आर्य स्मृतिकारों, पुराणकारों व लेखकों ने इन्हें शूद्र (वृशल), म्लेच्छ, पिशाच आदि नामों से संबोधित किया. मनु ने इन्हें ‘पतित क्षत्रिय’ या ‘वृषल’ कह दिया तो महाभारत में पिशाचों की तरह नरभक्षी. संत कवि इन्हें नीच व म्लेच्छ कह गए.
इतिहासकारों ने महत्वाकांक्षी सम्राटों की रणविजय में लड़ाकू वीरों का इन्हें स्थान तो दिया पर इनके युद्ध कौशल व शौर्य का उल्लेख नहीं किया. प्रागैतिहासिक काल में खश काश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड से नेपाल तक फैली एक जाति थी. यह हवाला एटकिंसन ने अपने गजेटियर में दिया और कहा कि खश देश यहाँ पर सिवाय कुमाऊँ के अन्य नहीं हो सकता तो शेरिंग ने लिखा कि खश भारत के सभी हिस्सों में हैं, कहीं ये बौद्ध हैं, कहीं मुसलमान तो कहीं हिन्दू. सर हेनरी इलियट की राय में खशों का सम्बन्ध काबुल के कटोरवंशी हिंदी राजा कनक और उत्तराखंड के कत्यूरियों से रहा तो ए.ब्राउन अपनी किताब ‘संप्रदाय और जातियाँ में लिखते हैं कि नेपाल में राजपूतों के बाद खस, फिर गुरंग, मगर और फिर सुनवार श्रेष्ठ गिने जाते. राय बहादुर पातीराम के अनुसार पहले कुमाऊं और गढ़वाल में खस ज्यादा थे.
एक पुरानी किम्वदंती है, ‘केदारे खस मंडले’. राय बहादुर धर्मानंद जोशी के हिसाब से पुराने क्षत्रियों व राजपूतों के अलावा यहाँ कुछ खसिये हैं जो प्राचीन जातियों के अवतंस हैं जिनमें शायद क्षत्रिय रक्त नहीं है. उनका पद डूमों से ऊँचा है. वे साधारणत: राजपूतों में शामिल किये जाते. वे सीधे-साधे और सच्चे होते हैं. वे खूब मजबूत होते हैं.
(Kalbisht Khasiya Kuldevta Book Review)
बैरिस्टर लक्ष्मी दत्त जोशी ने अपनी किताब में लिखा कि खश जाति बड़ी लड़ाका और गुस्सेबाज थी. आर्यों के रीति रिवाजों के साथ इनका सम्मिश्रण होता रहा और एक समय बाद दोनों की सांस्कृतिक परंपराओं में भेद करना मुश्किल हो गया. वे आज के आर्यों के सांस्कृतिक उत्पाद नहीं हैं, एक ओर उनमें आर्यो का सांस्कृतिक अनुकरण है तो दूसरी ओर उनकी विशिष्ट परंपराओं के प्रति जबरदस्त आक्रोश… मगर ऐसा कैसे हो गया कि आज के खश, जो मुख्य रूप से जाति-विहीन समाज थे, एक ही जाति की पहचान के रूप में सिमट गए और उस शब्द का आशय भी उसकी मूल गरिमा के अनुरूप न होकर व्यंगात्मक और अपमाजनक हो गया.
दस-पंद्रह पीढ़ी पहले की एक पुरखिन का श्राप जिसका अनिष्ट अब भी बिरादरी के परिवार लगातार भुगत रहे हैं. भूत-प्रेत पूजा पाठ में अंध विश्वास न रखने के बाद भी जब यह संकट न टला तो पुश्तैनी गाँव में जागर लगा. डंगरिये ने बताया कि पीढियों पहले थोकदार बुबू से ऐसा कुकर्म हुआ कि जिन्दा गाढ़ दिया घर के पिछवाड़े ‘ख्वाप ‘में. मेनका सी सुंदर उस विधवा को जो उनसे गर्भवती हुई. आज भी तड़पती वह अभागी औरत चीख रही है. सैकड़ों सालों से मैं अपने ही खून और पीब से भरी वैतरणी में गले-गले डूबी हूं… छोटी थी तब ऐसे पुरुष को सौंपी गई जिसमें अपने पति की छवि देख न पाई जब समझने की वय हुई तो वह मर गया. फिर ओठों पर थिरकती बिणई को सुनता मेरा चचिया ससुर जिसने मुझसे कहा कि सारे गाँव के सामने मैं उसे ससुर कहूं. सम्मान दूं पर बिस्तर पर उसका ही आदेश चलेगा.
(Kalbisht Khasiya Kuldevta Book Review)
वर्षों से चली आ रही बार-बार जुड़ती-कटती इस कथा में लोकजीवन ने न जाने कितनी बार कथाओं और चरित्रों को बदला. विसंगतियां पैदा की. द्वन्द हुए.
बहुत समय बीते कत्यूरी काल का पुरखा कलबिष्ट लोकजीवन में जाति, धर्म, संप्रदाय, ऊंच-नीच से परे कुमाऊँ के लोकदेवताओं की पांत में एकता का संदेशवाहक रहा था. कत्यूरी राजाओं द्वारा अपने अधिकार छीने जाने से आहत बोहरा जाति के वंशज झूंसी से चंद्रवंशी चंदेल राजा के भाई सोमचंद को पहाड़ ले आए जिसने चम्पावत पुरी को अपनी राजधानी बनाया. उनके साथ आये पांडेय ब्राह्मण राजपुरोहित आचार्य हरिहर जिन्होंने स्थानीय समाज का सामाजिक स्तरीकरण कर उसे वर्णों में बांटा व स्थानीय ब्राह्मणों व क्षत्रियों को निचले स्तर की जाति का दर्जा देते उन्हें ‘खश ब्राह्मण’ व ‘खश राजपूत’ नाम दिया. कुलीन ब्राह्मण उनके व कुलीन क्षत्रिय राज-परिवार के लोग ही समझे गए. हरिहर पांडे के वंशज बाद में अल्मोड़ा के पाटिया गांव में बसे. इनमें सकराम पांडे सोमचंद के वंशज राजा दीप चंद का दीवान था जिसकी पत्नी कमला अपूर्व रुपवती थी. वह बिनसर की पहाड़ी और कफड़खान की घाटी पर बांसुरी की तान से प्रकृति व जीवों को सम्मोहित करते गाय भैंस जंगल में चराते ग्वाले खूबसूरत युवा बलशाली मल्ल कलबिष्ट के प्रति आसक्ति से भर गई. अपनी रुपसी पत्नी की एक ग्वाले से आत्मीयता नौलखिया पाण्डे से कब तक छुपती. उसने कलबिष्ट को अपने रास्ते से हटाने के लिए सारे उपाय किये. संपत्ति झोंक दी, कलबिष्ट के जीजा व बहिन को प्रलोभन दिया, तांत्रिक व जादूगर बुला षड़यंत्र रचे पर कमला कलबिष्ट से मिल कर रही. कमला ने कलबिष्ट से एक वचन माँगा.
अब यह रहस्य ही है कि अपूर्व सुंदरी कमला जिसके पति उच्च पदस्थ अतुल संपत्ति के स्वामी हैं को मुरली की उदास धुन सुनाने वाले मल्ल देहयष्टि वाले आकर्षक भावुक खशिए युवा कलबिष्ट ने ऐसा कौन सा वचन दिया जिसके कारण उसे अपनी प्रेयसी की सुन्दर देह ही नहीं, अपना निर्मल मन और गठीली देह भी गंवानी पड़ी. मारा गया वह बलशाली मल्ल भितरघात से. छल से. प्रपंच से.
कलबिष्ट को आज भी सारे इलाके में परोपकारी लोक देवता के रूप में पूजा जाता है. ऐसा क्या था उस वीर खशिए में कि लोग उसकी विनती करते हैं उसकी पूजा करते हैं.
(Kalbisht Khasiya Kuldevta Book Review)
ओ रे कल्याण बिष्ट, तू जो कोटयूड़-मटयाव गांव में मल्ल के रूप में पैदा हुआ… ओ रे अभागे तू इस धरती पर हमें धोखा देने के लिए पैदा ही क्यों हुआ रे! असमय हमको छोड़ कर चला गया…
…तू बारह बिसी दूधारू और बारह बिसी गर्भिणी भैंसों, चनिया खस्सी, बिनुआ-सेतुवा बैलों, लखमा बिलाव और हिलुआ-तिलुआ बकरों की अपनी फौज को हाँकता चल पड़ा है बिनसर वन की ओर… अलख जगाती बिणई तेरे होंठों पर है, जुड़वाँ मुरली कमर में खुँसी है, घुँघरू बँधी खन-खनाती दराती हाथों में है, कंधे पर रतनार कमली लटकी है, शरीर पर मोटे ऊन का अंगरखा पड़ा है… वाह रे मेरे स्वामी कलबिष्ट, मैं तेरी बलिहारी जाऊँ!
जब सूरज का चेहरा धरती के क्षितिज को छोड़ चुका, तूने कमर में खुँसी अपनी रंगीली जुड़वाँ बांसुरी निकाली और मधुर तान छेड़ी… उदास पहाड़ी धुन. ओ रे कलबिष्ट! तूने जब अपनी मुरली से वैराग्य भरी तान फूंकी तो सारी धरती ही जाग गई, डयोड़ी पोखर के सुपिलाकोट में सोए सकराम पांडे के बाईस भाई जाग गए… बांसुरी की तान को सुन कमला बोराणज्यू का मन तेरे पास आने को मचलने लगा. कमला का मन तो तुम्हारे पास गिरवी है रे कल्याण बिष्ट. तुम्हारा मन सकराम पांडे के पीछे क्यों नहीं भागता कमला?
(Kalbisht Khasiya Kuldevta Book Review)
आमने सामने के दो पार्श्व. नदी के दो पाट. धरती के दो सिरे : कोट् यूड़ का कलबिष्ट और पाटिया की कमला महारानी… मिल कर एक हो गए. भितरघात कर गया कलबिष्ट का जीजा लछम, नौलखिया पांडे ने बिनसर का राजा बना देने का भूत जो भर दिया था कपाल में. जिस बांकुरे पर जादू टोने, चौराहे की धूल, बकस्वाड़ी की जादुई विद्या न चली उसकी बलिष्ट मल्ल देह अपने सगे रिश्ते वालों की बातों में आ दसों दिशाओं को गुंजाती ‘खच्च ss’ की आवाज के साथ दो भागों में कट गई.
कलबिष्ट का सिर उसकी देह से अलग हो गया है रे… ओ मेरे बाबू, कैसे फट कर अलग हो गया इस वीर का सिर उसकी देह से. जा छटका दूर बिनसर के जंगल में मेरे बाबू… उसका धड़ गिरा कफड़खान के गैराड़ मोड़ पर ओ मेरे बाबू. अब उसका कोई ग्वाल-गुसें नहीं, उसके मवेशियों का कोई रखवाला नहीं… उसके हाथों उसकी घुँघरू लगी दराती दूर छिटक कर गिर गई है… यह धरती पुत्र कलबिष्ट अब धरती की ही शरण चले गया है ओ मेरे बाबू!
बिनसर घाटी के गैराड़ मोड़ पर सोई हुई कलबिष्ट की सिर कटी भारी भरकम देह तब से आज तलक ज्यों-की-त्यों पड़ी हुई है. आज तक लोग उसी जगह पर मंदिर चिन कर उस अधूरी देह को पूजते चले जा रहे हैं. छिटका हुआ सिर कफड़खान तिराहे के मोड़ पर छोटी-बड़ी घंटियों लिए मनौती मांगते लोगों के लिए आस्था का प्रतीक बन गया है जहाँ अन्याय के खिलाफ अर्जी लगती है न्याय के लिए, सुरक्षा के लिए.
सुना है कि कलबिष्ट का जागर जब अपने आखिरी चरण में होता है तो उसका अवतार डंगरिये के रूप में नाचना छोड़ अट्टहास कर उठता है. गुस्से से भरा भूत की तरह चिल्लाने लगता है. पूछता है, “ओ रे सकराम पांडे, मैं तो कमला बौराणज्यू को, जो मेरे संगीत की आत्मा थी, उसका एकांत लौटाने जाता था. अपनी उदासी को वह पूरी तरह मेरे संगीत में सहेज भी न पाई कि तूने उसकी आत्मा ही छीन ली… तुझे यह भ्रम कैसे हो गया रे नौलखिए, कि आत्मा की भी जाति होती है, अरे नासमझ विवाह के बाद उसकी आत्मा को भी तूने अपनी जाति के रूप में खरीद लिया था रे?
(Kalbisht Khasiya Kuldevta Book Review)
कहते हैं कि ये बोल वचन कर डंगरिये की देह से निकल कलबिष्ट की आत्मा अपनी वास्तविक देह में प्रकट हो जाती है और अट्टहास कर मंदिर में धधकती धूनी में कूद जाती है… तभी अग्नि की लपटों के बीच से कमला बौराणज्यू प्रकट होती हैं और उगते सूर्य से दमकते कलबिष्ट का हाथ पकड़ अप्सरा की भांति बिनसर वन की वादियों में खो जातीं हैं.
कलबिष्ट के रहस्यमयता के साथ बांची कथा के जागर को सुन बटरोही इस पक्ष को ले अपनी असहमति प्रकट करते हैं कि इसे रोचक उत्तेजक प्रेमकथा का रूप क्यों दिया गया. यहाँ कलबिष्ट को उसी पुरोहिती परम्परा का हिस्सा बना दिया गया जिसके समानांतर एक आम पहाड़ी आदमी के मूल्यों को जमीन देने के लिए कलबिष्ट ने सारा जीवन संघर्ष किया. डाना गोलू का वह मंदिर, जहाँ कलबिष्ट की सिरकटी देह पड़ी है, उसे पुरोहिती धंधा करने का जरिया बना दिया गया. वहाँ बिखरी काले रंग की शिलाओं को कलबिष्ट की मृत्यु के बाद सदमे से मरी भैंसों के रूप में पूजा जाने लगा. मंदिर के गेट पर जो कथा लिखी है उसमें कलबिष्ट के बदले नौलखिया पांडे को ‘सम्राट पांडे’ कह नायक बनाने का प्रयास किया गया और तो और ‘पांडे जी’ द्वारा कलबिष्ट की हत्या को ‘गलतफहमी का शिकार’ कहा गया. मंदिर में कलबिष्ट देवता बना थाप दिया जहाँ वह धर्म के ठेकेदारों के हाथ की कठपुतली बना अंधविश्वासों से जकड़े निरीह पहाड़ी समाज को नचा रहा.
इतिहासकार बद्री दत्त पांडे ने तो कथा का मूल स्वरूप ही उलट दिया जहाँ नौलखिया पांडे के संबंधी श्री कृष्ण पांडे के साथ चली अपनी दुश्मनी में कलबिष्ट को मोहरा बनाता है, पत्नी से हुए प्रेम के कारण जीजा लछम सिंह से नहीं मरवाता. कलबिष्ट को एक अफवाह का हवाला दे स्त्री के आकर्षण से जोड़ा गया है पर वह नौलखिया पांडे की पत्नी नहीं उसके बैरी श्री कृष्ण पांडे की बताई गई. बद्री दत्त पांडे की कथा में कलबिष्ट की छवि को धूमिल करने की नीयत साफ है तो वहीं कमला पंडिताइन की जातीय विशिष्टता को सुरक्षित रखने का प्रयास भी. बद्री दत्त पांडे के इतिहास में अन्य जागर कथाओं में कोई बड़ा फेरबदल नहीं किया गया है सिवाय कलबिष्ट के संभवतः इस असमंजस से उबरने को कि एक उच्च कुलीन पांडे अपनी बहू-बेटी को एक ‘पतित क्षत्रिय’ की प्रेमिका के रूप में कैसे स्वीकारेगा?
बद्रीदत्त पांडे के द्वारा कलबिष्ट की कथा को विकृत रूप में प्रस्तुत करने के पीछे एक कारण यह भी समझ में आता है कि पढ़े-लिखे लोग यहाँ के लोक जीवन से कटे हुए थे. गाँव वालों के बीच न रहने व जमीनी समस्याओं पर उनसे संवाद न होने की दशा दिखाई देती रही. जो बात-चीत होती भी वह एकतरफा व पूर्वाग्रह से ग्रस्त होती. पढ़े लिखों की निर्णायक भूमिका में उनके आदेश जिनका अनुपालन आम जनों के लिए बाध्यता बन जाती थी तो साथ ही शासन व आम आदमी के बीच के दुभाषिये भी यही रहे. संभवतः इसी कारण उन्होंने इतिहास का मनमाना जातिवादी पाठ किया. यहाँ की भाषा-संस्कृति से अनभिज्ञ अंग्रेज प्रशासकों ने इन्हीं से पूछ-ताछ कर विवरण रचे. उस पर संस्कारों में पले समाज में वर्ण की सापेक्षिकता भी ऐसी कि यदि वह ब्राह्मण नहीं है तो उसके पास ज्ञान और अध्ययन को एक स्वाभाविक संस्कार के रूप में अपनाने का विकल्प है ही नहीं.
(Kalbisht Khasiya Kuldevta Book Review)
कलबिष्ट की यह गाथा धर्म और सामंती शोषण से घिरे उत्पादक वर्ग की पीड़ा का भी आख्यान है जहाँ धर्म शीर्ष पर विराजे ब्राह्मण का प्रतीक बन निचली जातियों का अपने हित में इस्तेमाल करता चला आ रहा है इस भ्रम के साथ कि वह उन्हें सांसारिक बंधनों से मुक्त करके मोक्ष का रास्ता दिखा रहा है.
बटरोही यह सोच कर परेशान भी होते हैं कि अपनी जिस ‘पुरानी दादी’ का संस्कार करने वह बिरादरी के साथ हरिद्वार के कुशाघाट जा श्राद्ध-तर्पण कर आए थे वह एक यथार्थ व्यक्तित्व था या एक मिथकीय चरित्र. इस पहेली को सुलझाने के लिए उनकी संगति इस तर्क से है कि आखिर इनके बीच फर्क क्या है? क्या मिथक कभी यथार्थ रहा होता है या मिथक अपने अतीत को न्याय संगत ठहराने के लिए अपनी कल्पना से गढ़ लिया जाता है? उनका खुद से सवाल यह भी है कि ‘सालों साल पहले मैं खसिया था, यह मेरे लिए गर्व का विषय है या शर्म का’? अगर समय एक परिवर्तन शील प्रक्रिया है तो सन्दर्भ के बदल जाने के साथ अर्थ भी तो बदल जाने चाहिये.
आज के अपने गाँव के हालात को जानने के लिए बटरोही लमगड़ा के लम्बे रास्ते बस पकड़ते हैं. गांव से पंद्रह किलोमीटर दूरी पर शहर फाटक है जो अल्मोड़ा शहर के दक्षिण पूर्व तो चम्पावत कस्बे के पश्चिम में बसा है. यहाँ ढलान में डोल से पनार नदी उभरती है और उभरी हुई पहाड़ी पर वीर मल्ल माधो सिंह सौन का इलाका डुंगरा और भनौली. बस रुकने पर सड़क के किनारे चाय की दुकान पर युवा दुकानदार से अपने गांव के हाल-चाल पूछते हैं तो वह तुरंत पलट कर यह बता उन्हें आश्चर्य में डाल देता है कि,’आजकल वहां ग्वालदेकोट की गोपुल्दी भुती रही है’.
…क्यों, आपने ग्वालदेकोट या गोपुल्दी का नाम कभी नहीं सुना? अगर आपने उसका नाम नहीं सुना तो फिर क्या जाना? चुड़ैल बन कर परेशान कर रखा है उसने. अजी यहाँ का बच्चा-बच्चा जानता है उसे. आपके ही गांव की धार वाले ग्वाल्दे कोट की रहने वाली हुई.
(Kalbisht Khasiya Kuldevta Book Review)
हां हां, अपने गांव का सबसे ऊँचा शिखर ग्वाल्देकोट. बचपन में गाय-बकरियों को चराने खूब गए वहां, लगता था यह हम ग्वालों का घर है.
ग्वाल हुआ ‘ग्वाला’ भी और ‘गोल्ल’ भी, और ‘दे’ हुआ देवता.
हां-हां, याद आया मल्ल देश के परोपकारी दबंग शेरुआ पैक की छोटी बहिन हुई वह गोपुल्दी जिसका ससुराल इसी शहर फाटक में हुआ. और किसी जमाने में वीर मल्ल शेरुआ पैक यहीं ग्वाल्देकोट में रहता था, जहाँ ऊँचे-ऊँचे पर्वत शिखर ही कोट कहे जाते. यहां भी तो चार कोट हुए उत्तर में ग्वाल्दे कोट, पश्चिम में त्युनराकोट, दक्षिण में शिमैलकोट और पूरब में द्योपड़ कोट… और इनके ठीक बीच नीचे घाटी में बहती पनार घाटी के किनारे शेरुआ पैक का किला घिंगरैल कोट, उसकी साढ़े सात बीसी भैंसें और गोपुली जो उसके साथ छाया की तरह लगी रहती.
क्या जमाना था वह, जब जल-जंगल-जमीन और धरती आसमान की नियामतें किसी एक की मिल्कियत न थीं. सब सामूहिक, कोई बंटवारा नहीं कोई जोर- जबरदस्ती नहीं. सारे पशु समुदाय के जिनकी देख-रेख मिल कर होती. कोई नियम नहीं. सब ऐसी बातें अपनाते जिनसे किसी का नुकसान न हो. प्रकृति के इस पूरे साम्राज्य को इस गांव के लोग एक इकाई समझते. जब प्रकृति का कोई कोप होता तो सामूहिक पूजा होती.
पूरे गांव की सामूहिक ऊर्जा जिसे शेरूवा पैक और गोपुल्दी नाम दे दिया गया था. मर्दों की सामूहिक ऊर्जा शेरूवा पैक में और सारी औरतों की ऊर्जा गोपुल्दी में. बच्चे उम्र बढ़ने के साथ खुद ही समझदार हो जाते, नीति-मर्यादा और श्रद्धा समझ जाते. यह सिलसिला पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलता रहता. जो भी अपने से बड़ी उम्र के लोगों को प्रिय था वह परंपरा की भांति चलता और जिसको सयाने ठीक न समझें उससे बच्चे परहेज करते. विशिष्ट आचरण वाले बुजुर्ग ‘सयाना’ या ‘बूढ़ा’ बन जाते. कुछ नया कोई कर गुजरता तो लोग खुशी से झूम जाते, गाते बजाते और कोई विपदा में होता तो उसे सुलझाने के जतन करते.
बुजुर्गों ने ही बताया फिर कि यह जमाना गुजर गया. आकाश और धरती का रंग बदल गया, हवा और पानी की रंगत बदल गई. शेरूवा पैक गाँव की सामूहिक छवि से टूट अलग-अलग इकाईयों में बंट गया अब वह सिर्फ शेरूवा पैक था और उसका अभिन्न हिस्सा रही गीपुल्दी उससे अलग पड़ गई… बुजुर्गों ने बताया कि ऐसा होना जरुरी होता है. आगे बढ़ने के लिए हमारी अपनी अलग चाल होती है और दुनिया की अपनी… दोनों के बीच भेंट कभी नहीं होती.
(Kalbisht Khasiya Kuldevta Book Review)
और नये जमाने की बात जब शेरुआ पैक के घर उत्सव मना. सामने की धार के गांव जाख का जख्वाल भीम जो आया गोपुली का हाथ मांगने. शेरूवा ने चाहा कि वह घर जमाई बन जाए साथ रहे पर भीम का पिता न माना. बहिन का घर बस जाए सोच, शेरूवा ने उसे जख्वालों के यहाँ भेज दिया. अपने व्यवहार बोल बचन से वह सबकी लाडली बनी और गांव की गोपुल्दी.
होनी किसके कहे टले? अचानक ही गोपुल्दी गायब ही गई. शेरूवा पैक तो बौरा गया. कहाँ नहीं ढूंढा, कितनी खोज खबर, एक-एक कोना छान मारा.
आई भी तो सपनों में यह बताने कि मेरे शौर (ससुर) ने मुझे धक्का दे दिया, मैंने नहीं मारी फटक. ईष्ट देव गोल्ज्यू ने मुझे पकड़ लिया तब से मैं बीच में लटकी हूँ. तुम भी उसे उसी धार से छटका देना हो ददा.
जखवालों के गांव पहुँच गया भीमकाय खशिया शेरूवा पैक और ललकारा गोपुल्दी के ससुर को कि निकल बाहर तू तो इतना गन्दा है कि तेरे खून को लुत लुते कीड़े भी न चाटेंगे, तू अगर न निकलेगा तो समझ ले, वहीं से तू पागलों की तरह फटक मारेगा और पहुंचेगा मेरे चनिया भैंसे के सींग के ऊपर. चनिया के सींग ने जख्वाल को छटका दिया उसे नीचे घाटी की तरफ जहाँ हूकते हुए सियार उसकी हड्डियां चबाने के लिए बेकरार थे… उसी दिन से उस जगह का नाम पड़ा सौर फाटक. किसी मंत्री ने इसका नाम धर दिया शहर फाटक. हुआ भी यही कि गांव के गांव खाली हो कर इस फाटक के रास्ते शहर की ओर भाग रहे. गाँव खाली होंगे तो शहर तो भरेंगे ही.
बड़ी कुशलता से बटरोही गांव से हो रहे पलायन के दंश का झटका देते हैं. बाहर से आए बिल्डरों के बने होटल और कोठियाँ. दारू की दुकान.सरकार की मिलीभगत. नई बनती सड़कें. सड़क के किनारे जंगल से कटी लकड़ी के गट्ठे बेचती गांव की औरतें. बंजर हो रहे खेत. राशन में बिकता गेहूं-चावल. अब कौन बचाए गांव!
तुम तो पढ़े गुने हो, तुम आबाद नहीं करोगे इस लोक को तो गाँवों को आबाद कौन करेगा? हमारे पुरखों का कितना खून-पसीना बहा इस धरती को बसाने में और तुम सब कितनी आसानी से इसे बंजर छोड़ शहर की ओर खिसक लिए. अब तो ऐसा लगता है कि जिसे तुम लाटा मान यहाँ छोड़ गए थे, वही आज तुम्हारे काम आ रहा है…
गांव तो बुला रहा है. पर कहाँ हैं वो पगडंडियाँ? लम्बी चढ़ाइयाँ. पैदल रास्ता वही पुराना, लेकिन सारा रास्ता बुझ सा गया है अब कोई चलता जो नहीं.
कफड़ खान होते गैराड़ मोड़ से ऊपर कलबिष्ट का मंदिर. चाय की काली केतली जलती भट्टी पर देख युवा दुकान वाले से बातचीत भी शुरू होती है. कलबिष्ट के बारे में पूछने पर वह बताता है कि ‘देवता ही ठहरा वो इलाके के कितने लोगों का भला करने वाला. ढाई सौ भैंस हुईं बल उसके पास’.
तुम दूध कहाँ से खरीदते हो?
दूध-दही तो आंचल कंपनी का लेते हैं. गाँवों का दूध भी वही ले जाते हैं.
इसी चाय की दुकान के बगल ही कलबिष्ट के सिर का मंदिर है. आरती का थाल, दो लोहे के त्रिशूल, पीतल की घंटी, चार लम्बे पत्थर के टुकड़े पिठ्या, रोली अक्षत, फूल पत्ती से छजे. पता नहीं इनमें कौन सा उसका सिर हो. भेंट वाला बक्सा जिसमें लाल अक्षरों में लिखा था, गोलू देवता की भेंट इस पात्र में डालें.
(Kalbisht Khasiya Kuldevta Book Review)
धड़ वाला मुख्य मंदिर यहाँ से दो किलोमीटर दूर गैराड़ मोड़ पर बड़े गेट के भीतर है. टाइल-संगमरमर लगा, रंग-रोगन पुता. आसपास चीड़ के बड़े पेड़ और चारों ओर काले रंग की शिलाएँ जिन्हें लोग कलबिष्ट की भैंसें मानते हैं जो उसके वध का दृश्य देखते बेहोश हो शिला में बदल गईं थीं. कलबिष्ट का मुख्य मंदिर जिसमें उसका धड़ एक आयतकार शिला के रूप में है, उसके ऊपरी हिस्से में त्रिपुँड बनाया है. चन्दन रोली से पुता, लाल कपड़े से ढका, सफेद फूल चढ़ा. सामने दिवार पर गुरु गोरखनाथ, गोल्ल, और कुमाऊँनी सामंतों वाली पारंपरिक पोशाक मिरजई और साफा धारण किये कलबिष्ट की मूर्तियां. पुरोहिती प्रतीक, चढ़ावा, धूप-दीप-प्रसाद की रस्म निभाते पंडित ज्यू. इस मंदिर के गेट के पास कलबिष्ट की आदमकद मूर्ति वाला नया मंदिर बन रहा जिसमें मूर्ति को मिर्जई-धोती पहना रखी है. उसका चेहरा भावहीन है, माथे पर त्रिशूल छापा, हथेली संत की तरह आशीर्वाद देती मुद्रा में तो बाएँ हाथ में कुल्हाड़ी. तीन डोरियों वाले कमरबंद पर एक बांसुरी और एक दराती खुँसी हुई. कानों में गोरखपंथियों के कुंडल और हाथों में कड़े.
सोचता हूँ वह पहाड़ी मल्ल कलबिष्ट कहाँ है यहाँ?
मंदिर के गेट पर कुर्सी पर बैठा मेज पर हिसाब-किताब व मंदिर समिति की नियमावली पत्रावली फैलाये, पास के ही हरिजनों के गाँव का निवासी बता दे रहा कि भक्त जन दूर-दूर से आते हैं, पाटिया वाले पांडे कम ही आते हैं. पंडित जी मिश्रा हुए. चढ़ावे की रकम के एक-एक पैसे का हिसाब रखते हैं हम. कोई हेर फेर नहीं. कोई इल्ज़ाम लगा सिद्ध कर दिखा दे… मैं समिति से उसी बखत इस्तीफा दे दूँ. हमारे पुरखों को कोई भी मंदिर के अंदर घुसने नहीं देता था, चाहे वह कलबिष्ट हो या सम्राट पांडेज्यू. इनको सब माफ हुआ. भिना-साले की लड़ाई से हमको क्या मतलब हो रहा.. क्यों पड़ें इनके बीच में! कर खाएँ जैसे चाहते हैं… हमें तो अपना हिस्सा घर बैठे मिल जाता है भैय्या!’
अतीत के ठूँठ और नये वर्तमान के बीच कैसे ताल-मेल बैठाया जाए?
मल्लदेश के खशिया देवता की गाथा है यह, उसी कलबिष्ट कुलदेवता की जिसे लोक-देवता के बहाने उत्तराखंड के सांस्कृतिक आख्यान के रूप में रचा गया जब दस पीढ़ी पूर्व की दिवंगत दादी के अंतिम संस्कार के क्रिया कर्म करने लेखक हरिद्वार के कुशा घाट पहुँच जाता है, अपने भीतर की छटपटाहट समेटे, उपज गए तनाव-दबाव और कसाव के बोझ से भरा जहाँ अपने परिवेश से उपजे सामाजिक व सांस्कृतिक स्तरीकरण में खशिया होने की हीनता ग्रंथि बार बार हिचकोले ले रही है.
कथा क्रम इसी सूत्र को पकड़ इतिहास के उन पेजों को बार-बार पलटता है जहाँ खश पराक्रम से भरे शूरवीर योद्धा थे पर तत्कालीन कई रीति रिवाजों से हट कर चलने से उनकी अनदेखी हुई. ‘खशियेकि रीस, भैंसेकि तीश’ में वह उनके पराक्रम के साथ कलुषित आवरण से देखे जाने का तथ्य जुटाते हैं तो ‘पैकेकि मौत, गजुआ लाटैक हात’ लोकोक्ति से अहंकारी व्यक्ति की कथा सुना उस घटना का ताना बाना बुनते हैं जिससे उनकी अपनी बिरादरी दस-पंद्रह पीढ़ी पहले की एक पुरखिन की हाय से श्रापग्रस्त बताई जा रही है. संस्कार न होने से जो प्रेत बनी रह गई. खस पूर्वजों का मातृ सत्तात्मक समाज और औरतों को भोग कर अत्याचार करने व जिन्दा जला देने जैसी घटनाएं. अपूर्व रूपसी खशिया बहू और प्यार करने वाले पुरुष का फणिधर नाग वाला रूप.. क्या वह रुपमती नागिन बन सहस्त्र वर्षों के बाद भी उन्हें परेशान कर रही? फिर मातृकाओं को दी जाने वाली अष्टकाएँ-किन्तु अविवाहित. जिस समाज में इनका उदभव था, उसकी दृष्टि में किसी पिता का होना जरुरी न था. आगे चल कर इनका विवाह किसी पुरुष देवता से होने लगा. उनके घालमेल भरे रिवाज. ये देवगण वीर और वो देवियाँ भी प्राण हर लेती हैं अगर इन्हें तुष्ट न किया जाए…
इसी ताने बाने में उलझी है कलबिष्ट की कथा, उसकी महिमा, उस पर घात और उसकी पुकार. उस वीर मल्ल की आपबीती जिसे उत्तेजक प्रेम कथा की तरह पेश करने पर लेखक बटरोही को आपत्ति है और इसे वह भारी विडंबना मानते हैं कि कलबिष्ट को आज उसी पुरोहिती परंपरा का हिस्सा बना दिया गया है जिसके समानान्तर एक आम पहाड़ी आदमी के मूल्यों को स्थापित करने के लिए उसका संघर्ष रहा.
डिस्क्लेमर- ये लेखक के निजी विचार हैं.
जीवन भर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुल महाविद्यालयों में अर्थशास्त्र की प्राध्यापकी करते रहे प्रोफेसर मृगेश पाण्डे फिलहाल सेवानिवृत्ति के उपरान्त हल्द्वानी में रहते हैं. अर्थशास्त्र के अतिरिक्त फोटोग्राफी, साहसिक पर्यटन, भाषा-साहित्य, रंगमंच, सिनेमा, इतिहास और लोक पर विषदअधिकार रखने वाले मृगेश पाण्डे काफल ट्री के लिए नियमित लेखन करेंगे.
इसे भी पढ़ें : अर्थ तंत्र -विषमताओं से परिपक्वता के रास्तों पर
काफल ट्री वाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिये यहाँ क्लिक करें: वाट्सएप काफल ट्री
काफल ट्री की आर्थिक सहायता के लिये यहाँ क्लिक करें
Recent Posts
हो हो होलक प्रिय की ढोलक : पावती कौन देगा
दिन गुजरा रातें बीतीं और दीर्घ समय अंतराल के बाद कागज काला कर मन को…
हिमालयन बॉक्सवुड: हिमालय का गुमनाम पेड़
हरे-घने हिमालयी जंगलों में, कई लोगों की नजरों से दूर, एक छोटी लेकिन वृक्ष की…
भू कानून : उत्तराखण्ड की अस्मिता से खिलवाड़
उत्तराखण्ड में जमीनों के अंधाधुंध खरीद फरोख्त पर लगाम लगाने और यहॉ के मूल निवासियों…
खाम स्टेट और ब्रिटिश काल का कोटद्वार
गढ़वाल का प्रवेश द्वार और वर्तमान कोटद्वार-भाबर क्षेत्र 1900 के आसपास खाम स्टेट में आता…
अनास्था : एक कहानी ऐसी भी
भावनाएं हैं पर सामर्थ्य नहीं. भादों का मौसम आसमान आधा बादलों से घिरा है बादलों…
जंगली बेर वाली लड़की ‘शायद’ पुष्पा
मुझे याद है जब मैं सातवीं कक्षा में थी. तब मेरी क्लास में एक लड़की…



View Comments
सुंदर, धन्यवाद मृगेश जी! मैं amazon पर किताब को हाथोंहाथ ऑर्डर कर चुकी हूँ ।